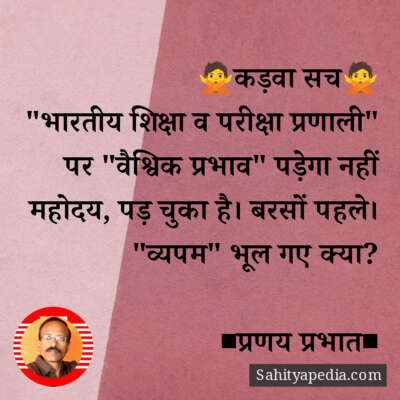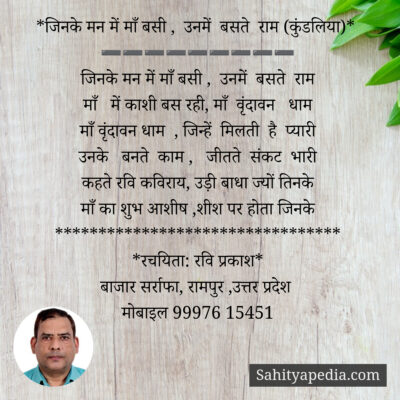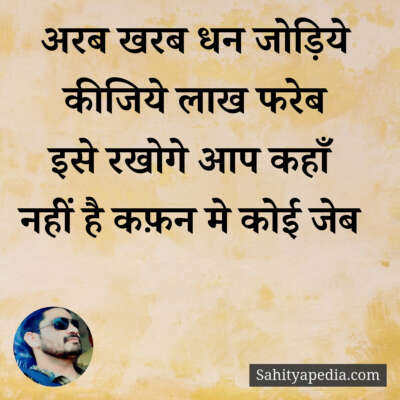दलित कविताएँ क्रांति का आह्वान हैं।
नवोदित कवि नरेंद्र वाल्मीकि ने “व्यवस्था पर चोट” नामक बेहतरीन कविता संग्रह को संपादित किया है; जिसमें कुल 36 दलित कवियों की 100 कविताओं को संग्रहीत किया है। इस संग्रह की मूल विशेषता यह है कि इसमें 9 दलित स्त्रियों की 25 कविताएँ हैं। व्यवस्था में जहाँ ब्राह्मणवाद मूल है, वहीं पुरुष प्रधानता के लिए, दलित कवित्रियों ने भी ब्राह्मणवाद को ही जिम्मेदार माना है। व्यवस्था का अर्थ वर्ण व्यवस्था अथवा ब्राह्मणवादी व्यवस्था से है। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट अर्थ उसके चार वर्ण और उसकी सीमाओं के अनुपालन से है, वहीं ब्राह्मणवाद का अर्थ जाति-व्यवस्था, ऊँच-नीच, छुआ-छूत, भेद-भाग, गैर-बराबरी की भावना से है। जाति-व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च है और शूद्र सबसे निम्न। सर्वोच्च ने निम्न को अपने अधीन बनाए रखने के लिए, दासता के लिए, निम्नतम कार्य के लिए, श्रम और श्रमिक के लिए अनेक नियम-नियमावली बनाए और ईश्वर विधान तैयार करके उन्हें डराए भी रखा। पूर्वजन्म और पुनर्जन्म, पाप और पुण्य, कर्मफल और प्रारब्ध, भाग्य और ईश्वर जैसी मान्यताएँ जरूर ऐतिहासिक विकास क्रम की उत्पत्ति हैं लेकिन कालांतर में ब्राह्मण जातियों ने आम जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए इसे जड़ मान्यता प्रदान कर दिया। दलित जातियों सदियों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था से त्रस्त रही हैं। कविता संग्रह का शीर्षक इसी व्यवस्था को संकेत कर रहा है तथा आधुनिक परिवेश में दलितों का चौतरफा नकार, प्रतिकार, प्रतिरोध, विरोध, विद्रोह इत्यादि ही वह चोट है जो शीर्षक के अनुभाग को पूरित कर रहा है।
इस व्यवस्था से जातियाँ तो त्रस्त रहीं हीं, देश का विकास बहुत पीछे छूट गया। आज जब मनुष्य को मनुष्य की पहचान हो जानी चाहिए थी, मनुष्य और भी अधिक गुमराह व जड़ हो गया है। यहाँ तक कि जातियों के आधार पर देश की शासन-सत्त्ता का संचालन किया जा रहा है। न्याय पालिकाएँ अपना न्याय जातीय आधार पर सुनिश्चित करती हैं। कौन सी विधान सभा और लोक सभा सीट से किस जाति का नेता अधिक वोट पाएगा और जीत सकने की संभावना है, उसी को टिकट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट जरूरी है।
नरेंद्र वाल्मीकि ने जिन वरिष्ठ कवियों को संग्रह में रखा है उनमें सर्वप्रमुख ओमप्रकाश वाल्मीकि और सूरजपाल चौहान जी हैं। इन्होंने व्यवस्था की गड़बड़ियों और इनके शोषकों की अमानवीयता का खुला वर्णन किया है बल्कि शोषकों और शोषितों दोनों को सम्मुख रखकर संबोधित किया है। इससे पूर्व की अन्य वरिष्ठ कवियों पर कलम चलाई जाए, जरूरी यह हो जाता है कि नरेंद्र वाल्मीकि की पुस्तक शीर्षक कविता “व्यवस्था पर चोट” की सबसे पहले चर्चा कर ली जाय। यह कविता ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर प्रश्नवाचक ललकार है। यह कविता दलित जातियों पर हो रहे अमानवीयताओं के साथ-साथ संविधान और आरक्षण पर हस्तक्षेप की ओर साफ संकेत भी है। यह अनिष्ट भविष्य का अनुमान भी है। यह ओमप्रकाश वाल्मीकि की तरह “तब तुम क्या करोगे” की आवाज है। वर्तमान में, दलितों पर हो रहे क्रूरताओं का भी ज़िक्र है इसलिए नरेंद्र वाल्मीकि की यह कविता क्रांति का आह्वान भी है। नरेंद्र वाल्मीकि ने लिखा:
रोज घटित हो रही अमानवीयताओं पर
कब तोड़ोगे अपनी चुप्पी
जब बन्द हो जाएंगे सारे रास्ते
क्या तुम तब खोलोगे अपने होंठ
आखिर कब करोगे व्यवस्था पर चोट?
(व्यवस्था पर चोट-पेज 84)
इस संग्रह के पहले कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ये ऐसे कवि, चिंतक, साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी दलित साहित्य का पुरोधा कहा जाना अनुचित नहीं होगा। इनकी कविताएँ नब्बे के दसक की कविताएँ हैं। उस समय की कविताओं में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का नकार, उसके प्रति घृणा और प्रतिरोध के भाव स्पष्ट दिखते हैं। उस समय के कुछ कवि सिर्फ कवि नहीं, बुद्धिजीवी और दलित चिंतक भी थे जिनमें कँवल भारती, ओमप्रकाश वाल्मीकि, मलखान सिंह का नाम उल्लेखनीय है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति घृणा भाव तो दिखता है, साथ ही साथ, उनकी कविताओं में तुच्छ सवर्णों के छल, छद्म, चालबाजियाँ, वैमनस्यता, घृणा, डराना, धमकाना, साजिश करना, दलितों को मारना, पीटना, घर फूँकना, घेरना, प्रताड़ित करना, स्त्रियों को छेड़ना, बलात्कार करना दिखता है। वाल्मीकि जी की कविताओं में एकहरा ब्राह्मणवाद ही नहीं है, वे साम्यवादियों और मार्क्सवादियों पर भी ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाते हैं। इसका सीधा अर्थ होता है कि वाल्मीकि जी ने मार्क्सवाद और साम्यवाद की गहराइयों को बड़ी ही गहराई से समझा है। उनकी कविता “कभी सोचा है” से यह पता लग जाता है कि भारतीय मार्क्सवादियों ने ब्राह्मणवाद को किसी प्रॉक्सी की तरह कवर किया है। तभी वे लिखते हैं:
खुश हो जाते हो
साम्यवाद की हार पर
जब टूटता है रूस
तो तुम्हारा सीना 36 इंच का हो जाता है
क्योंकि मार्क्सवादियों ने
बना दिया है छिनाल
तुम्हारी संस्कृति को।
(कभी सोचा है, पेज 7)
ओमप्रकाश वाल्मीकि इस कविता में ब्राह्मणवादियों के दुष्चरित्र और दोगलेपन को स्पष्ट लिखते हैं और यह भी कहते है कि जिसे तुम अपने वर्ण का निचला पायदान मानते हो, क्या कभी सोचा कि वे तुमसे घृणा क्यों करते हैं, तुम उन्हें पराए क्यों लगते हो? उनका इशारा स्पष्ट है कि ये ब्राह्मणवादी सवर्ण कभी भी दलितों को अपना नहीं समझते हैं, कभी भी उनके हित की बात नहीं सोच सकते हैं, कभी भी मनुष्य के बतौर प्यार नहीं कर सकते हैं। जानवर को फिर भी वे सीने से लगा लेते हैं लेकिन मनुष्य होने के उपरांत दलितों को गंदे जानवर से अधिक बुरा और अछूत समझते हैं। इसी क्रम की उनकी अगली कविता “ठाकुर का कुँआ” है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दलित उन्हीं की कब्ज़ा की गई जमीन में बसा-टिका है। दलित का अपना कुछ नहीं। सब कुछ सवर्णों का है। दलित डरा-सहमा अपनी भी जिंदगी को उन्हीं का बधुआ समझ रखा है। ओमप्रकाश वाल्मीकि ने एक कविता ही लिखा “तब तुम क्या करोगे”। उस कविता में सवर्ण संबोधित है। वे सवर्णों से सवाल करते हैं कि जो मेरी स्थिति है, मेरी बीवी की स्थिति है, मेरे बच्चों की स्थिति है, यदि वही तुम्हारी स्थिति हो जाय तब तुम क्या करोगे? इस कविता से कवि कहना चाहता है कि क्या ऐसी स्थिति में तुम दलितों की तरह सहन करते जाओगे अथवा अपने विरोधियों व विद्रोहियों के विरुद्ध विद्रोह कर दोगे? इस सवाल में उसका हल भी छिपा है कि यदि तुम गाँव से बाहर रहना नहीं पसंद करोगे, यदि तुम तालाब का पानी पीना स्वीकार नहीं करोगे, यदि तुम चिलचिलाती धूप में पत्थर नहीं तोड़ना नहीं पसंद करोगे, तुम भूख में भी जूठन खाना स्वीकार नहीं करोगे, तुम उतरन नहीं पहनोगे, तुम सिर पर मानव मल नहीं ढोना चाहोगे, तुम्हें स्कूल और पुस्तकों से दूर रखा जाय, तुम्हें रोज बेइज्जत किया जाय, तुम्हारी स्त्रियों की कभी कलाई पकड़ी जाय, कभी पुट्ठे पर हाथ मारा जाय, कभी स्तन पर हाथ फेरे जाँय और जब चाहें किसी खेत, खलिहान, मोहरे, दुआरे, अंधियारे, उजियारे संसर्ग कर दिया जाय, तुम्हारी स्त्रियों के मर्जी के विरुद्ध बलात्कार करते रहा जाय, उनको वेश्यावृति के लिए मजबूर करते रहा जाय, तुम्हें युगों-युगों तक खुली छत के नीचे विवश होकर सोना पड़े, तुम्हें बिना खेत-खलिहान के हमारे खेतों में जबर्दश्ती काम करना पड़े, तब तुम क्या करोगे? क्या ये सारी यातनाएं, ज्याजतियाँ, अन्याय, बलात्कार, भूख, प्यास और प्रतिदिन अपनी आँखों के सामने अपनी स्त्रियों की लुटती हुई इज्जत को बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं न? विद्रोह कर दोगे न? तब तुम्हीं बताओं, हम तुम्हारे इस कुत्सित और घृणित व्यवहार से कुपित होकर तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह क्यों न करें? ओमप्रकाश वाल्मीकि की उस कविता की कुछ पंक्तियाँ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:
यदि तुम्हें
सरेआम बेइज्जत कर दिया जाय
छीन ली जाय संपत्ति तुम्हारी
धर्म के नाम पर
कहा जाय बनने को देवदासी
तुम्हारी स्त्रियों को
कराई जाय उनसे वेश्यावृत्ति
तब तुम क्या करोगे?
जिस तरह ओमप्रकाश वाल्मीकि जी ने “ठाकुर का कुँआ” लिखकर दलितों के सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक जीवन को मजबूर बताया है उसी तरह सूरजपाल चौहान की कविता “मेरा गाँव” दलितों की ख़स्ताहाल को बयां करता है। वे कहते हैं दलितों के लिए गाँव में है ही क्या? न कहीं रहने की जगह है, न कोई घर है, न बैल है, न हल है, न खेत है, न खलिहान है, न कुँआ हमारा, न तालाब पर कोई अधिकार, न अच्छा खाना, न अच्छा पहनना, बारात, न घोड़ी चढ़ना। हमारे निस्बत तो कुछ नहीं, सिर्फ डांट-फटकार, जूता-लात, गाली और इज्जत के नाम पर बहु-बेटियों-बीवियों की अस्मत के साथ आएदिन खिलवाड़। क्या है गाँव में हमारा जिसे हम अपना कह सकें? उनकी कविता का एक अंश:
मेरा गाँव, कैसा गाँव?
न कहीं ठौर, न कहीं ठाँव।।
कच्ची मढ़ैया, टूटी खटिया
घूरे से सटकर
बिन फूस का मेरा छप्पर
मेरे घर न पेंड की छाँव।
उनके आँगन गइया-बछिया
मेरे आँगन सुअर-मुर्गियाँ
मेरा सिर उनकी लाठी
बेगारी करने को गाँव।
न कहीं ठौर, न कहीं ठाँव।।
साहित्य अपनी विविधता में प्रगति करती है। यह सार्वभौम असीमित है। सार्वभौम की गतिविधियां असीमित हैं। इसके अणु-परमाणु असीमित हैं। अंतरिक्ष असीमित है। इसी तरह मनुष्य की प्रवृत्तियाँ और उसकी सृजन विधियाँ और रूप असीमित हैं। इस पुस्तक के अध्ययन से प्रतिपल एक मोड़ मिलता है, एक रूप मिलता है, एक विधान मिलता है तो एक नई समस्या भी दिखती है। ब्राह्मणवाद का हर विधान उसके ईश्वर के सम्मुख एक रचना है, एक कर्तव्य है जिसका उसे ईश्वर को हिसाब देना है। ऐसा मैं नहीं सोचता, मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा ब्राह्मणवादी चिंतक और उसके अनुयायी सोचते हैं। सत्य का आभास उन्हें भी नहीं है लेकिन अपने मुर्दे को जलाने से पूर्व वे यह सुनिश्चित कर लेना जायज़ समझते हैं कि कहीं उस जगह पर इससे पूर्व कोई दलित मुर्दा तो नहीं जलाया गया था, नहीं तो उनका मुर्दा अपवित्र हो जाय और उसे परलोक में ईश्वर के सम्मुख जवाब देना पड़े कि वह अछूत कैसे हो गया। इस पर जयप्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है:
भगवान के दरबार में
तुम्हारी अच्छाई और बुराई का निर्णय
शायद इस बात से होगा कि
तुमने किसे छुआ किसे नहीं छुआ।
इसलिए मरघट के सन्नाटे में भी
तुम शव को जलाने से पहले
यह ध्यान में रखते हो कि
यहाँ पहले कोई अछूत तो नहीं जलाया गया।
यह कविता संग्रह ब्राह्मणवाद का पोल खोलता है। नरेंद्र वाल्मीकि ने कुछ ऐसी कविताओं को संग्रह में लिया है जो वर्ण-व्यवस्था की सबसे निचली पायदान की हरकतों का वर्णन करता है और कुछ कविताओं के विचारों से उस गलीज़ व्यवस्था को छोड़कर विद्रोह करने को उत्प्रेरित करता है। सफाई कोई बेजा कार्य नहीं है। घर, मुहल्ले, गली, सड़क, गाँव, शहर की सफाई एक उम्दा कार्य है। इससे व्यक्ति से लेकर एक देश एक राष्ट्र की प्रगतिशीलता का बोध होता है तथा दुनिया के संज्ञान में आता है कि हम कितने स्वच्छता के हिमायती हैं लेकिन जब यही स्वच्छता किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष की सामाजिक जिम्मेदारी बना दी जाती है और उस कार्य को इतना हीन बना दिया जाता है कि अन्य कोई और जाति व व्यक्ति उसे उसी तरह संपादित करने लगे तो लोग तमाशा देखने लगेंगे और कह उठेंगे कि क्या आप पगला गए हैं? क्या आप नीच हो गए हैं? क्या आप इतने गिर गए हैं? क्या आप मेहतर हैं? क्या आप हेला-भंगी हो गए हैं? शौच के बाद स्वयं का मल एक भिखारी से लेकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी करता है। वहाँ कोई बुराई न है, न प्रतीत होती है और न ही कोई उस पर हँसता है। कोई तोहमत नहीं। दिक्कत तो यह है कि भारत जैसे देश में सार्वजनिक सफाई का जिम्मा वाल्मीकि जाति पर है। बहुत ही निजी सफाई का जिम्मा भी वाल्मीकि जातियों पर ही थोपी गई थी जिसे अनेक जगहों पर आज भी चाहे मजबूरी वश, चाहे डर वश, चाहे जातिगत पेशा वश वाल्मीकि जातियाँ ही सम्पन्न कर रही है। इस कविता संग्रह के कई साथी वाल्मीकि जाति आए हैं। निश्चित ही, उन्हें उस गलीज़ व्यवस्था से घृणा है, होना भी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना, कूड़ा गाड़ी ढकेलना, नाली साफ करना, सीवर साफ करना, कहीं-कहीं ओल्ड फैशन के घुसलखाने आज भी संचालित हैं, उनका मल काछना और इसे टोकरी में रखकर किसी निर्धारित स्थल पर ले जाकर फेंकना एक असहनीय पीड़ा है। हमारे नवयुवकों के लिए तो पीड़ा से अधिक मान-मर्यादा और इज्जत का सवाल है। बहुत से बच्चे माँ-बाप से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उस नरक के लिए न प्रेरित करो और न ढकेलो। बच्चे उस कमाई को नहीं खाना पसंद करते हैं। वे विज्ञान के इस युग में सच को समझते हैं और प्रश्न भी करते हैं कि सभी एक जैसे हैं, फिर क्यों हम नीच हैं और क्यों वे ऊँच हैं। फेक दो झाड़ू-तसला, कोई और काम करो। डॉ. पूनम तुषामड़ की कई कविताएँ वाल्मीकि जातियों की इस स्थिति का वर्णन करती हैं। उनकी एक कविता का तेज देखिए:
बीन कर घर-घर से कूड़ा
मांग कर लाई जो रोटी
माँ मुझे मत दो।
मैं नहीं पहनूँगी उतरन
मैं नहीं खाऊंगी झूठन
मैं नहीं माँजूगी बरतन
ऐसी जिल्लत ऐसा जीवन
माँ मुझे मत दो।
फेंक दो ये झाड़ू-तसली
जानो तुम पहचान असली
झाड़ू, तसली और कूड़े की विरासत
माँ मुझे मत दो।
(माँ मुझे मत दो, पेज 37-38)
गाँव जातिवाद का कारखाना है। गाँव से ब्राह्मणवाद को खुराक मिलता है। गाँव वैमनस्यता की प्रायोगशाला है। गाँव में भातृत्व का अंत हो चुका गया है। गाँव की जातीय वैमनस्यता देखकर युवक शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। बेगार में पकड़े जाने के डर से दलित लड़के शहर भाग जाते हैं। जातीय उत्पीड़न के डर से दलित युवक-युवतियां कहीं अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। कुछ बच्चे इस ईर्ष्या से गाँव छोड़कर भाग लेते हैं जिससे सवर्ण जातियों के लड़के खेत का काम स्वयं करें, यह अहसास करें कि भूख-प्यास क्या होती है, गर्मी-वर्षा कैसे सहन करना पड़ता है, धान-गेहूँ कैसे बोया-काटा जाता है। उनकी “पत्र” कविता में कुछ इस तरह की सच्चाई जो हमें उन बच्चों के पलायन को प्रतिरोध कहना जरूरी हो जाता है। हालांकि, मशीन ने व्यक्ति को स्थानापन्न कर दिया है। खेत में हांडतोड़ परिश्रम खत्म हो गया है। दलित स्त्रियों के गँवई कार्य खत्म हो चुके हैं। स्त्री चाहे दलित हो अथवा सवर्ण उन्हें बतौर गृहणी ही कार्य करना रह गया है इसलिए दलित स्त्रियों के छोड़े हुए कोई भी कार्य सवर्ण स्त्रियों के सिर पर नहीं लदा। फिर भी, दलित युवक और युवतियों की यह सोच निश्चित ही क्रांतिकारी मंतव्य की है। डॉ. पूनम तुषामड़ की कविताओं में दलित युवक-युवतियों से संबंधित इस मंतव्य की अनेक कविताएँ तारीफ के काबिल हैं। उनकी एक कविता है:
हमने छोड़ दिए हैं गाँव
तोड़ दिया है नाता
गाँव के कुएँ, तालाब
मंदिर और चौपाल से
जो अक्सर हमें मुँह चिढ़ाते,
नीच बताते और कराते हमें
जाति का अहसास
हमने छोड़ दिए हैं गाँव
ताकि जानो तुम
चिलचिलाती गर्मी में
गर्म हवाओं के बीच
लगातार
अधनंगे-अधपेट श्रम करना
और, दो जून की रोटी कमाना
कितना कठिन है?
(हमने छोड़ दिए हैं गाँव, पेज 41)
नरेंद्र वाल्मीकि ने वाल्मीकि जातियों की दुर्दशाओं पर डॉ. सुरेखा की तीन कविताएं “मेरी पहचान”, “भंगी इन्हें हम कहते हैं” और “व्यवस्था” ली है और डॉ. राधा वाल्मीकि की एक कविता “आखिर क्यूँ” लिया है। लालचंद ज़ैदिया “जैदी” की कविता “दशा”, “मैं भंगी हूँ”, “भ्रम” और “झाड़ू” वाल्मीकि जीवन पर है। हंसराज भारतीय की कविता “भारत माँ की ढाल लिखूँ”, धर्मपाल सिंह की “मैले की मलिनता”, कांता बौद्ध की “मौत के सीवर”, दीपक वाल्मीकि की “सफाई वाला”, “एक सफाई कर्मचारी की अभिलाषा”, आशीष भारती की “जागो स्वच्छकार”, अनिल कुमार चावरिया की “चोट व्यवस्था की”, देव कुमार की “मैं ही”, नवीन लोहट की कविता “सफाई कर्मचारी की कहानी”, पीएल भारती की कविता “झाड़ू”, अरविंद भारती की कविता “नर्क” वाल्मीकि जीवन पर लिखी कविताएँ हैं। सभी उस नारकीय जीवन से मुक्ति चाहते हैं। सभी ने सवर्णों के व्यवहार, दुर्व्यवहार, मानसिकता और चिंतन को उद्धृत किया है। सभी परिवर्तन चाहते हैं। इन कविताओं को लिखते हुए हमारे ये कवि पुनश्च-पुनश्च उस दर्द को महसूस किए होंगे जिससे वे दिन के उजाले में इस सभ्य समाज में संभ्रांतों के सम्मुख महसूस करते हैं। दिल तो यही कहता है कि हथियार उठाओ और इनके पोषकों, अनुयायियों और नियन्ताओं को काट कर फेंक दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी लेकिन यह इतना आसान नहीं है, न ही नैतिक है, न ही विधिक है और न यह हमारे सोचने मात्र या प्रारम्भ कर देने मात्र से सम्पन्न होने वाला ही है। यह एक अदृश्य सत्ता है जो सभी के मन में घर कर गया है। यह एक आदमी के कहने, सुनने और रोकने से नहीं रुकने वाला है, चाहे इस बात को वर्ण व्यवस्था के सबसे सम्मानजनक व्यक्ति द्वारा ही क्यों न कहा गया हो। विचार वस्तुस्थितियों का उत्पाद होता है। विचार वस्तुस्थितियों को पुनर्निर्मित भी करते हैं। यह किसी पदार्थ के रूप परिवर्तन जैसी प्रक्रिया में निरंतर घटता रहता है। इसको परिवर्तित करने के लिए कोई ऐसा विज्ञापन होना चाहिए जो सतत और हर जगह एक ही बात दोहराए कि जातीय विषमता अभी से बन्द किया जा रहा है। इस घोषणा को न मानने वाले विद्रोहियों को तत्काल सजाए मौत दी जाएगी। उम्मीद है लोग इस कायदे का अनुसरण करें। असमानता के जितने भी सरोकार हैं, सभी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाने अनिवार्य कर दिए जाँय। यह मुझे भी लग रहा है कि कोरी बकवास है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यवस्था अपनी सत्ता अपनी हुकूमत को यह आदेश प्रदान कर दे और उसके अनुपालन में ईमानदार राजनयिक लगे रहें। कोई सत्ता ही किसी को यह आदेश दे सकती है कि अमुक से कोई व्यक्ति, संस्था व सरकार घृणित कार्य नहीं करवा सकती है। ऐसी व्यवस्था संसदीय राजनीति के द्वारा सत्ता प्राप्त कर नहीं लाया जा सकता है क्योंकि इस व्यवस्था का संविधान जाति, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र, उत्पादन और साधनों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है बल्कि निजी हाथ इन पर अपना नितंत्रण रखता है, बल्कि निजी मालिकाना का असर व नियंत्रण राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति और विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर भी रहता है। इसे परिवर्तित करने के लिए क्रांतिकारी सिद्धांत और क्रांतिकारी संगठन अनिवार्य है। संसदीय लोकतंत्र, संविधान और ये भ्रष्ट लोग किसी भी परिवर्तन के लिए अवरोधक हैं। इन कविताओं को केंद्र में रखकर परिवर्तन की एक लम्बी और अनिवार्य बहस हो सकती है। ऐसी किताबें लम्बी बातें करती हैं। लम्बी बातों के लिए लम्बा समय चाहिए। यह एक सार्थक प्रारम्भ है। परिवर्तन आवश्यक परिघटना है लेकिन हम चाहते हैं कि परिवर्तन एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो, प्राकृतिक परिवर्तन के इंतजार में सदियाँ बीत जाएंगी, ब्राह्मणवाद हमें नारकीय जीवन के लिए अभिशप्त रखेगा।
जातीय उत्पीड़न से त्रस्त दलित कवि सर्वप्रथम दलित जातियाँ हैं। दलित जाति होने के नाते यह उनका भोगा यथार्थ है। भोगे यथार्थ की छटपटाहट कोई अन्य महसूस नहीं कर सकता है।
नरेंद्र वाल्मीकि द्वारा संपादित कविता-संग्रह की कविताओं में दलित स्त्रियों की कविताएँ भी हैं। दलित स्त्रियों में सर्वप्रथम डॉ. सुशीला टाकभौंरे की कविताएं हैं। उनकी कविताओं में ब्राह्मणवाद के दोहरे चरित्र का रेखांकन बहुत स्पष्ट है। उन्होंने पुरुष वर्चस्व का भी सवाल उठाया है। दरअसल, शब्दों से भी पुरुष और स्त्री के सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर का पता चलता है। “कुत्ता” और “कुतिया” शब्द के भेद को स्पष्ट करते हुए मनुवादी दुर्गुणों को आरोपित किया है। वे कहती हैं कि “कुत्ता” और “कुतिया” एक प्रजाति के हैं लेकिन “कुत्ता” शब्द से वफादारी और “कुतिया” शब्द से गाली और स्त्री के नीचता का बोध होता है। उनका मानना है कि यह ब्राह्मणवाद जैसी व्यवस्था के कारण ही संभव है। हालांकि, भाषा विश्लेषकों ने भाषा के अर्थों के विकास में ऐतिहासिक विकास क्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना है। भाषा और उसके अर्थ का विकास किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे परस्पर संबंधों से उत्पन्न विचार के सार्वभौमिक अस्तित्व से बनता है। डॉ. सुशीला टाकभौंरे ने “गाली” कविता में “कुतिया” के अस्तित्व निर्धारण के लिए मनु को जिम्मेदार ठहराया है लेकिन विश्व मान्यताओं की व्यापकता में उतरा जाय तो वहाँ भी विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में “कुतिया” को नीच स्त्री के अर्थ में समझा गया है। वहाँ कौन सा मनु है? दरअसल, यहाँ पुरुष प्रधान समाज को ही दोष देना अधिक उचित है क्योंकि भाषा विकास के उस काल में जब स्त्रियों से मातृसत्ता छीनी गई और पुरुष वर्चस्व लादा गया, उस समय स्त्रियों को हर तरह से हीन बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भाषाई हमले किए जाने लगे थे जिससे स्त्री से सम्बन्धित अनेक पर्यायों को नीच बना दिया गया अथवा स्त्री संबंधित भाषा ने नीचता का अर्थ ग्रहण कर लिया। उस समय तक मनुवाद अस्तित्व में नहीं आया था। “कुतिया” बुद्ध के समय भी था और बुद्ध के पूर्व भी था जबकि मनु या मनुवाद या ब्राह्मणवाद ईसा के कई सताब्दी बाद अस्तित्व में आया। खैर, डॉ. सुशीला टाकभौंरे ने स्त्री विरोधी सत्ता व व्यक्ति को संबोधित किया है, और यह सत्य भी है कि मनु, मनुवाद व ब्राह्मणवाद स्त्री विरोधी सत्ता है, उसने यदि “कुतिया” शब्द को हीन बनाया नहीं है तो उसकी हीनता बोध को अक्षुण जरूर रखा है इसलिए मनु दोषी जरूर है। वे लिखती हैं:
कुत्ता और कुतिया एक दूसरे के पूरक हैं
चरित्र के नाम
“कुत्ता” वफादार
और “कुतिया” गाली क्यों बन जाती है
पुरुष प्रधान समाज में
समर्पण हो या विद्रोह
दुर्गुण का दोष
स्त्री पर ही मढ़ा जाता है
पुरुष के दुर्गुणों पर
मनु नाम की चादर
ओढ़ा दी जाती है।
(गाली, पेज 24-25)
परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। मानव जाति आदि मानव से सभ्य मनुष्य तक का सफर तय कर आया है तो हमारी अनेक विषमताएँ कालांतर में परिवर्तित होकर अत्यधिक सभ्य व सुसंस्कृत जरूर हो जाएंगे। सवाल यह है वह समय न जाने कब आएगा, क्या तब तक मनुष्य जाति और धर्म की मान्यताओं के नाम पर सवर्णों की ज्याजातियाँ सहती रहे? निश्चित हमें परिवर्तन को मनोगत रूप से तीव्र करना आवश्यक बना देना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे बंधनों-वर्जनाओं के उपरांत भी परिवर्तन हुए हैं। सच है कि स्त्री को पुरुष ने निजी संपत्ति समझकर सात तालों में रखा लेकिन सामाजिक स्त्री के रूप में स्त्री को जबरदस्ती खूब नंगा भी किया। सरे महफ़िल नंगा नचाया। कोठों पर निर्वस्त्र किया। मचल-कुचला। दासी बनाया। देवदासी बनाया। वेश्या बनाया। अभी तक घर की चहारदीवारी में कैद रखा। इस सब के उपरांत भी स्त्री स्वतंत्र हुई। स्त्री आगे बढ़ी। स्त्री ने स्वयं अपना वस्त्र चेंज किया। स्त्री ने अपना रूप-सृंगार बदला। वह बारह हाथ की धोती को छोड़ नैकर और बनियान में बाहर निकलना शुरू किया है। यदि वह प्रतिकार स्वरूप निर्वस्त्र होकर तुम्हारे सामने आने की हिम्मत करने लगे, मर्दों की मर्दानगी को चुनौती देने लगे तो बुरा ही क्या है? हालांकि, मैं इस प्रतिकार की चुनौती को संस्कृति के इस खुलेपन तक को विमर्श का विषय मानता हूँ। मैं न इसे जायज की श्रेणी में रखता हूँ और न ही नाजायज़ कहना चाहता हूँ। समय इस चुनौती को हल करेगा। देखिए डॉ. सुशीला टाकभौंरे की कविता का वह अंश:
तुमने उघाड़ा है
हर बार औरत को
मर्दों
क्या हर्ज है
इस बार स्वयं वह
फेंक दी परिधानों को
और ललकारने लगे
तुम्हारी मर्दानगी को
किसमें हिम्मत है
जो उसे छू सकेगा?
आज वह जंगल की आग है
बुझाए न बुझेगी
बन जाएगी आग का दरिया
उसके नए तेवर पहचानों
श्रद्धा, शर्म, दया, धर्म
किसमें खोजते हो?
संभालो अपने पुराने जेवर
थान के थान परिधान
आज ये खुद्दार औरत
नंगेपन पर उतरकर
परमेश्वर को लजाएगी
पुरुष के सर्वस्व को नकारकर
उसे नीचा दिखाएगी।
(आज की खुद्दार औरत, पेज 26-27)
देवदासी शब्द को सुनकर ही शरीर के रोवटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में सिहरन होने लगती है। मनुष्य ने अजीब-अजीब प्रथाएँ बना रखी है। ये मठ-मंदिर स्त्री शोषण के अनियंत्रित-अप्रश्नवाचक अड्डे रहे हैं। पुजारी ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते रहे हैं। इनकी वाणी देववाणी मानी जाती रही है। बड़े से बड़ा राजा-महाराजा भी इन पंडे-पुजारियों की मंशा पर शक नहीं कर सकते थे। गाँव-घर की सुंदर कन्याएँ मंदिर में पुजारी और ईश्वर की सेवा के लिए दान कर दी जाती रही हैं। बाद में, इस प्रथा को जीवंत बनाए रखने के लिए शूद्रों की कन्याओं को जबरदस्ती मंदिरों में उठा ले जाया जाने लगा। पंडे-पुजारियों के संसर्ग से उत्पन्न पुत्र-पुत्रियों को देवपुत्र और देवकन्या कहा जाने लगा। किसी ने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। मंदिरों की शोषित उन देवदासियों ने भी कोई शिकायत नहीं की। जिसने शिकायत की, वह या तो सुबह मृत पाई गईं या फिर मंदिर से फिर न प्राप्त होने के लिए गायब हो गईं। वास्तव में, वे देवदासियां न तो ईश्वर के श्राप से मरी थीं और न स्वतः कहीं गायब हुई थीं, वे या तो बात खुलने के डर से जान से मार दी जाती रही हैं अथवा उन्हें जान से मार कर किसी गुप्त जगह पर फेंक दिया जाता रहा है। ये अभिशापित परंपरा अभी तक अनेक मठ-मंदिरों में आज भी चल रहा है। वैसे अनेक प्रदेशों के विभिन्न मंदिरों की लाखों देवदासियों को वेश्याल पहुंचा दिया गया है जिसका कि सरकारी हिसाब-किताब मौजूद है। इनसे उत्पन्न बच्चों को ईश्वर की संतान कहा गया। ईश्वर का अर्थ है “हरि” और संतान का अर्थ है “जन”। दोनों मिलकर “हरिजन” हो गया। कालांतर में, गाँधी ने बड़ी चालाकी से दलित जातियों को “हरिजन” शब्द से संज्ञायित किया था जिसका कि डॉ. आम्बेडकर ने उस समय कड़ा विरोध किया था और आज दलित जातियों ने “हरिजन” शब्द का खुले मंच से विरोध करना शुरू कर दिया है। इस संग्रह में डॉ. सुरेखा की एक कविता है “देवदासी”। उसकी कुछ पंक्तियाँ आप के अवलोकन के लिए प्रस्तुत है:
वो कहते हैं
मैं सेविका हूँ ईश्वर की
उसी संग ब्याही हूँ
जीवन भर उसी संग रहने
दान स्वरूप मंदिर आई हूँ।
गर मैं हूँ ईश्वर की सेविका
तो इंसान से क्यों भोगी जाती हूँ।
ब्याहता हूँ जब ईश्वर की
तो इंसान की कैसे कहलाती हूँ।
(देवदासी, पेज 49-50)
दलित स्त्री की सिर्फ इतनी सी दिक्कतें नहीं हैं। वह अन्य औरतों के मध्य भी अबला है। एक दलित स्त्री मूक है, निरीह है, अबला है, अछूत है, सवर्ण संभोग के लिए सछूत है, नगर बधू है, देवदासी है। स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। नंगेली नामक दलित स्त्री ने इस गलीज़ व्यवस्था से खिन्न होकर अपने हाथ से अपने स्तन को काटकर फेंक दिया था जिससे उसकी जान चली गई थी। ब्याह के बाद दलित स्त्री की डोली सवर्ण के घर उतारी जाती थी। तीन रात उसे बाबू साहब व पंडित जी से संभोग करना पड़ता था। डॉ. राधा वाल्मीकि जी की कविताओं में दलित स्त्रियों के जीवन का जो सच मिलता है उसको पढ़कर दिल फट जाता है। इस पीड़ा को समाप्त करने की जो ललक जो प्रेरणा डॉ. राधा वाल्मीकि में है यदि दस प्रतिशत दलित स्त्रियों में भी वही ललक, वही उत्साह, वही जोश पैदा हो जाय तो ब्राह्मणवाद की न सिर्फ स्त्री विरोधी व्यवस्था व उनकी हिम्मत टूट जाय बल्कि दलित पुरुषों पर हो रहे जुल्म-अन्याय भी खत्म हो जाय। हमें डॉ. राधा वाल्मीकि के शब्दों से सबक लेना चाहिए:
धन से भी घनघोर हो चुकी पीड़ा निकालनी चाहिए।
असमान स्पृश्यतायुक्त व्यवस्था बदलनी चाहिए।।
उठो व जागो स्वयं को जानो वक्त की ये ललकार है,
दुख, संताप, व्यथा सहने की प्रथा को धिक्कार है।
अपने हक, अधिकार हमें मिलने ही मिलने चाहिए,
असमान स्पृश्यतायुक्त व्यवस्था बदलनी चाहिए।।
(व्यवस्था बदलनी चाहिए, पेज 53-54)
और अन्त में, सुशीला देवी वाल्मीकि ने हमारे संघर्ष को अपने क्रांतिकारी गीत के स्वर में एक ऊँचाई प्रदान कर दी है, जिसे बिना किए, बिना जिए हम न डॉ. आम्बेडकर साहब के सपनों को पा सकते हैं, न दलितों को सम्मान की जिंदगी दिला सकते हैं, न स्वयं अभिशप्त जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। सुशीला वाल्मीकि जी हम सब के तरफ से हम सब के लिए लिखती हैं:
कोटि कण्ठ एक साथ आम्बेडकर गान गाओ रे
इस महान देश के नवजवान आओ रे………….
मुश्किलों से लड़ना तुम्हें तुम कदम बढ़ाओ रे
मनुस्मृतियों के बीच से ढूँढना है राह तुम्हें
तुम कदम बढ़ाओ रे
इस महान देश के नवजवान आओ रे…………।
(नवजवान आओ रे, पेज 144)
पुस्तक- व्यवस्था पर चोट (साझा काव्य संग्रह)
संपादक- नरेन्द्र वाल्मीकि
प्रकाशक- रवीना प्रकाशन, दिल्ली।
समीक्षक
आर.डी. आनंद
मो. 9451203713