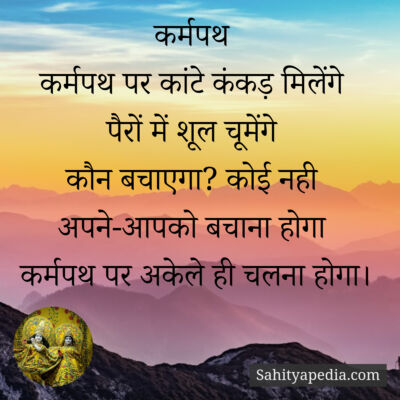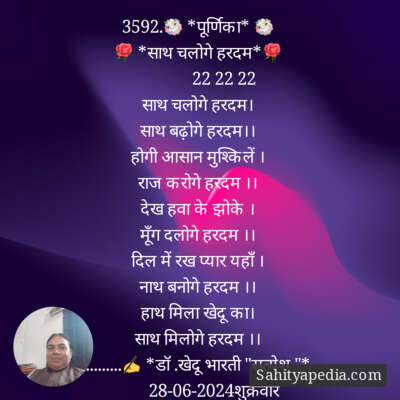डा. तुलसीराम और उनकी आत्मकथाओं को जैसा मैंने समझा / © डा. मुसाफ़िर बैठा

भारतीय समाज के मूल चाल-चरित्र को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि कोई गैरदलित साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका जब अपना विशेषांक किसी दलित हस्ती पर समर्पित करने जा रही हो तो यह अपनेआप में एक परिघटना है, एक राजनीतिक कार्यवाही है. कबीर-रैदास का हिंदी साहित्य समाज में सामने आना, महत्त्व पाना, हीरा डोम की कविता ‘अछूत की शिकायत’ को सहज स्वीकारा जाना और टटका-टटका आदिवासी युवा कवि अनुज लुगुन का हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित भारतभूषण अग्रवाल पुरस्कार पाना भी एक राजनीतिक कार्यवाही है! राजनीतिक कार्यवाही इसलिए भी कि कहीं आपके किसी के स्वीकार के साथ आपका किसी अस्वीकार का बड़ा एजेंडा भी सामने हो सकता है, साथ हो सकता है! नहीं तो क्या कारण है कि हिंदी दलित साहित्य के प्रमुखतम स्तंभ एवं अपनी ‘जूठन’ से हिंदी साहित्य में दलित चेतना की बरजोर धमक प्रस्तुत करने वाले ओमप्रकाश वाल्मीकि के निधन पर साहित्य जगत की ‘आह-वाह’ इस त्वरा के साथ न निकल सकी जैसी की डा. तुलसीराम के प्रति निवेदित हुई है!
अपनी बात को आगे बढाते हुए कहना चाहूँगा कि क्रांतिकारी कबीर-रैदास आपकी बौद्धिक कवायद का हिस्सा होते हैं पर जीवन में आप उनके विचारों को भरसक ही उतारने की कोशिश करेंगे, जीवन के लिए आप अपने संस्कृति-संस्कार के सुभीते के व्यक्ति मर्यादावादी तुलसीदास को चुनेंगे! कबीरपंथियों-रैदासियों की सामाजिक प्रास्थिति एवं प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए निम्न जातियों के लोग ही मिलेंगे. हाँ, कबीरपंथियों में जरूर कुछ उच्च जाति के लोग भी मिल जाएंगे पर इनमें से भी अधिक कबीर मठों के महंथ अथवा अन्य ताकतवर पदों पर सुशोभित लोग ही मिलेंगे, जो राजनीतिक कार्यवाही है, दिल से जुड़ना नहीं. दूसरी तरफ, साहित्य में देखिये तो रैदास एवं कबीर पर भी निम्न जातियों से आने वाले ‘आधिकारिक’ विद्वान माने जाने वाले लोग भरसक ही मिलेंगे, यहाँ विद्वता-विशेषज्ञता का कब्ज़ा कबीर एवं रैदास को सायास अपने जीवन से दूर रखने वालों का ही होगा. अठारहवीं सदी के दलित कवि हीरा डोम की ‘अछूत की शिकायत’ कविता को कथित मुख्यधारा के साहित्य में हाथोंहाथ लिया जा रहा है, इस कविता के सौ साल पूरे होने को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि वहां अधिकार-हनन की शिकायत भर है वह भी कथित ईश्वर से, सीधे सीधे अपने ऊपर जुल्म ढाने वालों से नहीं, इस कविताई को पुचकारने वाले वर्ग की सत्ता को इस स्वर से कोई खतरा नहीं है! पुरातन ‘अछूत की शिकायत’ को स्वीकारने एवं आज के अधिकार सजग दलित साहित्य को सिरे से ख़ारिज करने की कार्रवाई में पूरा विरोधाभास एवं वृहतर साहित्य समाज का पूर्वग्रह एवं उसकी पूरी राजनीति खुलकर सामने आती है. दूसरे मिसाल में जाएँ तो क्या कारण है कि द्विज समाज की अपनी कविताओं में कभी न चीरफाड़ करने वाले अनुज लुगुन की आदिवासी समाज पर शिकायती कविता को तो भारतभूषण अग्रवाल मिल जाता है पर अबतक किसी दलित कवि को यह पुरस्कार नहीं मिल सका है? साफ़ है, अनुज लुगुन अपनी पुरस्कृत ‘उलगुलान’ कविता में आदिवासियों के दुश्मन की पहचान छुपाते हैं, जाति-दुश्मनों को भी महज वर्ग-शत्रुओं में तब्दील कर, डायल्यूट कर देखते हैं. लुगुन की सारी कविताएं आत्मदया एवं सड़ी-गली त्याज्य आदिवासी चलनों एवं परम्पराओं तक के प्रति एक व्यर्थ मोह के साथ है जो वर्चस्वशाली सभ्य समाज को पसंद आता है, क्योंकि वहां सभ्यता (आधुनिक मानवाधिकार पूर्ण एवं सुविधाओं वाला जीवन) में हिस्सेदारी की मांग नहीं है, वरन उसमें महज कथित आदिवासी संस्कृति को सभ्य समाज से बचाने की रिरियाहट मात्र है. जबकि दलित साहित्यकार अपनी वंचनाओं का हिसाब मांगता है, अपने परम्परागत अधिकार-शत्रुओं के सरोकारों को प्रश्नांकित करता चलता है, ख़ारिज करता है और साहित्य-संस्कृति में अपने अवदान को अलग से रेखांकित कर आपके योगदान तो खरे-खोटे की कोटियों में बांटने का पहली बार पहल करता है. बीएचयू से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त लुगुन अभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय गया में हिंदी के सहायक प्राध्यापक हैं. बीएचयू में ही एक दलित प्राध्यापक ने फेसबुक पर लुगुन के साहित्य-सरोकारों का प्रसंग छिड़ने पर लिखा कि इस युवक को तो विश्वविद्यालय में दलित-आदिवासी मुद्दों पर हुए आंदोलनों, सेमिनारों, बहस-मुबाहिसों में कभी भाग लेते देखा-सुना नहीं गया.
किंचित अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि डा. तुलसीराम के ‘सर्वस्वीकार’ का मामला भी अलग नहीं है. अपनी आत्मकथा ‘मुर्दहिया’ से उनका हिंदी साहित्य की मुख्यधारा के बीच तूफानी स्वीकृत एवं सम्मान अनायास नहीं है. डा. तुलसीराम ने “भी” अपनी जमीन, अपनी आत्मकथाओं की जमीन मूल रूप से शिकायती ही रखी है, खुलकर, मुखर होकर अथवा धमक के साथ अपने अधिकार हनन की बात, सवर्णों द्वारा अपने पर अथवा दलितों पर अन्याय बरसाने की बात नहीं की है, दलित अधिकारों की खुली पैरवी भरसक ही की है. बल्कि उनने किया यह है कि अपने बनने में सवर्णों एवं सवर्णों के वर्चस्व के संगठन एवं विचारधारा, वाम की मुक्तहस्त प्रशंसा की है जो दलित साहित्य, अम्बेडकरवाद एवं इन दोनों की नींव बाबा साहेब के अस्वीकार तक ढके-छुपे चली जाती है. यह तो उनके जीवन के अंतिम वर्ष रहे जब उनका वामपंथ से मोहभंग होता है और वे खुले रूप से अम्बेडकरवादी बनते हैं, दलित लेखक संघ से सक्रिय रूप में जुडते हैं. हालांकि यह बात आत्मवृत्त के दूसरे खंड में (जो ‘मणिकर्णिका’ शीर्षक से है) में भी नहीं आती. ‘मुर्दहिया’ की भूमिका में डा. तुलसीराम की घोषणा है कि दूसरे खंड में जो उनका जीवन आया है ‘’मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है’’. ‘मणिकर्णिका’ की भूमिका में वे आत्मबयानी करते हैं कि “…एक दिन ऐसा भी आया, जब बुद्ध और मार्क्स ने मिलकर मेरे मस्तिष्क में बसे ईश्वर को भी ध्वस्त कर दिया”. हालांकि यह ध्वंस मार्क्स से ही हो जाना चाहिए था क्योंकि लंबे अरसे तक वाम संगठन से जुड़े रहने के बाद ही उनके जीवन में बौद्ध विचार का समावेश होता है. यह ध्यातव्य है कि डा. तुलसी राम बनारस के अपने छत्र जीवन की अपनी तमाम वाम संलग्नता
का अपनी आत्मकथा में बयान करते हुए भी दलित छात्र संगठनों एवं उनके क्रियाकलापों से अपने परिचय की चर्चा नहीं करते. उनका यह अपरिचय हमें चौंकाना चाहिए!
हिंदी दलित साहित्य की प्रभावकारी उपस्थिति सन 1995 के आसपास शुरू होती है जो मुख्यतः आत्मकथाओं के आने के बाद आकार लेती है। और मुख्यधारा के साहित्य में दलित लेखन की चर्चा एक अहम विषय बनती है जब मोहनदास नैमिशराय की आत्मकथा का पहला खंड ‘अपने अपने पिंजड़े’ नाम से 1995 में दिल्ली के एक बड़े प्रकाशन से छप कर आती है. हालाँकि ‘मुर्दहिया’ के आने से पहले तक जो करीब दस हिंदी दलित आत्मकथाएं प्रकाशित हुईं, उनमें ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा ‘जूठन’ ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई।
प्रसंगवश कहूँ कि जहाँ तक दलित आत्मकथा की बात है तो इसको बतौर आत्मकथा विधा नकारने की हिंदी प्रकाशकों और कुछ गैर दलित लेखकों की गर्हित मंशा रही है. नामवर सिंह, राजेंद्र यादव जैसे लेखकों ने डा. तुलसीराम की इन दोनों आत्मकथाओं को औपन्यासिक कलेवर का कहकर प्रशंसा देते खारिज ही करने की कोशिश की है. आप देखेंगे कि अनेक हिंदी में उपलब्ध हिंदी, मराठी आत्मकथाओं को प्रकाशकों ने या तो उपन्यास कहा है या फिर आत्मकथात्मक उपन्यास.और इनकी गैर दलित लेखकों से लिखवाई गयी भूमिकाओं में भी यही साबित करवाया गया है. गरज यह कि दलित आत्मकथाओं को ये लोग सायास साहित्य की एक रचनात्मक विधा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते. इनका प्रकट अथवा गुप्त-सुप्त एजेंडा यह होता है कि इसे रचनात्मक साहित्य न माना जाए, इससे बाहर रखा जाए. दलित आत्मकथाओं को साहित्य मानने के विरोधी इस तर्क के होते हैं कि चूंकि आत्मकथा में सच मात्र का बयान होता है, कल्पना का कथित साहित्यिक पुट शामिल नहीं होता अतः रचनात्मक साहित्य में इसे शामिल नहीं किया जाये. दरअसल, प्रभु जातियों में अपनी बेईमानियों-शैतानियों, छल-प्रपंचों, वर्चस्व लाभों को उघाड़ने का माद्दा प्राय: नहीं होता अतः वे सजीव-सम्पूर्ण जीवन की सचबयानी करती आत्मकथा लिख भी नहीं सकते. उनकी आत्मकथा झूठ और छलावों को गर्व-कथा में अवतरित करने का निदर्शन होगी. उनकी मिथ्या आत्मकथा अपने जीवनस्थितियों, प्रभुवर्ग के संग-साथ के सुखकर स्मरणों के वृत्त से ही अटे-पटे होंगे! डॉ तेजसिंह ने अपनी पत्रिका ‘अपेक्षा’ के दलित आत्मवृत्त अंक में इन साजिशों-अनगढ़ सच्चाइयों को अपने सम्पादकीय में बखूबी नग्न किया था.
डा. तुलसीराम की आत्मकथा के प्रथम भाग ‘मुर्दहिया’ पर अपना मत रखते हुए एक व्यक्ति ने फेसबुक पर प्रतिक्रिया की कि मैंने कविता, कहानी, उपन्यास पढ़ना छोड़ दिया था, पर जब एक मित्र ने सलाह दी कि ‘मुर्दहिया’ जरूर पढ़ो तो अपने को रोक नहीं पाया. इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि इसको एवं ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘जूठन’ मिलाकर मैंने डेढ़ दलित आत्मकथाएँ पढ़ी हैं. जूठन को उसने केवल आधा आत्मकथा का वैल्यू दिया. जबकि जूठन ही एक सम्पूर्ण (जीवन) की कथा है, मुर्दहिया में तो आत्मकथाकार ने खुद ही घोषणा कर रखी है कि इसका दूसरा खंड भी आएगा पर इसे उस व्यक्ति ने पूरी आत्मकथा माना. दसेक से अधिक हिंदी दलित आत्मकथाओं में से केवल डेढ़ को स्वीकारने की यह ग्रंथि क्या है?
अपने ब्लॉग ‘समालोचन’ पर दिनांक 28 फरवरी 2011 को कवि एवं ब्लॉगर अरुण देव ने ‘मैं कहता आँखिन देखी’ शीर्षक से डा. तुलसीराम पर अपना एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार प्रकाशित किया था जिसके एक एक प्रश्न का डा. तुलसीराम ने शानदार जवाब दिया. आप देखेंगे कि इंटरव्यू में सारे प्रश्न दलितों, दलित साहित्य, दलित राजनीति एवं आंदोलन के लिए पूर्वग्रह, आग्रह एवं कुंठा के साथ आते हैं पर प्रखर वाम, अम्बेडकरवादी एवं बौद्ध चेतना के सम्यक समागम प्रो. तुलसीराम ने मियां की जूती मियां के सर डालने के अंदाज़ में सहज शांत मगर पुरजोर उत्तर दिया है. यह इंटरव्यू साहित्य, समाज, बौद्ध मत एवं मौजूं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर तुलसीराम की साफ़ समझ, अंतर्दृष्टि एवं पैनी निगाह को सामने लाता है.
यहाँ एक और चर्चा कर लेने का मैं अवकाश चाहता हूँ. तुलसीराम की आत्मकथा जिन गुणों के कारण सर्वजन का कंठहार बनी हुई है उसमें उनके ‘गुस्से का गुण’ कभी दर्ज़ नहीं होता! ध्यान रहे कि ‘गुस्सा’ दलित साहित्य का सर्वप्रमुख गुण है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनमें वह दलित गुस्सा नहीं है जिसे सवर्ण समाज हेय मानता है. यह है मगर बहुत ही फुटकर पोजीशन लिए! उनके ऐसे ही गुस्से की गंभीर बानगी मैं उनकी पुस्तक एवं जीवन से देना चाहूँगा. ‘मुर्दहिया’ के अंत में आकर, पेज 182 पर उनके गुस्से का यह रंग देखें-”…डीएवी कॉलेज की एक अन्य विशेषता यह थी कि आरआरएस प्रभुत्व के साथ साथ वह कायस्थ-बहुल कॉलेज भी था. अतः सबसे ज्यादा शोक का केन्द्र यही कॉलेज बन गया था. हमारे अम्बेडकर होस्टल के ठीक सामने एक कायस्थ परिवार रहता था. उस दिन उनके घर वाले खाना नहीं खाए और वे दूसरे दिन ही (लालबहादुर) शास्त्रीजी की शवयात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए. जाहिर है लालबहादुर शास्त्री कायस्थ थे. यह वही समय था जब अचानक एक दिन मुझे ढूंढते हीरालाल मेरे हॉस्टल आ गए…ये वही हीरा लाल थे जिन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा के शुरू में ही मुझे पीट दिया था. वे मुझे देखते ही चिरपरिचित अंदाज़ में बोल पड़े: ’का रे चमरा, कइसे हउवे?’ मेरे ‘ठीक हूँ’ कहते ही, उन्होंने मेरे पाकेट में रखी एक नई फाउंटेनपेन को छीनते हुए कहा कि आज़मगढ़ आने-जाने का पांच रुपया खर्च लगेगा. यह पैसा मुझे तुरंत चाहिए. उस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं था….मुझे बड़ी राहत मिली थी कि उनकी मांग बहुत छोटी थी. चूंकि वे बड़े हिंसक प्रवृति वाले व्यक्ति थे!”
डा. तुलसीराम के गुस्से का एक रोचक रंग मैंने साक्षात् पटना में देखा था. “अगर तुलसीदास ने रामचरित मानस आज लिखी होती तो वह साहित्यिक चोरी के मामले में जेल चले गए होते। उनकी रचना और कुछ नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण की नकल है।“-
यह बात तुलसीराम ने साहित्य अकादमी और पटना यूनिवर्सिटी हिन्दी विभाग द्वरा संयुक्त रूप से दलित साहित्य पर सन 2009 में आयोजित पटना के एक दो दिवसीय सेमिनार में कही थी। मैं भी इस सेमिनार में एक प्रतिभागी एवं वक्ता बतौर उपस्थित था. पटना के कुछ हिंदी एवं अंग्रेज़ी अख़बारों ने इस वक्तव्य को प्रमुखता से छापा था. तब डा. तुलसीराम को महान समन्वयक एवं अन्य दलित साहित्यकारों से अलग बताता सवर्ण साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों का एक तबका उबल पड़ा था. तब ऐसे लोगों की तुलसीराम एवं दलित विरोधी टिप्पणियों से फेसबुक सहित ब्लॉगों आदि भरे पड़े थे. अचरज है कि इस सेमिनार में सहभाग किये दलित आलोचक एवं कवि कँवल भारती अपने एक आलेख में डा. तुलसी राम से मुलाकात की तो चर्चा करते हैं पर तुलसी राम के इस ‘मजबूत’ दो-टूक बयान का कोई सन्दर्भ नहीं लाते.
तुलसीराम अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिस मनःस्थिति में थे, मृत्युबोध से जो नित दिन का साक्षात्कार था उनका, उसमें उनका साहित्यजगत में अपना स्वीकार पाने की चाहत स्वाभाविक ही कही जाएगी, अन्यथा ऐसी बातें आत्मश्लाघा में आती हैं. अपने मुंह मियां मिट्ठू कहा सकती थीं. ‘मणिकर्णिका’ की भूमिका में वे लिखते हैं, “यह जानकार मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रो. पी. सी. जोशी, मणीन्द्रनाथ ठाकुर तथा बद्रीनारायण जैसे जाने-माने समाज वैज्ञानिकों ने ‘मुर्दहिया’ को एन्थ्रोपोलॉजी (मानव विज्ञान) पर किया गया काम बताया. वहीं नामवर सिंह का कहना है कि ग्रामीण जीवन का जो जीवंत वर्णन ‘मुर्दहिया’ में है, वैसा प्रेमचंद की रचनाओं में भी नहीं मिलता है. इन तमाम विद्वानों ने ‘मुर्दहिया’ को वैकल्पिक सामाजिक इतिहास भी बताया है. अभी तक ‘मुर्दहिया’ की सौ से अधिक समीक्षाएँ आ चुकी हैं. परिणामस्वरूप, पचास से भी ज्यादा शोध छात्र ‘मुर्दहिया’ पर देशभर में शोध कर रहे हैं”. दरअसल, यह टिप्पणी पुस्तक के प्रकाशक की ओर से आती तो बेहतर होता. दोनों खण्डों के प्रकाशक भी एक ही हैं. आप गहरी पैठ कर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ डा. तुलसीराम ने अपने पूर्ववर्ती एवं पश्चवर्ती हिंदी दलित आत्म कथाओं पर/के विरुद्ध कुछ न कहते हुए भी एक ‘बड़ी’ टिप्पणी भी जड़ दी है!
किडनी फेल्योर से लम्बे समय से जूझते, सप्ताह में तीन-तीन कष्टदेह डायलिसिस से गुजरते आत्मकथाकार ने दोनों पुस्तकों में मृत्युबोध से आतप्त शीर्षकें यूँ ही नहीं लगाई हैं। सर्वथा सैल्यूट योग्य जांबाज, जिंदादिल इंसान रहे डा तुलसीराम। ‘मणिकर्णिका’ आत्मकथा का द्वितीय खंड है। पटना के ‘बांसघाट’ की तरह बनारस का ‘मणिकर्णिका’ घाट भी ‘हिन्दू’ शरीर के लिए एक विख्यात अंतिम शरण्य है जहाँ से हर अकुंठ धर्म-कर्म विश्वासी खुद को एवं अपने परिजनों को गुजरना चाहता है। आत्मकथा के प्रथम खंड में भी मृत्युबोध वाले नाम का ही उनने चुनाव किया है ‘मुर्दहिया’। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि किडनी फेल्योर की इस बड़ी बीमारी के बाद ही वे अपनी आत्मकथाओं के दोनों खण्डों में आये विचार पुंज को लेखनीबद्ध करवाते हैं. संभव है, अगर इस लाइलाज गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने से पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा कलमबद्ध की होती तो चीजें बहुत कुछ दूसरे रूप में भी आतीं. मृत्यु का साया जब पग पग पर पीछा कर रहा हो तो मान में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे यह तो तुलसीराम जैसा कोई भुक्तभोगी ही बता सकता है. डॉ तुलसी राम गजब जिजीविषा के व्यक्ति हैं। विरोधी परिस्थितियों में उनकी अदम्य जिजीविषा और जीवन संघर्ष एक प्रेरक मिसाल है। दरअसल, किडनी फेल्योर से लम्बे समय से पीड़ित रहने के दौरान ही उन्होंने अपनी याददाश्त को संचित-एकाग्र कर अपनी जीवनकथा लिपिबद्ध करना शुरू किया. शुरू क्या किया, करवाया. अपनी आत्मकथा के अधिकांश हिस्से उन्होंने बोलकर किसी और से लिखवाये. अतः यह मृत्युबोध उनकी आत्मकथाओं के शीर्षक में भी सहज ही मुखरित है। मुर्दहिया यानी मरघट/श्मशान घाट। ‘मुर्दहिया’ में जहाँ आत्मकथाकार ने आजमगढ़ जिले में स्थित अपने पैतृक गाँव (धरमपुर), परिवार-जाति, आसपास के गाँव-समाज, बचपन एवं स्कूली जीवन के महत्वशाली टुकड़ों एवं घटनाओं को अंकित किया है वहीं ‘मणिकर्णिका’ में बनारस में बिताये कॉलेजिया जीवन को। बनारस में आकर तुलसी राम सक्रिय राजनीति से भी जुड़ते हैं। वामपथी राजनीति के सच झूठ को वे अपने जाती-अनुभवों के चलते नजदीक से देख पाते हैं एवं उसके कुछ मुख्य संदर्भों को ‘मणिकर्णिका’ में रखते भी हैं। आप देखेंगे कि बेहद आशावादी एवं हौसले की मिसाल डा. तुलसीराम ‘मणिकर्णिका’ की भूमिका लिखते हुए जीवन के आगे के हिस्से को लेकर आत्मकथा के तीसरे खंड को लाने की घोषणा भी करते हैं जिसमें दरअसल उनके जीवन में अम्बेडकरवाद के प्रवेश की कथा भी आनी थी और महानगर दिल्ली के जीवन से अनुभव के कुछ महत्वपूर्ण टुकड़े भी. पर दुखद संयोग कि आत्मकथा की तीसरी पुस्तक के लिए लेखनी से अपने अनुभव को संजोने-समेटने को अधूरा ही छोड़ उन्हें इस दुनिया को छोड़ देना पड़ा. जिन्होंने किडनी फेल्योर से गहरे जूझते डा तुलसीराम को नजदीक से देखा है वे शर्तिया पाएंगे कि दैनिक जीवन में जीवट व अदम्य हौसला वाला इंसान साबित होते रहे हैं। हर सप्ताह उन्हें तीन कष्टसाध्य लम्बे डायलिसिस से गुजरना पड़ता था। ऐसी विकट स्थिति में कोई बोल-बोलकर दो पुस्तकों की सामग्री लिखवा लेता है तो यह एक अनोखे आत्मबल एवं जीजिविषा का प्रदर्शन तो है ही, साथ ही आश्चर्यजनक स्मृति रखने का द्योतक भी है. और तो और, ऐसी नाजुक स्थिति में भी वे अपने निवास नगर दिल्ली से दूर पटना, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि को जाकर वैचारिक गोष्ठियों सेमिनारों में हो आते थे बशर्ते उन्हें हवाई जहाज से आने जाने की सुविधा मिल जाए जिससे कि डायलिसिस की अनिवार्य चिकित्सकीय प्रक्रिया उनकी बाधित न हो।
*****
【यह आलेख गौरीनाथ के संपादन की पत्रिका ‘बया’ के तुलसीराम विशेषांक, अतिथि संपादक श्रीधरम, में प्रकाशित है】