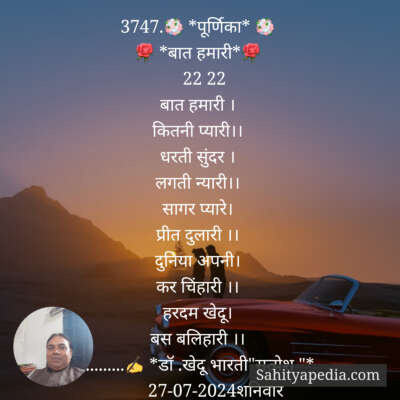चरागों को लहू से जलाते हैं
कभी नजरें झुकाते हैं कभी नजरें चुराते हैं
जिन्हें सीधा समझते हैं वह अक्सर गुल खिलाते हैं
फ़ज़ा फ़िरक़ापरस्ती की खड़ी है हाथ फैलाए
चले आओ मुहब्बत के दिये मिलकर जलाते हैं
ज़ियादा बोलकर हम कुछ न कह पाए कभी उनसे
वह चुप रहकर हमेशा ही बहुत कुछ बोल जाते हैं
अंधेरा नफरतों का मुल्क में अब आ नहीं सकता
मुहब्बत के चराग़ों को लहू से हम जलाते हैं
यहीं मंदिर यहीं मस्जिद, है गिरिजा और गुरुद्वारा
इसी मिट्टी से माथे पर तिलक अपने सजाते हैं
उन्हें आता है रिश्तों को निभाने का हुनर ‘अरशद’
जो बाज़ी जीतकर अक्सर खुशी से हार जाते हैं