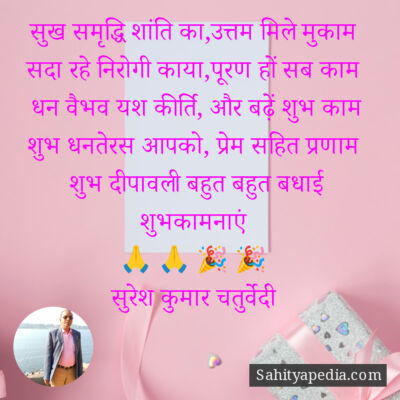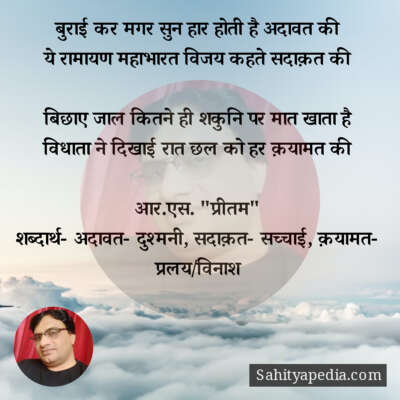गगरी का अंतस
इक रोज गई थी दरिया पर गगरी अपनी भर लाने को
सुन्दर सी अपनी गगरी में पावन जल भर इठलाने को
मोहक सी अपनी गगरी में जल भरकर बल खाने को
स्वच्छ सुनहरी गागर को तटिनी से पोषित करने को
चली जा रही आत्ममुग्ध सी, गगरी पर अभिमानी सी
स्वर्ण दीप्ति से चमकीली, गगरी पर अपनी गर्वित सी
हर्षित मन से आल्हादित, धुन में अपनी राह चली थी
ठुमक ठुमक कर गगरी लेकर तरंगिणी तट पहुँची थी
उत्साहित हो गगरी को मैने सरित-सलिल से सींचा था
उफ् लेकिन हाय पलभर में सपनों का मंदिर टूटा था
स्वच्छ सुनहरी गगरी का जल इतना कैसे दूषित था
व्याकुल सी और आहत सी मैं दिशाहीन सी बैठी थी
अज्ञानी और अल्पमति मैं बहुत सोच में विचलित थी
गागर को ही बहुत ध्यान से, देखा और फिर पाया था
स्वर्णिम आभा की मेरी गगरी बस बाहर से निर्मल थी
चमकीली मेरी गगरी का अंतस कई तरह से दूषित था
गगरी का जो अंतस है, वो मेरे मनवा की मानिंद है
गगरी के बाहर का हिस्सा, मेरी देह के रूपक जैसा
देह को मैंने खूब सजाया, मन को कैसे भूल गई मैं
मन को विस्मृत करके मैंने केवल तन चमकाया था
मेरी गगरी के अंतरतम में काला गंदला मैल जमा था
क्रोध, काम के संग वहाँ मद, मोह, लोभ का डेरा था
द्वेषभाव की कालिख के संग अहंकार का तम भी था
बाहर से चारू मेरी गगरी भीतर से हाय कलुषित थी
खूब प्रेम से रगड़ी गगरी, करुणा का लेप लगाया था
अहम् को बिसराकर फिर मैंने अंतस को चमकाया था
ईश के पावन प्रेम के जल से फिर गागर भर लाई थी
दर्पण से इस स्वच्छ नीर को पाकर सुख से मुस्काई थी
डाॅ. सुकृति घोष
ग्वालियर, मध्यप्रदेश