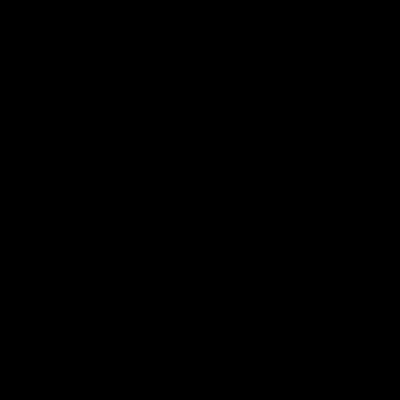काश्तकार
प्रस्तुत है एक छंदमुक्त रचना !
काश्तकार
—————–
उसकी मैली धोती फटी थी
कोट भी फटा था
कमीज भी फटी रही होगी
बनियान तो शायद नही ही होगी
उसकी आँखों में खोयापन था
पाँवों की गति में वृद्धापन था
वह काश्तकार था
वह अपनी नजर में
कुदरत का शिकार था
उसी ने कहे थे ये शब्द
“बाबूजी ! काश्तकार की जड़
जमीन से एक बलिश्त ऊँची होती है
हमारी तो डोर
परमेश्वर के हाथ होती है
काश्तार तो जुआरी होता है बाबू !
चाँदी को मिट्टी में फेंकता है
पासा चित्त आये
तो चाँदी ही चाँदी
पासा पट्ट पड़ा तो
बस आँधी ही आँधी ।
पिछले जनम में शायद हमने
बहुत पाप किये थे
तभी तो इस जन्म में काश्तकार बने हैं
सच कहता हूँ बाबूजी
हमारे खून पसीने को बेचकर
ये सब सेठ बड़े बड़े साहूकार बने हैं
अबकी बार आलू बोये हैं
उन्हें ठंड मार गयी है
ऐसा लगता है बाबूजी !
हमारी जिन्दगी
घिसटते घिसटते हार गयी है
कुछ गेहूँ भी लगाये हैं
देखो कैसी फसल होती है ?
सच कहता हूँ बाबूजी !
काश्तकार की जड़ तो
हकीकत में जमीन से
एक बलिश्त ऊँची होती है “।
—
महेश जैन ‘ज्योति’,
मथुरा ।
***