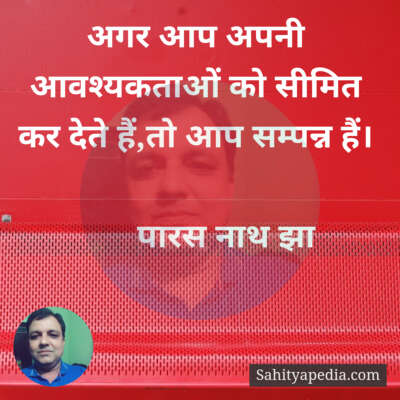काव्य में सत्य, शिव और सौंदर्य

सत्य का संबंध लोकमंगल या मानवमंगल की कामनामात्र से ही नहीं, मानव मंगल के लिए काव्य में अपनाए गए उस वैचारिक एवं भावात्मक पक्ष से भी है, जिसमें आचार्य शुक्ल के अनुसार-‘‘उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा आदि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखने को मिलती है, कवि जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होता है, उसी प्रकार अंधकार को हटाने में भी सौंदर्य का साक्षात्कार किया जा सकता है।’’
आचार्य शुक्ल ने काव्य में सत्य की स्थापना के लिए काव्य के जिस वैचारिक पक्ष की ओर संकेत किया है, उस मंगलकारी वैचारिकता का पूर्ण दर्शन हमें कबीर की उन रचनाओं में होता है, जिनमें क्रोध आदि के उग्र और प्रचंड भावों के विधान अपनी तह में करुणा का मार्मिक पक्ष संजोए हैं। इसलिए कबीर की दार्शनिक अभिव्यक्ति ही नहीं, खंडनात्मक अभिव्यक्ति में भी सौंदर्य का साक्षात्कार किया जाना चाहिए। लेकिन शैली के महाकाव्य ‘द रिबोल्ट ऑफ़ इस्लाम’ के नायक-नायिका के अत्याचारियों, आतातायियों के प्रति विद्रोही चरित्र की भूमिका की महत्ता स्वीकारने वाले आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, कबीर के धर्म-पाखंडियों पर किए गए प्रहारों को तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते? बल्कि उनकी लोकमंगल की सारी-की-सारी साधनावस्था मात्र तुलसी की साधनावस्था बनकर रह जाती है, जिसमें सत्य, शिव और सौंदर्य के नाम पर एक ऐसे मार्ग की खोज की जाती है, जिस पर चलने वाले भक्त के सहयात्री या शुभचिंतक वह मूल्य होते हैं जो संप्रदाय, व्यक्तिवाद, जातिवाद के उन लक्ष्यों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जहां लोक की एक ऐसी कीर्तनियां मुद्रा बन जाती है, जिसमें ‘‘भक्त लोग उपदेश, वाद या तर्क की उपेक्षा चरित्र श्रवण और चरित्र कीर्तन का ही अधिक नाम लिया करते हैं।’’
साहित्य के शिव या मंगलपक्ष को तर्कवाद, उपदेश अर्थात् वैज्ञानिक चिंतन से काटकर सौंदर्य के साक्षात्कार का भला इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? अवैज्ञानिकों तरीकों से की गई साहित्य की रसपरक, सौंदर्यपरक व्याख्याओं में जब तर्क की गुंजाइश ही नहीं हो तो चाहे जैसे कबीर की रचनाधर्मिता का खंडन किया जा सकता है और चाहे जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसी को लोकमंगल, मानवमंगल का दृष्टा, चिंतक घोषित किया जा सकता है।
‘काव्य की साधनावस्था, जब लोकमंगल की साधनावस्था है’ जैसा कि आचार्य शुक्ल कहते हैं। वह यह भी मानते हैं कि-‘‘सब प्रकार के शासन में ‘चाहे धर्मशासन हो, चाहे राजशासन या संप्रदायशासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राजशासन तथा नर्क का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्मशासन और मतशासन चलाते आ रहे हैं।’’
तब प्रश्न यह है कि आचार्य शुक्ल ने, ढोंगी, सांप्रदायिक, धार्मिक आडंबर से युक्त वर्ग की कलई खोलने वाले कबीर जैसे समाज सुधारक के काव्य को सत्य, शिव और सौंदर्य के पक्ष से क्यों काट डाला? इसी तरह शैली के काव्य की सार्थकता को स्वीकारते हुए टाॅलस्टाय के भ्रातृत्व प्रेम को खारिज करने के पीछे शुक्लजी की क्या मंशा रही है? देखा जाए तो इसके मूल में आचार्य शुक्ल की वह वैचारिक अवधारणाएं रही हैं, जो हर प्रकार के मंगल, लोककल्याणकारी, दयामय या उग्र और प्रचंड भावों के रूप में क्रोध और विद्रोह से युक्त अभिव्यक्ति का साक्षात्मकार अलौकिक शक्तियों जैसे राम-कृष्णादि के क्रियाकलापों में ही कर सौंदर्यसिक्त, रससिक्त होती है।
अतः यह कहना अनुचित न होगा कि आचार्य शुक्ल की सौंदर्य-दृष्टि के पीछे कहीं-न-कहीं ऐसे संस्कार अवश्य कार्य कर रहे हैं, जिनका कथित धार्मिक परंपराओं से कहीं-न-कहीं गहरा जुड़ाव है और यह धार्मिक जुड़ाव ही उनको वास्तविक और लौकिक सौंदर्य की पकड़ से परे कर डालता है।
भक्तिकाल की तरह सत्य के नाम पर जिस असत्य, अमंगल और असौंदर्य की स्थापना रीतिकाल में हुई है, वह व्यक्तिवाद का ऐसा जीता-जागता नमूना है, जिसमें नारी भोगविलास, कामुकता, रतिक्रिया में लीन नायिका का ऐसा बिंब प्रस्तुत करती है, जिसे न तो ब्रज में लगी आग की चिंता है और न भूखे-प्यासे बच्चों की। वह तो सामाजिक-पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा कर सिर्फ कृष्ण से मिलन में ही अपने उत्साह की जोर-आजमाइश करती है। दूसरी तरफ अलौकिक नायक कृष्ण, राधा और गोपियों के साथ ऐसी रस की होली खेलते रहते हैं, जिसमें डाले गये रंग, कपोल-चोली से लेकर जाने कहां-कहां अपना प्रभाव छोड़ते हैं।
सामाजिक दायित्वों, मर्यादाओं का यह खुला उल्लंघन लोकमंगल के नाम पर कैसे सौंदर्यात्मक मूल्यों की स्थापना करेगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, लेकिन इस अमर्यादा, असमाजिकता का जिक्र करने का साहस उन विद्वजनों में भला मिल ही कैसे सकता है, जिनकी बौद्धिक क्षमताओं को कथित अलौकिक शक्तियों का जादू निगल गया हो। वे तो काव्य की सार्थकता, मार्मिकता, उक्ति वैचित्रय, बिंबात्मकता ऐसे ही दृष्टांतों में खोजेंगे कि कोई गोपी पानी भरने के लिए जमुना तट पर जा रही होगी, तथा काली-काली घटाएं घिरेंगी, बरसात होगी और गोपी की यह हालत होगी-
रपट्यौ पग घाट चढ्यौ न गयो
कवि मंडन ह्वै कै विहाल गिरी
चिर जीवहु नन्द कौ बारौ अरी
गहि बांह गरीबन ठाढ़ी करी।
अर्थात् गोपी पनघट पर बरसात के कारण धड़ाम से गिरेगी। नंदलाल कृष्ण जहां कहीं भी होंगे, उन्हें इस घटना का पता तो लग ही जाएगा [ वह अंतर्यामी जो ठहरे ], वे करुणा से द्रवीभूत गोपी के सामने प्रकट होंगे और उसकी बांह पकड़कर उठाएंगे। गोपी इस एहसान से द्रवीभूत होगी। चूंकि बरसात हो रही है, नायक-नायिका आमने-सामने हैं, इसके बाद क्या होगा, अनुमान पाठक स्वयं लगा सकते हैं। बरसात में किस गरीब की छत गिरी, किस गरीब का बच्चा निमोनिया का शिकार हुआ, किसका घर बाढ़ में डूबा? नंद किशोर के मन में ऐसे ब्रजवासियों के प्रति दया और करुणा के भाव क्यों जागृत नहीं होते? क्या उन्होंने गोपियों के साथ रतिक्रियाओं के माध्यम से ही लोकमंगल का ठेका ले रखा है?
कहने का अर्थ यह है कि मात्र रूप या देह भोग के माध्यम से सौंदर्य की स्थापना करने वाले कवि या रसमीमांसक न तो सत्य की स्थापना कर सकते हैं और न शिव की। सत्य शिव की स्थापना के लिए आत्मा के उस सौंदर्य की आवश्यकता पड़ती है जो शारीरिक सौंदर्यात्मकता को लोकमंगलकारी बनाता है। प्रेम की सार्थक और शाश्वत अर्थवत्ता तो कुछ इसी प्रकार के सदंर्भों में देखी जा सकती है जिसमें सामाजिक-पारिवारिक दायित्वों के बीच पसरे संघर्ष की मार्मिकता को साहस और उत्साह, प्रेम के साथ और अधिक प्रगाढ़ करता हुआ चला जाता है-
‘‘पहले की तरह अब भी
अच्छी लगती हैं तुम्हारी बांहें
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम
उन्हें कुहनियों तक ढकी रखो
पहले की तरह तुम मुझे
अब भी विदा करती हो
लेकिन मेरी छाती पर खुली बटन
बंद कर देती हो।’’
सुदामा पांडेय धूमिल की ‘गृहयुद्ध’ शीर्षक से लिखी गई उक्त कविता में नायक-नायिका जिस सत्य की ओर इशारा करते है, वह सत्य हमें अजगरी व्यवस्था के उस चेहरे की पहचान कराता है, जो महंगाई के रूप में परिवार की सुख-शांति, प्रेम को निगलता जा रहा है। नायिका पारिवारिक संघर्षों में इतनी चुक गई है कि नायक उसकी कमजोर बांहों [ जो उसे अब भी अच्छी लगती हैं ] को कुहनियों तक ढंक देना चाहता था और नायक का शरीर इतनी दुर्बलता का शिकार हो गया है कि नायिका उसे काम पर भेजने से पूर्व, विदा करते समय, उसकी छाती के बटन रोज बंद कर देती है ताकि उसकी छाती पर उभरी पसलियां किसी को न दिखें।
उक्त कविता में कवि प्रेम के लिजलिजे कोरे रूप सौंदर्य से कोई प्रेम की सुखात्मक अनुभूति ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसे तो वास्तविक सुख की अनुभूति कर्मक्षेत्र में होती है। वास्तविकता तो यही है कि एक-दूसरे के सुख-दुख में हिस्सेदारी करने वाले पात्रों की आपसी सूझबूझ ही एक ऐसे राग तत्त्व का निर्माण करती है, जिसकी रसात्मकता शाश्वत और अखंड सौंदर्य की पूर्णता की ओर ले जाती है, जिसमें नायिका की आंखें आंखें नहीं रह जातीं, बल्कि गरीबी की मार से लड़खड़ाते नायक के लिए सहारा देने वाले हाथ बन जाती हैं-
‘‘पत्नी की आंखें, आंखे नहीं हैं, जो मुझे थामे हुए हैं।’’
प्रेम के चरमोत्कर्ष की भावात्मक अभिव्यक्ति भला इससे बढ़कर और क्या हो सकती है, जो किसी भी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रसादन, अवसादन या कुतूहल मात्र को जन्म न देकर ऐसे आनंद की सृष्टि करती है, जो रस के नाम पर पाठक या श्रोता को पलायनवादिता या व्यभिचार का विष नहीं देती। वह तो पाठक या श्रोता के मन में ऐसे माधुर्य का प्लावन करती है, जिसके कारण स्वार्थमय जीवन की शुष्कता और विरसता विलुप्त हो जाती है। अगर सही अर्थों में देखा जाय तो यही कविता का कवितापन है, सत्य है, मंगलकारी तत्त्व है तथा चिरसौंदर्य की स्थापना का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
———————————————————————
रमेशराज, 15/109, ईसानगर, अलीगढ़-202001
मो.-9634551630