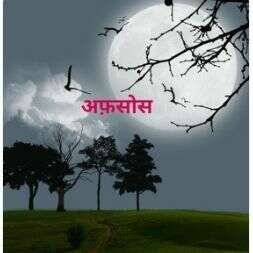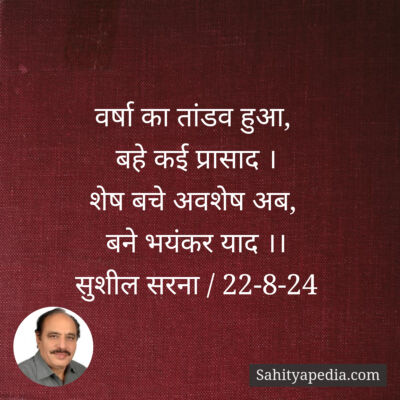कविता
समाज हमारा बन रहा क्यों प्रताड़ना का बाजार
मानवता हों रही कलंकित बनी वासना का औजार
हो रहा निस काल विसंगत, बढ़ रहा व्यभिचार
प्रलय घटा बन काम वासना कर रही हाहाकार।
अनैतिकता का कोहरा सघन हो रहा
दीन ईमान का दहन हो रहा।
स्वार्थांध में मनुष्यता की नित शिला ढह रही
आशाओं की ज्योति भी मलिन हो रही।
तड़पती मछली बन नारी इसी समाज के बीच बाजार
रहते देख बन मूक-बधिर, मानों जमा नसों का रक्त संचार
ओह!हे ईश्वर। कह विचलित होकर मन ही मन सिहरते
यूं बीच सड़क में छोड़ निर्भया को, पास से सब गुज़रते
बाद में केंडल मार्च निकालते बनकर के अवतार
स्वस्थ समाज के रहने वाले, मानसिकता से बीमार।
हैं सब भावनाएं दम तोड़ रहीं,श्वास छोड़ रही संवेदना
आत्मग्लानि पश्चात की भी क्षीण हो रही संभावना।
हो घड़ी रेत की निज जीवन झरता
डर दहशत ,ध्वज बनकर फहरता।
गंदी निगाहों से तेजाब बरसता
काम वासना का व्यभिचारी लगा ठहाके खूब हरसता।
क्यों होगयी तेरी सुप्त चेतना
जागती क्यों नहीं अंत: वेदना।
नहीं सुरक्षित रहीं बहन बेटियां
करो उपाय, कहीं रहे खेद न।
नीलम शर्मा