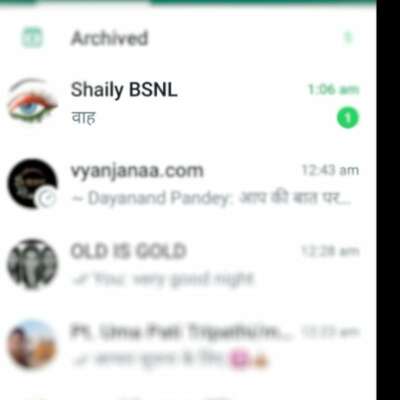कली बुझी बुझी हुई गुलों में ताज़गी नहीं
कली बुझी बुझी हुई गुलों में ताज़गी नहीं
सभी बहुत उदास हैं नसीब में ख़ुशी नहीं
बहार वादियों से छीन ले गई है ख़ुश्बुएं
चमन परस्त बागवाँ की नींद पर खुली नहीं
हमें भी देख एक दिन तो सरहदों पे भेज कर
उबल रहा लहू जिगर में आग़ कम लगी नहीं
जो कर सका पलट के पत्थरों से वार कर गया
निगाह खोजबीन की उधर कभी उठी नहीं
हजार बार बात ये कही गई सुनी गई
महज हो एक वोट तुम कहीं से आदमी नहीं
तुम्हें यकीन ही कहाँ मेरे किसी सबूत पर
उसी पे मर मिटे किसी का जो हुआ कभी नहीं
राकेश दुबे “गुलशन”
15/07/2016
बरेली