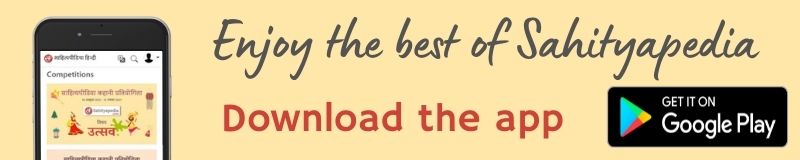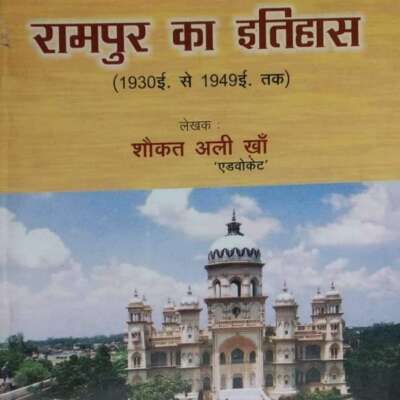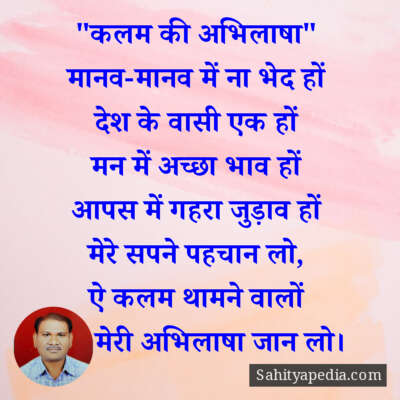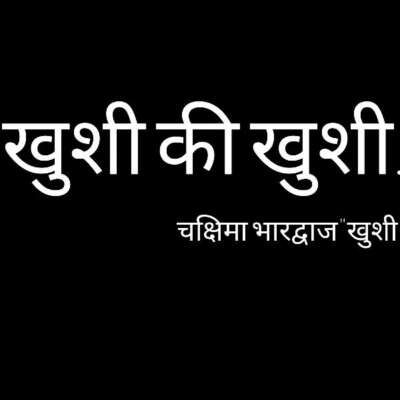हिन्दी दलित आत्मकथाओं में स्त्री संदर्भ / musafir baitha
अब तक मौलिक रूप से हिन्दी में जो करीब एक दर्जन दलित आत्मकथाएं प्रकाशित हैं उनमें महज एक की ही रचयिता महिला है। दोहरा अभिशाप की लेखक कौसल्या बैसंत्रा एकमात्र हिन्दी दलित आत्मकथाकार हैं। वैसे, आधी आबादी का हाल पूरे हिन्दी आत्मकथा लेखन परिदृश्य में ही बहुत आश्वस्तिपरक नहीं है। वस्तुतः आत्मकथा लिखने के लिए एक बड़े नैतिक और वैचारिक साहस की जरूरत होती है, जिसके बिना उसके साथ न्याय करना कदापि संभव नहीं है। ‘जो घर जारै आपनो…’ का माद्दा लेकर ही ऐसी आत्मछील लेखनी चलाई जा सकती है, जो कि काफी असहज काम है।
हिन्दी साहित्य की पहली दलित आत्मकथा ‘अपने अपने पिंजरे’ ;प्रकाशन वर्ष 1995द्ध, और पहली दलित स्त्री ‘दोहरा अभिशाप’ (प्रकाशन वर्ष-1999) में आती हैं जबकि 1977 में आई अमृता प्रीतम की आत्मकथा ‘रसीदी टिकट’ समूचे हिन्दी साहित्य की ही पहली स्त्री आत्मकथा के रूप में नमूदार होती है। पर बीच क तकरीबन तीन दशक के काल काल में स्त्रा आत्मकथा का अकाल ही नजर आता है। फिर तो एक लंबे अंतराल के बाद 2002 में आकर हमें ‘कस्तूरी कुण्डल बसै’ और ‘गुड़िया भीतर गुड़िया’ (मैत्रेयी पुष्पा) सामने आती मिलती है। इध्र के काल में स्त्रा पक्ष से जरूर कुछ अच्छी आत्मकथाओं का प्रणयन हो रहा है जो कि एक सकारात्मक ट्रेण्ड है। हिन्दी साहित्य में दलित आत्मकथा और स्त्रा-आत्मकथा लेखन की सवर्था नई क्रांतिर्ध्मी संभावनाएं दिनानुदिन बलवती होती जा रही हैं। मैत्रोयी के अलावा प्रभा खेतान की ‘अन्या से अनन्या’, रमणिका गुप्ता की ‘हादसे’, मन्नू भण्डारी की ‘एक कहानी यह भी’ दलितेतर आत्मकथाएं भी देखी जा सकती हैं जिन्होंने स्त्रा संघर्षों, वंचनाओं, उपेक्षाओं के स्वानुभूत पक्ष को कापफी तल्खी, निर्भयता एवं बोल्डनेस से रखा है। इनमें सामंती नैतिकता और तहखानों की बेड़ियों के बरक्स खुले औद्योगिक समाज की टकराहटें हैं। इन्हें पढ़कर कुलीनता की बेड़ियों में जकड़े उन जख्मी पैरों का बिम्ब सामने आता है जिनके सामने खुले रास्तों का प्रलोभन है। सन् 2007 में आई प्रभा खेतान की आत्मकथा ‘अन्या से अनन्या’ में आत्मस्वीकार का जो साहस है वह भारत जैसे रूढ़िप्रवण एवं बंद समाज में लीक से हटकर कुछ सकारात्मक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कितनों में इतना दम है कि वह सार्वजनिक रूप से प्रभा की तरह यह घोषित कर सके कि उसने एक पुरुष के साथ अठाईस साल बिना शादी के ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में गुजारे, मनचाहे गर्भधारण किए व गर्भपात कराये। ऐसी आत्मकथा के लिए जोखिम भरी जिंदगी जीने की कूवत भी तो चाहिए।
हिन्दी की मौलिक दलित आत्मकथाओं में स्त्रा विमर्श के संदर्भों की बात करें तो कौसल्या बैसंत्रा और सूरजपाल चौहान ने अपने अपने आत्मकथनों में अपने घर-परिवार की आमतौर पर गोपनीय रखी जाने वाली निजता को बड़े जीवट से सरेशाम उघाड़ने का हौसला दिखाया है। इन आत्मकथाकारों की आत्मबयानी इस हद तक अंतस् को खोलने वाला है कि पाठक इनकी करुण भावनाओं के साथ एकदम से एकाकार हो जाने को मानो विवश हो जाता है। इन दोनों आत्मकथाओं में स्वजनों-प्रियजनों के प्रति दिखलाई गई नाराजगी व शिकवे-शिकायतों में भी एक निरीहता और निश्छलता जैसी दिखती है। वैसे, मेरे इस कथन को किसी पक्षध्रता का संकेतक न मान लिया जाए। इन आत्मकथाकारों के परिजनों का पक्ष जाने बिना आत्मकथाकार के बयानों, परिवादों, उलाहना-उत्तापों को सही करार देना एकपक्षीय कार्रवाई होगी।
सूरजपाल चौहान ने अपनी प्रथम आत्मकथा पुस्तक ‘तिरस्कृत’ अपनी मां को समर्पित की है जो अकारण नहीं है। आत्मकथा की कई हृदयद्रावक घटनाओं के केन्द्र में बालक सूरजपाल के साथ उसकी माँ का जीवन संघर्ष, रोजी-रोटी, हाड़ी-बीमारी से लेकर मौत का संघर्ष चित्रित है।
‘तिरस्कृत’ में दैहिक विमर्श के प्रसंग में स्त्रा प्रसंग कापफी विस्तार और भिन्नता लिए हुए हैं। ये प्रसंग कापफी बेबाक, विडम्बनापूर्ण और बेध्क भी हैं। इन विवाहेतर या कि जार संबंधें की चर्चा ‘तिरस्कृत’ में दो बार आती है और दोनों ही बडे़ सार्थक ढंग से। पहली घटना लेखक के बचपन की है। गांव की ठकुराइन का संबंध् सूरजपाल के चाचा से था। यह रोचक है कि ठकुराइन लेखक के साथ छूत बरतती थी पर उसके चाचा के साथ ‘उलझी’ रहती थी। एक बार आपत्तिजनक अवस्था में लेखक द्वारा देख लिए जाने पर अपनी पोल खुल जाने के भय से ठकुराइन ने लेखक से छूत करना बंद कर दिया, स्नेह दिखाने लगी। अब वह अपने घर से चोरी-छुपे खाना लाती और लेखक को खिलाती। दूसरा प्रसंग स्वयं लेखक की पत्नी का है जिसमें उसके भतीजे के संबंध् बनते हैं और वह उसके साथ चली जाती है। सूरजपाल द्वारा वर्णित अपनी पत्नी का अपने भतीजे के साथ प्रेमालाप प्रसंग हृदय को कापफी विचलित कर देने वाला है। इस प्रसंग को कलमब( करने में यहां उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस प्रसंग पर विवाद और आलोचना भी हुए हैं। ‘जूठन’ के लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि तक इस हद तक निजता को सार्वजनिक करने पर आत्मकथाकार से अपनी असहमति जताते हैं। सूरजपाल की पूरक या कि उत्तरवर्ती आत्मकथा, जो सन् 2007 में ‘संतप्त’ नाम से आई, में इन प्रसंगों का अध्कि विस्तार के साथ वर्णन आया है। लेकिन दोनों ही करुण प्रसंगों की चर्चा लेखक ने बड़ी ही शालीनता व ध्ीरज के साथ की है, न तो उसमें उत्तेजना है, न ही अशिष्ट-अश्लील शब्दों का प्रयोग। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह कि उसमें संभावित घृणा की बजाय बड़ी गहरी करुणा या कि करुण उलाहना दिखती है- उसने मेरा और अपना बुढ़ापा तो बिगाड़ा ही, मध्ुर और भानु का जीवन भी नष्ट करके रख दिया। मध्ुर और भानु लेखक के बेटी-बेटे हैं। एक-दूसरे से भिन्न प्रकृति के ये दोनों अवैध् संबंधें के उदाहरण साबित करते हैं कि यह मामला जार ब्राह्मण-पुरुष अथवा दलित स्त्रा बनाम सवर्ण स्त्रा का नहीं है अपितु हमारे पूरे सामाजिक संगठन का है, उसमें बनने वाले स्त्रा-पुरुष संबंधें का है, जिस पर गंभीरता से विचार की आवश्यकता है। यहाँ चर्चित दलित लेखिका डा. रजत रानी मीनू के विचार भी द्रष्टव्य हैं- ‘‘आत्मकथा पुस्तक में लेखक वाकई डंडा लेकर खड़ा है। इस डंडे से उसका अपना घर भी बरबाद हुआ है। पत्नी पर भी डंडे की मार इतनी तीव्र पड़ी है कि वह घर से बाहर दूसरे की छत के नीचे कराह रही हैं। यहाँ बिना प्रमाण के एक पक्ष को तो दोषी मान लेना उस स्त्रा के साथ नाइंसाफी होगी जो आज अपना घर खो चुकी है। कारण क्या रहे, कौन दोषी है, यहां मैं गहराई में नहीं जा रही, न ही उसकी वकालत कर रही हूं, परंतु, मुझे ऐसा लगता है कि यह आत्मकथा के अंश नहीं होने चाहिए क्योंकि तत्काल घटी घटनाओं के रिजल्ट आने में समय लगता है। कई बार आपसी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रसंगों को देना क्या जल्दबाजी नहीं है? एक स्त्रा होने के नाते मैं स्त्रा के मर्म को समझ सकती हूं। यह त्रासदी है कि दलित स्त्रियां कथाकार मन्नू भंडारी नहीं हैं जो पतियों द्वारा लिखी आत्मकथाओं में अपनी आलोचना की सफाई दे सकें या अपना पक्ष प्रकट कर सके। अभी पक्ष ही पाठकों को सामने आ रहा है।’’1
दोहरा अभिशाप (कौसल्या बैसंत्री), सन् 1999 में प्रकाशित यह आत्मकथा दो मोर्चों पर प्रथम होने का गौरव रखती है। शीर्षक ‘दोहरा अभिशाप’ स्पष्टतः दलित के इसी सवर्ण समाज और दलित पुरुष समाज से मिली यंत्रणाओं को लक्ष्य कर रखा गया है, जबकि कारुणिक सच यह भी है कि एक दलित स्त्रा को दोहरे ही नहीं कितने ही स्तरों पर अपने जीवन में रह-रह कर अभिशाप भोगने पड़ते हैं। यानी स्त्रियों को अभिशाप-दर-अभिशाप भोगने पड़ते हैं। किसी मराठी भाषी द्वारा हिन्दी में लिखी यह पहली आत्मकथात्मक कृति है। लेखिका ने अपनी इस आत्मकथा में न केवल दलित होने की पीड़ा को जीवन्तता दी है बल्कि महिला होने की वेदना का अहसास भी संवेदनशील पाठकों को करा दिया है। आत्मकथा से यह बात छनकर आती है कि महिलाओं के मामले में सवर्ण पुरुष की सोच एवं दलित पुरुष की सोच एक जैसी ही सामंती हो जाती है। कौसल्या बैसंत्रा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उनके व्यक्तित्व-निर्माण में सर्वाध्कि बाधएं पति समेत उनके स्वजाति-समुदाय के पुरुषों ने ही खड़ी की। यह हिन्दी दलित आत्मकथा में पहली बार हुआ है कि लेखिका ने एक दूसरे पक्ष को भी सामने रखा है कि सिपर्फ सवर्ण ही दलितों का शोषण नहीं करते, बल्कि दलित भी दलित का शोषण करने से नहीं चूकते जबकि दलित पुरुषों की आत्मकथाओं में दलित-दलन के लिए प्रायः सवर्ण ही कठघरे में रखे जाते हैं। अलबत्ता, सूरजपाल ने जरूर दलितों में भी ऊंच-नीच की ब्राह्मणवादी संस्कार पलने की घटना को प्रमुखता से उभारा है।
बाहर से पिटे को घर में शरण मिल सकती है, किन्तु घर का पिटा कहाँ जाएगा? यह बड़ी ही दुविधपूर्ण एवं असहज स्थिति होगी न। लेकिन यह आत्मकथा लेखिका का भोगा सच है। उन्होंने दाम्पत्य-संबंधें की थोपी हुई कड़वाहट को पूरे 40 साल झेला। यहाँ उनके एक व्यक्तित्व की बड़ी कमी यह निर्णयहीनता जरूर कही जाएगी कि एक उच्च-शिक्षित, जीवटवाला जीवन जीने का माद्दा रखने वाली महिला होकर भी पति से अलग होने में 40 वर्ष लेकर इस दीर्घ जीवन-अवधि् को क्यों व्यर्थ होने दिया? हालांकि कम से कम आत्मकथा-प्रणयन तक आते-आते उनका यह भटकाव महज बीता कल हो जाता है। आत्मकथा की भूमिका में वे बेबाकी से लिखती हैं- ‘‘पुत्रा, भाई, पति सब मुझ पर नाराज हो सकते हैं, परंतु मुझे भी तो स्वतंत्रता चाहिए कि मैं अपनी बात समाज के सामने रख सकूं। मेरे जैसे अनुभव और भी महिलाओं को आए होंगे परंतु समाज और परिवार के भय से वे अपने अनुभव समाज के सामने उजागर करने से डरती हैं और जीवन भर घुटन में जीती हैं। समाज की आंखें खोलने के लिए ऐसे अनुभव को सामने लाने की जरूरत है।’’2
अपनी मां और पिता की बातों को स्मृति में रखते हुए लेखिका ने उनके संघर्षों को दिखाते हुए आत्मकथा की शुरुआत की है। पुस्तक में लेखिका की मां भगीरथी बाई का जो चरित्र है वह बड़ा ही प्रभावशाली है। वह अनपढ़ होते हुए भी मेहनतकश, जुझारू, शिक्षा का महत्व समझने वाली है तथा अपनी वर्तमान त्रासद स्थिति से बाहर निकलने की छटपटाहट लिए हुए है, जिसमें वह सपफल भी होती है। यहां मां का चरित्र प्रेरणास्पद है। अनपढ़ गरीब मां के चरित्रा की मजबूती देखिए कि अपने बच्चों को शिक्षित कर वह इस काबिल बना जाती है कि वे सम्मानजनक ढंग से जीवनयापन कर सकें। इस मायने में अनपढ़ मां सुपढ़ लेखिका पर कापफी भारी पड़ती है।
आत्मकथा में तीन पीढ़ियों के जीवन-संघर्ष को रखा गया है। पहली पीढ़ी में लेखिका की आजी ;नानीद्ध का जीवन-संघर्ष है दूसरी पीढ़ी में भागरथी ;लेखिका की मांद्ध का और अंततः खुद लेखिका का जीवन है। तीनों ही जिंदगियां संघर्षों, तकलीपफों से भरी हुई हैं। लेखिका की आजी बाल विध्वा है, किन्तु बाद में उनकी दूसरी शादी होती है। विध्वा विवाह की इस परंपरा को स्त्रा-अध्किर के खयाल से अच्छा माना जाएगा। पर लेखिका ने यहां स्त्रा-अध्किर हनन का भी एक पक्ष रखा है कि ऐसी शादी में जहां विध्ुर पुरुष को कुंआरी लड़की से विवाह करने की अनुमति है पर एक विध्वा को कुंआरे का वरण करने का अध्किर नहीं था। लेखिका की नानी एक स्वाभिमानी स्त्रा है जिसने अपने जीवन में अनावश्यक रूप से कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। आजी का ‘पाट’ ;दूसरी शादीद्ध मोडकूजी ;लेखिका के नानाद्ध से कर दिया गया था। मोडकूजी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, खास करके महार जाति में वे पैसे वालों में शुमार थे। मोडकूजी की पहली पत्नी मौजूद थी जो आजी पर रोब झाड़ती थी। मोडकूजी गुस्सैल थे, बात-बेबात आजी के साथ मारपीट कर देते थे। उनके अत्याचार से आजिज आकर आजी ने एक दिन अपने तीनों बच्चों ;श्रवण, सरस्वती और भगरथीद्ध के साथ पति का घर छोड़ दिया था और काम की तलाश में नागपुर चली आई थी। नागपुर आते समय बड़ी लड़की सरस्वती की बीमारी से मौत हो गई थी। नागपुर में आजी को उसके भतीजे ने ईंट-सींमेट ढोने का काम दिलवाया। आजी अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगी। आजी पर दूसरी आफत आई जब 18 साल का बेटा श्रवण टाइपफायड की वजह से चल बसा। उनकी जिंदगी अब सिपर्फ भगीरथी ;लेखिका की माँद्ध के लिए रह गई। आजी अपने आत्मसम्मान के कारण वापस पति के घर कभी नहीं लौटी।
कौसल्या बैसंत्रा लिखती हैं कि उनकी बड़ी बहन जनाबाई की चौथी कक्षा के पढ़ाई छुड़वाई गई क्योंकि उनकी उप जाति कोसरे में उस वक्त अध्कि पढ़ा-लिखा लड़का मिलना मुश्किल था और दूसरी उपजाति में विवाह करना मना था। यह लेखिका के लिए कापफी राहत की बात थी कि उनकी शिक्षा के आड़े यह बात नहीं आई। वैसे, पढ़ाई के दौरान जाति-भेद बाला व्यवहार लेखिका खूब झेलती है। कई बार जाति छुपाकर झूठ बोलने पर भी मजबूर होती है। सवर्ण लड़के परेशान करते थे- ‘ये हरिजन बाई जा रही है। दिमाग तो देखो, इसका बाप तो भिखमंगा है, साइकिल पर जाती है।’ कहकर वे भी साइकिल से गिराने की कोशिश करते थे। अपने को उच्च-वर्गीय समझने वाली औरतें भी मुझे साइकिल पर जाते देख बड़े कुत्सित ढंग से हंसती थीं। उन्हें ताज्जुब भी होता था कि हम अछूत और मजदूर के बच्चे इतना कैसे पढ़ पाते हैं?’’3
यहां सभी स्त्रियों, दलित-सवर्ण को समान रूप से दलित मानने वालों का भ्रम टूट जाना चाहिए। दलित स्त्रियों के दर्द का रत्ती भी सवर्ण औरतों को नहीं झेलना पड़ता। यह भी कि दलित स्त्रियों को स्वर्ण महिलाओं से भी नानाविध् छूतपरक व्यवहार झेलने पड़ते हैं।
आत्मकथा में सबसे अध्कि दुखद स्थिति तो कौसल्या के खुद के साथ ही है। उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन में बुराइयों को देखा-नकारा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली मां का साथ पाया जिसने जीवन के निर्णय खुद लेने में लेखिका को सक्षम बनाया, लेकिन अपनी जिन्दगी लेखिका की नारकीय रही। पहले से ही शादी-शुदा और बाल-बच्चेदार देवेन्द्र कुमार से शादी करना उसकी जिंदगी तबाह करने का सबब बनता है और यहीं पर ‘‘कौसल्या जी की आत्मकथा से उनके पति एक भयंकर खलनायक साबित होते हैं जिन्हें वे बेशक जज की कलम से सजा न दिला पाई हों पर अपनी कलम से उन्होंने बक्शा नहीं है। आध्ी आत्मकथा उच्चाध्किरी पति की करतूतों पर ही है।’’4 जिस व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक संलग्नता से प्रभावित होकर लेखिका ने जीवनसंगी बनाया वह आदमी तो व्यवहार में जाहिलों-अनपढ़ों के भी कान काटने वाला निकला। इस कुमति पति का व्यवहार तो देखिए- ‘‘देवेन्द्र कुमार को पत्नी सिपर्फ खाना बनाने और उसकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए चाहिए थी। पैसे आलमारी में ताले में बंद रखता था और रोज दूध् और सब्जी के लिए पैसे देता था। कोई बात पूछने पर दस मिनट तक तो कोई उत्तर ही नहीं देता। मुझे कपड़े, चप्पल की सिलाई के लिए पैसे लेने के लिए बहुत ही पीछे पड़ना पड़ता, तब पैसे देता था। कभी नहीं भी देता। जब अगले महीने पैसे देने की बात आती तब कुछ-न-कुछ कारण निकाल कर झगड़ा करता। मारने दौड़ता।’’5 शादी के बाद देवेन्द्र कुमार बड़ी बेशर्मी से स्वयं ही कहता है कि मैं बहुत शैतान आदमी हूँ। लेखिका कहती है- ‘‘उसने मेरी इच्छा, भावना, खुशी की कमी कद्र नहीं की। बात-बात पर गाली, वह भी गंदी और हाथ उठाना। मारता भी वह बहुत क्रूर तरीके से।’’6 विडम्बना यह कि यह पति स्वतंत्राता सेनानी भी है जो कि घर में एक पत्नी को कोई आजादी नहीं दे सकता।
बाहर से यदि कोई अशोभनीय, कटु अनुभव मिले तो आदमी अपने घर के लोगों से समर्थन-सहयोग पाकर लड़ सकता है, लेकिन घर में भी कोई बुरा बर्ताव करने वाला, आतताई ही बैठा हो, वह भी सबसे नजदीक का आदमी, पति, तो एक अबला कहाँ ठौर तलाशे, किसी शरण गहे?
बहरहाल, सब कुछ लुटने के बाद लेखिका को सद्बुद्धि् आती है ओर वह अपने अध्किरों के प्रति सजग होती हैं। उसी सजगता का प्रमाण यह आत्मकथा भी है। लेखिका ने अपनी आत्मकथा ‘दोहरा अभिशाप’ की भूमिका में ही जैसे अपने जीवनानुभवों एवं पुस्तक का निचोड़ रख दिया है-‘‘मैं लेखिक नहीं हूं, ना साहित्यिक लेकिन अस्पृश्य समाज में पैदा होने से जातीयता के नाम पर जो मानसिक यातनाएं सहन करनी पड़ीं, इसका मेरे संवेदनशील मन पर असर पड़ा। मैंने अपने अनुभव खुले मन से लिखे हैं। पुरुष प्रधन समाज औरतों का खुलापन बर्दाश्त नहीं करता। पति तो इस ताक में रहता है कि पत्नी पर अपने पक्ष को उजागर करने के लिए चरित्राहीनता का ठप्पा लगा दे।’’7
लेखिका दलित पुरुषों को दलित स्त्रियों का हिमायती मानने से एकदम इनकार करती है। यह आन्दोलन के लिए एक बड़ा प्रश्न चिह्न है और चुनौती भी। अपनी आत्मकथा के अंत में वे दलित स्त्रियों का प्रवक्ता बन कहती हैं- ‘‘आज के अनुभव से हमने सीख लिया है कि अगर हम स्वाभिमान से अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो हमें अपने पांव पर खड़ा होकर अपने पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपने अंदर शक्ति पैदा करनी होगी। किसी का सहारा लेकर चलने से काम नहीं बनेगा।’’8
‘झोपड़ी से राजभवन’ के आत्मकथाकार माता प्रसाद समाज की परंपरा के अनुसार लरिकाई में ही दाम्पत्य-सूत्रा में बंध गए। 10 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और 14 वर्ष की आयु में गौना के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी अवयस्क कंधें पर आ गई। लिखने-पढ़ने की उम्र में घर बसने से जीवन चौपट होना तय लग रहा था, पर चतुर, भविष्यद्रष्टा नाबालिग पत्नी ने पढ़ने में बाधा न बनकर प्रगति का ही रास्ता प्रशस्त किया। संयुक्त परिवार में लेखक के हिस्से आए काम का अतिरिक्त भार भी खुद पत्नी संभालती रही और लेखक पढ़ते-बढ़ते रहे। कुछ समय पढ़ाना-पढ़ना साथ भी चला। संतानोत्पत्ति में अभी की सरकार परामर्शित सीमा को ऊंचा लांघ गए माता प्रसाद अपनी संतान-विषयक जिम्मेदारियों में भी अतिरिक्त सतर्क रहे। उनके तीनों पुत्रा अच्छे ओहदों एवं आर्थिक स्थिति में हैं और दोनों बेटियां भी अध्यापिका हैं और सुखी-संपन्न ब्याहता जीवन जी रही हैं। पत्नी लखराजो देवी यह सुख साक्षात होते देख रही है कि कैसे उनके वटवृक्षी व्यक्तित्व तले इतने जीवन को सुघड़ भविष्य मिल पाया है। लाख दुख सहकर अर्जित इस सुख को देखना हिय को कितना जुराने वाला होगा, यह लखराजो के सिवा कौन बता सकता है? लेखक का बकलम खुद है कि ‘‘सन् 1957 ई. में प्रथम बार जब मैं विधन सभा का चुनाव लड़ने गाया, तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। श्रीमतीजी के चार थान चाँदी के गहनों को बेच गया। उससे लगभग पौने पांच सौ रुपये मिले। इसी रुपये से जमानत की राशि 125/- रु. जमा की गई। श्रीमती जी के गहने जो गए तो आज तक में उन्हें बनवा नहीं सका। कभी-कभी इसकी उलाहना सुननी पड़ती है।’’9
ओमप्रकाश वाल्मीकि ने भी अपनी आत्मकथा ‘जूठन’ में दलित कौम की स्त्रियों के साथ होने वाले अमानवीय व सवर्ण मंशा की परतों एवं इससे उपजी विडंबना को खोला है। जाति छुपाने का एक वाकया, जिसके सच होने से इनकार नहीं किया जा सकता, यह है कि ओमप्रकाश वाल्मीकि की भतीजी सीमा लेखक को अपना चाचा बताने से बचती है। संदर्भ लेखक की जुबानी ही सुन लीजिए-‘‘मेरी भतीजी सीमा बी.ए. कर रही थी। कथाकार डॉ कुसुम चतर्वेदी हिन्दी विभागाध्यक्ष थीं। एक दिन बातचीत के दौरान, मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरी भतीजी आपकी स्टूडेंट है। अगले रोज कक्षा में जाते ही डॉ. चतुर्वेदी ने सीमा से पूछ लिया कि ओमप्रकाश वाल्मीकि को जानती हो? सीमा ने कक्षा में एक नजर डाली और इनकार कर दिया।’’10
समाज में जातिगत भेदभाव की खाई की भयावहता को समेटे इस घटना का चरम तो सीमा के उस बात में अभिव्यक्ति पाता है जब सीमा लेखक के हृदय को छलनी करते हुए कहती है- ‘‘सभी के सामने अगर मान लेती कि आप मेरे चाचा हैं तो सहपाठियों को मालूम हो जाता कि मैं ‘वाल्मीकि’ हूं… आप पफेस कर सकते हैं, मैं, नहीं कर सकती… गले में ‘जाति’ का ढोल बांध्कर घूमना कहां की बुद्ध्मिनी है?’’11 यहां लेखक वाल्मीकि की वेदना की तीव्रता को हम महसूस कर सकते हैं। वाल्मीकि अपनी सतर्क?-संयमित टिप्पणी यों करते हैं- ‘‘सीमा के तर्क समूची व्यवस्था की विद्रूप तस्वीर बनकर सामने खड़े थे। सीमा और चंदा, दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया मेरे सरनेम के खिलापफ।’’12 उस परिवार की लड़की सविता से इस बारे में बात करते हैं। बातचीत में सविता के संस्कारगत जातीय दुराग्रह की परतें कापफी रोचक ढंग से उघड़ती हैं। संवाद द्रष्टव्य है13 –
‘उसे चाय अलग बर्तनों में पिलाई थी?’ मैंने सख्त लहजे में पूछा।
हां, घर में जितने भी एस.सी. और मुसलमान आते हैं, उन सबके लिए अलग बर्तन रखे हुए हैं।’ सविता ने सहज भाव से कहा।
‘यह भेदभाव तुम्हें सही लगता है?’ मैंने पूछा। मेरे शब्दों के तीखेपन को उसने महसूस कर लिया था।
‘अरे … तुम नाराज क्यों होते हो?…. उन्हें अपने बर्तनों में कैसे खिला सकते हैं?’ उसने प्रश्न किया।
‘क्यों नहीं खिला सकते? …. होटल में … मेस में तो सब एक साथ खाते हैं। पिफर घर में क्या तकलीपफ है?’ मैंने तर्क दिया।
सविता इस भेदभाव को सही और संस्कृति का हिस्सा मान रही थी। उसके तर्क मुझे उत्तेजित कर रहे थे। पिफर भी मैं कापफी संयत था उस रोज। उसका कहना था, एस.सी. अनकल्चर्ड ;असभ्य होते हैं। गंदे रहते हैं।
मैंने उससे पूछा, ‘तुम ऐसे कितने लोगों को करीब से जानती हो? इस विषय में तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं?’ वह चुप हो गई थी। उसका परिचय ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं था। पिफर भी पारिवारिक पूर्वग्रह उस पर हावी थे। उसका कहना था, आई ;मांद्ध, बाबा ;पिताद्ध ने बताया। यानी बच्चों को यह सब घरों में सिखाया जाता है कि एस. सी. से घृणा करो।
इस मौके पर मुझे अपने एक कबीरपंथी ओ.बी.सी. मित्रा के कहे शब्द बरबस याद आते हें। यह करीब एक दशक पूर्व की बात है जब सिंकदर बख्त बी.जे.पी. के एक द्वितीय पंक्ति के ही सही पर महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे। चार-पांच लोगों के साथ अखबार में छपी उनकी तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए कबीरपंथी / निर्गुणमार्गी मित्रा का कहना था कि यह शख्स देखने से ही ‘चाईं’ ;कसाई / कट्टरद्ध लगता है। जबकि यह बद्ध्मूल धरणा महज उसके मुस्लिमों के प्रति संघी एवं दिवालिया मस्तिष्क की उपज मात्रा थी।
परंपराओं ने दलित व सवर्ण समाज से मानवीय-सार को सोख लिया है। हालांकि ऐसी अपमानजनक प्रथाओं के प्रति दलितों के अस्वीकार भाव को वाल्मीकि ने अपने आत्मकथन में दर्शाया है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में लेखक के मां-बाप ने घर-बाहर के अनेक काम किए थे लेकिन सुखदेव सिंह ने एक मिठाई का टुकड़ा देने से मना कर दिया। पिफर सुखदेव ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके लेखक की मां से कहा ‘टोकरी भर तो जूठन उठा ले जा रही है… उप्पर से जाकतों के लिए खाणा मांग री है? अपणी औकात में रह चूहड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन।’ वाल्मीकि आगे लिखते है- ‘सुखदेव सिंह त्यागी के वे शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए थे, जो आज भी अपनी जलन से मुझे झुलसा रहे हैं।
‘अपने-अपने पिंजरे’ में स्त्रा विषयक कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो जुगुप्सा जगाने वाले हैं और सापफ गढ़े गए प्रतीत होते हैं। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा को कच्चा करार देने वाले नैमिशराय यहां खुद अपनी आत्मकथा में विश्वसनीयता के मोर्चे पर कठघरे में खड़े किए जा सकते हैं। जैसे, नपुंसक भाई, भाभी, वेश्याओं, रसवंती, बंबई में दो बहनों का स्वाभाविक आकर्षण वाले प्रसंग आत्मकथा में कल्पना के मिथ्या तत्व की अनगढ़ मिलावट का संकेत करते हैं। वैसे भी एक दलित आत्मकथा में इन प्रसंगों की कोई युक्तियुक्तता नहीं बनती। ‘मेरे जीवन में अनेक महिलाएं आईं। सामने कोई मोटी औरत अपने भारी चूतड़ खोल वही कर रही थी जो मैं करने जा रहा था’ आदि अश्लील वाक्यों का एक दलित आत्मकथा में क्या मतलब? नैमिशराय के भाई जानकी को शादी बाद नपुंसकता निवारण के लिए घर के लोगों द्वारा कई कोठों पर रंडियों के पास भेजे जाने का प्रसंग भी बिल्कुल बनावटी लगता है। मर्द बनाने का यह सायास उपाय और भाई का बिना ना नुकुर के यह सब करना एक सच्चाई नहीं, प्रहसन ही हो सकता है- ‘‘वे रंडियों को सापफ-सापफ बतला देते थे। कुछ समय तो रंडी कोशिश करती थी, पर जब भइया से कुछ न होता तो गालियां देकर भगा देतीं। वे लोग कोठे से उतर आते। अगली बार पिफर नया कोठा तलाशते। नये कोठे पर नई रंडी तलाशते।’’14
कुल मिला कर हम पाते हैं कि दलित आत्मकथाओं में दलित महिलाओं की श्रम की पहचान के साथ-साथ उसके दोहरे शोषण एवं दुख-दर्दों की सचबयानी की कोशिश मिलती है। यह जो दोहरे शोषण का कुटेव है वह दलित समाज में बाहर से घुस आया है जो ब्राह्मणवादी भारतीय समाज के प्रभाव में ‘अवतरित’ हुआ है। दलित नारियों को अपनी साहसिक आत्मकथनों के साथ आगे आना होगा और अपने समाज के सत्तापोषक बु(जीवियों के साथ-साथ गैरदलित समाज के नर, मादा दोनों के द्वारा अपने प्रति होने वाले खल छल-बल को सामने लाना होगा।
———————————————-
1. दलित साहित्य, 1999, रजत रानी मीनू का समीक्षालेख , पृष्ठ-320
2. दोहरा अभिशाप ;भूमिकाद्ध
3. दोहरा अभिशाप
4. दोहरा अभिशाप
5. दोहरा अभिशाप
6. दोहरा अभिशाप
7. दोहरा अभिशाप
8. दोहरा अभिशाप
9. झोपड़ी से राजभवन
10. जूठन
11. जूठन
12. जूठन
13. जूठन
14. अपने अपने पिंजरे ;भाग-1