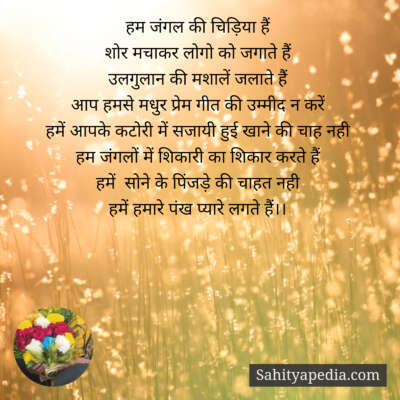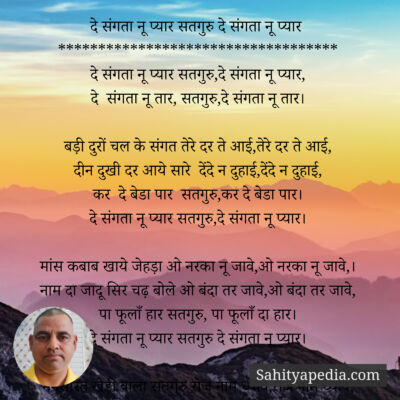अपनों की ठांव …..

गांव में अपनों की ठांव …..
भुल गए सब हंसी ठिठोली
भुल गए बचपन की यादें
सिमट गए है खुन के रिश्ते
बंट गया बहन – भाई का प्यार
ननद भौजाई की मीठी तकरार
सास बहु कि संबंधों की मर्यादा
धुमिल हो रहे सारे रिश्ते
चाचा – भतीजा, देवर – भौजाई
देवरानी – जेठानी, फुआ – फुफा
ढ़ीली पड़ गई राखी का बंधन
नहीं सुनाई देती है अब
तीज – त्यौहार के गीत
बहन – बेटियों की किलकारियां
इनके सरगोटियों के खेल
सावन में बहुरा के झुले
शादी-ब्याह में उत्साह
भेंट चढ़ गया है आपसी कलह के।
अब गांव-गांव न रहा
शहर बनने की होड़ में है
खो रहा है आपसी संबंध
एक दुसरे से बड़े बनने की होड़ में
लहलहा रहा है अंदर विषैले फसल
तैयार है मसलने को, डंसने को
ना बड़ों का लिहाज
ना छोटों से स्नेह
ना संबधों की मर्यादा
बुन रहे है जाल फंसाने को
जिसमें स्वंय ही फंसते जा रहे
उलझते जा रहे मकड़ी की तरह
गिरते जा रहे अनजानी खाई में
टांगी जा रही है अपनों की इज्जत
घर के पुराने मुंडेरो पर।
ब्रह्म बाबा भी सुखने लगे है,
जैसे वंशजों में भी सुखा रहा है
पूर्वजों के संस्कार, अपनत्व, प्रेम,
परम्परा, सौहार्द, और साहचर्य,
बरगद का बुढ़ा पेड़ भी उखड़ गया
जो देता था छांव रहगीरों को
जिसके डालों पर सारे बच्चे
खेलते थे ततवा-ततैया, लुकाछुपी
परदेशी लोग गांव से दुर हो गए
आते है पर्व, त्यौहार और शादी में
साल में एक दो बार यात्री सा
और, चले जाते है छोड़कर अपनों को
जिजीवषा के लिए दुर देशों में।
सुबह – सुबह नीम की दातुन
वास्तु शास्त्र के भेंट चढ़ गया
सिमटते गए आम – जामुन के बाग
सुखते गए शीशम
सरकार को न चिंता थी, न है
न जनसमुदाय इससे खिन्न है
नीरो सा द्रष्टा बन देख रहे
गांव के बुजुर्ग और बच्चे
समन्वय बना भुत – भविष्य का
ना वेदना है, न संवेदना, न चित्कार
घट रही प्राकृतिक संपदा को देख?
सुख रहे है तलाब और कुँए
सिमट रहे खेत खालिहान
फैल रहे कंक्रीट की मकान
झुलस रहे धुप में सब
कहीं नहीं पीपल की छांव
कहीं नहीं अपनों की ठांव ।