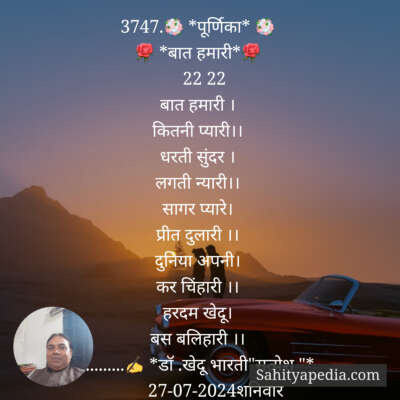अपने ही में उलझती जा रही हूँ,

अपने ही में उलझती जा रही हूँ,
लगता है जैसे बदलती जा रही हूँ।
तोड़कर वादों के घुटन भरे बंधनों को,
वक़्त के साथ जैसे ढलती जा रही हूँ।
नहीं है पारावार कोई पारावार का,
रत्नाकर में गहरे उतरती जा रही हूँ।
धरित्री सी झेलकर सौदामिनी को,
मेदनी सी क्षीण हो मरती जा रही हूँ।
परिभ्रमण कब होगा प्रत्यावर्तन होकर,
नहीं हैं स्वीकार्य समझती जा रही हूँ।
नहीं है बोधगम्य निश्चलता और ऋजुता,
प्रदक्षिणा संत्रस्त होकर करती जा रही हूँ।
निरूपाय नहीं है यूँ ही उद्वेतात्मक होना,
इकरार को इनकार में बदलती जा रही हूँ।
डॉ दवीना अमर ठकराल’देविका’