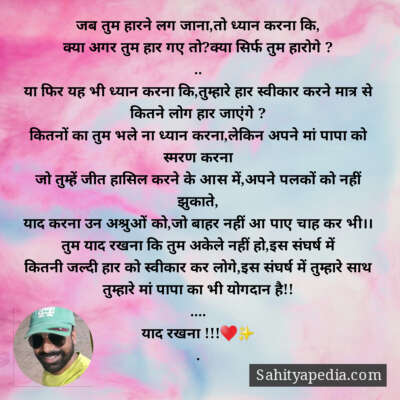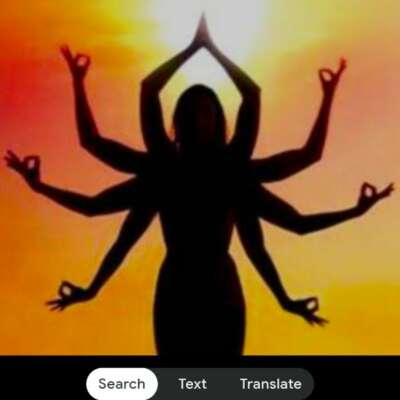अनगढ़ शब्द ,लंबी कविता
15–व्यक्तित्व
रहस्य की पर्तों से झांकता ,नेत्र वलय में ठहरता
कुछ तो हो सम्मोहित सा करने वाला
तन की दीवारों को भेद स्वयं में ही सिमटता
अजब आकर्षण बातों में भरने वाला।
साँवली सूरत ,बोलते से नयन ,जैसे झील शांत
ठहरी ,ठिठकती ,तलाश न जाने किसकी थी
हँसती जब धवल दंत पंक्ति ,पाकर विश्रांत
कोई स्मृति झीने सी चिलमन झांकती थी
गाँभीर्यता का ओढ़ लबादा ,जाल कोई बुनता।
न जाने किस डर से गुहा में आये उजालों को
धागा कोई ,या तंतु अंतस को था उधेड़ता
बंद मुट्ठियों में कसता था हृदय कपाट को ।
उस व्यक्तित्व के उलझे रेशे ,दायरे अपने अपने
हिचकता ,डरता ,उत्साहित हो फिर देखता सपने।
पाखी
14–अभिनय .।
आखर आखर शब्द जुड़े
मन हुआ न पर शांत ।
पीर गहरी अंतस पैठी
मुखड़ा हुआ यूँ क्लांत ।
जग सारा रंगमंच बना
होते रोज तमाशे यहाँ
व्यथा वेदना ले अंगडाई
जा पहुँची जाने कहाँ।
रोज जीते रोज मरते.
रोते नयन कहाँ विश्रांत।
पल भर भूल स्वयं का वैभव
लगा मुखौटा बना शिकारी
सफेद रंगा कभी लाल रंगा
रंग कर भी रहा अनाड़ी।
स्वांग भरता,जग को हँसाता
भीतर ही भीतर तपता मैं
आकुल व्याकुल होकर भी
जोगी बनता रमता मैं।
जीवन की सच्चाइयों को
अभिनय कर के देखूँ
एक पक्ष का सत्य दिखा
दूजा पथ कब लेखूँ।
घोर निराशा की कारा में
जकड़ा ,बंधा पाता हूँ।
कैसे उबरूँ ,कैसे निकलूँ
और जकड़ता जाता हूँ।
सोच विचार की मानस गलियाँ
झंझावात के वो झकोरे
निपट अवचेतन को घेर रहे
सुबह रात औ’ साँझ सकोरे।
दग्ध हृदय से निकली ज्वाला
शीतल जल से कब बुझती
निष्ठुर प्रेम की भीषण लपटें
इस पागल को हैं डँसती।
भूल स्वयं को जाता हूँ
अभिनय में खो जाता हूँ।
वाह वाही के लुटे खजाने
कुछ संतुष्ठ हो पाता हूँ।
कुछ करने की दमित इच्छा
जब जब सिर उचकाती है
नाटक,एकाकी के पात्रो में तब
संवादों में घुल मिल जाती है।
मंचन ,अभिमंचन या नर्तन
वाद्य बजाते थिरकी स्वर लहरी
अधुना यंत्र में सुकून खोजता
पीर हिलोरती जब गहरी।
शौक कहो या प्यासा हृदय
जीवन का दर्पन लगता
कोठों की कैदी सा फिर क्यूँ
मुझको हर क्षण-पल लगता।
संवादों में जब प्राण फूंकता
सँभावना बनती सहचरी मेरी
प्रतीक्षा पथ है तब बदलती
लक्ष्य प्राप्ति की बजती भेरी।
स्वर ,लय ,ताल ,गति पर
कदम चलते कभी थमते
उलझे सुलझे कथानकों में.
रंग अदाकारी के भरते।
क्रमशः
पाखी