भारतीय संविधान वेदों और उपनिषदों का आधुनिक, लौकिक, और न्यायसंगत संस्करण है
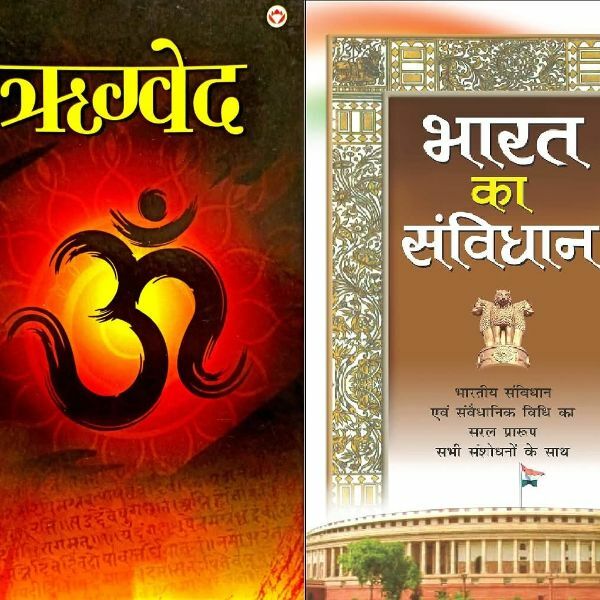
भारतीय संविधान वेदों और उपनिषदों का आधुनिक, लौकिक, और न्यायसंगत संस्करण है –
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया — एक ऐसे युग में जब भारत ने न केवल अंग्रेज़ी दासता से मुक्ति पाई थी, बल्कि सहस्राब्दियों से चली आ रही सामाजिक विषमता, जातिगत दासता, और वर्णाधारित विभाजन की जंजीरों को भी तोड़ने का प्रयास किया था। परंतु यह विचार कि संविधान ने जिस समानता और स्वतंत्रता की नींव रखी, वह कोई पश्चिमी उपहार नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा की प्राचीनतम चेतना — ऋग्वेद, उपनिषदों और गीता के सूत्रों में निहित थी, इसे समझना आज की आवश्यकता है।
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में समाज के चार अंगों का उल्लेख मिलता है —
“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्, बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥”
यहाँ जो विभाजन दिखता है, वह किसी ऊँच-नीच के भाव से नहीं, बल्कि कार्यविभाजन के तात्त्विक संकेत से है। वेदकार का आशय यह नहीं था कि मनुष्य जन्म से ही श्रेष्ठ या हीन होता है; बल्कि यह था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण, प्रवृत्तियाँ और क्षमताएँ होती हैं, और समाज तभी संतुलित रहता है जब ये सब अपने गुण और कर्म के अनुसार समाज-सेवा करें। यह सहयोगी विविधता का दर्शन था, न कि शोषणकारी भेदभाव का।
किंतु जैसे-जैसे वैदिक युग समाप्त हुआ और उत्तरवैदिक तथा स्मृतिकाल आया, यह व्यवस्था स्थायी वर्गों में बदल गई। वर्ण धर्म से जाति धर्म बना, और फिर मनु-स्मृति जैसे ग्रंथों में इसे जन्माधारित बना दिया गया। जहाँ वेद ने कहा था कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जाने, वहीं बाद की सामाजिक संरचना ने कह दिया कि ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण घर में जन्म ले। यही वह मोड़ था जहाँ वेदों की आत्मा मर गई और व्यवस्था का शरीर कठोर हो गया।
उपनिषदों का स्वर वेदों से भी अधिक उदात्त और समतावादी है। छांदोग्य उपनिषद कहता है —
“सर्वं खल्विदं ब्रह्म।”
अर्थात — यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्म है। हर प्राणी, हर जीव उसी परम सत्य का अंश है। जब समस्त सृष्टि में एक ही चेतना व्याप्त है, तो कोई कैसे श्रेष्ठ और कोई कैसे नीच हो सकता है? यही उपनिषदों का अद्वैतवाद है — जो सामाजिक दृष्टि से समानता का सर्वोच्च विधान है।
ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है —
“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।”
अर्थात — समस्त जगत ईश्वर से आच्छादित है। यहाँ किसी को दूसरे से कम नहीं माना गया। सब एक ही दिव्य सत्ता के अभिन्न अंग हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद भी इस समानता का प्रमाण है। मैत्रेयी — एक स्त्री — ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा रखती है और याज्ञवल्क्य उसे ज्ञान देने से संकोच नहीं करते। यह उस युग का उदाहरण है जहाँ ज्ञान का अधिकार लिंग या वर्ण से नहीं, जिज्ञासा से तय होता था।
कठोपनिषद में नचिकेता नामक बालक यमराज से संवाद करता है और मृत्यु के रहस्य को जानता है। वहाँ भी कोई वर्णाधारित अड़चन नहीं। उपनिषदों का सारा तत्त्व यही है कि आत्मा न किसी वर्ण की है, न किसी जाति की; वह तो अखण्ड, अजन्मा और समान है —
“न जायते म्रियते वा कदाचित्।”
इसी भाव से गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं —
“चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।”
यहाँ “गुणकर्मविभागशः” शब्द ही वह कुंजी है, जो संविधान की आत्मा से जुड़ती है।
संविधान कहता है — हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त होगा; किसी को उसके जन्म, धर्म, जाति, लिंग या स्थान के कारण वंचित नहीं किया जा सकता।
भगवद्गीता कहती है — मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और गुण से है, न कि उसके जन्म से।
यदि हम इन दोनों को साथ पढ़ें तो प्रतीत होता है कि संविधान ने गीता के इस सिद्धांत को ही विधिक रूप दिया है।
कृष्ण का “गुणकर्मविभागशः” — डॉ. अंबेडकर के “Equality of Opportunity” में बदल गया।
अब प्रश्न यह है कि क्या संविधान वेदों की मूल भावना का विरोध करता है?
उत्तर स्पष्ट है — नहीं। संविधान उस मूल वैदिक भावना का विरोध नहीं करता जो मनुष्य की गरिमा और सामूहिक समरसता की बात करती है; वह उस विकृत रूप का विरोध करता है जिसमें मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए वर्ण को जाति, धर्म को विभाजन, और कर्म को भाग्य बना दिया।
संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक “सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय” पर आधारित गणराज्य होगा। “समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व” इसके आधार हैं।
अगर हम इन शब्दों को ध्यान से देखें, तो यह केवल फ्रांसीसी क्रांति के नारे नहीं हैं, बल्कि उपनिषदों की आत्मा हैं।
बंधुत्व — वसुधैव कुटुम्बकम् का आधुनिक रूप है।
समानता — अहं ब्रह्मास्मि की व्यावहारिक परिणति है।
स्वतंत्रता — यदिच्छसि तदा कुरु का नैतिक संस्करण है।
इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान वास्तव में वेदांत के दर्शन का लौकिक रूपांतरण है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के शिल्पी माने जाते हैं, वे वेदान्त दर्शन और उपनिषदों के मूल तत्वों को समझते थे। उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि बौद्ध धर्म, वेदान्त का सामाजिक रूप है — जो समानता और करुणा का संदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि धर्म मनुष्य को समानता न दे सके, तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। यह वक्तव्य उसी उपनिषदिक भाव की आधुनिक व्याख्या है — जहाँ “धर्म” का अर्थ सत्य और न्याय है, न कि कर्मकांड और सामाजिक पदानुक्रम।
संविधान की अनुच्छेद 14 कहती है — “राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।”
यदि इसे दार्शनिक भाषा में कहें, तो यह वही विचार है जो छांदोग्य उपनिषद के
“तत्त्वमसि” में निहित है — “तू वही है”।
हर व्यक्ति में वही चेतना है, वही अधिकार है, वही गरिमा है।
वेदों में भी अनेक ऋचाएँ हैं जहाँ समानता की भावना स्पष्ट दिखती है। ऋग्वेद (5.60.5) में कहा गया है —
“अज्येष्ठासो कनिष्ठास एकरूपा बहुभ्रजा।
सहस्राणीव शृण्विरे नाना धामानि येषाम्॥”
अर्थात — न कोई बड़ा, न कोई छोटा; सब एक समान हैं। सबका योगदान अलग-अलग है, पर मूल्य समान है।
यही तो संविधान का भाव है — हर नागरिक, चाहे वह किसान हो या वैज्ञानिक, श्रमिक हो या विद्वान, सबका समान अधिकार है।
संविधान का अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन — वेदों के उस विचार को पुनर्जीवित करता है जहाँ मनुष्य को मनुष्य से अलग नहीं माना गया।
यजुर्वेद में कहा गया है —
“अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥”
यह भावना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है — क्योंकि जब पूरा विश्व एक परिवार है, तो भेदभाव की कोई जगह नहीं रह जाती।
अब यदि कोई कहे कि संविधान ने “वर्ण व्यवस्था” का पोषण किया है — तो यह अर्धसत्य है। संविधान ने सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) का प्रावधान दिया है, पर यह “वर्ण” नहीं, बल्कि “समान अवसर” का साधन है। यह दमन नहीं, प्रतिपूरण का उपकरण है।
जहाँ समाज ने किसी वर्ग को सदियों तक वंचित रखा, वहाँ संविधान ने उन्हें पुनः बराबरी के मंच पर लाने का प्रयास किया। यह वर्ण का पोषण नहीं, बल्कि वर्णाधारित विषमता का प्रायश्चित्त है।
यदि हम गीता के कर्मयोग को देखें, तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं —
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।”
यहाँ “स्वधर्म” का अर्थ जन्म से नहीं, बल्कि अपने गुण और कर्तव्य से है।
संविधान ने भी यही कहा — हर व्यक्ति को अपने कर्म से, अपनी क्षमता से आगे बढ़ने का अधिकार है, न कि उसके जन्म से तय होगा कि वह क्या कर सकता है।
वेदों में वर्ण-व्यवस्था का मूल भाव समाज की समरसता था; संविधान में भी यही भाव निहित है। दोनों ही व्यवस्था को कर्तव्य और अधिकार के संतुलन से चलाना चाहते हैं।
वेद कहते हैं — “संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।”
अर्थात — मिलकर चलो, मिलकर बोलो, अपने मन को एक करो।
यह शांति मंत्र केवल धार्मिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दर्शन है।
संविधान उसी एकता के सिद्धांत पर टिका है — विविधता में एकता।
अब प्रश्न यह भी उठता है कि संविधान और वेदों के इस समन्वय को क्यों लोग विरोधाभास की दृष्टि से देखते हैं?
इसका कारण यह है कि वेदों का जो रूप लोगों के सामने प्रचलित है, वह शास्त्रार्थ नहीं, स्मृत्यर्थ है।
वेदों में तो स्वतंत्र विचार, प्रश्न करने की परंपरा और आत्म-चेतना का विस्तार है;
किन्तु स्मृतियों और परंपराओं ने उसे स्थिर, जड़ और जातिवादी बना दिया।
संविधान उस जड़ता को तोड़ता है, पर वेदों की चेतना को पुनर्जीवित करता है।
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार कहा था —
“The Constitution of India is not an alien document; it is the modern continuation of the ancient Indian quest for Dharma.”
यानी यह कोई पश्चिमी चश्मे से देखा गया विधान नहीं, बल्कि भारत की नैतिक परंपरा का आधुनिक रूप है।
वेदों ने धर्म को कर्तव्य कहा, संविधान ने भी अधिकार के साथ कर्तव्य का विधान किया।
वेदों ने कहा — “ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत” नहीं, बल्कि “ऋणं कृत्वा यज्ञं कुरु” — अर्थात कर्म कर, समाज में योगदान दे।
संविधान ने भी यही कहा — Fundamental Duties में प्रत्येक नागरिक को यह स्मरण कराया गया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है।
इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय संविधान वेदों के दार्शनिक और उपनिषदों के आध्यात्मिक आदर्शों का लौकिक विस्तार है।
वेदों ने कहा — “न त्वं विद्वांस् तस्मात् अधीयस्व।” — “तू अभी नहीं जानता, इसलिए अध्ययन कर।”
संविधान ने कहा — “Right to Education.”
वेदों ने कहा — “मा हि हिंस्यात् सर्वभूतानि।”
संविधान ने कहा — “Right to Life and Liberty.”
वेदों ने कहा — “सत्यं वद, धर्मं चर।”
संविधान ने कहा — “Due process of law and justice.”
अर्थात, संविधान ने वेदांत की आत्मा को आधुनिक भाषा और विधि में रूपांतरित किया है।
संविधान ने “वर्ण” शब्द को नहीं अपनाया; उसने “समानता” को अपनाया।
वेदों में वर्ण कार्य का प्रतीक था, संविधान में पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार है।
वेदों में ब्राह्मण वह था जो ज्ञान दे, संविधान में शिक्षक या वैज्ञानिक वही भूमिका निभाते हैं।
वेदों में क्षत्रिय वह था जो रक्षा करे, संविधान में सैनिक और पुलिस वही भूमिका निभाते हैं।
वेदों में वैश्य वह था जो समाज की अर्थव्यवस्था चलाए, संविधान में उद्यमी वही कार्य कर रहे हैं।
वेदों में शूद्र वह था जो सेवा करे, संविधान में सेवा क्षेत्र (service sector) ही राष्ट्र की रीढ़ है।
अंतर केवल यह है कि संविधान ने इन सबको जन्म के बंधन से मुक्त कर दिया।
इसलिए संविधान वेदों की आत्मा का विरोध नहीं करता; वह उसे लोकतांत्रिक पुनर्जन्म देता है।
वह कहता है — अब ब्राह्मण होना जन्म नहीं, कर्म से सिद्ध होगा; क्षत्रिय होना सत्ता नहीं, सेवा से सिद्ध होगा।
यही आधुनिक धर्म का रूप है — जहाँ हर व्यक्ति अपने कर्म से देवता बन सकता है।
अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत का संविधान वेदों के मूल दार्शनिक तत्त्व — समरसता, कर्म, और सत्य — का विरोध नहीं करता; बल्कि उस भाव को पुनर्स्थापित करता है जिसे बाद के युगों में हमने खो दिया था।
यह संविधान आधुनिक भारत का श्रुति-संहिता है — जो न किसी जाति का है, न किसी पंथ का, बल्कि मानवता का धर्मग्रंथ है।
वेदों ने कहा था — “आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः।”
अर्थात — हमारे पास चारों दिशाओं से कल्याणकारी विचार आएँ।
संविधान ने इसी मंत्र को लोकतांत्रिक स्वरूप दिया — जहाँ हर विचार, हर समुदाय, हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले।
इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय संविधान वेदों और उपनिषदों का आधुनिक, लौकिक, और न्यायसंगत संस्करण है — जो मानवता के उस सनातन स्वप्न को साकार करता है जहाँ सब एक हैं, सब समान हैं, और सबका एक ही धर्म है — सत्य, करुणा और न्याय।
-देवेंद्र प्रताप वर्मा ‘विनीत’
