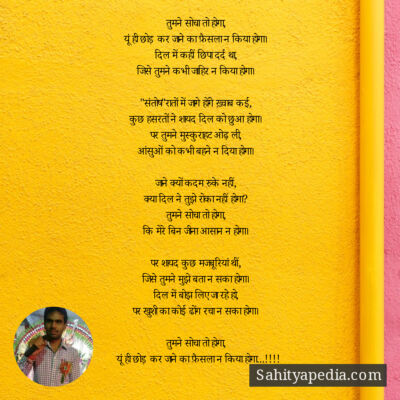(8) मैं और तुम (शून्य- सृष्टि )

शून्य से उपजा था जिस क्षण,
तुम्हारा वह गरिमामय तन
तुम्हारा सहयोगी का रूप
… तुम्हारा सह्भोगी का रूप
तुम्हारी पायल की रुनझुन
तुम्हारे अभय पदों की धुन
तुम्हारी निश्छल मोहक हंसी
तुम्हारी चितवन अर्थपगी
मनुज को ले जाती उस ओर
आदि और अंत जहां एक ठौर
जीव और ब्रह्म जहां पर एक
समष्टि व्यष्टि जहां अभेद
काल और दिक् का बीज बने
सर्व आयाम हमीं में घने
अर्धनारीश्वर मैं और तुम
तुम्ही मैं बने, और मैं तुम
वायु के सघन कणों से हम
कर्म और ज्ञान व इच्छा — सम |
तभी कुछ हुआ व्यतिक्रम एक
एक से बने द्वैत सविवेक
उनीदित सी आँखें खोले
भ्रमों का कीटजाल ओढ़े
देखते कुछ, दिखाते कुछ
चाहते कुछ तो करते कुछ,
प्रकृति ने दिए हमें अभिशाप
जीव ने भोगे जो अभिशाप
ब्रह्म ने भरमाया दिन रात
जगत ने पत्थर मारे घात,
विकल, बेकल, विह्वल, क्षोभित
यज्ञ में जले सर्प, पीड़ित
रेंगते हैं जीवन के लिए
जिन्दगी खड़ी दंड है लिए
मृत्यु उपहास उडाती है
प्रकृति धर धर ठुकराती है |
सोचता हूँ मैं अब इस क्षण–
कौन था मैं , कौन थे तुम
नहीं तुम तो कोई परिचित !
सिर्फ तुम पिंडों से निर्मित
तुम्हारा वह आकर्षक रूप
तुम्हारा अकथ अलौकिक रूप
मात्र मेरी ही कल्पना थी
मात्र मेरी ही जल्पना थी,
पिंड में देखी जो आत्मा
मात्र मेरी ही अल्पना थी |
मात्र मेरी ही अल्पना थी ||
स्वरचित एवं मौलिक
रचयिता : (सत्य ) किशोर निगम