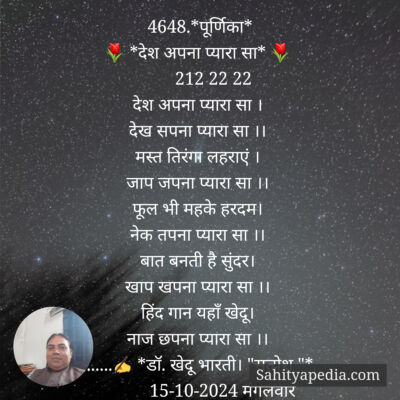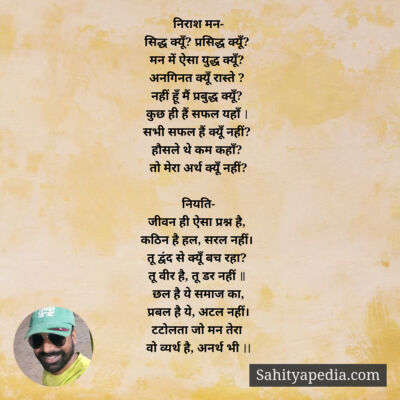■ यादों का झरोखा…

#संस्मरण-
■ रंग-बिरंगी यादें बचपन की
★ मांझे की सुंताई और पतंगबाज़ी
(दिली रिश्तों के स्वर्णकाल को समर्पित मेरा एक और भावपूर्ण #संस्मरण)
【प्रणय प्रभात】
चलिए साहब! आज फिर पलटता हूँ #अतीत का एक और पन्ना। अपने #बचपन के हवाले से। यक़ीन है कि आप में से तमाम को #दास्तान के हिस्से #आपबीती जैसे लगेंगे। बात 1970 के दशक के आख़िरी दौर की है। ये वो दौर था जब मनोरंजन भी #सीजनल होता था। गर्मियों की छुट्टी #मनोरंजन के माध्यम तलाशती थीं। सबसे पहले याद आती थी #पतंगबाज़ी। यह एक शग़ल था, जो हर तरह का भेद ख़त्म कर देता था। मोहल्लों की छतें प्रतिद्वंद्वियों का खेमा होती थीं। नीला खुला आसमान रंग-बिरंगी पतंगों का समरांगण। तपती हुई चूने की छतों पर पहुंचने की बेताबी दोपहर को सोने नहीं देती थी। पापा के दफ़्तर से लौटने का इंतज़ार आम बात था। जो अपने साथ लेकर आते थे दर्ज़न भर से भी ज़्यादा पतंगें। अलग-अलग रंग व आकार वाली। बड़े डिग्गे खुद के लिए। छोटी और मंझोली हम तीनों भाइयों के लिए। जिन्हें लम्बा पुछल्ला बांध कर उड़ाना व हवा में साधे रखना आसान होता था। रात को सोते में खटिया से बाँध दो, तो सुबह तक उड़ती मिले। हवा के साथ फर्र-फर्र करते और गच्चे खाते डिग्गों को संभालना बच्चों का खेल था भी नहीं। लिहाजा उन्हें उड़ाने व गोते खिलाने का विशेषाधिकार पापा को हुआ करता था। जो किसी भी शौक को पूरा करने के मामले में बेहद धुनी थे। उनके सब शौक़ दीवानगी की हद तक होते थे। कस्बानुमा श्योपुर में पतंग और डोर (मांझे) की उपलब्धता का इकलौता केंद्र चौराहा होता था। जो अब सूबात चौराहा कहलाता है। बोहरा बाज़ार को ओर जाने वाले मार्ग पर सबसे बड़ी दुकान शाकिर भाई की होती थी। जो बोहरा समाज के थे। गोली-बिस्किय, टॉफी, चॉकलेट की इस सबसे बड़ी दुकान पर गर्मियों में पतंगों का अंबार लग जाता था। पास ही एक गुमटीनुमा दुकान सलीम भाई उर्फ़ #आलाबन्दा की होती थी। जो मूलतः नीलगर (रंगरेज़) थे और यहीं पर कपड़ों को रंगने का काम साल भर करते थे। तीसरा केंद्र मेन बाज़ार की ओर जाने वाले रास्ते के नुक्कड़ पर लगने वाला हैदर भाई का ठेला था। वो भी बोहरा समाज के थे और मूल रूप से सिलाई में काम आने वाली चीजों के विक्रेता थे। चौराहे की पुरानी पुलिस चौकी की सीढ़ियों के पास दीवार से सट कर उनका ठेला लगा करता था। हाथ के पंजे को फैलाकर अंगूठे और छोटी उंगली के बीच मांझे की लच्छी बना कर बेचने में तीनों माहिर थे। हर मांझा #बरेली का बता कर बेचा जाता था। पेंच काटने तक मांझा असली सा लगता था। जिससे पतंग कटते ही मोह भंग भी हो जाता था। इसी पशोपेश में रास्ता खोजा गया, ख़ुद मांझा बनाने का। रोचक परंतु अच्छी-खासी मेहनत, मशक़्क़त वाला काम। अरारोट, सरेस के घोल को रंग डालकर लगातार चलाते हुए पकाना। उसमें बारीक पिसा और छना हुआ कांच मिलाकर गाढ़ी लुगदी तैयार करना।कांच के बेहद बारीक पाउडर के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता था बल्ब। जिन्हें अधिक संख्या में तलाशना भी एक समस्या थी। उस समय बिजली बहुत से घरों में नहीं होती थी। आती भी कम थी, लिहाजा बल्ब कम खराब होते थे। फुंके बल्बों का मोल और महत्व हमें पता था। लिहाजा उन्हें संभाल कर रखा जाता था। अडोस पड़ोस से खोज और मांग के लमने में भी कोई संकोच नहीं था। तैयार लुगदी के ठंडा होने से पहले बीच सड़क पर डीएमसी की सूती डोर को बिजली के खम्बों के बीच बांधना हमारा काम था। फिर लुगदी को कपड़े में लेकर डोर पर घिसते हुए परत की तरह चढ़ाना पापा का। परत कितनी बार चढ़ेगी और मांझा कितना कड़क रखा जाएगा, यह विशेष ज्ञान की बात थी। बाद में लुगदी की सामग्री में अंडा भी धीरे से शामिल हो गया। किसी ने सुझाया होगा ज़रूर इस बारे में। घर मे दादी, मम्मी और दो बुआओं के कारण भारी छुआछूत का संकट था। लिहाजा अंडा छुपाकर मंगाया व डाला जाता था। लुगदी बनाने के लिए पीतल की एक पुरानी सी भगोनी अलग थी। एक काला पड़ चुका स्टील का चमचा भी। ऊपरी मंजिल पर बनी रसोई में जाने की कोई छूट तब थी नहीं। नीचे ही किया जाता था सारा फोफंड। पीतल की गोल टंकी और तीन टांगों वाला एक स्टोव्ह इसी काम के लिए आरक्षित था। पापा बड़े जतन से यह सारा काम करते। हम केवल सामान की उठाई धराई में उनकी मदद करते। ज़ोखिम वाला कोई काम हमसे नहीं कराया जाता था। हम घर के मोड़ और गीता भवन के बाहर लगे बिजली के खम्बों के बीच डोर बांधते। सुंताई के बाद मांझे के सूखने तक गुज़रने वाले राहगीरों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कराते। बाद में उसे लपेटने के दौरान चरखी पकड़ते। मांझा बाज़ारू मांझे से ज़्यादा धारदार होता था। पतंग तो काटता ही था, उंगलियों में भी कट लग जाते थे। यही काम मोहल्ले के कुछ अन्य पतंगबाज़ भी करते थे। जिनका उल्लेख आगे आएगा। इस काम के लिए मेरे घर के पास बने चीड़ के गोदाम की बड़ी सी छत भी काम आती थी। जो अब “कास्ट्या हाउस” बन चुका है। मांझा सूतने और छत पर पहुंचकर पतंगबाज़ी का लुत्फ़ लेने के बीच एक आपदा कॉमन थी। वो थी मांझे में घुडी पड़ने यानि डोर के उलझने की। चरखी घुमाने की धीमी गति इस संकट का सबब बनती थी। यही समय होता था जब मांझे की दुर्गत से भन्नाए पापा में दुर्वासा ऋषि की आत्मा आ जाती थी। कभी कभी वो महर्षि भृगु बनकर प्रसाद भी दे देते थे। उनकी पतंगबाज़ी के दौरान चरखी पकड़ना अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम था। पेंच कटते या पतंग के गच्चा खा कर डूबते ही पापा के इकहरे बदन में मानो बिजली सी दौड़ जाती थी। पतले और लम्बे हाथों से बो सारी डोर तेज़ी से खींच लेते थे। उसे घुडी से बचाने के लिए डोर को खींचने के लिए वो पूरी छत पर घूमते थे। हम पैर में मांझा न उलझने देने को लेकर चौकन्ने रहते और तेज़ गति से चरखी घुमाने का प्रयास करते। सफल होते तो भरपूर शाबासी भी मिलती। #ये_काट्टा और #भक्काटा जैसी जोश भरी आवाज़ें तव मिनट मिनट पर गूंजती थीं। कितनी काटीं और कितनी कटी बाद में डींगमारी और समीक्षा के विषय होते थे। अगले दिन की रणनीति पर विचार भोजन और शयन के बीच हो लेता था। हमारा मोहल्ला बेहद चर्चित और जागृत रहा है हमेशा से। तब अधिक सुरम्य व चेतन था। आपस में जितना मेलजोल था उतनी ही होंडा-होड़ी भी। घर के सामने पूर्व दिशा की ओर अधिकांश मकान बोहरा समाज के हैं। हर छत पर एक झुंड मौजूद होता था। इसी दिशा में कुछ निचाई वाली छत पर मन्नू चाचा उर्फ़ रामभरोसे शर्मा (पोस्टमेन) पतंग उड़ाने और पेंच लड़ाने को तैयार दिखते। उनके सामने सेजने वाली गली की छतों पर हमारे संगी साथी अपनी पूँछदार पतंगें उड़ाया करते। जिनमें ज्ञानचंद गुप्ता, मुकेश गुप्ता, पोखरमल सिंहल, सत्यनारायण गुप्ता उर्फ़ सत्या, विशाल दुबे उर्फ़ टीटू, राकेश मुखीजा उर्फ़ राधे, संतोष बलोठिया और परिजन ख़ास थे। पश्चिम की ओर दबदबा हरिओम गौड़ भाई साहब, जगदीश मुदगल (काका), राजनारायण मुदगल उर्फ़ पप्पू, सुभाष जी शाहीवाले और कचहरी की छत से उड़ने वाली पतंगों का रहता था। घर से सटी छत पर मित्र संतोष गंगवाल कभी साझेदार तो कभी बड़े प्रतिद्वंद्वी होते थे। सामने बाबूलाल शर्मा जी की छत पर किराएदार राजकुमार उर्फ़ राजू पाठक की धाक होती थी। अंकल बाबूलाल जी भी अक्सर जोश में आ जाते थे। पास ही श्री निरंजन बूँदीवाले, लक्ष्मण सोनी भी कभी कभी हाथ आजमा लेते थे। गीता भवन की छत पर सत्यप्रकाश भगत जी के भाई रामप्रकाश गौतम उर्फ़ रामू भाई साहब का आधिपत्य होता था। पास ही सूरज नारायण शर्मा भी यह शौक़ रखते थे। रायपुरा वाले पटवारी जी और मजुमदार साहब के बाड़े की विशाल छतों पर भी तमाम पतंगबाज़ सक्रिय होते थे। हमारे इलाके यानि पंडित पाड़ा की पतंगें हवा की दिशा के मुताबिक बोहरा बाज़ार, छारबाग, अंधेर बावड़ी, सूबात चौराहे और कचहरी तक रुतबे से उड़ान भरती। कुछ फ़तह हासिल कर शान से लौटतीं और दो-दो दिन जौहर दिखातीं। कुछ उड़ान के बाद ही वीरगति पा जातीं। पतंगों में तंग व कन्नी बांधना तब हुनर माना जाता था। पतंग के ठड्डे को खोपड़ी पर घिसकर लचीला करना, बड़ी पतंगों को किनारों से पकड़कर ऊंचा उठाते हुए छुट्टी देना और उलझने पर सुलझाने के लिए दौड़-धूप करना भी आनंदप्रद होता था। कटी हुई पतंग के साथ मांझे को लूटने की कोशिश में किसी को महमूद गजनवी बनने से गुरेज़ नहीं होता था। शरारती तत्व उड़ती पतंग को लंगड़ डाल कर गिराने व लूटने की बेजा कोशिश भी पूरी विशेषज्ञता के साथ करते थे। मांझा छोड़ने व पतंग लौटाने की लेकर मान मनोव्वल के साथ तक़रार भी आम बात थी। झंझट भी हो जाती थी जिसे अगले ही दिन भुला दिया जाता था। पतंग के साथ कंदील उड़ाना भी तब प्रचलन में था। हालांकि मामला कुछ खर्चीला होने के कारण सबके बस की बात नहीं था। यही वो दौर था जब घरों से ज़्यादा छतें गुलज़ार होती थीं। आपस में जुड़ी छतें पड़ोसियों के प्रति प्रेम और विश्वास की प्रतीक होती थीं। आपस की तनातनी नाम को नहीं थी। बस पतंगों की पेंचबाज़ी से ही काम चल जाता था। आपस में बातचीत और मुलाक़ात की गवाह भी छतें ही होती थीं, जो समय के साथ वीरान होती गईं। अब इन्हीं सूनी छतों पर इंसान नहीं हिंसक बन्दर नज़र आते हैं। लोग अपनी चारदीवारी में क़ैद रहने को सुकून मानने लगे हैं। एक दूसरे से बातचीत भूले-भटके या प्रयोजनवश होती है। दीदार होना भी समय सुयोग पर निर्भर है। भौतिक संसाधनों की भरमार ने उत्साह व ललक को मार सा दिया है। शाकिर भाई, हैदर भाई और सलीम भाई अपने कारोबार बदल चुके हैं। बहुत से पतंगबाज़ दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बाक़ी अपने घर परिवार में सिमट चुके हैं। मोहल्ला तमाम चेहरों व परिवारों को गंवा कर वीरानगी की कगार पर है। मकानों का जीर्णोद्धार हो गया है और आपसी रिश्ते जीर्ण-शीर्ण होते हुए लगभग खंडहर हो गए हैं। अतीत की स्मृतियों को ताज़गी देने के पीछे का मेरा एक मक़सद इन्हीं खंडहरों में कृतज्ञता व सम्मान का एक चिराग़ रोशन करना भी है। क्योंकि जो कुछ हूँ, अपने इसी मोहल्ले की मिट्टी और आबो-हवा की वजह से हूँ। कृतज्ञ उस दौर के प्रति भी हूँ जो दिल के #रिश्तों_का_स्वर्णकाल होता था। दिखावे को नहीं बल्कि हक़ीक़त में। उड़ने को श्योपुर के आसमान पर अब साल भर पतंगें उड़ रही हैं, लेकिन वो बात नहीं। अब मामला नई पीढ़ी के शौक का है। जिन्हें नगरी में पतंगबाज़ी के इतिहास का एक अक्षर याद नहीं। इति।।
#प्रणय_प्रभात
#पुनश्च: :-
(लिखे हुए में कुछ घटेगा नहीं। हां, बढ़ ज़रूर सकता है। याद आने के साथ-साथ। इस आलेख में मैंने #मांझा शब्द उपयोग किया है। जो श्योपुर में नहीं बोला जाता। हम उसे #मंजा कहते रहे हैं हमेशा से। बहरहाल, आभार दादा हरिओम गौड़ के प्रति, जिन्होंने यह विषय सुझाया) 😊😊😊