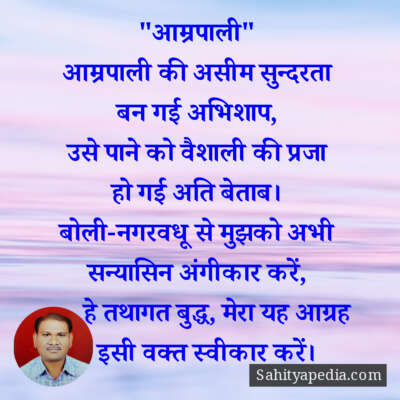■ मेरे संस्मरण

#स्मृति_दर्पण….
■ जब एक साइकिल ने बढ़ा दिया रुतबा
★ तब पैसा नहीं व्यवहार होता था गारंटी
【प्रणय प्रभात】
आज आप फरारी, बीएमडबल्यू, ऑडी जैसी कार में सवारी करने वाले पर भी शायद ही ध्यान केंद्रित करें। शायद ही उसमें बैठे इंसान के बारे में चर्चा करें या उसकी किस्मत पर रश्क करें। वजह एक से एक मंहगी और आलीशान कारों की भीड़। मतलब घोर विलासिता और भौतिकता का वो दौर, जिसमें लाखों की गाड़ी की कोई वेल्यू नहीं। यह आज का सच है, जब लोगों की क्रय शक्ति और महत्वाकांक्षा हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर छोटी-बड़ी चीज के लिए ऋण उपलब्ध है और नामी कम्पनियां ग्राहकों के पीछे घूमने पर मजबूर हैं। इसके विपरीत एक दौर तीन दशक पहले का था। जब एक अदद साइकिल आपको आम से ख़ास बना देने के लिए काफ़ी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महज चार दशक पहले की। यह वो दौर था जब किराए पर साइकिल देने वालों की भरपूर चाँदी हुआ करती थी। तब साइकिल खरीद पाना हर किसी के बस में नहीं था। लिहाजा चार आने घण्टा या दो रुपए दिन के हिसाब से साइकिल किराए पर देना एक बेहतरीन व्यवसाय था। बड़ों के लिए 22 और 24 इंची साइकिलें थीं तो नौसिखियों के लिए छोटे-छोटे अद्धे-पउए उपलब्ध थे। साइकिल किराए पर देने व बेचने की दो बड़ी दुकानें शहरी क्षेत्र में श्रीराम धर्मशाला के बाहर थीं। जो आज भी यथावत संचालित हैं। इनमें से एक का संचालन तब श्री हरिओम गुप्ता के बड़े भाई और पिताजी करते थे। दूसरी आज की तरह श्री सुरेश गुप्ता द्वारा ही संचालित थी। इनकी प्रतिस्पर्द्धा वाली दो दुकानें किला रोड पर नवग्रह के मंदिर के सामने हुआ करती थीं। एक महेंद्र मेहरा साइकिल स्टोर्स, दूसरी शराफ़त साइकिल स्टोर्स। एक दुकान बोहरा बाज़ार में फूटे मुकासे के ठीक सामने थी। जिसे नबी साइकिल स्टोर्स के नाम से जाना जाता था। वहीं खेड़ापति हनुमान मंदिर के सामने रोशनलाल गुप्ता (एड) के मार्केट में एक दुकान सूरज नारायण शुक्ला की थी। बाद में बुरहानी साइकिल स्टोर्स नाम की एक और दुकान बोहरा बाज़ार में ही खुल गई। यही दुकानें थीं जिनसे हमारा रोज़ का वास्ता था। कुछ छुटपुट दुकानें शहर के अन्य हिस्सों में भी खुलती जा रही थीं। यह 1980 का ही दशक था। सन 1981 में मुझे और छोटे भाई सहित मोहल्ले के सखाओं को साइकिल चलाने का शौक़ लगा। तब मैं कक्षा 09 का छात्र हुआ करता था। सुबह से शाम तक बस साइकिल चलाने की धुन न जाने कितने बच्चों की खोपड़ी पर सवार थी। ख़ास कर बाइक स्टाइल के उन सिंगल-सीटर अद्धों की, जिनकी शान ही निराली होती थी। यह अलग बात है कि उन्हें हासिल करने के लिए भारी इंतज़ार करना पड़ता था। अद्धे-पौवे गिने-चुने होते थे और चलाने वालों की भीड़ कम से कम दस गुना अधिक। एक बार जिसके हाथ लग जाता था वो तब तक छोड़ने को राज़ी नहीं होता था, जब तक जेब में पैसे खनखना रहे होते थे। कुछ अपना टाइम ख़त्म होने से पहले आधा या एक घण्टे के लिए समय बढ़वा लेते थे। ऐसे में सारे अरमानों पर पानी सा फिर जाता था। जबकि अगला उस पर चक्कर काटते हुए छाती पर मूँग सी दलता रहता था। इस स्थिति में एक दुकान से दूसरी तक भटकने में स्कूल की छुट्टी होना आम बात थी। नाम भी कट-कट कर जुड़ता था मगर इसकी चिंता मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी और उनके साथ बाल विद्या मंदिर में पढ़ाने वाली सुश्री उमा नाटेकर (बुआ) को करनी पड़ती थी। साल में आठ-दस बार नाम कटने और जुड़ने का कीर्तिमान पूरे स्कूल में शायद तब मेरे ही नाम रहता होगा। इसी तरह एक-एक कर तीन साल बीत गए। सन 1983 में हायर सेकेंडरी का छात्र होने तक मैं अद्धों से साइकिल तक आ चुका था। अब मेरी सबसे पसंदीदा दुकान मेहरा साइकिल स्टोर्स थी। इसका संचालन ब्राह्मण पाड़ा निवासी श्री रामप्रसाद शर्मा (ठेकेदार) करते थे। हम सब उम्र के लिहाज से उन्हें ताऊजी कहते थे। बेहद सहज, सरल व शांत होता था हमारे प्रति उनका बर्ताव। हमेशा सफेद धोती-कुर्ते और गांधी टोपी में नज़र आते थे वो। यही साल था जब पापा को विभाग ने लेखापाल के पद पर पदोन्नत करते हुए छह माह के प्रशिक्षण हेतु भोपाल भेज दिया। तब दो गृहस्थी होने से घर का बजट डगमगाने लगा मगर साइकिलबाज़ी का शौक़ बदस्तूर जारी बना रहा। परीक्षा शुरू होने से पहले मैंने पापा को एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि मुझे कॉलेज जाने के लिए साइकिल की ज़रूरत होगी। शिक्षकों की तरह पापा को भी मेरे एक बार में उत्तीर्ण होने को लेकर संदेह रहा होगा शायद। तभी उत्तर में पास होने पर साइकिल दिलाने का वादा कर दिया गया उनके द्वारा। इधर परीक्षा हुई और समय पर नतीजा भी आ गया। सबकी आशंकाओं के विरुद्ध अपने राम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो चुके थे। उत्साह गगनचुम्बी था और दिमाग़ अपनी साइकिल से कॉलेज जाने के लिए कुलांचे भरने लगा था। पापा की ट्रेनिंग को कुल ढाई महीने बीते थे। उनकी वापसी में साढ़े तीन माह अब भी बाक़ी थे। कॉलेज में दाखिला मुश्किल से डेढ़ महीने में हो जाना था। पापा को लिखे गए पत्र में उनका वादा याद दिलाया गया। यह भी पूछा गया कि क्या मैं आसान किश्तों पर साइकिल खरीद सकता हूँ? पापा को शायद हम बच्चों और ताऊजी के बीच डेढ़ साल में बने आत्मीय रिश्ते का इल्म नहीं था। तभी उनका जवाब सकारात्मक आया। मामी की सहमति मिल ही चुकी थी। उसी दिन मैं ताऊजी की दुकान पर पहुंचा। बड़ी झिझक के साथ ठेकेदार साहब को अपनी मंशा बताई। लग रहा था कि वे मना करेंगे। वजह यह थी कि उन्हें तब मेरे नाम के अलावा उपनाम तक भी पता नहीं था। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी वे पूरी तरह अनभिज्ञ थे। बावजूद इसके उन्होंने एक बार में “हाँ” कहते देरी नहीं लगाई। बस इतना पूछा कि कौन सी साइकिल चाहिए। मैंने 22 इंची एटलस साइकिल लेने की इच्छा जताई। ताऊजी ने तत्काल अपने कर्मचारी को साइकिल कसने का आदेश दे दिया। डेढ़ से दो घण्टे के बीच साइकिल कस चुकी थी। आगे-पीछे कैरियर, शानदार घण्टी, चैन कवर और पहियों में गजरों के साथ एक्स्ट्रा गुदगुदी सीट और लॉक भी साइकिल में लगवाया गया। बिल बना 555 रुपए का, जो 5 किश्तों में देना तय हुआ। बिना एक रुपया दिए हम नई साइकिल के साथ बाज़ार नापने निकल पड़े। सिने स्टार जितेंद्र की फिल्मों के प्रति तब भारी आकर्षण था। लिहाजा चैन कवर पर “हिम्मत वाला” भी लिखवा लाए पेंटर से। यह उस दौर की सुपर हिट मसाला मूवी थी। शाम को नई साइकिल के साथ घर लौटे तो मम्मी को ताज्जुब हुआ, जिन्हें आसानी से साइकिल फाइनेंस होने की शायद उम्मीद नहीं रही होगी। बिना किसी बड़े के साथ जाए। सारी बात पता चली तो उनके अचरज का भी ठिकाना न रहा। यह ख़बर ख़त के जरिए भीपाल तक भी भेज दी गई। परीक्षाफल से प्रसन्न पापा ने राहत की सांस ज़रूर ली होगी उस दिन। जुलाई में नई साइकिल पर शान से सवार हो कर किले में संचालित कॉलेज में पहुंचे। वहाँ न्यू ब्रांड साइकिल सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। जिसे रोज़ धो कर तेल-पानी से चमकाया जाता था। तब मुश्किल से आधा दर्जन से भी कम सीनियर्स थे, जिनके पास पुरानी लेकिन भारी भरकम बाइक्स थीं। तेल-पानी के पोंछे से चमचमाती नई साइकिल शायद मेरे ही पास थी। किले से नीचे आने के लिए साइकिल की सवारी कइयों की चाहत में होती थी। लिहाजा मुझसे दोस्ती गांठने वालों में अन्य संकायों के विद्यार्थी भी शामिल थे। छात्राओं को भी अक्सर लिफ़्ट मिल जाती थी। साइकिल और में उस दिन ख़ुद को धन्य मान लेते थे। भारी ढलान और ज़बर्दस्त घुमाव की वजह से आगे-पीछे सवारी बैठा लाना भी मुश्किल नहीं था। जिन्हें नीचे आने के बाद पहले गेट पर बाय-बाय कर दिया जाता था, क्योंकि आगे भारी चढ़ाई होती थी। साइकिल दौड़ाने में भारी निपुण हो गया था मैं। बाद में इसी पर बैठा कर मम्मी को छोड़ने व लाने के लिए जाने लगा। जो उन दिनों घर के अर्थशास्त्र को पटरी पर लाने के लिए होम ट्यूटर की भूमिका का निर्वाह कर रही थीं। कोशिश एकाध बार पापा को भी बैठाने की रही, जो नाकाम ही साबित हुई। वे गिरने की आशंका से कभी भी साइकिल पर सवार नहीं हुए। ज़्यादा ज़िद मैंने भी कभी नहीं की, क्योंकि वे उल्टे की जगह सीधे हाथ की तरफ पांव लटका कर बैठते थे। पापा के आने के बाद साइकिल की क़ीमत 5 की जगह 3 ही किश्तों में अदा कर दी गई। एक अदद नई साइकिल ने ज़िन्दगी को बहुत हद तक आसान कर दिया था। चक्की से गेंहू पिसाने हों, टाल से चूल्हे के लिए लकड़ियां लानी हों या फिर आए दिन बिजली फेल होने पर कुओं से पानी की ढुलाई करनी हो। साइकिल हर काम में मददगार थी। हाथ ठेलों पर होने वाला खर्च भी बचने लगा था। मित्र मंडली में रुतबा अलग से बोनस था। मोहल्ले वालों की मदद आए दिन उसी से होती थी। बदले में थोड़ी सी तारीफ़ मिल जाया करती थी। एक साइकिल पूरे मोहल्ले को मुझसे जोड़ चुकी थी। यह ठाठ अब बेशक़ीमती बाइक्स और कारों के भी नसीब में नहीं। क्योंकि उनकी तादाद इंसानों के बराबर हो चली है। किराए पर साइकिल अब कोई नहीं लेता। साइकिल बेचने और सुधारने का काम भी कम हो गया था। जिसे सरकार ने फिर से पटरी पर ला दिया है, स्कूलों में निःशुल्क साइकिल बाँटन की योजना चला कर। अतीत से जुड़े इस एक और अध्याय पर पूर्ण विराम लगाने से पहले सादर नमन स्व. श्री रामप्रसाद जी ठेकेदार उर्फ़ ताऊजी को, जिनकी बदौलत जीवन के पहले वाहन का मालिक बनना सहज सुलभ हुआ। इतनी कृतज्ञता तो उनके प्रति ईमानदारी से बनती ही है। साइकिलबाज़ी के दौर से जुड़े कुछ और किस्से फिर कभी। हाल-फ़िलहाल जय रामजी की।
😊😊😊😊😊😊😊😊