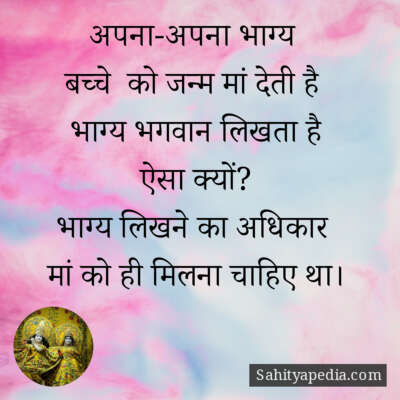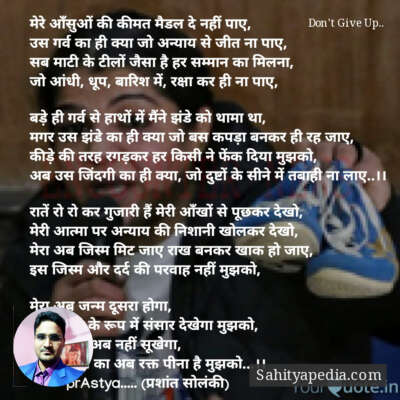हिंदी दलित साहित्य में बिहार- झारखंड के कथाकारों की भूमिका// आनंद प्रवीण

दलित साहित्य को मजबूती देने और एक मुकाम तक पहुँचाने वाले साहित्यकारों में बिहार और झारखंड के दलित साहित्यकारों का अहम योगदान रहा है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास एवं आत्मकथाओं का विपुल साहित्य बिहार-झारखंड में रचा गया है। दयानंद बटोर की कहानी ‘सुरंग’ की लोकप्रियता से हिंदी पट्टी के तमाम लेखक एवं संवेदनशील पाठक वाकिफ़ हैं। एक दलित शोध-छात्र किस प्रकार एक सवर्ण प्राध्यापक के जातीय भेदभाव का शिकार बनता है, किस प्रकार उसे दलित होने के कारण कई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दलित शोधार्थियों को विश्वविद्यालयों में होने वाली परेशानियों से परिचय कराती यह कहानी क्या आज भी प्रासंगिक है? जबकि आज विश्वविद्यालयों में दलित प्राध्यापकों की कमी नहीं है? मुझे लगता है हाँ, इस कहानी की प्रासंगिकता आज भी है। महाराष्ट्र के वर्धा विश्वविद्यालय में जब एक दलित छात्र को अपने शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए धरना देना पड़ता है और उसपर एबीवीपी के लड़कों का हमला होता है तब इस कहानी की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के लिए उचित योग्यता और वरीयता क्रम में श्रेष्ठ होने पर भी श्यौराज सिंह बेचैन को केवल इसलिए सड़क पर उतरना पड़ता है क्योंकि वे दलित हैं तब इस कहानी की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। जब देश की राजधानी दिल्ली के विश्वविद्यालय में आज भी इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं तो देश के अन्य विश्वविद्यालयों की बात ही क्या। केवल इस कहानी की नहीं, बल्कि प्रह्लाद चन्द्र दास की कहानी ‘लटकी हुई शर्त’ की प्रासंगिकता भी बनी हुई है। आज भी देश के सभी राज्यों के किसी न किसी गाँव में ऐसी प्रथा कायम है जहाँ ‘भोज’ में जातियों के हिसाब से ‘पंगत’ लगती है या कम से कम दलितों के लिए अलग लगती है और उन्हें पत्तल भी स्वयं ही उठाना पड़ता है। आजतक ऐसी अपमानजनक प्रथाओं को पुष्पित-पल्लवित करने वाला हमारा समाज आज से नब्बे वर्ष पहले गाँधी जी के हरिजन सेवक संघ की मिठी बातों से निश्चित ही थोड़ा भी नहीं बदला होगा। उनके इस कार्य का सम्मान अवश्य ही किया जाना चाहिए, पर यह कार्य समानता के लिए नहीं था, समाज में बराबरी लाने के लिए नहीं था, केवल छुआछूत को खत्म करने के लिए था। उनका मानना था कि वर्णव्यवस्था हिंदू समाज की रीढ़ है और इस व्यवस्था के हिसाब से जिसको जो कार्य सौंपा गया है, उन्हें वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसी में उसकी दक्षता है। गाँधी जी के इस विचार का खंडन करते हुए बाबा साहेब अपने लेख ‘ श्रमविभाजन और जातिप्रथा’ में लिखते हैं कि जब तक वर्ण के हिसाब से लोग अपना व्यवसाय चुनेंगे तब तक वर्णव्यवस्था और जाति अधिक मजबूत होती जाएगी। जाति और वर्ण के विनाश के लिए अलग व्यवसाय चुनना आवश्यक हो जाता है। हमारे भारतीय समाज में गैर बराबरी को नष्ट करने वाले जो भी बदलाव हुए हैं उन बदलावों के पीछे गैर सवर्णों का ही हाथ रहा है। संत कबीर और संत रैदास से लेकर बाबा साहेब अंबेडकर तक सारे के सारे शूद्र और अछूत जातियों के लोग ही हैं जिन्होंने समतामूलक समाज बनाने के लिए अपना जीवन दिया।
बिहार-झारखंड की दलित महिलाओं ने भी अपनी लेखनी से साहित्यिकों के बीच लोहा मनवाया है। इस श्रेणी में कावेरी का नाम अग्रगण्य है। औपन्यासिक रचना के मामले में वह देश के तमाम दलित महिलाओं में पहली महिला है। उनकी कहानी ‘सुमंगली’ में दलित और वंचित परिवार की महिलाओं की विकट परिस्थितियों का सचित्र वर्णन है। मजदूरों- दलितों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना जैसे कुछ अमीर और जातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। कहानी में सुगिया बीमारी की हालत में अपने पिछले दिनों को याद करते हुए पाती है कि उसके जीवन में और उस जैसी अन्य औरतों के जीवन में जो भी सुविधा सम्पन्न पुरुष आये हैं सब ने उन्हें नोंचा है, बलात्कार किया है। इस बीमारी की हालत में उसकी केवल एक साथी मंगली है जो मानव से इतर प्राणी कुतिया है। जब मानव हमारी संवेदना को समझने और महसूस कर पाने की स्थिति में नहीं रह जाता है तो ऐसे में मानवेतर प्राणी ही हमारा साथी होता है। मजदूर महिलाओं के जीवन को बखूबी बयां करती यह कहानी वास्तव में दलित साहित्य में महिलाओं की उपस्थिति को भी मजबूत करती है।
अजय यतीश की कहानी ‘द्वंद्व’ की चर्चा भी दलित साहित्यकारों के बीच खूब होती है। यह कहानी भी ‘सुमंगली’ कहानी की तरह दलित और मजदूर पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और महिलाओं की उसी संकट का जिक्र करती है। इसमें वाम विचार के शामिल होने से कहानी का फलक बड़ा हो जाता है। कहानी का नायक ‘रामपरीखा’ एक दलित होता है जो आरंभ में एक मजबूत वामपंथी होता है। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। उसके गाँव का दबंग झरी पांडेय और उसके लोग रोज रात में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। कुछ वामपंथी साथी भी दलित महिलाओं के साथ ही अपनी रात गुजारते हैं। दोनों में अन्तर बस इतना होता है कि दबंग जोर-जबरदस्ती करते हैं और वामपंथी साथी अपनी जातीय श्रेष्ठता, अमीरी का सहारा लेकर और उन्हें प्रलोभन देकर अपना काम निकालते हैं। रामपरीखा अपने आसपास की महिलाओं को इस नर्क से बाहर निकालने की सोच रखता है। वामपंथियों के बीच उसकी इस सोच का हल न पाकर वह अपना रास्ता बदल लेता है। वह अंबेडकरवादी हो जाता है। एक दिन उसका पुराना साथी सौरभ दा उससे मिलने आता है। उसके बदले विचार को देख और समझकर कहता है कि तुम्हारी इस लड़ाई में भी तुम्हें हथियार की जरूरत पड़ेगी। बिना हथियार के तुम दबंगों से जीत नहीं सकते। कहानी का अंत रामपरीखा की जीत से होता है। यह जीत अकेले रामपरीखा की जीत नहीं है, दलितों- शोषितों की भी जीत है; आंबेडकरवाद और मार्क्सवाद के गठजोड़ की भी जीत है। वास्तव में भारतीय समाज के रग-रग में बसे जातिवाद से लड़ने के लिए अंबेडकरवाद की जरूरत है तो आर्थिक आजादी के लिए मार्क्सवाद की जरूरत है। हम तब हार जाते हैं जब या तो मार्क्सवाद को नज़रअंदाज़ कर शुद्ध आंबेडकरवादी हो जाते हैं या फिर अंबेडकरवाद को नज़रअंदाज़ कर शुद्ध मार्क्सवादी हो जाते हैं। हमें दोनों विचारधाराओं को अलगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों को साथ लाने की जरूरत है। भारत की बहुसंख्यक मजदूर आबादी दलित हैं जो एकसाथ जातीय और आर्थिक दोनों स्तरों पर संघर्षरत हैं। उनके आर्थिक रूप से सबल हो जाने पर भी समाज में बराबरी का स्थान नहीं मिलता है। उनकी जाति उन्हें तब भी डंक मारती रहती है। इसलिए अंबेडकरवाद को नकारने वाला मार्क्सवादी और मार्क्सवाद को नकारने वाला अंबेडकरवादी दोनों भारतीय समाज के कमजोर तबकों के लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं और हमें उनसे बचने की जरूरत है, समाज को वैसे लोगों से बचाने की जरूरत है। तब जाकर समतामूलक समाज का निर्माण हो पाएगा, सभी लोग कम से कम जाति के आधार पर एक-दूसरे के बराबर हो पाएंगे।
इसी कड़ी में एक और नाम विपिन बिहारी की कहानी ‘लागा झुलनिया का धक्का’ का लेना आवश्यक हो जाता है। प्रसिद्ध अंबेडकरवादी आलोचक डॉ० मुसाफ़िर बैठा के शब्दों में – ” विपिन बिहारी के रूप में बिहार को अबतक का भारत का सबसे अधिक कथा साहित्य रचने वाला अंबेडकरवादी लेखक प्राप्त है।” उनकी कहानियों के दलित पात्रों के बारे में प्रसिद्ध आलोचक कँवल भारती कहते हैं- ” वे अपने सार्वजनिक जीवन में अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और स्वाभिमानी हैं, पर अपने पूर्वजों की तरह चेतना विहीन और भीरू नहीं हैं, बल्कि विद्रोही हैं। ”
‘लागा झुलनिया का धक्का’ एक दलित- मजदूर दम्पति की कहानी है। कहानी की नायिका मानवती की बचपन से ख्वाहिश है कि उसका पति उसे झुलनिया लाकर देगा। उसकी इस ख्वाहिश का पता जैसे ही बबुआन टोले के बिकरमा को लगता है, वह उसके पीछे पड़ जाता है। मानमती अपनी शादी तक जैसे-तैसे खुद को बिकरमा से बचाने में क़ामयाब हो जाती है, पर शादी के बाद उसके पति के कलकत्ता चले जाने पर वह पुनः अपने माता- पिता के पास आ जाती है जहाँ फिर से बिकरमा से उसका सामना होता है। कहानी का अंत बिकरमा की मौत और मानमती के ग़ायब होने पर होता है।
दलित साहित्य में लगभग सभी रचनाओं में स्त्री पात्रों की मजबूत उपस्थिति इसे और अधिक बल देती है इसके बरक्स मुख्यधारा की प्रसिद्ध रचनाओं में कम ही स्त्री पात्रों की ऐसी उपस्थिति दर्ज हुई है। बिहार- झारखंड के हिंदी दलित कथाकारों में और भी कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिनमें बुद्ध शरण हंस, देवनारायण पासवान आदि का नाम प्रमुख है। बिहार- झारखंड के दलित युवा कथाकारों का नाम फिलहाल अज्ञात है, तत्काल मेरा नाम लिया जा सकता है।
मेरी कहानी ‘ब्राह्मण की बेटी’ 2019 में डिप्रेस्ड एक्सप्रेस में छप चुकी है। जिसमें एक ब्राह्मण और एक पिछड़े समाज की लड़की की दोस्ती और उनकी मान्यताओं की वजह से अलगाव का जिक्र है। इन रचनाकारों को पढ़ते हुए बिहार- झारखंड के दलित- पिछड़े समाज को समझने और उनकी परेशानियों से रूबरू होने में सहायता मिलती है। ये कहानियाँ हमारे समाज के खामियों का सशक्त चित्र प्रस्तुत करती हैं जो भविष्य में समाज को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
आनंद प्रवीण
छात्र, पटना विश्वविद्यालय।
सम्पर्क-6205271834