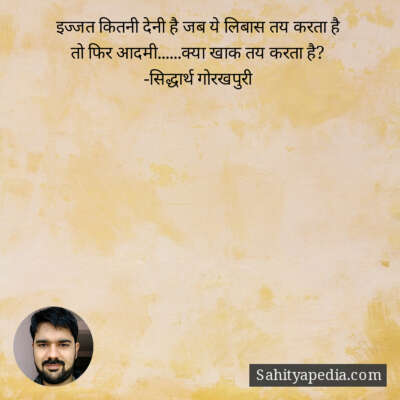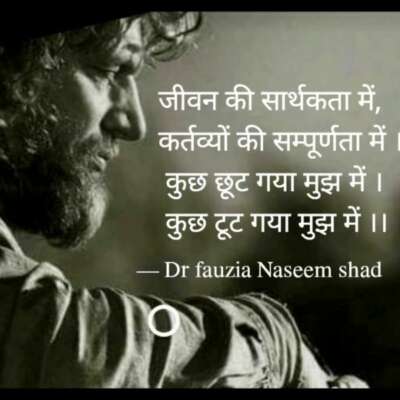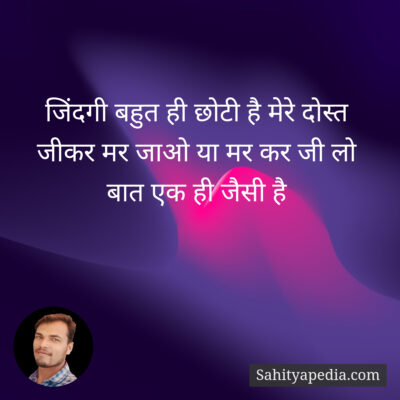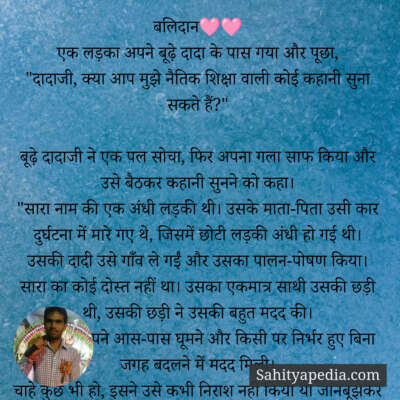#स्मृति_के_गवाक्ष_से-

#स्मृति_के_गवाक्ष_से-
■ शिवनगरी के गरिमापूर्ण गौरव का अमृत वर्ष
◆ सदियों पुराना परिसरों, दशकों पुराना आयोजन
◆ जहां इंच-इंच धरती का होता था अग्रिम आरक्षण
◆ जहां उमड़ती थी सामाजिक समरसता
◆ जहां देर रात तक जुटते थे नगरी के परिवार
◆ जहां के कण-कण में बसी है एक आयोजन परम्परा
【प्रणय प्रभात】
इस समय आप एक चित्र देख रहे हैं। जो लौकिक रूप से एक मंदिर परिसर जैसा है। जैसा क्या है, मंदिर परिसर ही है। सामान्यतः वैसा ही, जैसा होता है। की जा रही साज-सज्जा के बिना साधारण सा दिखाई देने वाला। जहां सप्ताह के किसी विशेष दिन भक्तों की भीड़ लगती है। जहां वर्ष में एकाध या दो-चार बार आस्था का ज्वार उमड़ता है। किसी विशेष पर्व या उत्सव के चलते। निस्संदेह यह परिसर भी अन्य देवस्थलों की तरह जनास्था व उपस्थिति का एक केंद्र है। जिसे “राम-तलाई” कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, यहां कभी ताल या तालाब की छोटी बहिन “तलैया” रही होगी।
पास ही कुछ ऊंचाई पर एक छोटी सी मढ़ैया। जहां पीपल के एक छतनार वृक्ष के नीचे हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई होगी। क्षेत्र-रक्षक के रूप में, सदियों पहले। वो भी तब, जब यह क्षेत्र निर्जन रहा होगा। रियासतकालीन रियाया के किले की चारदीवारी में आबाद होने के कारण। विशाल सिंहद्वारों और अभेद्य परकोटे के पीछे। शिव-पहाड़ नामक ऊंचे टीले पर बने उस बड़े किले के अंदर, जिसे संरचना के कारण “दुर्ग” कहना अधिक उचित होगा। यह और बात है कि गौड़ राजवंश द्वारा 14वीं सदी में बनवाया गया यह किला “बाला किला” भी कहलाता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। जो कालांतर में सूख कर एक भूखंड में बदल गई।
अनुमान लगाया जा सकता है कि राम-तलाई का निर्माण गौड़ राजाओं ने विजन-वासी जीव-जंतुओं के लिए एक जल-स्त्रोत के रूप में कराया गया होगा। जहां कालांतर में विराजित हनुमान जी ऊंचाई पर होने के कारण “रामतलाई के बालाजी” के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्पष्ट है कि तलाई मंदिर से पहले की है। ऐसा नहीं होता, तो इसका नाम “हनुमान तलाई” होता। इस दृष्टिकोण से हम तलाई व मंदिर को 14वीं और 15वीं सदी के बीच का मान सकते हैं। इसका एक आधार “सिंधिया राजवंश” भी है। जो गौड़ राजा को पराजित कर किले व क्षेत्र का अधिपति बना और धर्मस्थलों के निर्माण को लेकर सक्रिय रहा। जिनके मंदिर या परिसर की किसी भी संरचना से यह स्थान मेल नहीं खाता।
यह हुआ तर्क, तुलना व अनुमान के आधार पर इसकी प्राचीनता का एक परिचय, जिस पर जानकारों और विद्वानों के मत-मतांतर हो सकते हैं। मैं न स्वघोषित इतिहासवेत्ता, न स्वयम्भू पुरातत्वविद्, जो आंकड़ों व तथ्यों की खोज के नाम पर सफेद काग़ज़ काले करूं। अपनी कल्पनाशीलता के बूते कुछ समझने व समझाने की सामर्थ्य अवश्य रखता हूँ। इतना कुछ इसी लिए लिखा कि सनद रहे और वक़्त-ज़रूरत काम आए। वस्तुतः आज के आलेख की विषय-वस्तु इस परिसर के अतीत से जुड़ा एक काल-खंड है। उस काल-खंड से जुड़ा एक आयोजन है। वो आयोजन, जो इस वर्ष अपने गौरवमयी अतीत के शुभाशीष से अमृत वर्ष में पदार्पण कर रहा है। अर्थात “हीरक जयंती” मनाने की दिशा में गरिमा के साथ अग्रसर है।
जी हां। आलेख का केंद्र है शिवनगरी श्योपुर का श्री रामलीला महोत्सव, जो 75 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। प्रभु श्री राम की दिव्य कथा को जनमानस तक पहुंचाने के पुनीत संकल्प के साथ। श्री रामचरित मानस पर आधारित एक पखवाड़े के क्रमिक मंचन के रूप में। हरमोनियम व ढोलक के सुर-ताल की जुगलबंदी के साथ। पात्रों के संवाद श्री राधेश्याम रामायण से। वो भी काव्यात्मक शैली में। कभी वीर, कभी करुण, कभी हास्य, कभी रौद्र तो कभी भक्ति या शांत रस के भाव में। एक धार्मिक उत्सव के रूप में श्रीगणेश के बाद यह समागम नगरी की सांस्कृतिक पहचान बनता चला गया। जिसने संस्थापक पुरोधाओं के अथक प्रयासों से 25 वर्ष की यात्रा अपने बलबूते पूर्ण की। वो भी साधनों-संसाधनों के व्यापक अभाव वाले समय में।
यह वो समय था, जब देश को स्वतंत्र हुए मात्र 2 ही वर्ष बीते थे। राष्ट्र-विभाजन के बाद की विभीषिका आम जन को भयाक्रांत किए हुए थी। भीषण रक्तपात व नरसंहार से मानवता विचलित थी। समूचा देश नए घावों से कराह रहा था और संवेदना स्वयं सिसक रही थी। विकृत परिवेश में सुसंस्कृत मुट्ठी भर वैश्य व द्विज परिवार के मुखियाओं ने इस पावन समागम का बीड़ा उठाया। तन, मन, धन से जुटे और श्री रामलीला उत्सव का सूत्रपात किया। सीमित आबादी वाले छोटे से लेकिन शांतिपूर्ण श्योपुर कलां कस्बे में। जो मूलतः शिवपुर का अपभ्रंश था। तब न बिजली थी, न माइक और लाउड-स्पीकर। मशाल से पेट्रोमैक्स तक की रोशनी में उत्सव ने वर्ष-प्रतिवर्ष सफलता के नए आयाम स्थापित किए। जिसके पीछे निश्चित हीँ प्रभु श्री राम की कृपा रही। आशीष मां जानकी जी का और प्रेरणा हनुमान जी महाराज की। जिनके दाहिने भाग में टीन-शेड वाला एक चबूतरा इस आयोजन का मंच बना और सामने का चौरस प्रांगण दर्शक-दीर्घा।
आश्विन माह के गुलाबी
मौसम में खुले आकाश के नीचे मंचन की लोकप्रियता बढ़ी। स्वीकार्यता के साथ बढ़ा जनसहयोग, जो आयोजन प्रबंधों के क्रमिक विकास का माध्यम बनता चला गया। वर्ष 1974 में रजत-वर्ष मनाने वाले इस आयोजन को स्वर्णकाल में ले जाने का काम किया अगली पीढ़ी ने। जिसने पुरखों की जायदाद ही नहीं धरोहर भी चाव से संभाली। पैतृक कारोबार के साथ पूर्वजों की धरोहर का भी संरक्षण व सुपोषण अपना दायित्व मान कर किया। नए-नए साधन-संसाधन ही नहीं, कलाकार भी जुड़े। देखते ही देखते आयोजन युवा से प्रौढ़ होता चला गया। केवल उम्र के मामले में। चमत्कार यह था कि अधेड़ आयोजन समय के विरुद्ध उल्टी चाल चल रहा था। मतलब उसकी यात्रा तरुणाई की ओर थी।
मेरा जुड़ाव इस आयोजन से 1971 में हुआ। मात्र 3 साल की उस कच्ची उम्र में, जब दूध के दांत भी शायद नहीं आए होंगे। टोड़ी बाज़ार की श्रोत्रिय गली (जिसे तब की तरह अब भी सोती गली कहा जाता है) में स्थित श्री मोतीलाल सुनार के बाड़े में परिवार का ठिकाना था। बाड़ा एक चॉल (जाग) की तरह था। दर्ज़न
भर परिवार एक कुटुंब की तरह रहते थे। खान-पान से लेकर छोटे-बड़े सुख-दु:ख में साझेदारी थी। न कोई दूरी, न कोई मजबूरी, न कोई भेदभाव। लगभग एक सा रहन-सहन, एक सी सोच और एक सी जीवन-शैली भी। सब कुछ एक सा था, तो शौक़ अलग कैसे होते? इकलखोर बनाने वाले टीव्ही, मोबाइल तब कल्पनाओं से भी परे थे। मनोरंजन के नाम पर ले देकर एक अदद रेडियो था। बड़ा और भारी-भरकम सा, मरफ़ी कम्पनी का। पापा को दहेज में मिला था शायद। शाम-सवेरे बजता था। सब मिल-बैठ कर सुनते थे। बच्चों के अपने खेल थे, बड़ों के अपने। कुल मिला कर जीवन में रोचकता की कोई कमी न थी। वहीं मनोरंजन का भरपूर टोटा था। ऐसे में स्थानीय स्तर का छोटे से छोटा आयोजन एक बड़े वरदान जैसा था। मरुभूमि में वर्षा की भांति।
यह विषयांतर नहीं, आलेख का प्रबल पक्ष है। आप इसे विचार-सरिता का उद्गम भी मान सकते हैं। परिवार और पड़ोसियों का संगम न होता, तो रामलीला की सरस गंगा में डुबकी का चस्का कैसे लगता? चस्का न लगता तो आयोजन से जुड़ाव न होता। जुड़ाव न होता तो यह सब न लिखा जाता, जो लिखा जा रहा है। आगे का सब कुछ देखा-भाला है, जिसका श्रेय उक्त परिवेश व परवरिश को ही है। इसीलिए यह सब बताना पड़ रहा है। बताना यह भी चाहता हूँ कि मैं इस आयोजन के तीन सोपानों का स्वयं साक्षी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे रामलीला समारोह के रजत, स्वर्ण व हीरक वर्ष के साक्षी बनने का सुख मिला। अपनी दादी, मां, बड़ी-छोटी बुआ व अड़ोस-पड़ोस वाली ताई, चाची, भैया-दीदी व सखा-सहेलियों की वजह से। जिसके आधार पर मैं एक गौरव-गाथा का मंगलाचरण कर पा रहा हूँ। उन स्मृतियों के गवाक्ष में बैठ कर, जहां सब कुछ एक चल-चित्र की तरह आंखों में तैर रहा है। एक शब्द-चित्र के रूप में अपने आभास की जो अभिव्यकि कर रहा हूँ, उसे मेरी पीढ़ी की ओर से वंदन-अभिनंदन भी मान सकते हैं आप।
धर्म-संस्कृति के अंकुर को अंकुरण के बाद पल्लवन का समुचित अक्सर वर्ष 1974 में मिला। किराए के घर से निजी घर में आने के बाद। जहां रामलीला के दीवाने मित्रों व परिवारों की संख्या दूनी थी। यहां रामलीला देखने के साथ घर पर करने का भाव जागा। जो लगभग डेढ़ दशक तक रहा। एक जुनून की तरह। रात में रामलीला देखना और दिन में घर-घर करना चाव बनता चला गया। जिसमें मोहल्ले भर के मित्र तन, मन, धन से मददगार बनते थे। युवावस्था तक रामलीला के एक-एक पात्र तक कोई न कोई सरोकार इसी रुचि के चलते स्वतः स्थापित होता चला गया। जिससे जुड़े तमाम वृत्तांत बेहद रोचक हैं। कभी न कभी अलग से लिखूंगा उन पर भी।
आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्टतः निवेदित करना चाहता हूँ। वो यह कि इस आलेखन का उद्देश्य न ठकुर-सुहाती है, न महिमा-मंडन, न किसी का तुष्टिकरण। लिहाजा, किसी भी एक नाम का उल्लेख करने से स्वयं को रोक रहा हूँ। विनम्र वंदन नींव के पत्थरों से लेकर शीर्षस्थ कंगूरों तक को है। आलेख के अगले संस्करण नामों व गुणों से परिपूर्ण होंगे, यह विश्वास दिला सकता हूँ। स्पष्ट कर दूं कि अगले संस्करण या संस्मरण का लेखन इस आलेख की स्वीकार्यता व जन-सम्मतियों पर निर्भर करेगा। इस श्रंखला को कहां तक ले जाना है, यह उन सुधि व सुविज्ञजनों को तय करना है, जो धरोहर और विरासत के संरक्षण व संग्रहण का मोल समझते हैं। जिनके मन में अपने पूर्वजों व उनके द्वारा स्थापित परम्पराओं के प्रति तनिक भी श्रद्धा है। आलेख को लेकर अरुचि या उपेक्षा के भावों का आभास हुआ, तो आगामी आलेख अन्यान्य विषयों पर होंगें। जिनकी अकिंचन के पास कोई कमी नहीं, आराध्य प्रभु राम जी की अहेतुकी कृपा व परम् सद्गुरुदेव हनुमान बाबा की अनुग्रहपूर्ण प्रेरणा से।
मैंने ईश्वरीय अनुकम्पा से उक्त समारोह का वो स्वर्णिम युग देखा है, जो अभूतपूर्व रहा। वर्ष भर कस्बे के सैकड़ों परिवारों का इस आयोजन की प्रतीक्षा करना कोई छोटी बात नहीं था। रात 8 बजे के आसपास आरंभ होता था मंचन। पक्के मंच के सामने कच्चे प्रांगण में अच्छी जगह घण्टों की तपस्या से मिलती थी तब। दोपहर से पहले हमारी तरह सभी मोहल्लों के बाल-गोपाल निकल पड़ते थे घरों से। बगल में दरी, चादर, चटाई, तिरपाल या टाट की बोरी दबाए। सबका गंतव्य होती थी यही रामतलाई। मन्तव्य होता था मंचन देखने के लिए आगे की ओर अच्छी जगह की घेराबंदी। मैदान में दरी, चादर, बोरी बिछाने के बाद चारों कोनों पर पत्थर रख दिए जाते थे। क़ब्ज़ाई हुई जगह की निगरानी पारियों में की जाती थी। एक दल मौके पर पहुंचता था तो एक घर लौटता था। रोटी-पानी से निपटने के लिए। यह क्रम देर शाम तक चलता। थोड़ी सी देरी का मतलब था, उस दिन का आनंद छिन जाना। आंख बचा कर बिछावन आगे-पीछे करने में बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी आगे होती थीं। नोकझोंक, कहा-सुनी, तना-तनी देर शाम तक चलती रहती थी।
मंचन से घण्टा आधा घण्टा पहले सारे रास्ते इस प्रांगण की ओर मुड़ जाते थे। दर्शकों के दल अधिग्रहित जगहों पर जम जाते थे। कुतरने के लिए मूंगफली की थैलियां गोद में लेकर। नई मूंगफली छलनी में डाल कर चूल्हे पर सेकने व बेचने का धंधा ज़ोर-शोर से चलता था। जिसके लिए प्रांगण के कटहरे के बाहर चौगान में दर्ज़न भर से ज़्यादा ठेले शाम से लग जाते थे। मिट्टी की सोंधी महक व कच्चेपन की नमी वाली मूंगफली के बिना मंचन का मज़ा अधूरा सा लगता था। सच मानिए, यह आनंद मल्टीप्लेक्स के पॉपकॉर्न, चिप्स व स्वीट कॉर्न में आज तक नहीं मिला। सैकड़ों रुपए स्वाहा करने के बाद भी। थिएटर की नर्म, गुदगुदी सीटें आज भी वो चैन नहीं दे पातीं, जो धूल भरे मैदान पर बिछे टाट के पुराने बोरे देते थे। मामला लौकिक विरुद्ध अलौकिक आभास का जो है। किसी को, ख़ास कर नई पीढ़ी को अजीब लगे तो लगे। सच यही है इस भीड़ में धनाढ्य व संभ्रांत परिवारों की संख्या भी बराबर की हुआ करती थी।
आज जिस “समरसता” की डींग हम थोथा आदर्श बघारने के लिए करते हैं, वो 1970 व 80 के दशक तक इसी प्रांगण में अठखेली करती दिखती थी। ऊंचा-नीचा, छोटा-बड़ा, अगड़ा-पिछड़ा जैसा कोई लफड़ा था ही नहीं। “व्हीआईपी कल्चर” या “राजनैतिक रसूख” जैसी कोई महामारी भी तब अस्तित्व में नहीं थी, जो सह-अस्तित्व के नैसर्गिक सिद्धांत के लिए चुनौती या पनौती साबित हो पाती। सबकी समरस दृष्टि केवल सरस् मंचन पर टिकी होती थी। जो बरसों-बरस इस नगरी की सौहार्द्र परम्परा का आधार बनी रही।
बदलते समय के साथ इस परिसर में भी बहुत कुछ बदला। मंदिर, मंच, मैदान व सभागार पक्का व सुंदर हुआ। मंच के पास भगवान गणपति व शिव जी के मंदिर का भी स्वरूप बदल गया। आयोजन के लिए स्वागत-द्वार लगने लगे। मंदिर परिसर में साज-सज्जा होने लगी। दर्शकों के लिए कुर्सियों का प्रबन्ध किया जाने लगा। नई ड्रेस, नए पर्दे, नए अस्त्र-शस्त्र आ गए। सब आ गए, बस दर्शक रूप में परिवार व मोहल्ले आने बंद हो गए। काल के गाल में समा चुकी छोटी रेल-लाइन से जुड़े दूर-दराज के ग्रामीण और वनांचल के वो दीवाने दर्शक आने बंद हो गए, जिन्होंने बाद की नस्लों को छोटी सी ट्रेन के इंजन व पायदान से लेकर छत तक पर सवारी करने का गुर चाहे-अनचाहे सिखा दिया। परिसर के सामने सड़क के पार वन विभाग के परिक्षेत्र (रेंज) के कार्यालय से लेकर आसपास के भवनों की उन छतों को सुना व पराया कर दिया, जहां 15 दिनों तक अटाटूट भीड़ दिखाई देती थी।
परिसर के पिछवाड़े मामूली दूरी पर स्थित रहे उस रेलवे-स्टेशन व मेला मैदान को वीरान कर दिया, जो ग्रामीण और वनवासी दर्शकों के लिए मुक्ताकाश रैन-बसेरे जैसा था। मनोरंजन के क्षेत्र में हुए बेतहाशा विकास ने इस आयोजन के भविष्य पर प्रश्न-चिह्न लगा दिए। एक दौर ऐसा भी आया, जब कलाकार दर्शकों के दर्शनों तक को तरस गए। दो साल के महामारी काल से काफी पहले भी तीन-चार साल के संक्रमण काल ने आयोजन-परम्परा को बहुत दुष्प्रभावित किया। लगा कि आयोजन का क्रम बंद हो जाएगा। देवयोग कहें या समिति व कलाकारों का संघर्ष, आशंकाओं पर विराम लग गया। जिसे हम राम जी व बजरंग बली की परोक्ष कृपा मानें, तो उचित होगा। वरना एक समय ऐसा भी आया था, जब समिति में मनमुटाव ने आयोजन को दो-फाड़ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि रामलीला का समानांतर आयोजन सांस्कृतिक गतिविधियों के सर्वमान्य केंद्र टोड़ी बाज़ार में आरम्भ कर दिया गया। सुखद बात यह रही कि इस विवाद का पटाक्षेप जल्दी ही हो गया। यह बात करीब 3 दशक से अधिक पुरानी है।
सुयोगवश, कुछ वर्ष पहले एक बार फिर से परिसर में दर्शकों का आगमन फिर से होने लगा। नए कलाकारों व कुछ नवाचारों ने परम्परा को नवजीवन दिया। इसी दौर में एक वर्ष ऐसा भी आया, जब तत्कालीन ज़िलाधीश व पुलिस कप्तान इस आयोजन के प्रशंसक व दर्शक बन गए। जिससे समिति सदस्यों व कलाकारों का मनोबल बढ़ा। मंचन पूर्व अतिथि रूप में विविध कर्मक्षेत्रों के विशिष्ट जनों से प्रभु-स्वरूप की मंगल-आरती भी नवाचार का हिस्सा बनी। आयोजन परम्परा के दीये की फड़फड़ाती व मन्द पड़ती लौ एक बार फिर स्थिर व आलोकित होती दिखाई दी। जिसे उत्साह व ऊर्जा का घृत देने का काम “अमृत-वर्ष” कर रहा है।
नवाचार की दिशा में श्री राम-बारात के चल-समारोह को जन-भागीदारी से भव्य बनाएं जाने, श्री राम राज्याभिषेक के लिए विजया-दशमी उपरांत एक अतिरिक्त दिवस निर्धारित किए जाने जैसे निर्णय स्वागत-योग्य हैं। जिनका अभिनंदन धर्मप्राण नगरी के एक-एक धर्मनिष्ठ परिवार का नैतिक व समयोचित दायित्व है। दायित्व का निर्वाह नगरजन स्वयं को “मिथिलावासी” मान कर करें, तो आनंद स्वतः परमानंद बन जाएगा। बारात के मार्ग में स्वागत-द्वार, बैनर्स, पताकाएं लगा कर, घरों को बिजली व दीपमालिकाओं से सजा कर, रंगोली-सज्जा व पुष्पवर्षा कर चल-समारोह को प्रतिवर्ष अविस्मरणीय बनाया जा सकता है। जो इसमें समर्थ या बारात-पथ से सम्बद्ध नहीं, वे अवध-वासी (बाराती) बन सकते हैं। जो आज के राजनैतिक व धार्मिक संक्रमण काल में समरसता से भरा एक सराहनीय, साहसिक व स्तुत्य प्रयास होगा। सद्भाव और सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने वाली घृणित व कुत्सित मानसिकता के विरुद्ध। साम्प्रदायिक एकता व सद्भाना के हित में। शेष-अशेष व हरि-इच्छाधीन। जय-जय सियाराम। जय-जय हनुमान।।
-सम्पादक-
●न्यूज़&व्यूज़●
(मध्य-प्रदेश)
😊😊😊😊😊😊😊😊😊