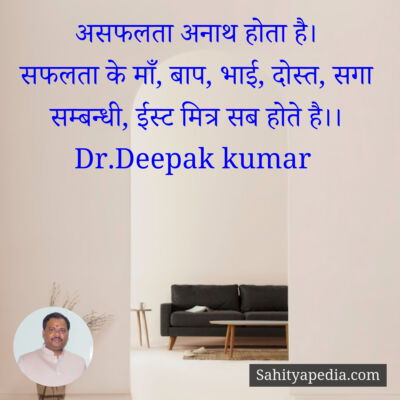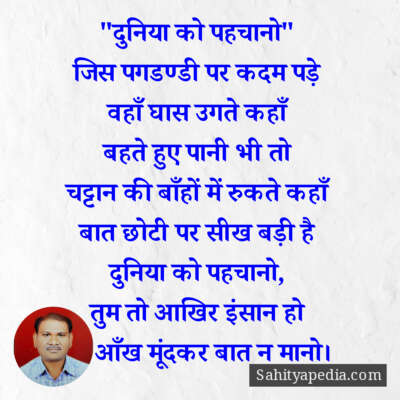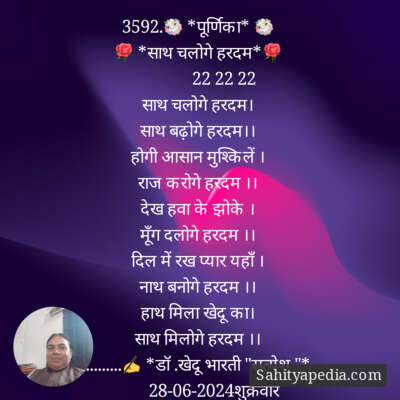सुनो प्रद्युम्न!
सुनो प्रद्युम्न
तुम्हारी निर्मम हत्या पर मैंने
शोक नहीं मनाया
और न ही मनाया मैंने
एक पल का भी मातम
बल्कि अनगिनत सवालों से घिरा मेरा रोम रोम
हो गया शर्म से पानी पानी
और रात-दिन, हर पल
बस यहीं विचार आते रहे
क्यूँ हम इंसान हो गए हैं
इतने निर्लज्ज और बर्बर
और क्यूँ दिनों दिन होते जा रहे हैं
जानवरों से भी बदतर
कहाँ गई हमारी वो मानवता
हमारे संस्कार
वो सभ्यता
हमारे सारे जीवन मूल्य
क्या हम इतने गिर चुके हैं कि
अपने क्षणिक सुख की चाह में
तनिक भी नहीं झिझकते अब बनाने से पहले
कल के सुनहरे भविष्य को अपना खिलौना
पार करके सारी हदें
निकाल कर मुखौटा
दिखा रहे हैं अपना असली
घिनौना इंसानी चेहरा इस संसार को
जिसे देखकर बर्बर जानवर भी शरमा जाये
सुनो प्रद्युमन
मैं तुमसे नहीं मिली
न ही तुम्हें देखा है कभी
पर आजकल रोज ही दिख जाते हो तुम मुझे
कभी पड़ोस की स्कूल जाती अवनी में
तो कभी माँ की ऊँगली थामे बस का इंतज़ार करते अम्बर में
और फिर
साँसे थम जाती हैं मेरी
बेचैन हो जाती हूँ मैं
दिनभर के लिए
तुम ही बताओ प्रद्युम्न
अब किस पर विश्वास करूँ मैं
और किस पर नहीं
पहले तो सिर्फ
आधे वर्ग की चिंता ही खाये जाती थी मुझे
और रात भर नींद नहीं आती थी
पर अब तो
दिन में भी बेचैन सी रहने लगी हूँ आजकल
तुम ही बताओ प्रद्युम्न
अब कौन सुरक्षित हैं यहाँ, कौन नहीं
अब मुझे नींद कैसे आये
अब मुझे चैन कैसे आये
लोधी डॉ. आशा ‘अदिति’
बैतूल म. प्र.