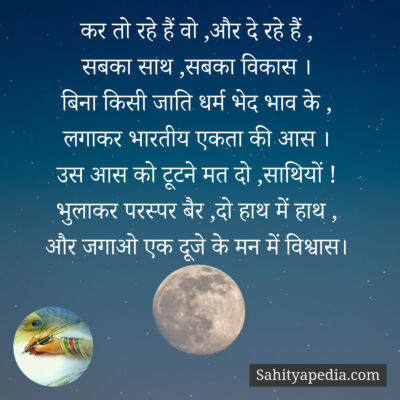साहित्य नपुंसक चरित्र जी रहा है +धीरेन्द्र शर्मा
भाई रमेशराज जी युग की जिस दाहकता को भोगकर पत्रिका निकाल रहे हो, उसके विभिन्न आयामों में से एक यह भी है कि कदम-कदम पर तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सतत् आश्वासन करने वाला मुझ जैसा तुम्हारा दोस्त भी वक़्त-जैसी बेवफाई पर आमादा हो गया। मैं तुम्हारा मनोबल और हौसला बढ़ाने के बजाय तुमसे यह पूछकर अपनी तथाकथित दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ कि ऐसे बेशर्म दौर में पत्रिका क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारी बीमार सेहत के लिये ऐसा सुझाव क्या किसी डाक्टर ने दिया है?
भाई , मैं कहता हूँ कि वक्त की नब्ज और धड़कन को पहचानने की कोशिश करो। मेरे भाई यह दौर, यह जमाना भौतिक प्रगति का है, बेईमानी का है, भ्रष्टाचार का है, वतनफरोशों का है, हलाकुओं और कानूनी चंगेजों का है। कोटा, परमिट, ठेकेदारी, दलाली, घूसखोरी, मक्कारी, चालबाजी के चक्रब्यूह में अब पूरा राष्ट्र आपादमस्तक जकड़ा हुआ है, तब तुम भगतसिंह, रामप्रसाद ‘बिस्मल’ जैसे अप्रासंगिक [अतः अवांछित] तत्त्वों की चर्चा करके अपनी सनक का ही परिचय दे रहे हो।
सच तो यह है कि अपनी निजी संवेदना, भावुकता और अनुभूति से लेकर घर-परिवार, मित्र-परिचय तथा नाते-रिश्तेदार तक की संवेदनाएँ और अनुभूतियाँ मिलावट का नमूना बन कर रह गयी हैं। देश के कैनवास पर कहीं असम का नाटक हो रहा तो कहीं पंजाब और खालिस्तान का। लोग हैं कि जन्मभूमि को तार-तार करने पर आमादा हैं। जयचन्द और मानसिंह की सन्तानें पूँजीपति धन-पिशाचों से निजी लाभ की सन्धियाँ आयोजित कर रही हैं। बहादुरशाह जफर ने जिस लाल-किले को 1857 में आजादी के शंखनाद से पवित्र कर दिया था, उस पर कालीमाई की काली छाया दिन-प्रतिदिन गहराती जा रही है। वोटों का समीकरण भ्रूणहत्या कर रहा है और तुम बे-मौसम का राग अलापे जा रहे हो।
मैं कहता हूँ कि इस देश में और इस दौर में तुम जिन्दा रह लो, यही बहुत बड़ी बात है। जमाने का दर्द अपने सर पर रखकर मत चलो मेरे भाई! वर्ना मुझ जैसे-दोस्त-यार ही तुम्हारी इतनी तर्कपूर्ण और ठोस आलोचनाएँ करेंगे कि तुम संघर्ष की जगह आत्महत्या का मरघट ढूँढना ज्यादा पसंद करोगे। तुम्हारे विरुद्ध इतनी ठोस गवाही खड़ी हो जायेगी कि तुम खुद अपनी बे-दाग शख्सियत और अपने निर्दोषपने पर शक करने लगोगे।
शायद भूल गये हो कि जिन ‘महान’ लोगों के खिलाफ और जिन प्रवृत्तियों के खिलाफ तुम पत्रिका या तेवरी को हथियार बनाकर आक्रमण कर रहे हो, वह रक्तबीज की परम्परा में आ गई हैं और उनकी बौद्धिक शक्ति तथा दिमागी चालें तुम्हें बड़ी खूबसूरती के साथ मिटाने में सफल हो जायेंगी और जिनके पक्ष में तुम युद्धक्षेत्र की अग्रपंक्ति के युयुत्सु बन गये हो, उनकी नजर किसी भी समय तुम्हारी पीठ को निशाना बना सकती है।
प्रिय भाई , आम आदमी नामक जन्तु अब आदमी नहीं रह गया है एवं आदमी से ही उसे नफरत हो गई है। यह आम आदमी कहीं तुम जैसे पैरवीकार के खिलाफ गवाही देकर तुम्हें ही अपराधी के कठघरे में लाकर न खड़ा कर दे। भाई, इस देश के आम आदमी की भावुकता और संवेदना काम, क्रोध, मद, लोभ का पूरा शस्त्रागार है। वे बड़ी सफाई से इसका इस्तेमाल करते हैं।
प्रिय भाई, ‘उनके’ पास प्रचार-तन्त्र है, दानकोष है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं , संसदीय सदस्यता है, भाषण हैं, नाटक करने क्षमता है। ‘उनके’ चाँदी के चंद सिक्कों के आगे बड़े-बड़े शेर दुम हिलाने लगते हैं। गार्गी और मैत्रेयी की सन्तानें पैर में पायल की जगह घुँघरू बाँध लेती हैं और प्रखर गर्जनाएँ आकाशवाणी और दूरदर्शन के माइक के सामने ‘उन्हीं’ का गुणानुवाद करने लगती हैं । मेरे बड़े भैया क्या तुम्हारी आँख नहीं खुली?
‘तेवरीपक्ष’ के अंक-दो में क्या तुमने मुख्य पृष्ठ पर ही नहीं पढ़ा-
‘जिसने हिला दिया था दुनिया को एक पल में,
अफसोस क्यों नहीं है वह रूह अब वतन में’।
भाई मेरे, अब अगर किसी बाल्मीकि ने किसी निरीह जीव की हत्या पर आँसू बहाया तो शिकारी का दूसरा तीर बाल्मीकि की आँख को बींध डालेगा। यह बात मैं तुम्हारी कसम खाकर कह सकता हूं। ‘गंगाराम’ और ‘होरी’ की नियति अब नकली मुठभेड़ों के साये तले लिखी जा रही है।
शिवकुमार थदानी, अरुण लहरी और निशान्त से लेकर सुरेश त्रस्त, अनिल कुमार ‘अनल’, योगेन्द्र शर्मा, जगदीश श्रीवास्तव और तुम खुद भी इस अंक के 48 पृष्ठों में कई जगह बखूबी से ‘स्पाॅट लाइट’ डालकर नेपथ्य की अन्दरूनी खबर से वाकिफ करा देते हो। लेकिन डर यही है कि कलम की ईमानदारी बचाने के लिये आप लोग यदि शहीद हो गये तो इस बेरहम जमाने की आँखों से घडि़याली आँसू भी नहीं बह सकेगा और दूसरी ओर ‘वे लोग’ सभी इतना बड़ा उग्रवादी करार कर देंगे कि ‘रख दे कोई जरा-सी, खाके वतन कफन में’ जैसी आरजू पर इतिहास के पन्ने मुखौटों के भीतर ठहाके लगाएँगे और दुनिया फिर अपने राग-रंग में डूब जायेगी।
जन-जागरण की विचार प्रधान त्रेमासिकी की ईमानदार कोशिशों से मुझ जैसा कोई बेईमान नागरिक भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जरा आँख उठाकर अपने उस परिवेश को भी देखने की हिम्मत करो, जिसमें डाॅ. बुद्धसेन जैसे बबूल, गुलमोहर के फूल की तरह सम्मान पी रहे हैं और हम-तुम भाषायी आजादी और अस्मिता की बुनियाद डालने के नाम पर अकेले में मातमपुर्सी करने के लिए मजबूर हो जाया करते हैं। भाई, सच तो यह है कि इस पत्रिका पर तुम्हें बज्मे-सुखन की दाद देने की जरूरत मैं उतनी नहीं महसूस कर रहा हूँ, जितनी कि इस मजमूने-बगावत की लौ को मुसलसल तौर पर जलाते रहने की दिक्कतों से निपटने की दुआ तुम्हें दूँ।
भाई, बात कविता और शायरी की हो रही है तो यहाँ मैं यह कहना भी जरूरी समझ रहा हूँ कि आज के सूरते-हाल में साहित्य नपुंसक चरित्र को जी रहा है। यूरोप में 18 वीं और 19 वीं सदी के साहित्य ने इन्कलाबी चरित्र जिया था और सामाजिक परिवर्तन में उसकी भूमिका एक अहमियत रखती है, लेकिन इस देश में हम-तुम क्यों असफल हो रहे हैं? क्या वजह है कि साहित्य की मूल धार कुन्ठित हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथी और हमारी बिरादरी के लोग ‘उन्हीं’ लोगों की किसी खूबसूरत साजिश के शिकार हो गये हैं?
भाई , व्यवस्था की विषकन्या की पहचान गर नहीं हो सकी तो एक-एक कर के हम सभी खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएँगे। कभी-कभी मैं खुद नहीं समझ पाता कि साहित्य का बुनियादी सरोकार आखिर क्या रह गया है? हम लोग अधिकांशतः प्रशंसा, प्रशस्ति और पुरस्कार पाने के लिये लिख रहे हैं या लेखन को साधन बनाकर ‘उन्हीं’ नराधमों की जमात में सिक्का जमाने के लिए हमारी तर्क-बहस, बौद्धिकता-विचारशीलता तक मानसिक एय्यासी व दिमागी विलासिता की द्योतक बन गई है। सभी लोग या तो अपने आप को छल रहे हैं या अपने बगलवाले या सामनेवाले को छल रहे हैं। ‘उनकी’ विभेदवादी नीति की एक सफलता यह भी है।
भाई, एहसास और जज्बात की सरजमीन पर मैं भी तुम्हारे दर्द को महसूस करते हुए जी रहा हूँ। तुम्हारे दिलो-दिमाग की सात पर्तों की गहराई में छुपी तुम्हारी उस वेदना और पीड़ा को, जो आदमी और आत्मीयता से बावस्ता है, मैं महसूस करता हूँ। तुम मुझे ढाढ़स दो और मैं तुम्हें ढाढ़स दूँ तो शायद हम अंधेरों और कुहासों के पार जा सकें |