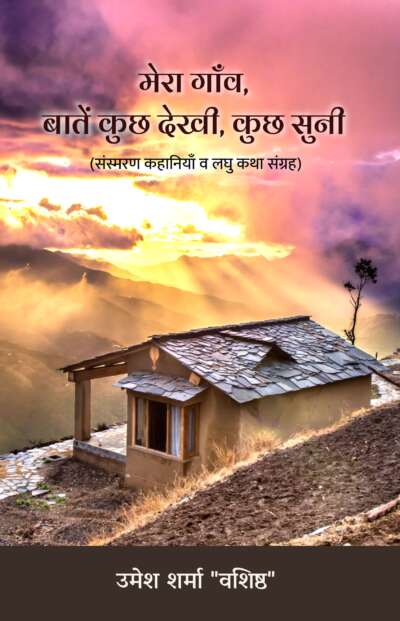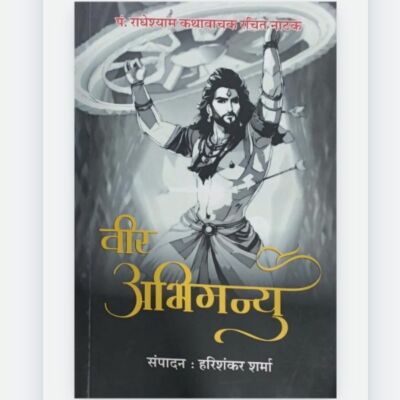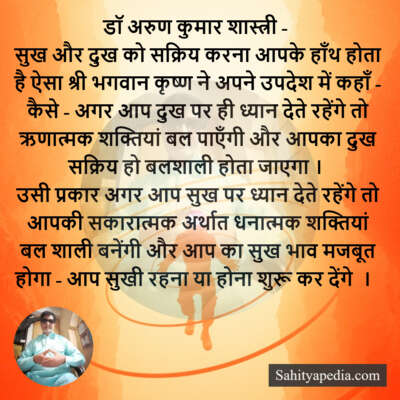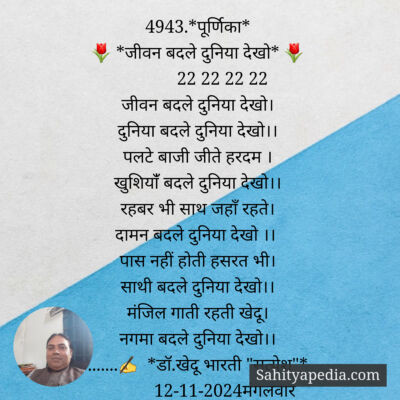शिव कुमारी भाग ४
मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, दादी से मेरी पहली औपचारिक बात चीत मुझे जब चेचक निकली थी तब शुरू हुई थी। उस वक़्त मेरी उम्र तीन चार वर्ष रही होगी।
इसके पहले भी कुछ बातें जरूर हुई होगी,पर वो स्मृति से मिट चुकी है,
अरे हाँ याद आया, दो साल के होने पर भी मैं माँ का दूध पीने की जिद करता था, तो दादी ने मां को नीम के पत्ते घिस कर लगा देने की सलाह भी दी थी, मुँह मे कसैला स्वाद आने पर ही मैंने वो आदत छोड़ी थी।
रात मे दादी के पास सोता था, एक दिन उन्होंने खुसपुसाते हुए पूछा कि दूध पियेगा क्या। इस तरह चोरी छिपे मेरी आदतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और कभी चोरी पकड़े जाने पर फिर मुझे ही दोष भी दे देती, पता नही ये कब बड़ा होगा? माँ फिर कह देती, आप जाने और आपका पोता जाने।
दादी ने ही बताया था, कि मै खुद को बनारस का पंडा भी बताया करता था, थोड़ी बहुत भिक्षा भी ले आता था,
साथ मे किसी महिला को बेटी या बेटा होगा कि नही, ये भविष्यवाणी भी कर देता था।
एक दो बातें सच भी हुई तो दादी ने तो मुझे पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष भी मान लिया था।
कई लोग मेरी ये सेवाएं लेने आते भी थे। फिर माँ के कहने पर ये काम बंद हुआ।
दादी ने भी सोचा होगा कि कहीँ साधु सन्यासी न बन जाये, इसी डर से, उन्होंने फिर लोगों को ये कहना शुरू कर दिया,कि अब उनका पोता ये उल्टे सीधे काम नही करता।
मेरी अदृष्य शक्तियों ने भी फिर मुझसे विदा लेने मे अपनी भलाई समझी। वो बेचारियाँ भी फिर कितने दिन निठल्ली बन कर रोटी तोड़तीं। फिर कहाँ गयी ये नही बताया। एक बार चली गयी तो इधर का रुख नही किया। अगर मुझे हल्की भी भनक होती कि भविष्य मे बाबा बनने के क्या फायदे होने वाले है, तो यकीन मानिए, मैं उन्हें कदापि न जाने देता।
मेरे सारे शरीर मे छोटे छोटे गोल गोल दाने निकले हुए थे, वो मेरे बदन को नीम की पत्तियों से भरी एक छोटी सी शाख़ से सहला रही थी।
माँ मुझे थोड़ी देर पहले नीम की पत्तियां डाल कर गर्म किये हुए पानी से नहला चुकी थी।
अब दादी की बारी थी, वो हर वक़्त मेरे पास बैठी रहती थी, मां और मझली ताईजी को घर के सारे काम होते थे, इसलिए ये जिम्मेदारी दादी की थी कि वो अपने बीमार पोते की देखभाल करें।
दादी मेरे साथ जुटी रहती थी। दादी ने एक लवण भास्कर चूर्ण के खाली छोटे से डब्बे मे, एक, दो, तीन् और पांच पैसे के बहुत सारे पैसे डाल कर मुझे थमा दिए थे। उसको हिलाकर पहली बार पैसे की खनक सुनाई थी।
साथ मे ,एक ताश की पुरानी गड्डी भी थमा दी। पहले दो पत्तों को पकड़ कर त्रिभुज की दो भुजाओं की तरह जोड़ कर खड़ा करके दिखाया, फिर उससे सटे सटे तीन चार और त्रिभुज बना दिये, तीसरी भुजा जमीन बनी बैठी थी।
उन त्रिभुजों के सर पर एक पत्ता रख कर पहले तल्ले की ढलाई की गई। फिर उस पर पत्तों से ठीक उसी प्रकार त्रिभुज लगाए गए। इस तरह कई तल्ले तैयार हुए।
छत पर एक त्रिभुज आखिर मे लगा दिया।
थोड़ी हवा चलने , या खुद का ही हाथ लग जाने,से वो महल ढह जाता, उसे बनाने की दोबारा कोशिश करती।
मुझे भी सिखाती रही,जब मैं भी बना लेता तो बहुत खुश होती।
इसके अलावा उन्होंने एक काम और भी किया, मुझे ताश के इक्के, बादशाह, बेगम और गुलाम को भी दिखा कर पहचान करना भी सीखा दिया था।
मुझे अक्षर ज्ञान से पहले ही, दादी ने ये शिक्षा दे दी थी।
उनकी नजर मे ज्ञान देने का कोई क्रम नही था, जो सामने दिखा वो बता दिया।
अपने इस सबसे छोटे पोते को उन्होंने उसके नाम से कभी नही पुकारा,
उनके लिए मैं प्यार से “म्हारलो या म्हारला”(मेरे वाला,अपना वाला),
हल्के गुस्से या हंसी मे “रामार्यो”(मूर्ख, अनाड़ी, भोला)
और गुस्से मे “बालन जोगो”(जला देने योग्य)
या फिर श्राप मुद्रा मे “ मायतां क भाटा मारणियों”(भविष्य मे माँ बाप को पत्थर मारने वाला), या खोटी घड़ी का(खराब समय/घड़ी मे जन्मा)
और भी विशेषण और उपमाएं थी जो उनके चित्त के अनुसार उनके मुंह से झरती थी।
अपनी छड़ी गुस्से मे जरूर उठाती , पर आज तक मारा नही,
एक दो बार कान जरूर पकड़े होंगे, वो भी हल्के से।
एक दम सुरक्षित छांव की तरह थी, कुछ भी करलो मार नही पड़ने वाली ।
कुछ गलतियां करके भाग कर आने पर छुपा और लेती थी, कोई गुस्से मे ढूंढता आता भी तो कह देती कि यहाँ नहीं है, वो तो उस तरफ भाग कर चला गया है। उनकी शह पाकर एक दम बेफिक्री सी रहती थी।
दादी के इन संबोधनों से उनके मिज़ाज़ का भी पता लग जाता था और ये भी कि अभी कितनी रियायत की गुंजाइश है।
वो मुझे एक दम निरीह सी लगती थी, जो कभी क्षति नही पहुंचा सकती। चाहे कुछ भी कर लो ,
उनकी डांट कान तक पहुंचती ही नही थी और अगर पहुंचती भी, तो कान ही खुद कह देता, अभी थोड़ी देर बड़बड़ करेगी, चिंता की कोई बात नही है।
फिर थोड़ी देर के बाद, वही घोड़े और वही मैदान, होने वाले हैं।
दादी, मारवाड़ी भाषा ही बोलती थी और घर पर भी ये चाहती थी कि सब यही जुबान बोले।
अपनी जुबान मे मिट्टी की खुशबू, मिठास और अपनापन जो वो महसूस करती थी, इसमें सारे घरवाले भी हिस्सेदार हों।
खुद की जड़ों और संस्कृति की विशेषताओं को अक्षुण्ण रखने का ये सतत प्रयास था, कि दूसरी संस्कृतियों के मेलजोल मे रह कर भी अपनी पहचान मिटने न पाए।
उन्हें कभी कोई शर्म महसूस नही हुई कि ये जुबान उन्हें अनपढ़ दिखाने पर तुली हुई है। उन्हें तो गर्व था अपनी विरासत पर।उनके भाव और विचार अपनी देसी जुबान मे पूरे विश्वास से दूसरों के पास जाते थे , एक दम बराबरी के साथ।
बांग्ला उन्होंने टूटी फूटी सीख ली थी और उसका भी अपने हिसाब से मारवाड़ीकरण करने मे एक योद्धा की तरह अपने जीते जी जुटी रहीं। या यों कह लीजिये, वो एक मिश्रित भाषा विकसित करने मे लगी हुई थी, जो भाषाओं की दूरियों को जोड़ने मे एक पुल का काम करेगी, कम से उनके लिए तो दूसरों तक जाने की एक पगडंडी तो उन्होंने बना ही ली थी।
ये पगडंडियां बननी भी जरूरी थी, भीड़ बढ़ेगी तो फिर जल्दबाजी मे रास्ते कैसे बनेंगे?
जैसे सब्जी खरीद कर पैसे देते वक्त वो कुछ यूं कहती थी, “ रामर्या, तेर कन एक रीपिया का खुदरा आछे की?(मूर्ख आदमी, तेरे पास एक रुपये के खुल्ले है क्या?
इसमें सिर्फ “आछे की”(हैं क्या) ही बांग्ला भाषा का था।
बांग्ला शब्द आटे मे नामक की तरह इस्तेमाल करती थी,जुबान की मिठास भी बनी रहे और फीकी भी न लगे।
मजे की बात ये थी, कि सब्जी वाला समझ भी जाता था और माँ जी या ठकुराइन(बांग्ला मे पंडित को ठाकुर कहा जाता है) कह कर सब्जी और खुल्ले पैसे भी दे जाता था।
उसके जाते जाते बड़े प्यार से पूछती, बालनजोगा,फेर कद आशबे?(बेटा, फिर कब आओगे) ,
कम से कम बेचारा सब्जी वाला तो यही समझता था। और अगर सही अर्थ समझ भी जाता, तो भी दादी को कौन सा फर्क पड़ने वाला था,समझे तो समझे अपनी बला से!!!
इस तरह के संवाद किसी को कमतर समझ कर नही,
ये बड़ी उम्र को मिलने वाली छूट थी और इसका लाभ वो घरवालों और बाहरवालों पर समान रूप से प्रयोग मे लाकर खुश होकर देती थी।