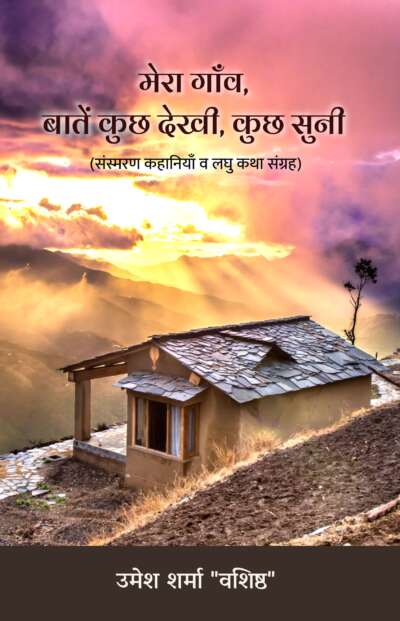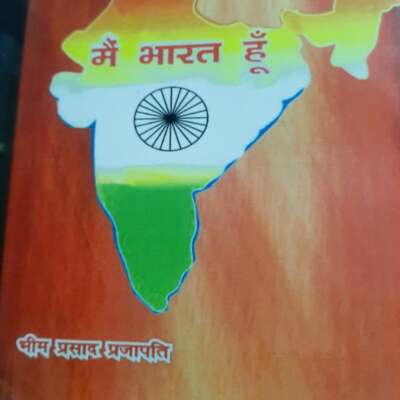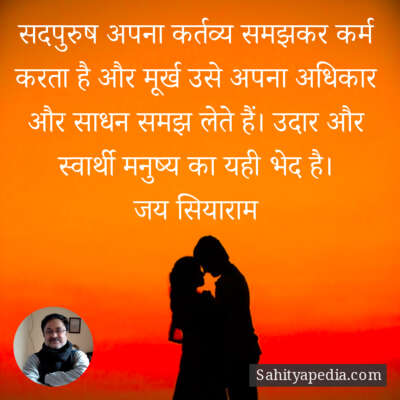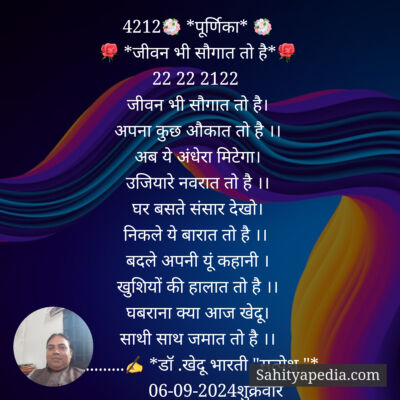शिव कुमारी भाग १४
तीज त्यौहारों में उनकी जान बसती थी। सावन की तीज पर तो उनका गांव में प्रसिद्ध झूला डलता था।
घर के बाहर नीम के पेड़ ने अपनी चौथी भुजा ऊंची फैलाकर, फिर उसमें से निकली एक डाल को थोड़ा सपाट रख छोड़ा था उनके लिए।
दादी झूले की इस डाल को गेहूं चावल के खाली बस्तों से बंधवाती, उसके बाद उसपर मोटी रस्सी से झूला डाला जाता। ताकि उस डाल को ज्यादा कष्ट न हो और उसकी छाल भी घर्षण से ज्यादा प्रभावित न हो।
जब ये हिंडोला डल जाता तो दादी के पिटारे से एक मजबूत पाटकी निकलती जिसे झूले की रस्सियों पर बैठा दिया जाता। दादी उस पर बैठ कर झूला झूलकर इस उत्सव का आगाज करती।
खड़े होकर पेंगे लेने में उनके बूढ़े हो चुके घुटने अब सक्षम नहीं रहे थे। झूले पर बैठते ही, चेहरे की रंगत बदलने लगती थी, कुछ पल के लिए चेहरे की झुर्रियां कसने लगती, चेहरा थोड़ा लाल होता हुआ आनंद से तमतमाने लगता।
एक बार झूला झूलते वक़्त, दादाजी कहीं बाहर से लौटे, दादी ने तुरंत अपने पल्लू को दांतों में फंसा कर चेहरा और सर ढकने की नाकाम कोशिश की। एक षोडसी कन्या सी अपने बन्ने को देखकर लजा गयी थीं।
दादाजी के नीची नजर करते हुए घर में प्रवेश होते ही, दांतों ने पल्लू को छोड़ दिया, पीछे की ओर झुककर पेंगें अब तेज हो चली थीं, उनका आँचल हवा में बेबाकी से लहरा रहा था।
गांव भर की औरतें और युवतियाँ इस झूले का महीने भर आंनद लेती थीं। दो दो की जोड़ी बनाकर खड़े होकर झूला झूलने का वो दृश्य देखते ही बनता था।
दादी उत्साह में उन युवतियों को तेज पेंगे लगाने को कहती और फिर अपनी मस्ती में तीज के गीत गाने लगती थीं।
नीम का पेड़ भी इस उत्तेजना, हँसी व खिलखिलाहट को देख कर झूमने लगता था। उसे भी दादी की तरह हर साल सावन की तीज का इन्तजार रहता था।
वो जब राजस्थान से चली थीं, तो अपने साथ वहाँ की संस्कृति और त्यौहारों की एक प्रतिलिपि भी अपने अंतर्मन में सहेज कर ले आयी थीं। इसमें एक नई प्रविष्टि छठ पूजा की भी हुई, जो माँ और मझली ताईजी अपने साथ दहेज में लायी थीं, दोनों का पीहर बिहार(अब झारखंड) में था।
दादी को तो सिर्फ त्यौहारों से मतलब था, सारे अपने ही तो थे।
गणगौर के गीत रात को घर के आंगन की हवा में तैरने लगते, सुबह सुबह हरी दूब की तलाश और गौरी की पूजा के समय घर की दीवार पर सुहागनें गणगौर माता की वंदना करते हुए मेहंदी की बिंदियां लगाने लगतीं।
दादी पीढ़े पर बैठ कर मुख्य पर्यवेक्षक की भूमिका में रहती कि रीति रिवाजों का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं?
बासेड़ा, बछबारस, नागपंचमी, एकादशी, नवरात्र, होली , दीवाली और न जाने कितने ही पर्व त्योहारों से उन्होंने घर के माहौल को एकरसता से दूर कर रखा था।
दीवाली तो दादी की आमदनी वाला त्योहार था। दादाजी अपने यजमानों के यहां लक्ष्मी पूजा कराते थे। दूसरे दिन पूजा विसर्जन के समय, चढ़ाए हुए फल, मिठाईयां, मेवे और सिक्के दादी के पास आकर जमा होने लगते। दादी बड़े मनोयोग से इन पोटलियों को खोल खोल कर ये चीजें अलग करती । रुपये और सिक्के उनके गल्ले में जाकर बैठ जाते। हम बच्चों को उनकी इस कार्य में सहायता के लिए पारिश्रमिक के रूप में एक आध सिक्के वो हमारी छोटी छोटी हथेलियों पर रख ही देती थीं ।
यजमानों से फिर दक्षिणा उगाहने का काम कई महीनों तक दादी की देख रेख में चलता। सीधे साधे दादाजी संतोषी प्रवृत्ति के थे, यजमानों से संकोच करते थे, पर दादी के दबाव में उन्हें फिर उगाही पर निकलना पड़ता।
यजमान भी दादी से दक्षिणा वसूल न होने तक गालियां ही खाते,
“रामर्या पूजा करा लेसी, दक्षिणा देंण म बावली पेर लेसी, पंडत जी माँगता फ़िरो अब”
(पूजा तो करा लेंगे पर दक्षिणा देने के समय भूलने का नाटक करेंगे, पंडित जी उनसे मांगते फिरें अब)
होली के दिन घर का आंगन शोर शराबे से गुलज़ार हो उठता। दादी आंगन की ओर खुलती छोटी खिड़की से दर्शकों की तरह उत्साह से चींख चींख कर एक दूसरे को रंग लगाने को कहती,
फिर दूसरे दिन आंगन को रंग के धब्बों से पटा देखकर कहती,
“रामर्या सारा आंगणा को सत्यानाश कर दियो”
(कमबख्तों ने सारे आंगन का सत्यानाश कर दिया)
नीम के पेड़ की वो झूले वाली डाल दादी के साथ ही चली गयी।
गांव की गलियों में अब बिजली के खंबे लग रहे थे और रास्ता रोके खड़ी वो डाल उनके आड़े आ रही थी, जब वो कट कर गिरी तो बहुत दिनों तक एक किनारे पर पड़ी रही। उससे जुड़ी छोटी छोटी शाखायें और पत्तियां कई दिनों तक साँसे लेती रहीं।
वैसे भी दादी के बाद उनको भी तो अपने अस्तित्व का कोई औचित्य नज़र नहीं आया होगा।