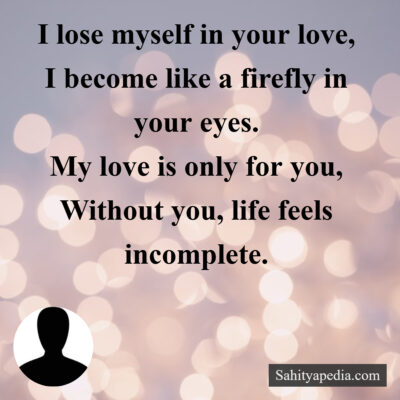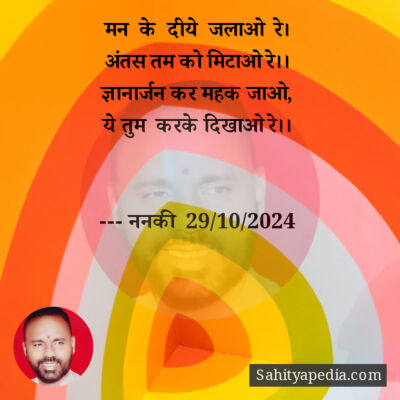“वृद्धाश्रम “
.
अपनों को उन्नत करने की चाह ने,
आज इस मुक़ाम पर ला खड़ा किया,
ना अपने हैं, ना आशियाना,
वृद्धाश्रम ही मेरा ठिकाना,
सोचा था उनके साथ,
मैं भी उडूँगा,
अपने गम भूल,
सुकून के कुछ पल जीयूंगा,
पन, अपने तो आये,
हवा के झोंके की तरह,
समेटा और चल दिए,
एक मौके की तरह,
मैं देखता ही रहा,
एक धोखे की तरह,
जान थी तब तक,
बोझ ढोता रहा,
एक खोते की तरह,
उम्र ढली, आँखें धुँधलाई,
फेंक दिया, पर कटे तोते की तरह,
अपलक, निगाहें ढूँढ़ती रहती हैं,
अपनों के निशाँ,
हर आहट पे जागते हैं,
दिल के अरमां,
शायद आ गया मेरे दिल का मेहरबा,
अँधेरे दिल में आस जगती है,
“शकुन” कसमसाती है,
बुझ जाती है,
बिन तेल दीया,
ज्यों टिमटिमाता है,
जीवन लौ बुझती जाती है,
दीदार को तड़पते – तड़पते,
ऐसा न हो दम ही निकल जाये,
नहीं चाहता रुसवाई का दाग,
उनके माथे पे लग जाये,
मौत कैसे भी नसीब हो लेकिन,
चहनियों की लकड़ी,
तुलसीदल और गंगाजल,
बस, उनके हाथों मिल जाये,
इतनी तमन्ना लिये,
अपलक राह निहारता हूँ,
सांस गले में अटकी है,
बखान उन्हीं के गाता हूँ,
कपाल – क्रिया हो बेटे के हाथों,
न चाहते हुए भी, यही भ्रम पालता हूँ।।
– शकुंतला अग्रवाल, जयपुर