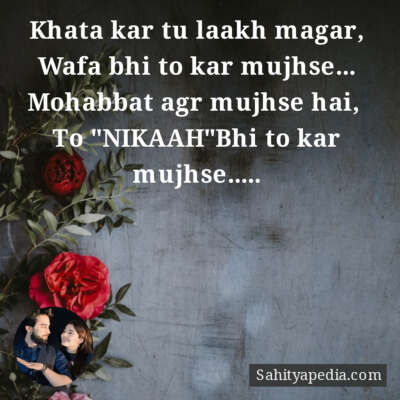मैं
गुस्ताख ‘मैं’ की ज़िद ही क्या?
न मेरी सुने,
ना खुद की;
ना कुछ जाने,
ना कुछ माने,
पहचाने बस उसे जिसे अपना माने।
इस छोटे से ‘मैं’ की दुनिया ही क्या?
छोटा सा ,
प्यारा सा,
बेजुबां है,
दो पसलियों में कैद नन्हा सा जहां है;
बित्ते भर की जमी है,
मुट्ठी भर आसमां है।
इस नाजुक से ‘मैं’ की दास्तां ही क्या?
न कोई दिशा,
न दशा,
कभी औरों को फसाया कभी खुद फसा,
किसी ने मुंह चिढ़ाया,
कोई खूब हंसा;
फिर भी एक जिद कायम : कोई नहीं मुझसा। बित्ते भर जमीन पर सारी दुनिया बसाता है, मुट्ठी भर आसमान में ख्वाबों के पतंग उड़ाता है,
पर शीशे का टुकड़ा दो चोट नहीं सह पाता है;
एक ख़नक के साथ टूट कर चूर-चूर हो जाता है;
बेजुबा अपनी ख़नक में ऐसे बोल कह जाता है,
नेपथ्य में छिपे, अनकहे, गूढ़ राज़ खोल जाता है।
कभी गुस्ताख,
कभी नाजुक,
कभी छोटा,
कभी उलझा ;
यह दिल है, दिमाग है, या है अंतर्मन?
जीवन से ‘मैं’ है या ‘मैं’ से जीवन?
क्या यह ‘मैं’ वही है जिसकी शाश्वत तलाश जारी है,
और आगे भी जारी रहेगी?
इस ‘मैं’ की पहचान ही क्या!!!