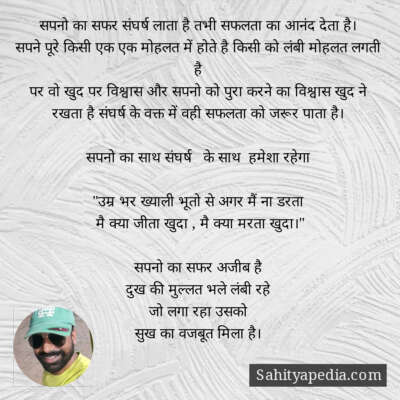मैंने चाहा हर वक्त मन का होना…..मिला नहीं।
मैंने चाहा हर वक्त मन का होना…..मिला नहीं। मन के अनुकूल न हो तो दुख होता है। पर मन के टुकड़े हो जाना दुखों को भी रुलाता है। रोज की एक ही किच-किच सुनते-करते रहने पर मन मुझसे रूठ जाता है। इस रूठे को मनाने मैं अक्सर सफर में निकल जाता हूं।
तो बात ऐसी है की उस शाम भी मैं अपनी चिंताओं को छोड़ लंबे सफर पर निकल गया। धीरे-धीरे चलते हुए शहर की तेज गतिविधियों को देखता हूं। वे गतिविधियां धीरे होना तो चाहती है पर कुछ तो है जो उन्हें उनके अनुकूल होने नहीं देती है। लोग अपने अपने कर्तव्यों को बड़ी सरलता से कर रहे है, कोई किसी को गालियां दे रहा तो कोई उसे सुन रहा तो कोई पलट जवाब दे रहा, कोई बेच रहा तो कोई खरीद रहा तो कोई उधार मांग रहा। सारी चीजें बड़ी सुंदरता से अपनी अपनी जगहों में ठीक बैठते है, मगर इनमे इनका मन का होना नहीं दिखा। खूब ढूंढा, फिर आगे बढ़ा, उस रास्ते जहां से पिछली दफा नहीं गुजरा।
उन रास्तों में इमारते तो थी। शायद घर और मोहल्ले नहीं थे। सूर्य अब अपनी लालिमा समेटते जाने लगा था। विरान सड़कों पर लोगों के न दिखने पर डर सा लगता है, तो मुझे भी लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी उस अंधेरे से आम लोगों वाली टूटी फूटी सड़कों पर आया। काफी दूर चलते चलते पांव में थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी दर्द हो गई। मैंने किस्मत को कोषा और बड़बड़ाने लगा। चढ़ाव वाली सड़क पर तभी एक रिक्शावाला अपनी रिक्शा खींचता हुआ आया। उसने उस टीले पर रिक्शा चढ़ाई जहां से शहर की गति धीमी होती है। उसने बड़े कठिनाई से अपने पैरों को, टीले पर रख धीरे धीरे घसका कर रिक्शा की सीट पर बैठा। रिक्शे पर बैठे यात्री को हैरान देख कर रिक्शेवाले ने बड़े ही उदार भाव में कहा – “ऊ…एक जरा पैरा में दरद हो भे गइल हो”। और रिक्शा ले गया। यह सबकुछ देख मैं भी हैरान खड़ा था। मन के होने न होने से फर्क तो पड़ता है, पर जरूरतें रुकती नहीं है। न ही रुकता है मन।