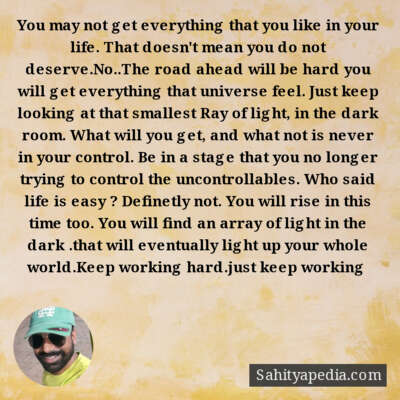मेरा बचपन
फुरसत के पलों में कभी कभी जब अपने जीवन के अतीत की कुछ घटनाओं की याद करता हूँ तो अपने ऊपर हंसी आती है, खुशी भी मिलती है और मन यकायक कहने को मजबूर हो जाता है कि ‘ वो भी क्या दिन थे, काश जिंदगी में भी एक रिवाइंड का बटन होता तो अच्छा रहता तो बचपन लौट के आ जाता।’ पिताजी प्राइमरी में मास्टर थे, कस्बे में ही सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल की चाभी हमारे घर पर ही रहती थी इसलिए चाभी लेकर मैं स्कूल समय से पहले ही पहुंच जाता था। स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए बच्चों में होड़ सी लगी रहती थी। आजकल तो पढ़ने वाले बच्चो से स्कूल में झाड़ू लगवाना अपराध की श्रेणी में आता है। मोबाइल में फोटो खींचकर अधिकारियों से शिकायत कर या अखबार में निकलवाकर लोग मास्टर को दफा 302 का सा मुजरिम समझने लगे हैं। खड़िया को बारीक पीस पीस कर इंजेक्शन की खाली शीशी में भरकर सैंटा की खत बनी कलम पट्टी पर अध्यापक द्वारा बनाए गए किटकिंनो पर फिराना बहुत सुखदायक लगता था। पट्टी की बड़ी सेवा होती थी उस समय। तवे के नीचे की कालिख को छोटे से कपड़े के टुकड़े से पोता जाता था। सूखने के बाद हरी घास की पत्तियां ढूंढ कर लाई जातीं, उनको पट्टी पर मसलकर लगाते फिर एक काँच की शीशी से घोट घोट कर चमचमा देते थे। शीशी में घुली हुई गीली खड़िया में एक धागा भिगो कर पट्टी पर लाइन बनाई जातीं। एक ओर ओलम के लिए सीधी लाइने और दूसरी तरफ गिनती के लिए चौकोर लाइनें। पट्टी की मुठिया पर एक ओर ॐ लिखा जाता, दूसरी ओर दो लाइन खींचकर तारीख लिखी जाती। स्कूल की प्रथम पाली में ओलम और इंटरवेल के बाद गिनती का काम, और छुट्टी से पहले ओलम और गिनती मौखिक बोले जाते, इतनी सा बोझ था पढ़ाई का उस समय। रूसो का प्रकृतिवादी दर्शन उस समय की शिक्षा व्यवस्था में परिलक्षित होता था। आजकल तो विद्यालयों को प्रयोगशाला बना कर रख दिया गया है। रोज नए प्रयोग किए जा रहे हैं मासूम बच्चों के साथ।
ग्रामीण जीवन बहुत कठिन भी होता है, बहुत सरल भी। हमारा कस्बा कहने भर के लिए कस्बा था, वहां का रहन सहन रीति रिवाज सब ठेठ देहाती था। संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। दादा जी चार भाई थे दूसरे नंबर के दादा जी ससुराल में खेती बाड़ी के लिए जमीन पा गए थे इसलिए वहीं के बस गए थे। बाकी तीनों दादा जी यहीं संयुक्त रूप से रहते थे। मैंने अपने दादा जी को यानि अपने पिताजी के पिताजी को नहीं देखा, वे मेरे जन्म से पूर्व ही स्वर्ग सिधार चुके थे। दादियां चारों देखीं थीं मैंने। बड़ा तालमेल था परिवार में। सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। उम्र में छोटे लोग बड़ों की बात मानते थे। चारों मकान आमने सामने और बीच में चारों घरों का संयुक्त बड़ा सा आंगन। और आंगन के एक तरफ विशाल नीम का पेड़ जिस पर तोता, कौआ, कबूतर, गौरैया, तीतर, उल्लू चील, बाज आदि बीसियों प्रजाति के पक्षियों के अलावा मधुमक्खियों के तीन बड़े छत्ते और बहुत सारी चुलबुली गिलहरियां रहतीं थीं। पेड़ के पास ही भैंस और उसके बच्चे भी वहीं बांधे जाते। बाहर की ओर यानि घर के मुख्य प्रवेश द्वार के एक ओर विशाल झोपड़ी जिसमें 8 -10 चारपाई पड़ी रहतीं। आने जाने वाले रिश्तेदार और बाहर के उठने बैठने वाले लोग यहां आराम करते। झोपड़ी के सामने बहुत सारा खेल का मैदान जहां सारे मुहल्ले के बच्चे आकर खेलते थे। पूरे दिन चहल पहल सी रहती थी। मैदान के एक ओर बहुत गहरा कुआं था जिससे सब लोग पीने योग्य पानी निकालकर बाल्टियों, गगरियों और कलशों में भरकर ले जाते। गाय , भैंस को भी यहीं लाकर पानी पिलाया जाता। पुरुष और बच्चे कुएं के पास ही एक समतल पड़े पत्थर पर बैठकर नहाते। गर्मियों के दिनों में पक्षी, मधुमक्खियां और बर्र यहां अपनी प्यास बुझाने आते। गांव में बच्चे अपना खेल कम संसाधनों में ही खोज लेते हैं। भैंस की पूंछ से बाल उखाड़कर गेंहूं की सूखी पोली डाली तोड़कर उसमें डालते और चुपके से कुएं पर पानी पी रही बर्र को बाल में फंसा लेते, उसका डंक तोडते और हवा में उड़ाकर छोड देते।
गरीब को तीनों ही मौसम संघर्ष के साथ गुजारने पड़ते हैं, गर्मी आराम से कट जाती है क्योंकि बिना कपड़ों के काम चल जाता है। जाड़ा सबसे कष्टदायक होता है क्योंकि गरीब के पास कपड़े नहीं होते, और बारिश में सिर पर छत का अभाव रहता है। पैदा होने के बाद जब होश संभाला तो जहां तक मैंने गणित लगाया हम गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। एक कच्ची मिट्टी का बना कमरा जिसकी छत भी मिट्टी की बनी हुई थी। छत में हर एक फुट पर लकड़ी की मोटी सोटें पड़ी थीं, उनके ऊपर पतेल से निकले सैंटो के बंडल सटा सटा के लगाकर चिकनी मिट्टी डाली गई थी। एक छोटा सा चौखट और दरवाजा था, फर्श भी कच्चा ही था। लिपाई के दौरान उंगलियों के निशान घर-आंगन को सुन्दर बना देते थे। गर्मी के मौसम में कच्चे मकान गर्म नहीं हो पाते इसलिए गर्मी बहुत अच्छी बीत जातीं थीं। जाड़े में गरम कपड़ों के नाम पर एक मात्र स्वेटर था, हालांकि बचपन में खेल कूद ही इतना हो जाता था जिसके कारण ठण्ड दूर दूर तक पास नहीं फटकती थी। शाम को दादा जी बाजरा के भुल्ले में मक्का के सूखे पेड़ (मकोबर) रख कर अघियाना (अलाव) जलाते तो सब बच्चे हाथ सेंकने के लिए वहीं इकट्ठा हो जाते। उस समय गेहूँ की मढ़ाई के लिए थ्रेसर न के बराबर थे, इसलिए किसान बैलों की मदद से दाँय चलाकर या घर पर ही बालें काट कर डंडे से पीटकर गेंहूँ निकालते थे। बाकी बचे गेहूं के पेड़ के हिस्से से महिलाएं घरों में जमीन पर बैठने के लिए आसन एवं सामान रखने की टोकरी आदि बना लेती थीं। अघियाने पर बच्चे दादाजी की नकल करने के लिए उसी गेंहूँ के पेड़(नरई) को आग से जलाकर बीड़ी की तरह पीते और मुंह में धुआं भर जाने पर छोड़ते। सरसों की कटाई के बाद बंडल(बोझ) बनाकर खुले स्थान पर ढेर लगा दिए जाते , बच्चों की तो लॉटरी लग जाती थी मानो। बच्चे उनमें खूब लुका छुपी का खेल खेलते।
गर्मी के दिनों में सभी की चारपाई आंगन में बिछती। मां मिट्टी के बने चूल्हे पर गरमागरम रोटियां बनाती हम लोग बड़े चाव से खाते। मां के हाथ की बनी चूल्हे की रोटियों के आगे दुनियां का हर लजीज व्यंजन फीका था। रात को सब बच्चे दादी से कहानी सुनने की जिद करते और सुनते सुनते एक एक कर सोते जाते। कभी कभी तो सब सो जाते और दादी कहानी कहती रहतीं।
हमारे घर में एक पुरानी साइकिल थी, पिताजी घर से बाहर साइकिल से ही आते जाते थे। मेरी उम्र 7 या 8 साल की रही होगी, मेरा मन भी साइकिल की सवारी का बहुत होता था। लेकिन पिताजी के डर से उसको छूने में भी संकोच रहता था। जब कभी पिताजी घर पर नहीं होते तब स्टैंड पर खड़ी साइकिल के पेडल को घुमाकर पहिये की रफ्तार देखने में बड़ा मजा आता था। पुराने टायर को सड़क पर लकड़ी से चलाना बड़ा सौभाग्य लगता था। साथ के लड़कों के संग पहिए की रेस की हार जीत देखने लायक होती थी। समय के साथ खेल बदल जाते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जीवन में जब आदमी के पास समय ही नहीं होता खेल के लिए। उस समय खेल में इतने मगन रहते थे खाने की परवाह ही नहीं रहती थी।
होली का त्यौहार आने वाला था। हमारे कस्बे में ज्यादातर मकान कच्चे थे इसलिए लोग उनकी लिपाई पुताई का इंतज़ाम करने में लगे थे। हमारा घर भी कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। एक छप्पर और बाहर कच्चा ही आंगन था। छुट्टी का दिन था तो मां के साथ मैं भी पीला मिट्टी लेने दूर चल दिया, स्कूल वाले थैले को खाली करके। थोड़ी सी मिट्टी लाते लाते हालत खराब हो गई, उस दिन मां की मेहनत का अहसास हुआ। माँ सुबह से उठकर देर रात सोने तक एक पांव पर दौड़ दौड़ कर काम में लगी रहती है हमारी लिए। हमारे घर से सड़क थोड़ी ही दूर है। बहुत व्यस्त सड़क है लेकिन। घर से उस सड़क तक बहुत तीब्र ढाल है, साइकिल बिना पैडल मारे ही सड़क तक पहुंच जाती है।
उस दिन पिताजी घर पर नहीं थे। साइकिल घर पर ही थी। दिमाग मे खुराफात सूझी चुपचाप साइकिल उठाई और निकल दिए साइकिल की सवारी करने। पहले तो पैदल ही इधर उधर घुमा के हाथ फरहरे किए। फिर यकायक एक चबूतरे का सहारा लेकर गद्दी पर बैठ गए। पैर पैडल तक आंशिक रूप से पहुंच रहे थे। ब्रेक भी ज्यादा अच्छी तरह से नहीं लग रहे थे। साइकिल की गद्दी को मैं राजगद्दी से कम नहीं समझ रहा था उस समय। राजसी अन्दाज में साइकिल को थोड़ा सा बल दिया तो लगी ढलकने। मुख्य सड़क की ओर हैंडिल घुमाते ही ढलान के कारण रफ्तार बढ़ गई। मैं साइकिल पर बैठा जरूर था किन्तु साइकिल भगवान के भरोसे थी। सड़क पर बड़े बड़े वाहन फर्राटा भर रहे थे। सामने से तेज गति से आता हुआ ट्रक देखकर मेरे हाथ पांव ही फूल गए। उस दिन मौत से आमना सामना हुआ समझो। जिंदगी और मौत के बीच कुछ ही सैकंडो का अंतर होता है ये सच्चाई उस दिन मैंने जानी। अगर अंतिम क्षणों में आंख बंद कर हैंडिल मैंने न घुमाया होता तो घर में मातम मन रहा होता। मौत के उस साक्षात्कार ने जिंदगी के कई पाठ पढ़ा दिए थे।
नरेन्द्र ‘मगन’
कासगंज (उ0प्र0), 207123
मोबाइल +919411999468