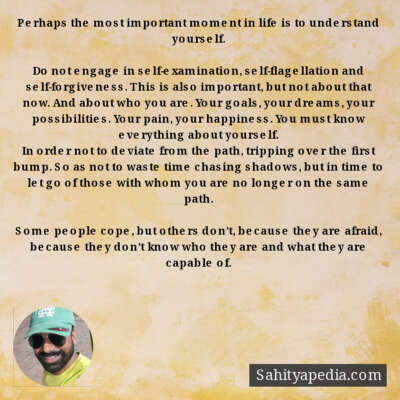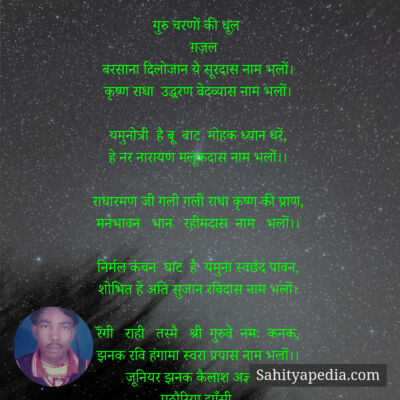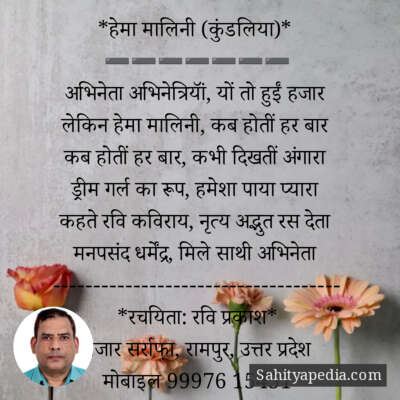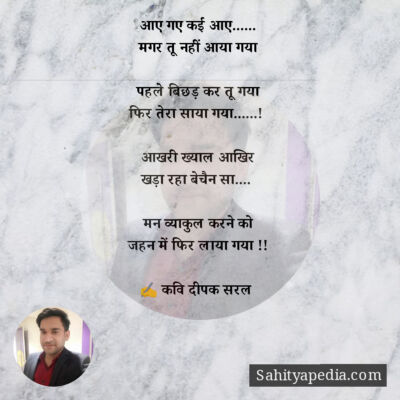मृग-तृष्णा
कभी थिर सी कभी अधीर सी
कभी बैचेन सी कभी निश्चिन्त सी
मन दौड़ता रहा है
पाने की इच्छा स्वर्ण-मृग की
तोड़ता है मर्यादा की वर्जनाएं
लांघता है संस्कार की मर्यादाएं
तोड़-लांघ अपनी सीमाएं
मन दौड़ता रहता है
पाने को स्वर्ण-मृग
वहशी संसार की दौड़ में
हवस तन-धन की होड़ में
मन दौड़ता रहता है
हवस-वासना की छोह
संस्कार को कर विछोह
मन दौड़ता रहता है
पाने की इच्छा स्वर्ण मृग की
अंधी दौड़ में दौड़ता
अंत मे थक जाता
और मन क्या पाता
पाता कुछ भी नही
मिलता कुछ नही,
जीवन खो जाता है
लगाते लगाते दौड़,
पाने स्वर्ण-मृग को
सब कुछ पाने के तिलिस्म में
तोड़ वर्जनाएं लांघ सीमाएं
मन दौड़ता रहता है
पाता है जो वो,
“मरीचिका” है मृग-तृष्णा है।