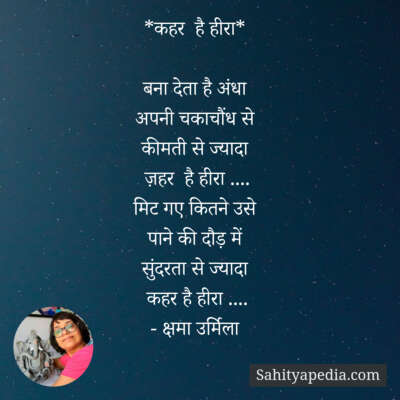मुजरिम तुम…..
मुजरिम तुम…..
मुजरिम हो मेरे मन की अदालत में…
ऐसा क्यों है कि सम्पूर्ण होकर भी अपूर्ण हूँ मैं,
और तुम अपूर्ण होकर भी. ..हो गये सम्पूर्ण !
क्यों ये नियति है ..नारी की इसलिये ??
क्यों वो सहे पीड़ा बार – बार इस जीवन की ??
जब जीवन में आती कोई कठिन सी बेला…
तुम खामोश या तटस्थ रहते हो हर बार ..
सब कुछ छोड़ उदासीन हो तथागत सा बन जाते हो ….
तुम वैज्ञानिक बन नूतन खोज किया करते हो…
भ्रम का ही सही धरा –गगन का मिलन करा सकते हो..
चाँद –तारों की गणना का ..गुणन तुम कर सकते हो..
पर क्या मेरे मन की सालों तपती …
रेत पर सतरंगी ..फूल खिला सकते हो??
नित – नूतन वैज्ञानिक कृति पर
तुम्हारा अहं विकसित हो सकता है..
और मेरा अस्तित्व सिरे से ..नकार सकता है..
किंतु स्मरण रहे …मैं जरूरी हूँ…
तुम्हारी बड़ी से बड़ी ये सफलताएँ..
मेरे समकक्ष खड़ी नहीं हो सकती ..
कि तुम्हारी कोई भी कल्पना..
मेरे सत्य से बड़ी नहीं हो सकती..
मैंने तुम्हारी सृष्टि को नित दृष्टि दी..
तुम्हारी सोच को मैने ही पंख लगाए…
मुझे विष भी स्वीकार्य है और समस्त पीड़ाएँ भी..
क्योंकि मैं धरती सी हूँ .सब कुछ सह सकती हूँ..
तुम सुनो न सुनो पर एक बात .कहना चाहती हूँ केवल तुमसे …
मनुष्य देवता बन जाता है ..निष्काम चाहत में..
तुम स्वीकार करो न करो पर….
तुम मुजरिम हो मेरे मन की अदालत में….
…..अमृता निधि



















![तेवरी इसलिए तेवरी है [आलेख ] +रमेशराज](https://cdn.sahityapedia.com/images/post/8d7cfaf4e3b7754bc547efb92e0fe63c_5f95a019bf3daf8d2f0d414c4ae1b6f5_400.jpg)