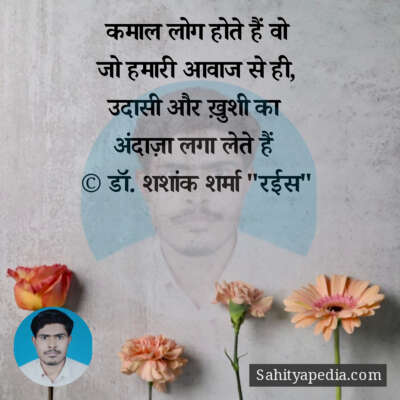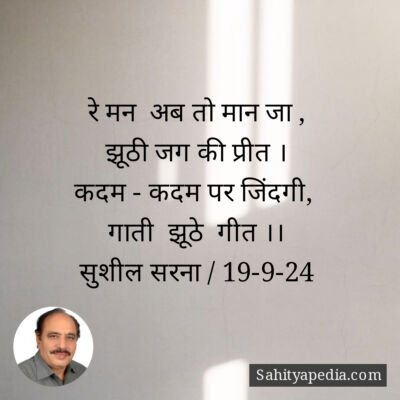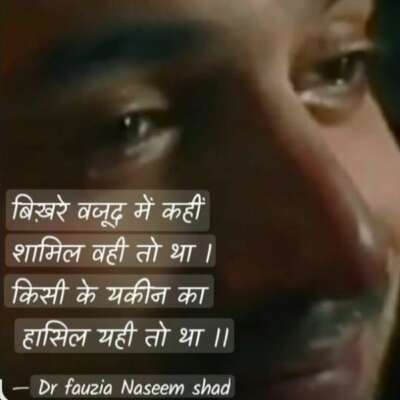मास्टर जी: एक अनकही प्रेमकथा (प्रतिनिधि कहानी)

मास्टर जी: एक अनकही प्रेमकथा (प्रतिनिधि कहानी)
कथाकार : महावीर उत्तरांचली
“मोहन जी,” ठीक मेरे पीछे से पुकारे गए किसी स्त्री स्वर ने मेरी तंद्रा भंग की। मैं पनवाड़ी की दुकान पर खड़ा सिगरेट सुलगाने मे व्यस्त था। मैं हैरान था! क्योंकि यहाँ नैनीडांडा (उत्तरांचल) मे, मेरे इस नाम से कोई परिचित नही था। गढ़वाल के इस ख़ूबसूरत पहाड़ी इलाके में आम ग्रामीणों के बीच मैं प्राय: स्कूली सम्बोधन से ही जाना जाता था। अर्थात् अधिकांश लाग मुझे ‘मास्टर जी’ कहकर ही पुकारते थे। या फिर मैं अपने स्टाफ साथियों के बीच ‘यादव जी’ के नाम से ही विख्यात था। कुल मिलाके निष्कर्ष ये कि अपना वास्तविक नाम ‘मोहन’ मैं आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व देहरादून में ही छोड़ आया था। जहाँ तकरीबन जानने वाले मुझे ‘मोहन’ कहकर ही संबोधित करते थे।
मैंने जिज्ञासावश घुमाकर पीछे देखा तो रुकी हुई बस में बैठी एक युवती का हाथ मेरी और हिलता जान पड़ा। अरे ये सचमुच गीता ही है या मेरा भ्रम? भला गीता यहाँ कैसे हो सकती है? मेरा भ्रम ही है शायद! फिर भी मैंने चश्मा ठीक करते हुए, सिगरेट का एक ज़ोरदार कश लगाया। धुआँ आँखों के आस-पास वातावरण में तैरने लगा।
“मोहन जी” इस बीच उसने मुझे पुनः पुकारा।
अब तो संदेह की कोई गुंजाइश ही न रही। यक़ीन पुख़्ता हो गया कि ये मेरा भ्रम नही है वाकई बस में गीता ही बैठी है। गीता, यानि गीता नेगी। मेरे देहरादून प्रवास की साक्षी। यानि देहरादून में मेरी मकान मालकिन सरोजनी देवी की सबसे छोटी बेटी। अन्य दो लड़कियों मे सबसे बड़ी मालती और मंझली ममता थी। दोनों का ही विवाह हो चुका था बल्कि ममता का विवाह तो मेरे ही सामने हुआ था। उन दिनों गीता बी.ए. में पढ़ रही थी और मैं उसे ट्यूशन पढाता था। उन दिनों उसकी इच्छा थी कि बी.ए. करने के बाद बी.एड. करके, वह मेरी तरह किसी सरकारी स्कूल मे टीचर बन जाए। उन दिनों मैं उनके परिवार का अटूट हिस्सा बन चुका था। उनके साथ ही उठना-बैठना, खाना-पीना हुआ करता था। मकान मालकिन सरोजनी देवी मुझे अपने बेटे जैसा ही मानती थी; क्योंकि उनके कोई बेटा न था। पति के निधन के बाद तीनों बेटियां ही उनके जीने का सहारा थीं। मैं भी सरोजनी देवी को मकान मालकिन से ज़्यादा माँ का दर्ज़ा देता था। मेरे आ जाने के बाद वह निश्चिंत होकर नौकरी कर रही थीं। यह नौकरी उन्हें अपने पति के स्थान पर मिली थी, उनके निधन के उपरान्त। उनकी ग़ैर हाज़िरी में घर की देखभाल का ज़िम्मा मेरे ऊपर था। घर में सबसे छोटी होने की वजह से, मैं गीता को ‘छुटकी’ कहता था, तो वो मुझे ‘मोनू’ कहकर चिढ़ाती थी। हम दोनों में एक अजीब-सा रिश्ता क़ायम हो गया था। हंसी-मज़ाक़, छेड़छाड़-गपशप, बात-बिन-बात एक-दूसरे को चिढ़ाना। चिढ़ना। हम दोनों की उम्र मे बारह-तेरह साल का फ़र्क़ था, मगर हमारी दोस्ती ऐसी हो गई थी कि ये फर्क़ न तो कभी मुझे महसूस हुआ और न ही छुटकी को कभी लगा कि वह उम्र मे मुझसे इतनी छोटी है। कभी-कभी हमारे बीच में बचकानी बहस भी हो जाती थी और हम दो-चार दिन तक बातचीत भी न करते थे। तब सरोजनी देवी ही मध्यस्ता करके, हमारे मध्य संधि करवाती थी। एक अजीब-सी कशिश, एक अजीब-सा आकर्षण था हम दोनों अनोखे दोस्तों के मध्य उन दिनों। जिसको कोई रिश्ता या नाम नही दिया जा सकता शायद! यदि कहीं महसूस किया जा सकता है तो इस रूप में कि, वह आदर्श दोस्ती का रिश्ता था, जो विषय-वासना से दूर था।
सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। बस उन दिनों स्कूल में एक अप्रिय घटना घट गई थी। मेरी एक बेबाक टिप्पणी पर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य मिस्टर अनिल मिश्रा मुझसे ख़फ़ा हो गए थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि बात-बिन-बात, मौक़े-बे-मौक़े, वो मुझे नीचा दिखाने लगे। मेरा मन स्कूल से उचाट हो गया था। एक अजीब-सी वितृष्णा से मेरा हृदय भर उठा था। देहरादून के माहौल मे अब मेरा दम घुटने लगा था। अगर मेरा तबादला न होता तो दो सूरतें मेरे पास थी और मैं उनमे से कोई एक सूरत इख़्तियार कर लेता। एक—या तो मैं इस्तीफ़ा दे देता; दो—या फिर मैं उस प्रिंसिपल के बच्चे का गला घोट देता। उन दिनों मुझे हर उस व्यक्ति से नफ़रत हो गई थी, जिसका नाम अनिल था। मुझे हर अनिल मे उस ज़ालिम और कमीने मिश्रा का प्रतिबिंब नज़र आता था, जो दुर्भाग्य से हमारा बॉस (प्रिंसिपल) था।
मेरे तबादले में, मेरी सबसे ज़्यादा सहायता, मेरे स्टॉफ के एक अन्य अध्यापक महिपाल रावत ने की थी। जो नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल) के मूल निवासी थे, मगर पिछले बीस वर्षों से देहरादून में ही रह रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि वर्तमान शिक्षा मंत्री के पी.ए. उनके खासम-ख़ास रिश्तेदार हैं और यदि मैं चाहूँ तो मेरा तबादला वह नैनीडांडा के स्कूल मे करा सकते हैं। दो करणों से मैंने तत्काल हामी भर दी। एक—मैं अनिल मिश्रा का चेहरा नही देखना चाहता था। दूसरे—आवास की कोई समस्या नहीं थी। नैनीडांडा मे रावत जी का पुश्तैनी घर खाली पड़ा था। चार वर्ष पूर्व उनकी माताजी के निधन के उपरांत से ही उनके गांव वाले घर मे ताला लगा हुआ था।
ये सब घटनाएँ क़रीब तीन वर्ष पूर्व की हैं अर्थात वर्तमान में अब भूत की इन घटनाओं की कोई प्रासंगिकता और सार्थकता नही रह गई थी। रह गई थी तो सिर्फ़ कुछ खट्टी-मीठी यादें। उन मीठी स्मृतियों में कुछ गीता और उसके परिवार से जुड़ी थीं; तो खट्टी अनिल मिश्रा और उसके देहरादून वाले स्कूल से जुड़ी थीं। उन दिनों गीता बच्ची-सी लगती थी, मगर बस में से उसका झांकता चेहरा देखकर, आज लगा कि वह पहले से कुछ मैच्योर (परिपक्व) हो गई है। मैं इसी उधेड़बुन मे खोया हुआ था कि यकायक गीता मेरे सामने अपना सूटकेस उठाए आ खडी हुई। उसके कंधे पर एक बैग भी झूल रहा था।
“हैलो! कहां खो गए? क्या पहचाना नही?” सूटकेस नीचे रखते हुए वह बोली।
“क्या बात कर रही हो छुटकी! भला मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं?” कहकर मैं मुस्कुरा दिया, “मगर तुम यहाँ कैसे?”
“गाँव में चाचा के लड़के की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। मैं तो हफ़्तेभर से गढ़वाल में ही थी। आज ही वापिस देहरादून जा रही हूँ।” कहकर उसने कंधे पर लटका बैग भी सूटकेस के ऊपर रख दिया, “कि अचानक बस खराब हो गई…., दूसरी बस शायद दो घंटे बाद आएगी?”
“आज ही चली जाओगी, ऐसा कैसे हो सकता है?” मैंने बिगड़ते हुए कहा, “और हफ़्तेभर से तुम यहाँ थी, एक बार भी मुझसे मिलने का प्रयास नही किया!”
“समय ही नहीं मिल पाया, भाई की शादी में ही व्यस्त थी,” गीता ने सफ़ाई दी, “फिर नैनीडांडा में किस तरफ रहते हो, इसका भी ठीक से कोई अंदाज़ा नही था मुझे?”
“नैनीडांडा के स्कूल से तो पता कर सकती थी!” मैंने नाराज़गी व्यक्त की, “वो पीछे देखो, स्कूल का बोर्ड चमक रहा है।”
“ओह! आय एम सॉरी।”
“सॉरी से काम नही चलेगा, आज तुम नैनीडांडा में ही रहोगी।”
“मगर?”
“मगर-वगर कुछ नहीं।” कहकर मैंने बैग और सूटकेस उठा लिए।
“आप बेकार ही तकलीफ़ कर रहे हैं।”
“मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, छुटकी जी।” मैंने हँसते हुए कहा, “अच्छा, कभी मैं देहरादून आऊँगा और गेट से ही हाल-चाल पूछकर विदा हो जाऊँगा, तो कैसा लगेगा तुम्हें?”
“ज़ाहिर है, बहुत बुरा लगेगा।”
“तुम्हारी बेरूख़ी पर, ठीक ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे।”
“ठीक है हुज़ूर, तो आज हम आपकी मेहमान-नवाज़ी कबूल करते हैं।” गीता ने बिंदास अंदाज़ में कहा और हंस पड़ी।
“ये हुई न बात,” प्रत्युत्तर में मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “जहां मैं रहता हूँ, चार-पांच कमरों का मकान है, पूरा खाली। तुम्हारे लिए ऊपर का कमरा खुलवा दूंगा।”
“किराया क्या लोगे?” गीता ने मज़ाक़ मे कहा।
“अकेले खाते-खाते बोरियत हो गई है, बस मेरे साथ खाना-पीना होगा।”
“अच्छा जी!”
“फिर पिछले तीन सालों से तुम्हारे हाथ की जली रोटियाँ भी तो नहीं खाईं हैं।” मेरी इस टिप्पणी पर हम दोनों की हंसी छूट पड़ी और स्मृति मे साथ गुज़ारे गए पुराने दिन हरे हो गए।
“मेहमान से रोटी पकवाओगे!”
“मेहमान अगर बेईमान हो, तो रोटी पकवाने मे क्या हर्ज़ है?”
“अच्छा जी, क्या बेईमानी की हमने?”
“भूल गई, तुम मुझे क्या कहकर चिढ़ती थी, छुटकी?”
“याद है मुझे।”
“तो फिर मोनू कहकर क्यों नहीं चिढ़ाती मुझे?”
“तब मैं छोटी थी।”
“ओह! मैं तो भूल ही गया, इन तीन वर्षों में तुम काफी बड़ी हो गई हो! अब तो तुम्हें बड़की कहकर पुकारना पड़ेगा।” मैंने हँसते हुए कहा, “कैसा लगेगा, जब मैं कहूंगा तुम्हें, नमस्ते बड़की जी, या फिर गुड मॉर्निंग गीता जी, हा … हा … हा … ”
“अच्छा मोनू जी।” गीता भी खिलखिलाकर हंसने लगी।
“हा, अब आई न लाइन पर।”
“एक बात तो है।”
“क्या?”
“तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। अब भी वैसे ही हो छोटे बच्चे की तरह, जैसे देहरादून में थे।”
“सच!” मैंने एक अजीब-सी खुशी महसूस करते हुए कहा। एक टीस-सी उभर आई, “कहाँ खो गए वो दिन गीता …?”
इस बीच एक मौन-सा उभर आया हम दोनों के मध्य।
“गीता … ओह सॉरी छुटकी जी।” मौन को भंग करते हुए मैंने पुनः कहा, “ज़रा एक मिनट रुको, सामने दुकानदार को सामान की लिस्ट दे दूँ; ताकि उसका लड़का समय पर सामान घर पहुंचा दे।”
“समनया, मास्टर जी (नमस्कार, मास्टर जी)।”
“समनया … समनया और कन छई गोविंदू, त्यरी दुकनदारी ठिक चलणी च (नमस्ते … नमस्ते और कैसा है गोविन्द, तेरी दुकानदारी ठीक चल रही है)।” मैने स्थानीय बोलचाल की भाषा (गढ़वाली) मे कहा।
“सब देवी भगवतीक कृपा च (सब देवी भगवती की कृपा है)।”
“अच्छा गोविंद, इन कैरी कि ये लिस्ट मा जदगा आयटम लिख्यां छन, तू अपुर बेटा, देबूक हती जल्द-से-जल्द म्यार घोरम भिज्य दे (अच्छा गोविन्द, ऐसा करना कि इस लिस्ट में जितनी भी आइटम लिखी हैं, तू अपने बेटे, देबू के हाथ जल्द-से-जल्द मेरे घर भिजवा देना)।” मेरे मुंह से प्योर (शुद्ध) गढ़वाली सुनकर गीता हतप्रभ-सी खड़ी मुझे देखती रह गई। शायद वह यह विश्वास कर पाने को तैयार न थी कि मैं इतनी अच्छी गढ़वाली कैसे बोल सकता हूँ?
“मास्टर जी, देबू तो ब्याल बटी, भर्ती बान लेन्सीडॉन ग्यूं च। ख़ैर आज दिनक गाड़ी म ऐ जाल …. और कुई सेवा (मास्टरजी, देबू तो कल ही, भर्ती के इरादे से लेन्सीडॉन गया हुआ है। ख़ैर आज दिन की गाड़ी से वापिस आ जाएगा … और कोई सेवा)?” दुकानदार ने हाथ जोड़कर औपचारिकतावश पूछा।
“न बस इदगा (इतना) ही कैर (कर) दे।” मैंने आभार व्यक्त किया।
“या दगड म को च (ये साथ में कौन है)?” दुकानदार का इशारा गीता की तरफ़ था।
“हमारी रिश्तेदार है।” मैंने अटैची दूसरे हाथ में पकड़ते हुए कहा।
“अच्छा मास्टर जी।” गोविन्द ने सर हिलाया।
“चलो गीता।” कहकर हमने गांव की राह पकड़ी। हम पक्की सड़क से कच्ची पगडंडी पर उतर आए।
“क्या बात है, आप तो गढ़वाल मे रहकर, पूरे गढ़वाली हो गए हैं।” गीता ने संभलकर कदम रखते हुए कहा, क्योंकि रास्ते की ढलान नीचे को थी।
“आधा गढ़वाली तो मैं, तुम्हारे घर मे रहकर ही बन गया था। शेष स्थानीय लोगों से गढ़वाली मे निरन्तर बातचीत करते रहने से गढ़वाली सीखने मे काफ़ी सहायता मिली। फिर कुछेक पत्र-पत्रिकाओं और गढ़वाली साहित्य को पढ़ने से भी भाषा मे निखार आया। सचमुच गढ़वाली जान लेने के बाद अहसास हुआ कि हिंदी का सबसे खूबसूरत पहाड़ी रूप है यह।” मैने मुक्तकंठ से गढ़वाली बोली की प्रशंसा की, “बड़ी मीठी बोली है गढ़वाली।”
“ये गाँव कितनी दूर है अभी?” गीता ने जम्हाई लेते हुए पूछा।
“यही सामने ही तो है इस पहाड़ पीछे, बस एक लतडाक (latdaak) और।” मेरे मुंह से लतडाक सुनकर गीता को हंसी आ गई।
“जानते हो, एक लतड़ाक कितना होता है?”
“चाहे, दो कदम चलो या पांच-दस मील। यहाँ के भोले-भाले ग्रामीण उसे एक लतड़ाक ही बोलते हैं। इस संदर्भ मे एक क़िस्सा है, कहो तो सुनाऊँ?” मैंने गीता की तरफ़ देखकर कहा।
“हाँ-हाँ, सुनाओ।”
“जानती हो, एक बार एक अंग्रेज़ पर्यटक गढ़वाल मे घूमने की दृष्टि से आया। उसके साथ जो गढ़वाली गाइड था, वो उससे निरन्तर पूछता रहा — और कितना चलना है भाई? इस बात पार् वो गाइड कहता रहा—बस एक लतड़ाक और, बस एक लतड़ाक,” कहकर मैने लम्बी सांस ली, “और जानती हो, वो गाइड उस अंग्रेज़ को पूरा दिन घुमाता रहा। आख़िरकार थक-हारकर उस विदेशी पर्यटक ने अपने कान पकड़ लिए और बोला—’बाप रे बाप, ये गढ़वालियों का एक लतड़ाक तो कभी ख़त्म नहीं होता!'” क़िस्सा सुनकर हम दोनों ही हँसते-हँसते दोहरे हो गए।
“अच्छा, ये पहाड़ों की ज़िन्दगी तुम्हें कैसी लगी?”
“पहाड़ पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए तो अच्छे हैं, मगर यहाँ ज़िन्दगी बितानी पड़े, तो बहुत कठिन है।” एक अजीब-सी थकावट को अपने भीतर महसूस करते हुए मैंने कहा।
“तो फिर वापिस देहरादून क्यों नहीं लौट आए?” शिकायती अंदाज़ में गीता ने पूछा।
“ख़ैर, अब ऐसी कोई बात नहीं। पहाड़ अब तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ के लोग; यहाँ की आबो-हवा; शहरों मे वो बात कहां? यहाँ के रहन-सहन मे बड़ी सादगी है और दिखावा नहीं है, जो मुझे बहुत पसंद है।” मैंने बड़ी आत्मियता से कहा।
“नैनीडांडा तो काफ़ी ऊंचाई पर लगता है।” सड़क से नीचे खाई की तरफ़ देखते हुए गीता बोली।
“हाँ, समुद्रतल से इसकी ऊंचाई कोई दो हज़ार फ़ीट के क़रीब है। इसकी चोटी दूर से ही नज़र आती है। अब तो दूरदर्शन का टीवी टावर भी यहाँ लगा है। जो कि दूर से ही किसी मुकुट की भांति नज़र आता है।”
“गाँव आकर तुमने हमे ख़त क्यों नहीं लिखे?” स्वर मे नाराज़गी थी।
“क्या करूं, ख़त तो कई लिखे, मगर उन्हें डाक मे डालने की हिम्मत न जुटा सका। सोचा क्या है ऐसा, जो लिखा जा सके। कुछ भी तो ऐसा ख़ास नहीं घट रहा था यहाँ, जो ख़त का विषय बन सके। एकदम निराशावादी हो गया था, मैं उन दिनों। ऐसा लग रहा था, जैसे यकायक हरी-भरी डाल को काटकर जड़हीन कर दिया गया हो और उसके सूखे तने को सड़ने के लिए इन निर्जन पहाड़ों में फैंक दिया गया हो।” कच्ची-पक्की, टेडी-मेड़ी, ऊबड़-खाबड़ संकीर्ण पगडण्डियों से होते हुए हम दोनों बातों मे गुम बेख़बर से चलते रहे। सामने एक जगह हमें किनारे होना पड़ा, जब एक चरवाह भेड़-बकरियों को लिए उसी तंग रास्ते से आ गया। वह कोई पहाड़ी गीत गुनगुना रहा था।
“मास्टरजी नमस्कार।” चरवाह बोला।
“और श्यामू कन छई (और श्यामू कैसा है)?” मैंने जवाब में कहा।
“बस दिन कटेणा छिन (बस दिन कट रहे हैं)।” वह चरवाह मवेशियों को हांकता हुआ आगे बढ़ गया।
“सुन श्यामू?” मैने पीछे से पुकारा, “शाम को एक किलो दूध भिजवा दियो।”
“अच्छा मास्टरजी।” कहकर वह चरवाह अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ, मवेशियों को हांकता हुआ, आगे बढ गया।
“कौन था ये?” कुछ कदम चलने पर गीता ने पूछा।
“गाँव का ही है। ज़रा संभलकर चलना यहाँ पे, फिसलोगी तो तगड़ी चोट लगेगी,” मैंने टेड़े-मेढे पत्थरों पर संभल के क़दम रखते हुए गीता को सतर्क करने की दृष्टि से कहा, “बड़ी दर्दनाक कहानी है बेचारे की। कभी इस इलाके का माना हुआ ठेकेदार हुआ करता था मगर आज गाय-बकरियाँ चरा रहा है।”
“क्यों क्या हुआ था इसके साथ?”
“वो गढ़वाल मे कहावत है न, ‘स्वारा के का नी हुंदी।'”
“मतलब?”
“मतलब, ‘सगे किसी के नहीं होते।’ श्यामू के अपने भाइयों ने ही इसे बरबाद कर दिया। इसकी जन्मभर की पूँजी हड़प ली। जिन भाइयों की परवरिश, पढ़ाई-लिखाई, शादी-ब्याह आदि सारे काम इसने खुद अपने हाथों से किए। उन्हें मकान और दुकान भी दिलवाए। उन्हीं भाइयों ने एक दिन नशे में इससे हस्ताक्षर करवा के इसकी सारी जमा-पूंजी अपने नाम करवा ली; और इस पर प्राण घातक प्रहार करके, इसे मरा समझके, खाई में भी फैंक दिया था।”
“अच्छा फिर!”
“फिर क्या? शायद इसके भाग में अभी और नरक भोगना लिखा था। इसलिये ये खाई मे गिरकर भी ज़िंदा बच गया। अब ग़रीबी के आलम में इसे अपनी पत्नी की बातें याद आती हैं। जो इसे समय-समय पर सचेत करती रहती थी।”
“क्या कहती थी वो?”
“वक़्त रहते संभल जाओ, वरना ये भाई-बंधु तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तब श्यामू अपनी पत्नी को दारू के नशे मे पीटते हुए कहता था—साली तू जलती है मेरे भाइयों से। दरार डालना चाहती है हमारे बीच। तू नही चाहती कि हम सारे भाई-बंधू मिल-जुलकर रहें।”
“अच्छा।”
“और देख लो गीता, आज ये सगे भाई जन्म-जन्म के बैरी बने हुए हैं।”
“श्यामू ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की?”
“बड़ा भाई होने के नाते वह आज भी यही मानता है कि अपने भाइयों को मैं अच्छे संस्कार न दे सका। शायद मुझमें ही कुछ कमी थी, जो भाइयों ने मेरे साथ ऐसा सलुक किया। मैं तो वैसे ही उन्हें सब कुछ दे देता, अगर वे मुझसे कहकर देखते। अक्सर श्यामू मुझसे कहता है कि मास्टरजी, मुझे बस यही दुख है कि एक ही माँ का दूध भी हम भाइयों को एक क्यों न रख सका?”
“ऐसे महान किरदार भी रहते हैं इन पहाड़ों में।” गीत श्यामू की महानता के आगे नतमस्तक थी।
“लो बातचीत में कुछ पता ही नही चला कि गांव कब आ गया?” मैंने इशारा किया, “वो रहा बिल्कुल उंगली की सीध में हमारा ग़रीबख़ाना।”
“घर तो बड़ा आलीशान है, पूरे गाँव मे अलग चमक रहा है।”
“अब तो पहाड़ों में भी लैंटर के घरों का चलन बढ़ने लगा है। पहले पत्थर-मिट्टी के मकान हुआ करते थे। जिनकी छत पहाड़ी पत्थरों को जोड़-जोड़ कर बनाई जाती थी।” कुछ ही देर में हम घर के अहाते में प्रवेश कर गए। सामान के वज़न से मुझे कुछ थकावट-सी हो गई थी। अत: गीता यकायक बोल उठी, “उम्र का तक़ाज़ा है, मास्टरजी।”
“अभी थकी हुई हालत मे भी, मैं तुमको कंधे पर उठाकर वापिस नैनीडांडा छोड़ सकता हूँ छुटकी।” और हँसते हुए हमने कक्ष में प्रवेश किया।
०००
पर्वतों में सूर्यास्त का दृश्य हृदय को छू लेने वाला होता है। डूबते सूरज की लाल किरणें ऐसे प्रतीत होती हैं, जैसे सारी संध्या एक लाल चादर मे सिमट गई हो। उस वक्त पहाड़ों की चोटियों, वृक्षों, नदियों, झरनों आदि समस्त प्रकृति का सौंदर्य और भी निखर उठता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना ऐसे ही किसी क्षण में की होगी। रोज़ ही ऐसे दृश्य उत्पन्न होते थे, मगर इतने मनोहरी मुझे कभी न लगे, जितना आज जान पड रहा थ।
ऐसे कई विचार चाय बनाते वक्त मेरे ज़हन में उठ रहे थे। कलाई पर दृष्टि पड़ी तो घड़ी की सुइयाँ छह बजा रही थी और सैकेंड की सुई अपनी रफ़्तार से भाग रही थी। मन हुआ सुइयों को पकड़कर समय को यहीं रोक दूँ। चाय कपों में उड़ेलकर मैं उस कक्ष में पहुंचा, जहाँ गीता बेख़बर-सी सोई हुई थी। नींद में उसका सौंदर्य और भी खिल उठा था। अपलक, मैं उसे यूँ ही देखता रहा।
घर में क़दम रखते ही मैंने गीता को खाना परोसा, जो मैं सुबह ही बनाकर गया था। हालांकि मैं ताज़ा भोजन बनाना चाहता था मगर सफ़र की थकावट ने गीता को काफ़ी थका दिया था और उसने बड़े अलसाये स्वर में कहा था, “जो कुछ भी तैयार है, उसी से काम चल जाएगा, इस वक्त तो ज़ोरों की नींद आ रही है।” खा चुकने के उपरांत लगभग दो-ढाई बजे से गीता अब तक सो रही थी। इस बीच श्यामू साढ़े पांच बजे के आस-पास गाय का किलो भर दूध दे गया था। शुद्ध एवं ताज़ा। ऐसा दूध शहरों में कहां? उसके बाद मैं चाय बनाने में जुट गया था और खीर बनाने के उद्देश्य से सूप में कुछ चावल भी मैंने निकाल लिए थे।
“गीता मैडम, अब उठ भी जाओ, बाक़ी नींद रात में पूरी कर लेना।”
“ओह!” कहकर गीता ने जम्हाई ली और आँखें मलते हुए बोली, “काफ़ी गहरी नींद आ गई थी, कितना समय हो गया?”
“मात्र साढ़े तीन-चार घंटे से सो रही हो।” मैंने चाय का प्याला थमाते हुए कहा और गीता मुस्करा दी।
“ओह गॉड! अब जाकर सर थोड़ा हलका हुआ है।” कहकर गीता भी चाय की चुस्की लेने लगी।
“चाय के साथ-साथ संगीत का भी आनन्द लो।” और मैंने डैक स्विच ऑन कर दिया। नरेंद्र सिंह नेगी की आवाज़ मे प्रसिद्ध गढ़वाली फ़िल्म ‘घरजवै’ का सदाबहार गाना बज उठा–‘तू दिख्यान्दी जन ज्यूनाली सच्ची त्यारा सौंउ (तू दिखती है जैसे चाँद, सच तेरी कसम)…’
“किसकी आवाज़ है ये?”
“मैडम, गढ़वाल के मुहम्मद रफ़ी को कौन नहीं जानता?”
“तो नेगी जी आपको भी पसंद हैं।”
“बेशक़…” कहकर मैने चाय की चुस्की ली, “एक ही तो क्लासिक गायक है, पूरे गढ़वाल में।”
“ख़ैर, और सुनाओ अपनी दास्तान।” कहकर मैंने जेब टटोली और अगले क्षण सिगरेट सुलगाकर माचिस और सिगरेट का पैकेट मेज़ के ऊपर रख दिए। सिगरेट का कश लगाने के बाद चाय का गिलास पुनः हाथ में ले लिया, “अरे मैं तो पूछना ही भूल गया, मम्मी जी कैसी हैं?”
“ठीक हैं, मगर कभी-कभार वी.पी. हाई रहता है।”
“क्या डॉक्टर को नहीं दिखाते?”
“दवाइयाँ चलती रहती हैं, मगर डॉक्टर कहते हैं कि ये बढ़ती उम्र का नतीज़ा है। घबराने की बात नही है। व्यर्थ के चिंता-फ़िक्र, तनाव न पाला करें, सब ठीक हो जाएगा।”
“मालती और ममता?”
“दीदियाँ भी ठीक हैं। मालती दीदी के इसी बैशाख मे लड़का हुआ है जबकि ममता दीदी की एक लड़की है। दोनों अक्सर हमें मिलने आती रहती हैं।”
“और वो प्यारा-सा जैकी।”
“उसे मरे तो डेढ़ साल हो गए।”
“अरे कैसे मरा?”
“एक दिन उसकी चेन खुली रह गई,” गीता को जैसे वो घटना याद हो आई, “बेचारा सड़क की तरफ तेज़ रफ़्तार ट्रक की चपेट में आ गया और … ऑन द स्पॉट ही।”
“काश! मैं उसे अपने साथ यहाँ पहाड़ों में ले आता।” मेरे सामने उस नटखट पॉमेरियन डॉग का चेहरा घूम उठा। जो किसी मासूम बच्चे की तरफ ही जान पड़ता था, “इस तरह मेरा अकेलापन भी कट जाता, और वो मरने से भी बच जाता।”
“भला होनी को कौन ताल सकता है?” मौत पर किसका वश है?” गीता के स्वर में वेदना थी और अर्थ में दार्शनिकता, “हमसे तो दो दिन तक कुछ खाया-पिया भी नहीं गया।”
“ऐसा होना स्वाभाविक है, वो था भी तो कितना प्यारा, नटखट। कहने को कुत्ता था मगर बिलकुल परिवार के एक सदस्य की तरह ही था।” इस बीच एक छोटी-सी चुप्पी और बेमन से चाय पीते हम दोनों। कुछ ही क्षणों बाद ख़ाली प्याले मेज़ की शोभा बढ़ा रहे थे।
“शायद तुम ठीक कहती हो गीता। मौत के आगे हम सभी बेबस हैं। पिछले साल मेरी माताजी का भी स्वर्गवास हो गया।”
“अरे कैसे? क्या हुआ था उन्हें?”
“कैंसर!”
“ओह! कम-से-कम एक ख़त लिखकर हमें तो बता देते।” गीता ने सहानुभूति दर्शायी।
“अंतिम समय में उनकी ज़ुबान पर मेरा ही नाम था। दुर्भाग्य से मैं खुद भी उनके अंतिम दर्शन न कर सका। मेरे पहुँचने से पूर्व ही ….।” आँखों के कोरों में उभर आये आँसुओं को मैंने तुरन्त ही हाथों से पोंछ लिया।
“बड़ी तकलीफ़ होती है, अपनों के गुज़र जाने से।” गीता के स्वर में आत्मीयता थी।
“कुछ लोग मरकर भी नहीं मरते … यादों की शक्ल में ज़िंदा रहते हैं और कुछ लोग जीते जी भी, मरे हुए समान हैं क्योंकि उन्हें कोई याद नहीं करता!”
“ऐसा क्यों कहते हो?”
“अक्सर तन्हाई में ये ख़्याल आता है मुझे!”
“ये एकान्त भी तो तुमने खुद ही चुना है अपने वास्ते। हम तो आज भी तुम्हें काफ़ी मिस करते हैं।”
“जानकर अच्छा लगा मुझे, मैं भी तुम लोगों को भुला नहीं पाया हूँ।”
“तभी तो काफ़ी ख़त लिखे हैं आपने?”
“वैसे माता जी की एक अन्तिम इच्छा थी; जो पूरी न हो सकी।” मैंने धुआँ उड़ाते हुए बंद आँखों से कहा।
“क्या?”
“वो चाहती थी, उनके जीते जी मेरा घर-परिवार बस जाता।”
“तो तुमने उनका कहा, मान क्यों नहीं लिया?”
“ऐसे ही इच्छा ही नहीं हुई,” अपने भीतर एक अजीब-सा अधूरापन महसूस करते हुए मैंने बेमन से कहा, “सच कहूं तो मुझे इस एकान्त और तन्हाई में जीने की आदत-सी हो गई है।”
“सच ये है या कुछ और…?” कहकर गीता ने मुझे चौंका-सा दिया।
“क्या?” मैंने मंद-मंद मुस्कुराते हुए कहा।
“इधर देखो …।” थोड़ा और क़रीब आकर गीता मेरी आँखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी।
“मैं कुछ समझा नहीं? ऐसे क्या देख रही हो मेरी आँखों में?” मैं इस नए खेल के लिए तैयार था, “तो फिर क्या लगा तुम्हें?”
“तुम जैसे बोरिंग आदमी से इश्क़ करके कौन अपने भाग फोड़ेगी!” गीता ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा।
“अच्छा आज हम बोरिंग हो गए। अभी तुम्हारी चुटिया पकड़ कर कमरे के दस चक्कर लगवा देंगे छुटकी।” मैंने भी मज़ाक़ में कहा और ग़मगीन होते माहौल में एक बार फिर खुशनुमा पल तैर गए।
“तुम तो बुरा मान गए मोनू।”
“नहीं-नहीं, वर्षों बाद ऐसा सुनते और कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है! मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे देहरादून वाले घर में बैठा तुमसे दिल्लगी कर रहा हूँ। क्या दिन थे, खाते-पीते, उठते-बैठते कैसे बच्चों की तरफ लड़ते थे हम दोनों।”
“हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है! लेकिन मेन (मुख्य) बात तो वहीँ की वहीँ रह गई।”
“क्या?”
“तुम्हारा वाकई कहीं कोई अफ़ेयर है क्या?”
“सच कहूं या झूठ?”
“झूठ!”
“तो सुनो, मेरा अफ़ेयर तो तुमसे ही था!”
“हा…हा…हा…, व्हाट अ जोक?” गीता ठहाका लगाते हुए बोली, “अब सच भी बता दो, कहीं मरे ख़ुशी के, मैं आज ख़ुदकुशी न कर लूँ?”
“अभी कुछ देर पहले तुम ही तो कह रही थी!”
“क्या?”
“कि मुझ जैसे बोरिंग आदमी से इश्क़ करके कौन अपने भाग फोड़ेगी!” अब ठहाका लगाने की बारी मेरी थी। गीता ने भी हंसी में सहयोग दिया।
“मैं तो सीरियस हो गयी थी!” गीता ने स्वर बदलकर मेरी नक़ल करते हुए कहा और पुनः तेज़-तेज़ हंसने लगी।
“बहुत ख़ूब तुम इतनी अच्छी नक़ल कर लेती हो, फ़िल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती!” मैं भी हँसते हुए बोला।
“मुझे फ़िल्मों में लेकर कौन अपने भाग फोड़ेगा। खैर छोडो….” गीता ने बात का विषय बदलते हुए कहा, “ये बताओ, आज खाने में क्या बनाना है?”
“जो कुछ भी आप खिला दो मैडम।”
“वाह मेजबान खुद मेहमान से पूछ रहा है, क्या मेजबानी है?”
“वैसे मैंने खीर के लिए चावल निकाल लिए हैं। वहां सूप में रखे हैं।”
“गुड!”
“गोविन्द का लड़का भी अभी तक सामान लेकर नहीं आया। दिन की गाडी तो कबकी निकल गई है।” मैंने ख़ाली प्याले को उठाते हुए कहा।
“लाओ कप मुझे दे दो।”
“अरे नहीं, आप मेहमान हो छुटकी जी, प्याले मैं धोऊंगा।”
“मास्टरजी होकर आप मेरे सामने कप धोते हुए अच्छे लगेंगे क्या?” कहकर गीता ने जूते कप जबरन मेरे हाथों से छीन लिए। उसका ये व्यवहार मेरी समझ से परे था मगर हृदय को अत्यन्त सुकून देने वाला था।
“चलो तब तक मैं अपना स्कूल का काम भी निपटा लूंगा।” कहकर मैंने बैग निकाल लिया। जिसमे बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बण्डल पड़े थे। इस बीच गीता रसोई में चली गई।
“स्कूल लाइफ़ में बस यही दो-तीन काम मुझे ख़राब लगते हैं। एक—बच्चों को डांटना या पीटना। दो—पेपर जांचते हुए सही नम्बर न दे पाना। तीन—प्रत्येक विद्यार्थी की सालाना रिपोर्ट बनाना या छोटी कक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करना। कक्ष से ही मैंने ऊँचे स्वर में गीता को ये सब सुनाते हुए कहा।
“मैं समझी नहीं मास्टर जी।” सामने रसोईघर से बर्तन धोते हुए गीता बोली। दिनभर के अन्य जूठे बर्तन भी पास में पड़े हुए थे।
“बच्चों के डाँटने और पीटने पर मेरे मन एक अपराध बोध की-सी भावना घर करने लगती है। लगता है, जैसे मैं खुद गुनहगार हूँ। मैं उन्हें ठीक से समझा नहीं पाया हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है, देहरादून में प्रिंसिपल अनिल मिश्रा से मेरी अनबन के बारे में।”
“हाँ, हल्का-सा याद है।” सामने रसोईघर से ही गीता ने उत्तर दिया।
“उन दिनों एक विद्यार्थी को मैंने इतना पीटा था कि बेचारा बेहोश हो गया था। उसका कसूर इतना ही था कि उनसे नाम ‘अनिल’ था। दो बोतल गुलूकोस चढाने के बाद जब उसे होश आया, तब मैंने प्रण किया कि अब मैं बच्चों को नहीं पीटूंगा। मगर आज भी कुछ ऐसे ढीठ और ज़िद्दी किस्म के बच्चे मिलते हैं कि उन पर डण्डे का प्रयोग उचित हो जाता है। फिर भी पीटते समय मैं एहतियात ज़रूर बरतता हूँ, कहीं किसी को ज़्यादा चोट न आ जाये।” कहते-कहते मैंने दो-तीन विद्यार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर डाली। इतनी देर में गीता भी बर्तन धोकर कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी।
“बर्तन धोकर आख़िर तुमने मेरे सिर पर पाप चढ़ा ही दिया।” मैंने गीता की तरफ़ देखते हुए कहा। फिर अगले रिपोर्ट कार्ड पर एक सरसरी निगाह डाल।
“वैसे इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है।”
“वो कैसे?”
“रात के बर्तन धोकर।”
“बहुत ख़ूब काफ़ी हाज़िर-जवाब हो गई हो।”
“क्या करें, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है?” हंसी-मज़ाक़ से वातावरण काफ़ी खुशनुमा हो गया था गीता ने खुद को वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे ढाल लिया था कि मेरी स्मृति में देहरादून के वे दिन पुनः हरे हो गए।
“ये क्या कर रहे हो?” रोकते हुए पूछा।
“फिलहाल मगज़मारी कर रहा हूँ … मैंने अपना सर धुनते हुए कहा, “कभी टीचर मत बनना, सबसे ख़राब ज़िंदगी है टीचरों की।”
“कैसे?”
“परीक्षा के दिनों में पेपर जांचना, मेरे लिए भी एक इम्तिहान की घडी होती है। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं किसी बच्चे को पासिंग मार्कस नहीं दे पाता हूँ। उस वक्त बाल नोचने का मन करता है और खीज मिटाने के लिए मैं पूरा चेन-स्मोकर हो जाता हूँ। एक दिन में सिगरेट की आठ-दस डिब्बियां फूंक डालता हूँ। कई बार तो मन करता है कि फाड़ दूँ ये उत्तरपुस्तिकाएं और पड़ा रहूं सन्यासी की तरह समाधि या योग-ध्यान की मुद्रा में, किन्तु कर्म से भागना मनुष्य के वशीभूत नहीं है शायद इसी द्वंद्व का नाम जीवन है, जो मृत्यु तक एक संघर्ष है। फिर मृत्यु के उपरान्त एक असीम शांति और महामोक्ष; जबकि जीवन से पलायन कायरता है। यही सब आदि-अनादि भाव पेपर जांचते समय ह्रदय से स्फुटित होते हैं।” कहकर मुझे राहत सी महसूस हुई। शेष बेचैनी को मैंने सिगरेट के धुएँ में उडा दिया था। इस बीच गीता बड़ी एकाग्राचित होकर मुझे सुन रही थी।
“कुछ यही हाल विद्यार्थियों की सालाना रिपोर्ट बनाते या प्रश्नपत्र तैयार करते समय भी रहता है इसलिए इन पर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ कुछेक रटे-रटाये शब्द मैं हर सालाना रिपोर्ट में दोहरा देता हूँ। मसलन—’पढाई में ठीक है, लेकिन समझता देर से है’ या ‘बहुत अच्छा है, थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है’ या उम्मीद से कहीं बेहतरीन, होनहार’ फिर जैसे-जैसे इस काम में बोरियत होने लगती है, एक-एक लाइन की रिपोर्ट एक-एक शब्द में बदल जाती है। मसलन —’संतोषजनक’ … ‘उत्तम’ …. ‘कमज़ोर’ …. ‘होनहार’ आदि से ही काम चलाना पड़ता है।”
“प्रश्नपत्र तैयार करते समय सिरदर्दी और भी बढ़ जाती है। पहले पूरी किताबें पढ़ो। फिर उसमे से प्रश्नपत्र तैयार करो। जगह-जगह काटो-पीटो बदलाव करो। सचमुच ये प्रक्रियाएं मुझे अजीब -सी थकावट और परेशानी से भर देने वाली होती है। एक एकांकी जीवन व्यतीत करते हुए मेरा दम-सा घुटने लगा है और उस पर ये व्यर्थ की सिरदर्दी, ईश्वर किसी को टीचर न बनाए।” मेरी बातें सुनकर गीता की हंसी छूट पड़ी।
“मैडम बड़ी मगज़मारी है इन कामों में। सुकून छीन जाता है और नींद उड़ जाती है।”
“अच्छा।”
“मेरी हालत तो मोहन राकेश के उपन्यास ‘न आने वाला कल’ के मास्टर जैसी हो गई है, जो इस्तीफ़ा देकर सब फ़िक्रों से निजात पा लेना चाहता है। मैंने व्यंग्यात्मक लहज़े में कहा, “मुझमे और उस मास्टर में यही फ़र्क है कि वह शादीशुदा था और मैं कुंवारा ही मर रहा हूँ।”
“क्या बात है?” गीता खुलकर हंसी।
“मैडम आपको हंसी आ रही है, मेरी व्यथा सुनकर।”
“नहीं, वो बात नहीं है, आपके कहने के अंदाज़ पर हंसी आ रही है।”
“मास्टरजी।” बाहर से किसी ने पुकारा।
“ये तो देबू की आवाज़ है।” मैंने स्वर को पहचानते हुए कहा।
“कौन देबू?” गीता ने पूछा।
“दुकानदार गोविन्द का लड़का, शायद सामान लेकर आया है।” मैंने गीता को बताया, फिर स्वर को थोड़ा ऊँचा करके कहा, “देबू, बेटा अंदर आ जाओ।”
“मास्टर जी नमस्कार, ये रहा आपका सामान।”
“दो बजे वाली गाड़ी में आये क्या?”
“हाँ, मास्टरजी।” कहकर देबू ने सामन रख दिया और गीता को भी ‘नमस्ते’ किया।
“और क्या परिणाम रहा, लैन्सीडॉन की यात्रा का, फौज में भर्ती हुए कि नहीं?”
“कहाँ मास्टरजी सब जगह सिफारशी टट्टुओं की भरमार है, गरीबों को कौन पूछे?” देबू के स्वर में सिस्टम के ख़िलाफ़ आक्रोश था, “यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने इस देश में जन्म लिया। जहाँ बेरोज़गारों की भरमार है। एक बात कहूं मास्टर जी।”
“क्या?”
“मास्टरजी, आग लगा देनी चाहिए इस शिक्षानीति को जो हमें जीने लायक एक ढंग की नौकरी भी नहीं दे सकती।”
“हाँ बेटा, तुम्हारा आक्रोश है। वाकई हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या बड़ी विकट है, पर इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। अपना धैर्य और संयम नहीं खोना चाहिए। मैं भी स्वीकार करता हूँ कि हमारी शिक्षानीति में अनेक दोष हैं, पर इन्हें दरुस्त करने का प्रयास भी हमें ही करना होगा। अकेले सरकार को दोष देना ग़लत होगा। हमें शिक्षा के साथ-साथ स्वरोज़गार की भावना भी विद्यार्थी काल से ही नौजवानों में जागृत करनी चाहिए।”
“क्या उन नेताओं को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो अपने घोषणा-पत्र में ग़रीबी-बेरोज़गारी उन्मूलन के नारे उछालते हैं और फिर हमारे ही वोटों से राजपाट पाकर हमारा उपहास उड़ाते हैं? क्या नैतिक तौर पर इन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार है मास्टरजी?”
“बेटा नैतिक तौर पर तो हमें भी मास्टरगिरी से इस्तीफ़ा दे चाहिए क्योंकि इस दोषपूर्ण शिक्षातंत्र का भाग तो हम भी हैं। तुम्हें उज्जवल भविष्य देने की जगह इस बेरोज़गारी के अँधेरे कुएं में धकेलने के लिए कुछ तो दोषी हम भी हैं।”
“नहीं मास्टरजी, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था।”
“बैठो चाय पियोगे?”
“नहीं मास्टरजी, पिताजी ने कहा था जल्दी आना। वहां दुकान पर कोई नहीं है।” कहकर देबू ने विदा ली।
“बड़ा आक्रोशी लड़का है।” देबू के जाने के बाद गीता ने उसके बारे में राय दी।
“मज़ा आ जाता है इसके साथ बातचीत करके। कई बार हमारे बीच अनेक रोमांचक बहस हुई हैं।” मैंने उत्साहपूर्वक कहा।
“किस विषय में?”
“लगभग हर विषय पर हम बहस कर चुके हैं। जैसे अध्यात्म, राजनीति, समाज, साहित्य, नैतिकता, अनैतिकता, जीवन-मूल्य, सांस्कृतिक-मूल्य, प्राचीन संस्कृति, ब्रह्माण्ड और उसके रहस्य आदि-आदि विषय। कुछ भी तो अछूता नहीं रहा हमारे मध्य। प्राय: वर्तमान घटनाओं और राजनीति पर तो हमारी बहस अक्सर होती ही रहती है। बाज़ार में तो कई बार मज़मा तक लग जाता है हमें सुनने के लिए। कभी चायवाले की दुकान पर तो कभी खुद देबू की दुकान पर भी हम दोनों अक्सर बहस करते रहते हैं।”
“क्या बोर नहीं होते?”
“नहीं, समय काटने के लिए तो यह अच्छा साधन है। कई बार देबू की अपने पिता से अनबन हो जाती है तो वह मेरे घर पर ही रात गुज़ार लेता है। उस दिन तो फिर सारी रात बहसबाज़ी में ही बीतती है।”
“अच्छा काफ़ी गहरी दोस्ती है आप दोनों में।”
“हाँ, हम दोनों दोस्त पहले हैं, शिष्य और गुरु। मैंने देबू और अपने रिश्ते के मार्फ़त कहा और मेरी नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी, तो पाया साढ़े सात बज रहे थे, “ओह इस बातचीत के चक्कर में कितना समय बीत गया है?”
“क्या फ़र्क़ पड़ता है?”
“फ़र्क़?” बड़ी हैरानी के साथ मैंने गीता को देखा और कहा, “अभी खाना भी पकाना है मैडम जी!”
“वो मैं बना लूंगी … बस आप मेहरबानी करके तब तक स्कूल का ये काम निपटा लीजिए।” गीता ने हाथ जोड़ते हुए कहा और कृपया ये बताइए ऊपर के कमरे की चाबियाँ कहाँ हैं?”
“अरे नहीं, स्कूल का ये काम तो आधे-एक घंटे में रात को भी हो जायेगा। तब तक मैं खुद ही कमरा ठीक कर लेता हूँ। आख़िर आप जैसी भी हैं, हमारी मेहमान हैं।”
“कहाँ से मेहमान, हम तो बेईमान हैं।” गीता ने मंद-मंद मुस्कराते हुए बिन्दास स्वर में कहा और मैंने जेब से चाबियाँ निकालकर गीता के हवाले कर दीं।
०००
“और हाँ, उस साले मिश्रा को मैंने अगले दिन बहस में हरा दिया था।” रोटी का कौर तोड़ते हुए मैंने कहा। सामने दीवार घडी पर इस वक़्त ठीक नौ बज रहे थे।
“तभी जाके आप उसकी नज़रों में खटकने लगे।” गीता ने गिलास में पनि भरते हुए कहा और जग पुनः मेज़ पर रख दिया, “बाई दी वे, अगले दिन बहस का विषय क्या था?”
“उस रोज़ मेरा पीरियड ख़त्म हो गया था और आधी छुट्टी का वक्त था। हम सब टीचर लोग स्टॉफ रूम में जमा थे। चाय की चुस्कियों के साथ गपशप चल रही थी। प्रिंसिपल मिश्रा भी गपशप के इरादे से हमारे मध्य आ गया और बात ही बात पर बहस छिड़ गई आतंकवाद पर।”
“अच्छा।” गीता पानी पीते हुए बोली।
“साला मिश्रा बोला, अमेरिका आतंकवाद के खात्मे के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है। इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। मेरी चाय गिरते-गिरते बची।” कहते-कहते आँखों के आगे पूरा दृश्य सजीव हो उठा……
“तुम क्यों हंसे, मिस्टर मोहन?” प्रधानाचार्य ने स्पष्टीकरण माँगा।
“ऐसे ही!” मैंने मुस्कराते हुए उसी अंदाज़ में कहा।
“तुम यदुवंशियों की कूटनीतिज्ञ मुस्कान को क्या मैं पहचानता नहीं? अवश्य ही तुम मेरी बात के विरोध में कुछ कहना चाहते हो?” अनिल मिश्र तिलमिला उठा।
“सर्वप्रथम आपका ये कथन ही हास्यास्पद है सर कि अमेरिका आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए प्रयासरत है। वो अमेरिका जो खुद मुस्लिम उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करता है। आप उसे आतंकवाद का शत्रू बता रहे हैं। क्या यह हास्यास्पद बात नहीं है?” सारा स्टॉफ़ हंसने लगा।
“देखो मोहन, मैं तुमसे फालतू बहस नहीं करना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे छोटे लोगों के मुंह लगने की आदत नहीं है।” चिढते हुए प्रिंसिपल महोदय बोले।
“हाँ, राष्ट्रपति के बाद आप ही हैं बड़े नवाब …” मैंने धीरे से कहा, अगल-बगल में बैठे अन्य लोग हंसने लगे, “क्या कहा, फिर से तो कहना?” या तो मिश्र ने सुना नहीं था, या वह चाहता था कि मेरी यही बात एक बार ऊँचे सुर में सब सुनें।
“कुछ नहीं सर!”
“यू …!” कहकर कुछ रुक से गए प्रिंसिपल महोदय, “मैं तुम्हारी सालाना रिपोर्ट ख़राब कर दूंगा।” कहते-कहते अति उत्तेजना में मिस्टर अनिल मिश्रा काँपने लगे।
“छोडिए भी सर क्या ….?” प्रिंसिपल के बगल में बैठे रावतजी ने हस्तक्षेप किया और एक-दो अन्य साथियों ने हाथ के इशारे से मुझे शांत रहने के लिए कहा।
“पता नहीं, क्यों मेरी हर बात काटते हैं. मिस्टर मोहन!” मिश्रा ने रावतजी की तरफ़ देखते हुए ही कहा।
“जो बात हमें ग़लत लगेगी, हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे।” मैंने भी मिश्रा की ओर देखे बिना कहा। मेरी दृष्टि भी रावतजी पर ही केन्द्रित थी, “आख़िर लोकतन्त्र हैं, कोई तानाशाही तो नहीं!”
“तेरे लोकतन्त्र की तो मैं!” अनिल मिश्रा उत्तेजना मापने स्थान पर खड़े हो गए। शायद वो मेरी तरफ़ बढ़ना चाहते थे मगर आस-पास खड़े लोगों ने उन्हें समझाकर बैठाया।
“मोहन हम बाहर चलें।” वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए रावतजी ने मुझसे बाहर चलने का आग्रह किया।
“ले जाओ इसको बाहर वरना मेरे हाथों से आज एकाध लाश …।” मुझे बाहर जाता देख अनिल मिश्रा पीछे से गरजा। मैं रूककर कुछ कहना चाहता था कि रावतजी ने मुझे इसका अवसर नहीं दिया और बिना कुछ कहे हम कक्ष से बाहर आ गए।
“अब यहाँ मेरा गुज़ारा होना मुश्किल है।” मैंने सिगरेट सुलगा ली, “पानी सर से ऊपर गुज़र चुका है।”
“तो ओखल में सर क्यों डालते हो? क्या ज़रूरत थी प्रिंसिपल से उलझने की? हमारी तरह तुम भी चुपचाप उसकी बात क्यों नहीं सुनते?”
“रावत जी आप मेरा नेचर (प्रकृति) जानते हैं, मुझे फालतू बातें पसंद नहीं और ग़लत तथ्यों को मैं सहन नहीं कर सकता … चाहे प्रिंसिपल हो या डिप्टी कलेक्टर। पता नहीं इसे प्रिंसिपल किसने बना दिया, ये तो जमादार बनने लायक भी नहीं था! शक्ल देखो साले की ….।” मैंने लगभग खीज उतारने वाले अंदाज़ में कहा।”
“तुम चाहो तो मैं तुम्हारा तबादला पौड़ी गढ़वाल में करवा सकता हूँ। शिक्षा मंत्री के पी.ए. से मेरी अच्छी-खासी जान-पहचान है।”
“हाँ, ठीक है जल्द-से-जल्द मेरी बात चलाओ, वरना या तो मैं पागल हो जाऊंगा या इस प्रिंसिपल के बच्चे का ख़ून कर बैठूँगा।” मैंने भीतर एक अजीब-सी घुटन को महसूस करते हुए कहा और सिगरेट का एक लम्बा-सा कश खींचा।
“ठीक है एकाध हफ़्ते में सब फ़ाइनल हो जायेगा। हो सकता है कि तीन-चार दिन में ही तुम्हें सामान बांधने की नौबत आ जाये।” रावत जी ने बड़े इत्मीनान से कहा।
“इसके बाद की कहानी तो तुम जानती ही हो गीता। आज तीन बरस होने को आये हैं, पहाड़ों में ज़िंदगी गुज़रते हुए।” इस बीच हम दोनों खाना भी निपटा चुके थे।
“अब तुम सो जाओ कल सफ़र में रहोगी दिनभर।” हाथ धो चुकने के उपरान्त मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा।
“मेरा तो मन कर रहा है आज यूँ ही बातें ही होती रहें। ये सिलसिला ख़त्म न हो।”
“मेरा भी कुछ ऐसा ही मन कर रहा है गीता।”
“अच्छा यहाँ के ग्रामीण जीवन और देहरादून के शहरी जीवन में क्या फ़र्क़ किया?”
“काफ़ी फ़र्क़ है गीता। शहर दिन-रात भागता है, जबकि गाँव आज भी साँझ ढले सो जाते हैं। यहाँ दिन की अपेक्षा रातें लम्बी होती हैं। मुझ जैसे अकेले आदमी को तो यहाँ दिन काटना भी बहुत कठिन लगता है। कभी-कभी एक-एक घण्टा भी एक-एक युग समान जान पड़ता है। शहरों में समय गजारने के अनेक साधन मौज-मस्ती के अनेकों सामान हैं। मगर यहाँ पुरातन परम्पराएँ, संस्कृति और लोकसंगीत ही ग्रामीणों के मनोरंजन का एकमात्र अच्छा साधन है। वैसे यहाँ असीम शांति है और शोर-शराबा बिल्कुल नहीं है। दुर्गम पहाड़ी इलाक़ा होने के कारण अभी केवल टीवी की दूषित संस्कृति ने यहाँ के लोगों को ख़राब नहीं किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम ही बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। वैसे औसतन लोग-बाग आठ-नौ बजे तक सो जाते हैं। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त (चार-साढ़े चार बजे) तक ये लोग उठ जाते हैं। तत्पश्चात दैनिक क्रिया-कलापों से निवृत होकर अपने रोज़मर्रा के कार्यों में जुट जाते हैं। आमतौर पर हर कुनबा कृषि पर ही निर्भर है। कृषि के साथ-साथ कभी-कभार मेहनत-मजदूरी के अन्य छोटे-मोटे कार्य करके भी ये अपना पेट भरते हैं।”
“छोटे-मोटे कार्यों से आपका अभिप्राय:?”
“सरकार की तरफ़ से जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। सड़क निर्माण होता है। भवन-स्कूल, नहर इत्यादि बनते हैं या पानी की पाइप-लाइन हो अथवा बिजली के खम्भे गाड़ने हों, यह सब कार्य स्थानीय लोगों द्वारा ही संभव हो पाते हैं। इस तरह इन लोगों को अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है।”
“आपने तो पहाड़ के जन-जीवन का सूक्ष्म अध्ययन कर डाला है मास्टरजी, वैसे एक राय दूँ।”
“क्या?”
“आप इस विषय पर पी एच डी क्यों नहीं कर डालते? शीर्षक होगा—गढ़वाल और उसका जन-जीवन।” गीता काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगी।
“वैसे राय बुरी नहीं है मैडम, अगर तुम भी यहाँ ठहर जाओ तो दोनों मिलकर इस शुभ कार्य को अंज़ाम दे डालते हैं।”
“मैं, न-बाबा-न अपने बस कि तो नहीं गढ़वाल में रह पाना।” गीता ने अपने कान पकड़ते हुए कहा।
“याद है एक बार जब हम रामलीला देखकर लौटे थे, तो मैंने तुम्हें त्रिजटा कहा था।”
“हाँ, याद है विभीषण जी।” गीता ने हँसते कहा, “लेकिन आपको ये बात अचानक कैसे याद आई?”
“क्योंकि उस रोज़ भी तुमने ऐसे ही कान पकडे थे।”
“हाँ, अच्छी तरह याद है। मैं चिढ गई थी और मैंने तुम्हें विभीषण कहा था। तब हमारे मध्य दो दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई थी।”
“फिर मम्मीजी ने सुलह करवाते हुए, तुमसे क्या कहा था छुटकी?”
“हाँ, अच्छी तरह याद है। मम्मीजी ने कहा था कि कान पकड़के मास्टरजी को सॉरी बोलो।”
“ठीक वैसे ही जब आज तुमने कान पकडे तो मुझे वह बात याद आ गई।” इसी तरह पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कब दो-तीन घण्टे गुज़र गए इसका पता भी तभी चला जब दीवार घड़ी पर हमारी नज़र पड़ी। साढ़े बारह बज चुके थे।
“चलो छुटकी अब जाकर सो जाओ वरना सुबह सफ़र में थकावट महसूस होगी।”
“जो आज्ञा गुरुदेव।” और हँसते-हँसते ही गीता ने कक्ष से विदाई ली।
गीता तो ऊपर के कक्ष में सोने के लिए चली गई मगर मुझे नींद न आ सकी। कभी इस हाथ, कभी उस हाथ, करवटें ही बदलता रहा। फिर भी लेटा रहा और जब लाख प्रयत्न करने पर भी नींद न आई तो आदतन डायरी लिखने बैठ गया। घडी में दो बजने वाले थे। डायरी लिखते वक्त मन में कई विचार अनायास ही आ गए … ‘क्यों चली आई तुम इस निर्जन एकान्त में, इस विश्वामित्र का तप भंग करने, मेरी प्यारी मेनका। तुम्हारे बग़ैर जीने की आदत डाल चुका था मैं। क्या मिला, तुम्हे मेरा मौन भंग करके? यह सब क्या है — छलावा! मोहमाया! मृगतृष्णा! दिवास्वप्न है या फिर वास्तविकता? क्यों हृदय आज इतना व्यथित, द्रवित, विचलित और अशांत है। ये सब क्या हो रहा है मुझे? जो भावनाएं मैं हृदय में ही दफ़न कर चुका हूँ क्यों पुनः सर उठा रही हैं?’ आदि-आदि ऐसे अनेक विचारों की सुनामी लहरें मेरे हृदयतट से टकराने लगीं और मैं न जाने कब तक उन्हें डायरी में लिखता रहा। यकायक घडी पर दृष्टि पड़ी तो पौने चार बज रहे थे। लगा अब मुझे भी कुछ समय सो जाना चाहिए। अन्यथा मेरी आँखें रातभर की कहानी गीता को कह देंगी। वो बात जो मुद्दत से मेरे होंठों पर है कभी ज़ुबान पर न आ सकी। कुछ यही भाव लिए मैं सो गया।
०००
बस चलने में अभी देर थी। क़रीब दस-पंद्रह मिनट का समय और शेष था। बस के ठीक सामने बने ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ थी। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो यह कि ढाबे वाले का रोज़गार गरम था। उसके रेडियो पर फ़िल्मी गीत बज रहे थे और चूल्हे पर चाय गरम थी। अन्य लोगों की भांति ड्राइवर-कंडेक्टर भी ढाबे पर बैठे चाय-पानी पी रहे थे। कुछ सवारियाँ भी जलपान ग्रहण कर रही थी तथा शेष सवारियाँ हमारी तरह बस में बैठे-बैठे बस के चलने का इन्तिज़ार कर रही थी। मुझे यकायक हंसी आ गई। वजह यह थी कि सुबह साढ़े छह बजे गीता ने ही मुझे उठाया था। ये कहकर कि ‘अरे कुम्भकरण जी कब तक सोते रहेंगे, मेरी बस छूट जायेगी?’ और मैं हँसता हुआ उठ गया था। उसे कैसे बताता कि रातभर कैसे-कैसे विचार हृदय में उठ रहे थे?
“क्या हुआ ये यकायक क्यों हंसने लगे?” गीता ने पूछा।
“तुम्हारी कुम्भकरण वाली बात पर हंसी आ गई।” मैंने हँसते हुए कहा और गीता को भी हंसी आ गई।
“और क्या कुम्भकरण ही तो हो तुम, वर्ना मेरी बस नहीं छूट जाती।”
“अरे मैडम, सुबह से कह रहा हूँ कि बस के चलने का समय आठ बजे है और कभी-कभी सवा आठ और साढ़े आठ भी बज जाते हैं। ख़ैर पहुँच गए न समय से। वो देखो आठ बजने को आये हैं मगर अभी भी गप्पों में लीन हैं ड्राइवर और कंडेक्टर। क्या तुम भी चाय पियोगी?”
“नहीं सफ़र में खाने-पीने से मुझे परहेज़ है। वैसे आप भी अपने खाने-पीने का ध्यान रखा कीजिये। मुझे तो आप पहले से कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं।”
“अच्छा ध्यान रखूँगा भई।”
“सुबह जब मैं सफर के लिए तैयार हो रही थी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे! कुछ ख़ास बात थी क्या?”
“नहीं कोई ख़ास बात तो नहीं थी।”
“अरे एक बात तो मैं भी भूल ही गई!” कहकर गीता ने पर्स में से एक लिफ़ाफ़ा-सा निकाला और मेरी तरफ़ बढ़ा दिया।
“क्या है ये?” मैंने लिफ़ाफ़ा खोलते हुए कहा।
“उनका फोटो।”
“किनका?”
“बड़े बुद्धू हो, समझते नहीं!”
“ओ आई सी! बधाई हो, कब हुआ ये सब?”
“बस पिछले महीने ही वे मुझे देखने के लिए आये थे। आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं।”
“बहुत-बहुत बधाई हो!” मैंने हाथ मिलाकर मुबारक़बाद दी।
“थैंक्यू। कैसा है फोटो?” गीता ने होने वाले दूल्हे के बारे में मेरी राय जाननी चाही।
“बहुत सुन्दर है तुम्हारी तरह।” कहकर मैंने फोटो गीता को वापिस कर दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ लज्जा गई।
“29 सितम्बर, ये तारीख़ याद रख लेना मास्टरजी। कार्ड मिले-न-मिले, आपको मेरी शादी में ज़रूर आना है।”
“ज़रूर-ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे मोहतरमा।” मैंने लगभग वचन-सा दे दिया, “कहो तो अर्ज़ कर दूँ … मौक़े का है, मरहूम ग़ालिब फरमा गए थे।”
“इरशाद …”
“मेहरबाँ होके बुला लो मुझे, चाहो जिस वक़्त। मैं गया वक़्त नहीं हूँ, कि फिर आ भी न सकूँ।”
“क्या बात है?” गीता ने बड़े अदब से कहा, “बहुत ख़ूब!”
“पसंद आया तो लो इसी बात पर एक और शेर सुनो… ‘जी में ही कुछ नहीं है हमारे, वगरना हम; सर जाए या रहे, न रहें पर कहे बग़ैर!”
“लगता है आज शायरी ही करते रह जाओगे, मगर वो बात नहीं कहोगे, जो मैं पूछ रही हूँ।”
“कौन-सी बात?”
“वही, जो सुबह कहने वाले थे आप?”
“क्या कहूं? कुछ ख़ास नहीं था!”
“फिर भी कुछ तो था!”
“शायद तुम जानती हो, मैं क्या कहना चाहता था?”
“मैं कुछ नहीं समझी मास्टरजी?”
“तुम हमें कभी समझ भी न पाओगी गीता?”
“क्या मतलब?”
“मतलब जानने के लिए फिर से ग़ालिब का एक और शेर हाज़िर है…”
“कौन-सा?”
“गई वह बात, कि, हो गुफ़्तगू तो क्योंकर हो; कहे से कुछ न हुआ, फिर कहो, क्योंकर हो?”
“पहेलियां मत बुझाओ, साफ़-साफ़ कहो? ये शायरी छोड़कर सीधे क्यों नहीं कहते!”
“अरे पगली, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने अर्से तक हमारा साथ रहा। पिछले क़रीब छह-सात सालों से हम दोस्तों की तरह रहे हैं। लड़ाई-झगड़ा, हंसी-मज़ाक़ और न-जाने क्या-क्या चलता रहा हमारे मध्य। पिछले तीन वर्षों से कभी लगा ही नहीं कि मैं यहाँ अकेला जी रहा हूँ। ये यादें लेकर मैं ज़िंदगीभर जीता रहूँगा। शादी के बाद तुम मुझे भूल तो न-जाओगी छुटकी!” भावुकता में कुछ आँसू आँखों में तैर गए। जिन्हें आँखें बंद रोकने की व्यर्थ चेष्टा की।
“ये क्या हो गया है मास्टर जी आपको! सम्भालो अपने आपको! लोग हमारी तरफ़ देख रहे हैं।”
“काश! हम दोनों उम्रभर साथ रह पाते छुटकी!” कहते हुए भावुकतावश मैंने गीता का हाथ पकड़ लिया।
“काश! ऐसा हो पाता मास्टरजी?” गीता भी फ़फ़्क कर रो पड़ी। उसने भी मेरे हाथ पर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली। माहौल काफ़ी भावनात्मक हो गया था। सामने बैठी दो ग्रामीण स्त्रियाँ भी नाम आँखों से हमारी ओर देख रही थी। एक अजीब-सा शून्य बस के भीतर वातावरण में तैर गया था। जिसे ढाबे वाले के रेडियो से आते फ़िल्मी गीत की कुछ पंक्तियाँ भंग कर रही थी — “वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे इक ख़ूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों।”
काफ़ी देर तक नाम आँखों से हम दोनों ही एक-दूसरे को देखते रहे। इस बीच हमारे हाथों की पकड़ वैसी ही थी। फिर जैसे ही महसूस हुआ कि ढाबे से उठकर लोग गाड़ी में बैठने लगे हैं। तो हमारे हाथ खुद-बी-खुद अलग हो गए। “अच्छा, आंटीजी को मेरी तरफ़ से नमस्ते कहना।” जब ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर चलने की आज्ञा मांगी तो मैंने अपनी भावनाओं को समेटते हुए कहा और भारी क़दमों को लिए मैं बस से नीचे उतर गया।
“मैं समझ गई मोनू! तुम क्या कहना चाहते थे!” गीता यकायक बोल उठी। मैं बाहर बस की उस खिड़की के निकट खड़ा था जहाँ से गीता मुझे देख रही थी।
“लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है छुटकी!” मैंने जेब से काग़ज़ का एक पुर्ज़ा निकालकर गीता की तरफ़ बढ़ा दिया, “खैर, चिट्ठी-पटरी भेजती रहना, ये मेरा पता है और इसमें स्कूल का फोन नंबर भी लिखा है। कभी-कभी फ़ोन भी कर लेना। बाय।” मैंने हाथ हिलाते हुए कहा।
बस स्टार्ट हो चुकी थी।
“बाय …” प्रत्युत्तर में गीता ने भी हाथ हिलाया। धीरे-धीरे बस और मेरे मध्य फ़ासला बढ़ता चला गया। ‘शायद पहाड़ों में आना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ग़लती थी?’ एक ठण्डी-सी आह मेरे होंठों से निकली।
***