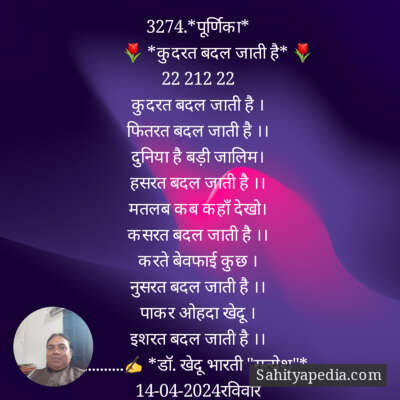मन की भ्रांतियाँ
मन की भ्रांतियाँ टूट चुकीं अब, कहने को कुछ बचा ना था।
शब्द मौन हो चुके थे ऐसे, साँसों का भी पता ना था।
फूल हो तुम मेरी बगिया की, यह कह माली ने पाला था।
विश्वास के छल में आ, दूजे हाथों में उसे डाला था।
उर्वर भूमि की गोद में, जो दिल कभी मुस्काया था।
मरुभूमि की तपिश ने, उस मन को झुलसाया था।
राम समझ जिस विध्वंशी को, वरमाला पहनाया था।
उसी ने दामन खींच सभा में, दुशासन कृत्य दुहराया था।
मुख तक आकर चीख रुक गयी, दिल ऐसा घबराया था।
हृदयशून्य उस दानव की हंसी ने, तन-मन थर्राया था।
नायक का भ्रमजाल बिछा, वो खलनायक जब आया था।
टुटे तारे सी गिरी क्षित्तिज पर, कभी जिसने नभ चमकाया था।
तन के घाव तो भर चले, पर मन ने तड़पाया था।
अब न्याय करेगा कौन सोचकर अश्रु को छलकाया था।
तब हृदयविदारक पीड़ा सुन, वो कृष्णा धरती पर आया था।