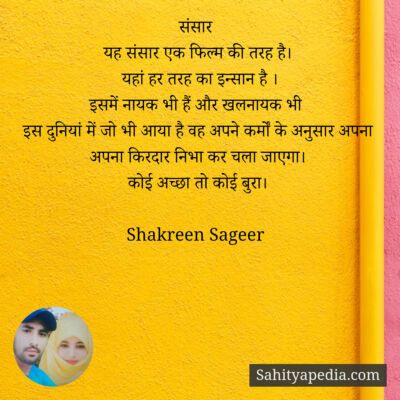“मन का चोर”
“मन का चोर” दो भागों में रची कविता है जिसमें एक बाहरी चोर और दूसरी कविता में चोर भीतर का ही है पर एक बात जो दोनों में है वह यह कि डर चोर को लगा ही रहता है कि पकड़ा न जाऊँ :-
————————-
“मन का चोर”-“१”
————————-
बहुत दिनों से थी
खटपट खटपट
मन के भीतर
झांका कई बार
कुछ आया नहीं नज़र
फिर कुछ खटका
चंद दिनों के बाद
मैनें भी ठान लिया
चोर अब पकड़ा
तब पकड़ा
घुसा मन में
पिछवाड़े से
चुप के से
पकड़ लिया
दबोच लिया
गर्दन से
अंधेरे कोने में छिपे
चोर को
पूछा क्यों आये
तुम ,जैसे काले साये
है मेरे पास क्या जिसे तुम चुरा पाये
कुछ बेलगाम विचार हैं
भटकते इधर से उधर
नहीं है दुर्विचार
किसी के प्रति
शंकायें है मन में दुबकी
डरी सी सहमी सी
साध लेता हूँ कभी कभी
कहीं खोट मिला?
नहीं न !
बस खाया हुआ चोट मिला।
निशान लिये,
बेचैन हुआ मन !
ख़ाली है मन मेरा ,कोरा
माँग लेते तो दे देता
यूँ ही
देख लो
खंगालो
जो भी है इसके अंदर
तुम्हारे काम यदि कुछ आ सके
खुला है मन मेरा
तंग नहीं है ज़रा
देख लिया न तुमने हर कोना
मेरे मन के चोर।
————————-
राजेश”ललित”शर्मा
————————–
“मन का चोर”—-२
————————
मन में चोर हो तो
क्या कुछ
अच्छा लगता है?
डरा डरा रहता है?
हल्की सी आवाज़
या करे धीमे से कोई बात
शंकित रहता है मन ?
आशंकाओं के बादलों में
गरजते /टकराते शब्द
जैसे अनकहे गूँजते कानों में
मेंह बरसता आँखों से
जैसे झरझर निर्झर
मन में बैठा चोर
समझता कोई है
और भी ,यहीं कहीं।
विचलित होता रहता
चौकन्ना हो कर /अंधेरे का अभ्यस्त
तलाशता नये से अवसर
बचने के/लपकने के
दूसरे की जो भी हो
ले जाऊँ उसे ही उठा कर
रहता सदा ही
मेरे मन में बैठा चोर
————————
राजेश”ललित”शर्मा
.