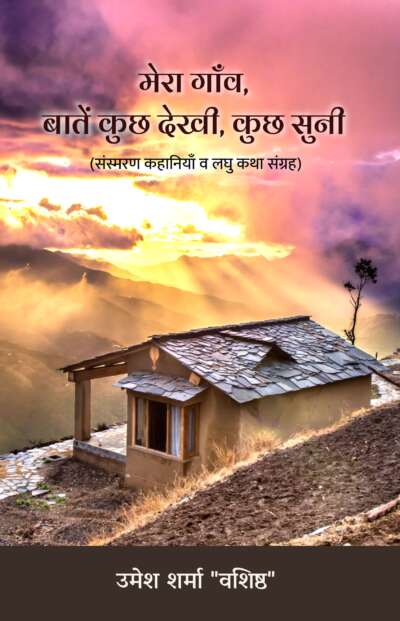मझली दीदी
बचपन में माँ द्वारा दी जाने वाली अक्षरज्ञान की दीक्षा के असफल प्रयासों की हताशा के बाद जब उनकी ये चिंता प्रबल होने लगी कि उनका ये नालायक पुत्र शायद अनपढ़ ही रहेगा तो फिर आखिरी उम्मीद के तौर पर मुझे अपनी दबंग मझली दीदी के संरक्षण में मजबूरी के तहत सुपुर्द कर दिया गया, जो उस वक़्त खुद ८ वीं या नौवीं की छात्रा रही होंगी।
इस कदम के बाद से ही, मुझे अपने शुरू होने वाले बुरे दिनों की आहट एक दम साफ सुनाई देने लगी थी।
माँ के अथक प्रयासों के बावजूद मैं रोते, बिलखते और कभी मौन प्रतिवाद में बड़ता(स्लेट पेंसिल) चबाते चबाते विगत छह महीनों में सिर्फ “च” लिखने तक ही पहुंच पाया था।
मेरे तेजी से साक्षर होने के इस प्रतिरोध का सबसे मजबूत संबल मुझे मेरी दादी से प्राप्त था, जो सबसे छोटे पोते पर अपना सारा प्यार लुटाकर, कहीं अपना भी बचपन मेरे साथ जी रही थी और मुझ पर अपना एकक्षत्र अधिकार जमा बैठी थी।
मझली दीदी के इस नए पदभार ग्रहण करने के पश्चात से ही कुछ दिनों तक घर में एक गृहयुद्ध का सा माहौल बना रहा।
दीदी और दादी दोनों प्रतिद्वंदियों की तरह मैदान में उतर आए थे मुझ पर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए।
खैर, कुछ अनकही शर्तो के साथ मौखिक समझौतों के हस्ताक्षर के बाद घर में थोड़ी शांति बहाल होनी शुरू हो गयी थी।
ये बिल्कुल आज के हॉन्गकॉन्ग का चीन में विलय जैसा था।
मुझे भी स्पष्ट आभास हो चला था कि अब जिंदगी की सारी बेफिक्री और स्वछंदता पर लगाम तेजी से कसने वाली है।
मेरे नए आका के मजबूती से टिके शुरुआती दो चार थप्पड़ों के बाद, बची खुची गलतफहमी ने विदा लेते वक्त अपनी भर आयी आंखों से ये संकेत भी दे दिया था कि अब सुधरने के अलावा कोई और रास्ता शेष नहीं बचा है।
धीरे धीरे मैं भी इसे अपनी नियति मान कर , बोझिल कदमो से ही सही, मदारी की डुगडुगी बजते ही, अपना पढ़ाई का बस्ता लेकर उनके पास जाकर पढ़ने बैठ ही जाता था।पढ़ने लिखने लिए अब राजी हो जाना , थप्पड़ों से दूरी बना कर चलने के लिए उठाया गया सुरक्षात्मक मजबूर कदम था।
अब वो जमाना लद चुका था कि माँ के पढ़ाते वक़्त कुछ खरी खोटी की आवाज़ से दादी का हस्तक्षेप शुरू हो पाता।
मेरा बीच बीच में रोना धोना सुनकर दादी एक योद्धा की तरह मैदान में उतरती भी तो, उन्हें समझौते की याद दिलाकर चुप करा दिया जाता, ये कह कर कि इसकी पढ़ाई के समय किसी की भी कोई सुनवाई नहीं होगी और न ही किसी किस्म की रियायत की कोई गुंजाइश है।
दादी का, उनको घर से निकालने का अनास्था प्रस्ताव भी जब पारित नहीं हो पाया और माँ ने भी अपनी बेबसी दिखाई कि इसको अभी शादी करके ससुराल भी नहीं भेजा जा सकता क्योंकि अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है।
तो दादी के पास , भगवान से रातोरात उन्हें बड़ा करके शीघ्र ही ससुराल भेज देने की प्रार्थना ही बची थी, जिसकी अब वो दिन रात माला जपती रहती।
मैं भी समझ गया दादी अब कहानियां सुनाने और पढ़ने के बाद सुबकता देखकर अपने गल्ले से कुछ पैसे देने के लिए रह गयी है।
दादी के कतरे हुए अधिकार अब मुझको उनके बैठने की जगह के पास बने आले में नज़र आते थे।
मेरी कल्पना कुछ ऐसा ही कहती थी, उस खाली पड़े आले में रखने को भी कुछ तो होना चाहिए था। जिन्हें मैं उदास नज़रों से एक टीस के साथ देख लिया करता था।
मझली दीदी वैसे उनका पूरा ख्याल रखती थी, घर में खाना बनते ही सबसे पहले उनको खाना खिलाना, पूजा करके उठते ही चाय देना, रात में पीने के लिए पानी गर्म कर के उनके सिराहने के पास रखना, पर इन सब से वो कहाँ खुश होने वाली थी।
पिताजी को दो चार महीनों में ही अपने इस तोते के गले में दीदी के पढ़ाये हुए सारे सबक सुनने को मिले, तो उन्होंने खुश होकर मेरा पहली कक्षा मे दाखिला करवा दिया।
कहाँ “च” पे अटका उनका नकारा बेटा अब थोड़ा तेजी से सुधर रहा था। माँ ने भी एक लंबी चैन की सांस ली।
बीच बीच में, थोड़ा फुदकने और ढील लेने की कोशिश में, जीते हुए कंचे कुएं के सुपुर्द कर दिए जाते।
फिर तो धीरे धीरे, पास के मैदान में खेलते हुए भी, अगर घर के दरवाजे पर वो दिख जाती , तो आंखे खुद ही चक्षु:श्रवा हो जाती, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सीधे घर की ओर दौड़ पड़ता था।
एक बार ननकू चाचा की पान की दुकान से घर के लिए कुछ पान लेने गया, तो उनके एक दो सहपाठी वहाँ खड़े दिखे, एक मेरी तरफ देख दूसरे को बोला, बच्चे को थोड़ी जगह दो, अपनी दीदी का छोटा भाई है,
मैं सोच में पड़ गया, ये तो उसका सहपाठी है, ये क्यों उनको दीदी कह रहा है, फिर समझ में आया कि उनका रुतबा घर की तरह अपनी कक्षा में भी चलता है, और सहपाठी भी उनकी अक्ल और समझदारी का लोहा मानकर अपने से कद में बड़ा समझ कर इज्जत देने के लिए शायद दीदी कह बैठा था।
उनके द्वारा मुझे दी गयी इस प्राथमिकता ने एक गर्व का अहसास दिया और ये भी कि मैं एकदम सही गुरु की देख रेख में हूँ।
दीदी के कई सहपाठी उनकी कॉपियां लेकर अपनी कॉपियों से मिलान कर लेते थे,कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो बिल्कुल सही होगा।
बचपन में इन सब बातों को अनजाने में गौर से देखता रहता था।
दीदी का पढ़ाने का अपना अंदाज था, गणित के अलावा सब विषयों में किसी भी अध्याय के कठिन शब्द का मतलब बताकर उन्हें अलग से लिखने को कहती। शब्द के बगल में सरल भाषा में उसका का अर्थ लिखवाती। फिर उस अध्याय के संभावित प्रश्नों का उत्तर शुरू शुरू में अपनी भाषा में खुद लिखवाती और याद करने को कहती। दूसरे दिन, उस प्रश्न के उत्तर को पहले मुँहजबानी सुनाना पड़ता ,फिर उसको लिखकर भी दिखाना पड़ता।
धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कहती पहले तुम किसी प्रश्न का उत्तर पुस्तक देखकर खुद तैयार करो, उसमें कुछ सुधार की जरूरत होती तो बताती कि इसको इस तरह से लिखो।
जब मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने अच्छे अंको से उत्तीर्ण कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आना जाना पड़ता, ये उस वक़्त की मान्यताओं के खिलाफ था।
उनके बगावत के स्वर, घर की मान मर्यादा की बोझ तले कहीँ दब से गए।
अपने लड़की होने का ये बेहद दुखद अनुभव रहा उनके लिए।
एक बार पढ़ाते हुए बोल बैठी,
कि जैसे उनके हाथ पांव काट कर उन्हें घर पर बैठा दिया गया है। मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि वे कॉलेज क्यों नहीं जा सकती, माँ से मैंने पूछा भी था, पर वो भी पुरानी परंपराओं के आगे विवश दिखीं।
धीरे धीरे उन्होंने भी परिस्थितियों से समझौता करना शुरू कर ही दिया।
अब उनके पास घर के काम काज में माँ की मदद करने और अपने छोटे भाई की शिक्षा की जिम्मेदारी के अलावा अपने लिए कुछ भी नहीं बचा था।
दोपहर को कामकाज निपटा कर पेट के बल लेटकर बिस्तर पर तरह तरह की पुस्तकें पढ़ते रोज दिखती थी, दिन के वक़्त सोना उनकी आदत नहीं थी। घर के चाय के एक पुराने बड़े बक्से में उनका एक पुस्तकालय था, घर का कोई भी सदस्य हो, लायी हुई किताबें संभाल कर उनके पुस्तकालय में जमा हो जाती थीं।
एक बार उन्होंने मुझे “रूसी लोक कथाएं” पढ़ने को दी। इसके बाद धीरे धीरे ऐसी छोटी मोटी रियायतें मिलती गयी।
कक्षा में प्रथम आने पर मिठाई खिलाने के बाद, अपने बचाये हुए पैसों में से दो रुपये भी उनसे मिलते थे कोई अच्छी फिल्म देखने के लिए, ये भी वो तय करती थी कौन सी फ़िल्म देखनी है। इस पुरस्कार की हर वर्ष प्रतीक्षा रहती थी।
बिनाका गीतमाला के कई वर्षों तक के, एक से सोलह पायदान में आने वाले गाने सुन सुन कर अपनी एक कॉपी मे नोट करना उनका एक और शौक था।
चौके में काम करते करते ये गाने गुनगुनाती अक्सर दिख जाती थी। चौके में आसन पर बैठा, उनका चेला भी पढ़ाई करते करते उनकी धुनों पर नजरें बचाकर गर्दन हिला ही लेता था।
भाभियां गाना सुनते वक़्त, ट्यून बजते ही ये अनुमान लगाने के लिये दीदी को तकती, फिर दीदी गाने का मुखड़ा बता देती।
उनसे कई वर्ष बड़े घर के सदस्य भी, उनकी राय को ध्यान से सुनते थे, माँ तो उनसे पूछे बगैर कोई निर्णय लेती ही नहीं थी। दादी अक्सर बोल पड़ती, इसके घर में तो इसकी बेटी की ही चलती है।
ये भी एक विरोधाभास दिखा, कि दादी घर के सारे बड़े निर्णय खुद लेती थीं, यहाँ तक कि भोले भाले विद्वान दादाजी भी उनसे तर्क करने से दूर ही रहना पसंद करते थे, पर दादी को दीदी को दी जाने वाली तरजीह कुछ कम जँचती थी।
जो बातें स्वयं के लिए ,व्यक्तित्व की सक्षमता के कारण जायज मालूम होती है, किसी दूसरे को वही महत्व मिलता देख ये बात फिर गलत लगने लगती है।
ये खीज कभी कभी बातों में झलक पड़ती थी, मसलन दोपहर में दादाजी और दादी को खाना खिलाकर, जब दीदी चौके से निकल जाती थी, तो फिर शाम से पहले उधर का रुख भी नहीं करती थी,
मझला भाई, जो उनसे दो तीन साल छोटा था, इसका फायदा उठाकर, उनके चेहरे पर लगाने को रखी मलाई पर हाथ साफ कर जाता था। कभी शामिल होने का प्रलोभन मिलने पर, मैं साफ मुकर जाता,अपने गुरु के साथ धोखाघड़ी करने को मैं कतई राजी नहीं था।
इस बात पर दोनों में फिर जम कर झगड़ा होता।
दो तीन घंटो का ये वक़्त उनका खुद के लिए होता, जहां वो अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती, इस बीच यदा कदा एक अंगूठा उनके मुंह में बच्चों की तरह छुप कर बैठा रहता। बस इतना सा बचपना किसी कोने में था उनके अंदर।
किसी सदस्य के फिर खाना मांगने पर, कोई और ही उठ कर खाना परोस कर लाता। दादी ये मौका हाथ आया देख, बोलने से नहीं चूकती, भई महाराज तो खाना बनाकर चला गया है, अब जिसको खाना हो या तो खुद परोस ले, नहीं तो कोई और परोस के दे, ये तो अब तीन घंटे अपनी किताबों में डूबी रहने वाली है।
बीच बीच में आये तेज गति के इस बाउंसर को पूरा सम्मान देकर दीदी चुप रह जाती, जैसे कि सुना ही नहीं।
मेरे परीक्षाफल का हर साल बेसब्री से उनको इंतजार रहता कि उनकी साल भर की माथा पच्ची का आखिर क्या बना?
तब तक उनका सिखाया पढ़ाया शिष्य भी कक्षा में बढ़ती अपनी इज्जत को भी थोड़ी बहुत समझ बैठा था।
पढाई के दौरान होने वाली हिंसक घटनाएं भी अब कम होने लगी थी। कभी कभार एक आध चपत बस अभ्यास के लिए होती थी, कि आदत बनी रहनी चाहिए।
१९७८ का साल मेरे लिए बहुत बुरा गुजरा, दादी अपनी लंबी उम्र गुज़ारने के बाद, दादाजी से मिलने के लिए, हम सब को रोता हुआ छोड़ गई और कुछ महीनों के बाद अब दीदी के ससुराल जाने की बारी थी।
जून के महीने में ,संचालकों के खुद के झगड़े के कारण, धर्मशाला न मिल पाने की वजह से, बारात को फिर उसी विद्यालय में ठहराया गया जिससे वो पढ़ कर निकली थीं और मैं भी अपनी कक्षाओं की डेस्क और बेंच हटाने में मदद करता, अपनी आंखें छलकने से रोक नहीं पाया।
मेरे सकून की दो पनाहगाहें एक साथ मुझसे छिन गयी थीं।
आगे का सफर अब ११ वर्ष की उम्र में कमोबेश खुद ही तय करना था। पढ़ाई में मदद करने को तो खैर और भी लोग थे घर में ,पर ये कमी कहाँ पूरी हो पाती।
अब सिर्फ खतों का इंतजार रहता था, जो मेरे बारे मे जरूर पूछते थे, इसलिए खत आने से ,जवाब देने के वक़्त तक, मैं एक दम अच्छे बच्चे का रूप धारण कर लेता था ताकि उन तक कोई शिकायत न पहुँच जाए।
माँ के पास मुझको नियंत्रण में रखने का यही एक मात्र ब्रम्हास्त्र बचा था, जिसे चलाने की धमकी देकर जब चाहे मुझ पर काबू पा सकती थी।
उनके ससुराल से लौटने के एक महीने पहले से ही मेरी मासूम बच्चे में तब्दील होने की कवायद भी शुरू हो जाती।
जानवर और इंसान की आदत ठीक एक जैसी ही होती है, किसी एक का साया वो अपने सर पर मजबूती से पकड़े रखना चाहता है। एक सुरक्षित आँचल जिंदगी में सचमुच बहुत जरूरी होता है सबके लिए ,खासकर बचपन में!!!
कोलकाता आकर पढ़ाई के दौरान उनको एक पत्र अंग्रेजी में क्या लिख दिया, फौरन जवाब आ पहुँचा और ये ताकीद भी कि पत्र अपनी भाषा में ही लिखा करो।
आज भी घरवाले ये तो बोल ही देते हैं,कि इसको किसी बात पर राजी कराना हो तो मुम्बई में पहले “भाई” से बात करलो, और वो भी इतने दिनों वहाँ रहकर, “अपने को ये समझने का है या फिर बरोबर बरोबर” बोलकर अपनी राय दे ही देती हैं, जो किसी आज्ञा से कम नहीं होती।