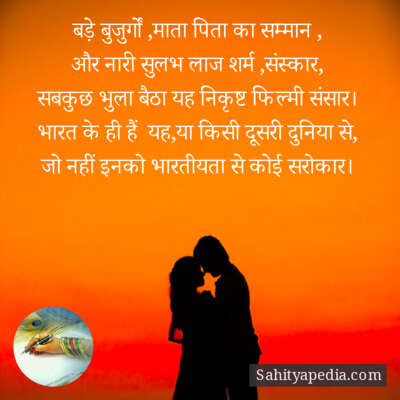*मंज़िल पथिक और माध्यम*

अहले सुबह उठ कर चले गए थे जो,
दरख्तों पर लौट आते हैं परिंदे शाम को,
आसमान उतर आयेगा अपने आंगन की आस में,
हम थे जो घोंसलों से उड़े ही नहीं।
मुट्ठी में लहरों की गर्दनें भींच लेते,
वो उफान जवानी का कि सागर भी सोख लेते,
हम बासिंदे हैं ठहरे पानी के और समंदर की बात करते हैं,
यहां कुएं में लहरें कभी उठी ही नहीं।
कई राहगीर गुजरे इसी रास्ते से,
राह तो वहीं पड़ी है,
क्या वास्ता इसे मंजिलों से।
कई शहर रोशन किए हमने भी,
कई घर के टिम टिम बल्ब हैं जलाए।
अंधेरे उजाड़ बियाबान में
बिजली के खंबे बांहे फैलाए।
मंजिल नहीं हूं,
ना ही पथिक हूं,
माध्यम हूं
औरों के गंतव्यों का।
दुख नहीं कुछ किया नहीं, कुछ बना नहीं,
बोए जो शब्द हैं प्रस्फुटित होंगे,
सुनहले हर्फ चमकेंगे किताबों में,
मैं प्रहरी हूं मेरे काव्यों का।