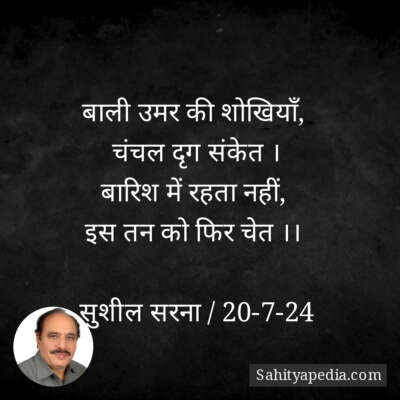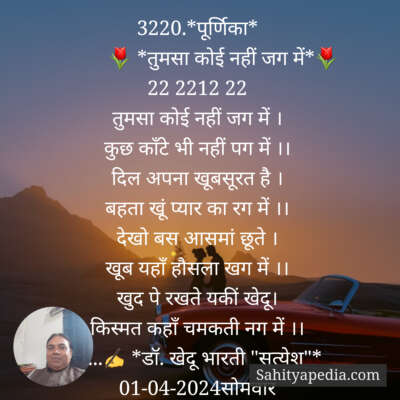“बारात देहाती-मस्त बाराती”
चन्द दिनों पहले की है बात इक़ शादी थी कहीं
यूँ तो साज़ सज्ज़ा थी फ़िर भी बर्बादी थी कहीं
शोरगुल माहौल में ख़ूब ढोल-नगाड़े बज रहे थे
दुल्हा-दुल्हन से ज़्यादा साहब बाराती सज रहे थे
क्या कहें हम फटीचर भी जा पहुँचें कि बुलावा था
देखने लगे चकाचौंध जो कुछ बारात में छलावा था
कुछ कूद रहे थे रस्सी सी कुछ गर्दन हिला रहे थें
वो मजबूरी में थिरकतें दिखे कुछ पांव हिला रहे थें
नशे में डोलते वो शराबी करतब मन को भा रहे थे
कुछ जा रहे थे ज़बरन बैंड पर बेसुरा सा गा रहे थे
इक़ बाराती दूल्हे को अर्जुन समझ जाने लगा था
कृष्ण बनकर मदमस्त हो रथ को चलाने लगा था
कुछ नुमाइश करने लगे कपड़े वपड़े सब उतार कर
हाथापाई भी चल पड़ी नायकी खलनायकी रार कर
बेगानी शादी में बने वो अब्दुल्ला कुछ थक गए थे
अब क्या बतलाए रुपैये उड़ा उड़ाकर वो नप गए थे
दूल्हे के बापू ने फिर शामियाने की तरफ़ इशारा किया
इक़ बार में भला कौन सुनता बेचारे ने दोबारा किया
बारातियों का भूख के मारे बुरा हाल मानो मुहाल था
टूटने को थे आतुर नाश्ते पर जैसे पड़ गया अकाल था
लेखक भी बेगाना था उसे तो जल्दी लौटकर आना था
वो कहाँ विदाई देख पाता उसे लिफ़ाफ़ा देकर आना था
___अजय “अग्यार