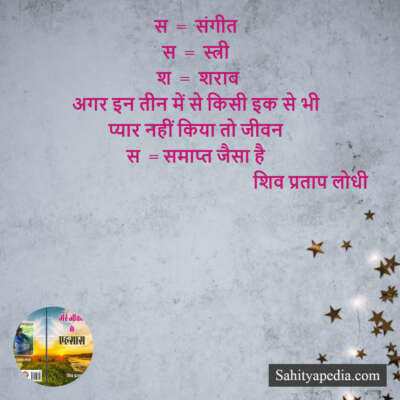पर्वतीय क्षेत्रों से होते पलायन के दर्द से कराहती देवभूमि
देवभूमि उत्तराखण्ड का स्मरण आते ही मन में उत्पन्न हो चुके अशांति के बादल स्वतः ही छँट जाते हैं। कैलाश पर्वत पर सूर्य की प्रथम रश्मि के विहंगम दृश्य का स्मरण एक नवचेतना प्रदान करती है। शान्त जीवन, चारों ओर हरियाली, आकाश को चुनौती देने वाली पर्वतमालायें, प्रत्येक पर्वत पर देवी-देवताओं के मंदिर, मंदिरों में बजने वाले घण्टे, घड़ियाल की मधुर ध्वनि, सुरम्य पहाड़ियों पर बैठे युवक की बांसुरी से आते मधुर तान, सर्पीलाकार पगडंडियाँ, मकानों की खिड़की और दरवाजों के रास्ते अन्दर आते बादल, कल-कल बहता झरने का पानी, शान्त स्वभाव से बहने वाली नदी, एकान्त बीहड़ों में मनुष्य के साथ-साथ रास्ते के किनारे चलते जंगली जानवर आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो देवभूमि की प्राकृतिक और नैसर्गिक छटा को व्यक्त करते हैं।
आरम्भ से ही उत्तराखण्ड में कई सारी समस्यायें विद्यमान रही, कभी उत्तरप्रदेश जैसे वृहद् राज्य का अंग होने से इस पर्वतीय क्षेत्र को विकास के स्वाद से अलग-थलग रखा गया, प्राकृतिक सम्पदा का बेतरतीब दोहन, रोजगार का अभाव, कृषि का बारिश पर निर्भर होना, आधारभूत संसाधनों का अभाव, इत्यादि। पहाड़ों से होता पलायन एवं उससे भी अधिक समस्या मैदानी क्षेत्र में आकर फिर कभी पहाड़ों की सुध न लेना शायद यह एक गंभीर प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। आज विचार करें और कभी वापिस उन वादियों में जायें जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। क्या गर्व करने को कुछ रह जाता है? जिस देव भूमि का स्मरण करते ही मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। आज उसका हाल देखकर एक पीड़ा होती है, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं, मकान की देहरी पर बैठे बूढ़े, माँ-बाप की सूनी आँखें परदेश गए उस बच्चे की राह तक रही है जो पहली बार घर से निकलते समय कई सारे संकल्प, गाँव और मातृभूमि के प्रति पवित्र भाव मन में संजो कर गया था। लेकिन जाने के बाद वापस नहीं लौटा और कभी लौटता भी है तो एक परदेशी पर्यटक बनकर। जिस मडुए की रोटी को वह बड़े चाव से खाता था, परदेश से लौटने के बाद वह उसे देखकर मुँह मोड़ लेता है। यही नहीं पहाड़ के कठोर जीवन एवं विषम परिस्थिति को अभिशाप तक करार दे बैठता है।
आज एक विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हो चुका है कि हम उस देवभूमि अपनी जन्मभूमि को याद कर गौरवान्वित तो होते रहते हैं लेकिन क्या परदेश में बसने के बाद अपने बच्चों को वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, लोकजीवन से रुबरु कराते हैं? क्या हम अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव उत्पन्न करा पाने में सफल हो पाए हैं? आज जब बच्चे अंग्रेजी भाषी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अब तो अन्य विदेशी भाषायें जानने, सीखने की होड़ मच चुकी है क्या कभी घरों में कुमाऊँनी भाषा के विषय में चर्चा हो पाती है? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी कुमाऊँनी भाषा एवं संस्कृति के विषय में बता पा रहे हैं? यहीं नहीं सत्तर-अस्सी या नब्बे के दशक में पहाड़ों से जीवन यापन के लिए मैदानों में आ चुके लोग भी आज आपस में मिलते हैं तो उनके मुँह से कुमाऊँनी भाषा के शब्द नहीं निकल पाते। इतिहास गवाह है यदि किसी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखना है तो उसकी भाषा और बोली को जीवित रखना होगा, जो समाज जितना विकसित होगा वह अपनी भाषा और बोली को नहीं छोड़ेगा। इस तथ्य की पुष्टि मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, इत्यादि के सम्पर्क में आने से स्वतः हो जाती है। इन समाजों के बंधु जब भी आपस में मिलते हैं। चाहे वह किसी भी पद, स्थिति में हो लेकिन बातचीत अपनी भाषा में ही करते नजर आयेंगे।
पहाड़ों से पलायन यद्यपि एक आवश्यकता बन चुका है, क्योंकि जीवनयापन, उच्च शिक्षा एवं उत्थान के लिए यह आवश्यक है लेकिन आने के बाद वहाँ के विषय में न सोचना या सुध न लेना यह निश्चित तौर पर दर्द देने वाला है। आज कमोबेश यही स्थिति है, पहाड़ों से उतरकर मैदान में पाँव रखते ही मानसिकता बदल जा रही है, जिस खुली हवा में पहली साँस ली जाती है, जिन पगडंड़ियों पर चलकर आरभिक जीवन आरम्भ किया था, जिन नौहल्लों का पानी अमृत रूप मानकर पीया था, जिन घाटियों में सूर्य का प्रकाश जाने पर घड़ी देखने की जरुरत नहीं पड़ती थी। खुद ब खुद समय का अंदाज हो जाता था। हिसालु, किलमौड़ और काफल देखते ही मुँह में पानी भर आया करता था। क्या परदेश जाने के पश्चात् यह सब सपना जैसा हो जाता है? यहाँ यह भी सत्य है कि पलायन यदि भावी जीवन के उत्थान एवं विकास के लिए आवश्यक है तो अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही आवश्यक है, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम, गर्व व सम्मान का भाव मन में होना आवश्यक है भगवान रामचन्द्र जी कहते हैं:
‘‘जननी जन्म भूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी’’
हमारे पास अपनी जन्मभूमि पर गर्व करने को बहुत कुछ है। सहयोगात्मक भावना, आपसी प्रेमभाव, दूसरों को भी अपना बना लेने की कला, पवित्रता, निश्छलता, प्रकृति का सौन्दर्य, कठोर परिश्रम, त्याग इत्यादि अनेको ऐसी विशिष्टतायें मौजूद हैं जो हमें अन्य से विशिष्ट बनाती है। आज भी परिश्रम, ईमानदारी, सहृदयता के लिए पर्वतीय क्षेत्र के नागरिकों के प्रति सम्मान की भावना से देखा जाता है। यह क्या यह हमारे लिए गर्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों में जितने भी चारित्रिक विशिष्टतायें विद्यमान हैं वह देवभूमि के कारण हैं जो सदैव परोपकार की भावना को धारण कर चलती है। किसी एक के घर में कोई आयोजन होने पर वह एक का नहीं रह जाता, उसके सफल आयोजन की जिम्मेदारी सभी की हो जाती है। सहयोगात्मक रूप से प्रत्येक त्यौहार को मनाना, खुशियों में सबको सम्मिलित कर लेना, दुःख के समय दुखियारे को अकेला न छोड़ना, आपसी सहयोग से फसल बोना, रोपाई करना, कटाई करना यह सहयोगात्मक व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण है। किसी के घर में पुरुष नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है तो गाँव के ही अन्य लोगों द्वारा सहयोग देकर उसका काम करना एक पवित्र भावना को दर्शाता है, भले ही कितने अभाव में हों लेकिन लोगों में संतोषी प्रकृति के चलते वह अभाव हावी नहीं होते, यहाँ तक कि प्रकृति में भी वह सहयोगात्मक गुण मौजूद है। जंगल में मौजूद पेड़ों को देखकर आभास होता है कि एक बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को बढ़ने से रोक नहीं रहा बल्कि एक ही दिशा में एक ही उद्देश्य को लेकर क्या बड़े, क्या छोटे सभी पेड़ बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजाति के पशु-पक्षियों में आपसी तालमेल और सामंजस्य देखा जा सकता है।
आज सर्वाधिक आवश्यकता यदि है तो वह है अपनी जन्मभूमि पर गर्व करने की, वहाँ के तीज-त्यौहार, मेले, धार्मिक स्थल, इतिहास, संस्कृति के सम्बन्ध में भावी पीढ़ी को बताया जाए, उत्तरायणी कौतिक एवं अन्य सांस्कृतिक आयोजन इस दिशा में सराहनीय प्रयास है, इसके अतिरिक्त पहाड़ों से आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कर चुके उन शिक्षण शालाओं से सम्पर्क कर ऐलुमिनी मीट जैसे आयोजन भी करवा सकते हैं। गाँव की आवश्यकताओं के मद्देनजर वहाँ से बाहर निकल चुके लोगों से सम्पर्क कर समन्वित रूप से सहयोग करने की योजनायें बनानी होंगी। वैसा रहने दें, जो जैसा है हम क्या कर सकते हैं, गाँव में कुरीतियाँ आ चुकी है, हमारे करने या न करने से क्या होने वाला है? गाँव में हमारी सुनता ही कौन है? यह उपेक्षापूर्ण भावना जब तक रहेगी तब तक पहाड़ आँसू बहाता रहेगा, किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी अन्यथा आने वाले दस-बीस वर्षों में खंण्डर हो चुके मकानों के पत्थर भी नहीं मिलेंगे और वहाँ जाने पर ढूढ़ना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा मकान कौन-सा है? किस जगह हमने पहली बार आँखें खोली थी। वह थान कहाँ है जहाँ जाकर दीया बाती करते थे? यदि समय रहते नहीं चेते तो ऐसी अनेक परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ सकता है।
पहाड़ों से होते पलायन के दर्द एवं देहरी में बैठे बूढ़े माँ-बाप की आँखों में उतर आए दर्द का बयां मैंने मेरे नव प्रकाशित उपन्यास ‘वसीयत’ में करने का प्रयास किया है, जिसमें एक ओर पहाड़ों से पलायन का उल्लेख है वहीं परदेश गए बेटे के इंतजार में बैठे माँ-बाप का दर्द झलकेगा। लेकिन आज भी अपनी जन्मभूमि पर गर्व करने को बहुत कुछ है, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, एकता व सहयोग का भाव यह सब कुछ समेटने का प्रयास भी किया गया है। देश के अन्य प्रान्तों एवं अन्य भाषायी लोगों का उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक एवं प्रकृति के अनछूए पहलुओं से यह उपन्यास साक्षात्कार कराने में सफल होगा। साथ ही पलायन से उत्पन्न समस्याओं का किस प्रकार समन्वित रूप से प्रयास कर दूर करने का प्रयास किया जा सकता है यह भी उपन्यास के उत्तरार्द्ध में उल्लेखित करने का प्रयास किया गया है।
डॉ. सूरज सिंह नेगी
लेखक, कहानीकार एवं उपन्यासकार
मोबाईल नं0 9660119122