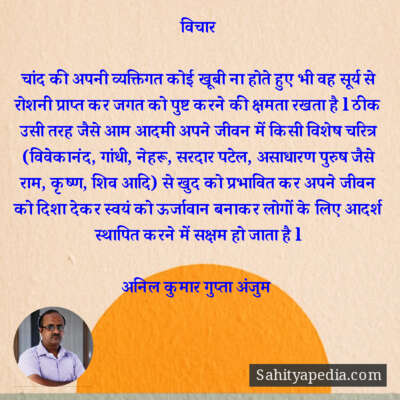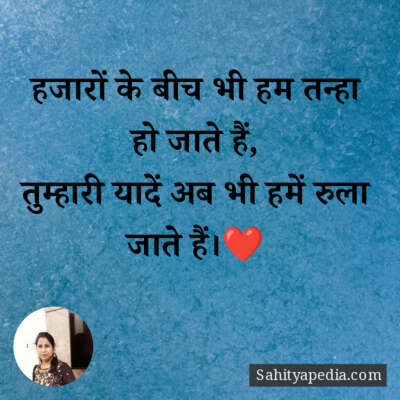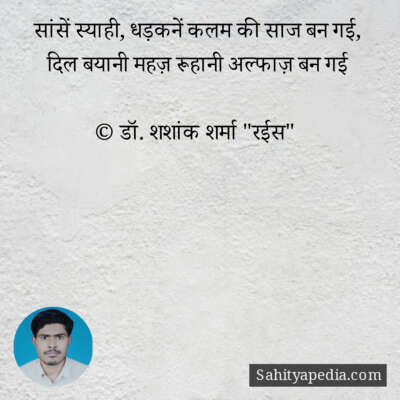पढ़ने की रंगीन कला / MUSAFIR BAITHA

‘जनसत्ता’ में ‘दुनिया मेरे आगे’ स्तभ में मेरा यह आलेख/व्यंग्य Monday, 21 October 2013 को छपा था :
बिहार में एक लोकल ट्रेन में सफर का अनुभव किसी के लिए खास भी हो सकता है। मेरे लिए भी हुआ। पर अपना अनुभव साझा करने से पहले पढ़ने के एक तरीके पर एक बात!
पुस्तकों को पढ़ने वाले कुछ थूक-अभ्यासी लोग भी होते हैं जो अपनी जीभ पर तारी लार या तरल द्रव्य से अपनी तर्जनी के अग्र भाग को भिगो कर पन्ना पलटने में उसके प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। जो पन्ने सहज ही उलटने-पलटने को तैयार नहीं होते, उन्हें यह तरलता मना लेती है। जब आपकी जीभ रंगी होगी तो स्वाभाविक रूप से उसकी तरलता का प्रभाव भी उसके योग से उलटे पन्ने पर रंगीन-मिजाज ही पहुंचेगा! जैसे, कोई पान खाकर अगर इस उलट-पुलट के कार्य को अंजाम दे तो परिणाम बेशक टहटह लाल, यानी रंगीन असर का होगा!
उस यात्रा में मेरा सहयात्री भी पान चबा रहा था। लिखंत-पढ़ंत के प्रति आम उदासीनता के इस घोर कलि-काल में अधेड़ अवस्था, मगर पढ़ने की ललक बाकी। मेरे लिए तो यह इत्मीनान से अधिक सुखद आश्चर्य की बात थी इस यात्रा-संहाती में! मैं सफर को सहज काट्य बनाने और बोरियत-रहित करने के लिए आमतौर पर पुस्तकों-पत्रिकाओं को उपादान बनाता हूं। इस बार ‘इंडिया टुडे’ इस भूमिका में थी। सुबह की ‘पीजी भौजी’ (गौतम सान्याल की ‘हंस’ में प्रकाशित एक कहानी में कथा समेत पटना-गया लोकल डीएमयू ट्रेन को यही नाम मिला है) को पटना जंक्शन से गया जाने के लिए पकड़ा था। ट्रेन के मीठापुर बाइपास फ्लाईओवर से आगे निकलने और पटना शहर के सघन नगरीय हिस्से के पीछे छूटने के साथ ही मैंने अपने दफ्तर के थैले से पत्रिका निकाल कर उसमें अपनी आंखें गड़ा दीं। सहयात्री खिड़की पर था और मैं उसकी बगल में। वह पिच्च-पिच्च थूक कर बार-बार अपनी पान-पीक गाड़ी-बाहर कर रहा था। जब उसके मुंह से पीक लगभग नि:शेष हो गया और अभी ठोस पदार्थ अंदर ही था तो यह पदार्थ, यानी पान की गिल्लोरी मुंह में दाबे और मुंह चबर-चबर चलाते हुए वे भी अपना सिर मेरे ही साथ मेरी पत्रिका में घुसेड़ कर अध्ययन में प्रयासपूर्वक दाखिल हो गए! उनकी यह ‘मान न मान, मैं तेरा मेहमान’ वाली कार्रवाई मुझे बेहद असहज कर रही थी। थी तो यह अतिरेकी अध्ययन-उत्सुकता, एक असभ्यता का नमूना, पर इधर से भी समभाव तो नहीं हुआ जा सकता था न!
मेरे प्रत्युत्पन्नमतित्व ने यहां काम किया और मैंने झट पत्रिका उस बेकरार बगलगीर को ही थमा देने में भलाई समझी। वह अनन्य पाठक बिना किसी ना-नुकर के, बल्कि मुखड़े पर हुलस के छींटे जाहिर करते हुए, ‘बस, थोड़ी देर में लौटाता हूं’, का आश्वासन थमा कर पढ़ने में मगन हो गया और मैं खिड़की से बाहर के दृश्य झांकने में। मगर यदा-कदा मेरी निगाहें तो पत्रिका की तरफ चली ही जा रही थीं। अचानक देखा कि जनाब पत्रिका को अंगुली के सहारे अपनी जीभ से उधार ली रंगीनी का बार-बार इस्तेमाल बड़े इत्मीनान से पन्ना पलटने में किए जा रहे हैं। देखते-देखते पत्रिका के अधिकतर पन्नों पर रंगीनी का पुरजोर असर दिखने लगा।
जब मन भर अपनी अनोखी जिह्वा-सह-हस्त कला का प्रदर्शन और पत्रिका-पठन का कार्य उन्होंने पूरा कर लिया और उनका गंतव्य स्टेशन अब अगला ही था, तो उतरने की गरज से अपनी सीट छोड़ते हुए धन्यवाद की औपचारिकता के साथ विहंसित-मुख वे पत्रिका लौटाने को मेरी तरफ मुखातिब हुए। मैंने पत्रिका को छुआ भर, उनके हाथों में ही रहने दिया और कहा- ‘भाई साहब! खैर, पत्रिका पढ़ तो नहीं पाया था मैंने, उलटाया भर था, पर अब यह आपके रंग में रंग कर आपके पास ही रहने की अधिकारिणी हो गई है। आप निस्संकोच इसे अपने साथ लेते जाएं।’ यह सुनते ही उनका चेहरा विस्मय, शर्म और संकोच भरे आवरण से आच्छादित हो गया, जिसमें कुछ अंदरूनी आक्रोशजनित तनाव के तत्त्व भी सम्मिलित थे।
एकबारगी मेरी तरफ से हुई इस प्रतिक्रिया के लिए वे बिल्कुल तैयार न थे। डिब्बे में आसपास बैठे कुछ लोगों की निगाहें भी हमारे संवाद पर थीं। माजरा वे बखूबी महसूस रहे थे। उन्होंने झिझक के साथ अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब से पत्रिका की कीमत के बराबर मूल्य के दो छुट्टे नोट निकाले और मेरी ओर बढ़ा दिए। मैंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा- ‘भाई साहब! कृपया अन्यथा न लें। पत्रिका मैं बेचने के लिए थोड़े ही खरीदता हूं! और जैसा कि मैं समझता हूं, आपको पत्रिका दाम देकर ही पढ़ने में अभिरुचि रहती तो आप इस तरह से नहीं पढ़ते।’ इस बात-बहस बीच ट्रेन धीमी होने लगी थी। आगे कुछ बतियाने-समझाने के लिए भाई साहब के पास वक्त भी नहीं बचा था। वे अलविदा का संकेत कर ट्रेन के दरवाजे की तरफ हड़बड़ा कर बढ़ गए। पता नहीं, बाद में भी उन्होंने मुफ्त पढ़ने की वह आदत, खासकर, अजनबियों के साथ अपनी रंगीन-असर वाली, बदली कि नहीं!