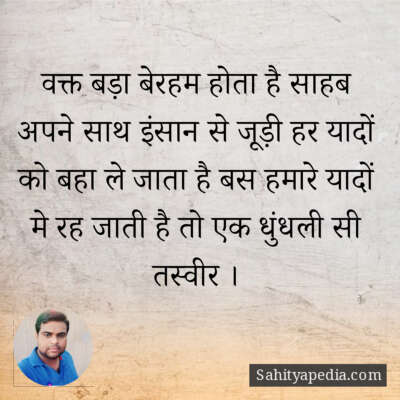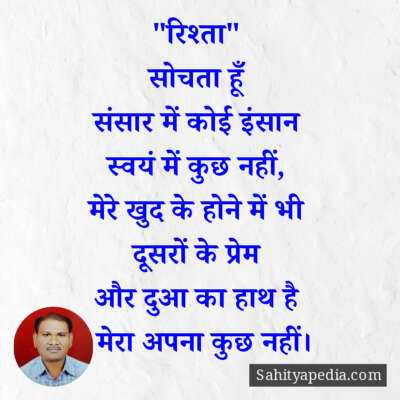न हम सभ्य हो पाए न समाज बन पाए
न हम नागरिक हो पाए
न हम आदमी बन पाए
असभ्य बर्बर
आदिम खानाबदोश
जनजातियाँ
हम से बेहतर थीं
कपड़े नही थे
लेकिन आबरू महफूज थी
संसाधन नही थे
लेकिन सम्वेदनाएँ मौजूद थीं
आज
लिबासों को चीर कर
जिस्म को छेदा जा रहा है
बोटियों को तोड़कर
चमड़ी को भेदा जा रहा है
न हम इंसान हो पाए
न हम समूह बन पाए
विकास की अंधी दौड़ में
भाग रही
बदहवास भीड़
बन कर रह गए हैं हम
इस अंधी दौड़ में
कोई आगे दौड़ रहा है
कोई पीछे छूट गया है
कोई भाग रहा है
कोई घुटनों के बल चल रहा है
बदहवास भागती
इसी भीड़ में
कुछ वो हैं जो
संसाधनों के शिखर पर
विराजमान हैं
और
अपनी भावी संततियों के लिए
रुपये का पेड़ बो रहे हैं
इन्ही में
कुछ वो भी हैं जो
बिखर चुके ख्वाबों के
बचे खुचे अवशेषों को साथ लेकर
रीढ़विहीन जिंदगियों को ढो रहे हैं
न हम सभ्य हो पाए
न समाज बन पाए
-शकील प्रेम