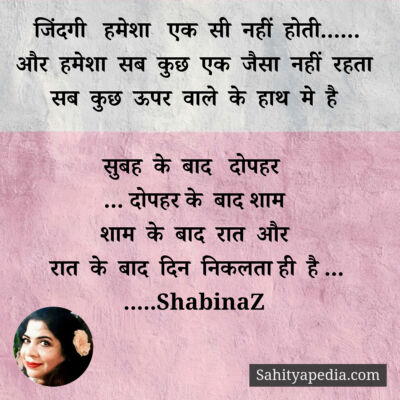न तो कोई साथी अपना न कोई हमदर्द
चली सफारी धूल उड़ाती दे आँखों में गर्द
एसी बोगी क्या जाने जनरल डिब्बे का दर्द
लाज लूटकर किसी बहन की चले गए कामांध
लगा मुखौटे खड़े थे हिंजड़े कहते खुद को मर्द
देख बदलती परिभाषाएं रोए दास कबीर
सम्पूर्ण वस्त्र वाले असभ्य और सभ्य हुए बेपर्द
उम्मीदों की चिता जली हर ओर धुंवा के चर्चे
रोयीं रातें आंसू भर-भर आँखें हो गयीं ज़र्द
मुझको तो कंपाकर चली गयी वो शीतलहर की रात
तेरी बाहों में पिघल गया जाने क्यों मौसम सर्द
सपनों सरीखी इस दुनिया में भटक रहा ‘संजय’
न तो कोई साथी अपना न कोई हमदर्द