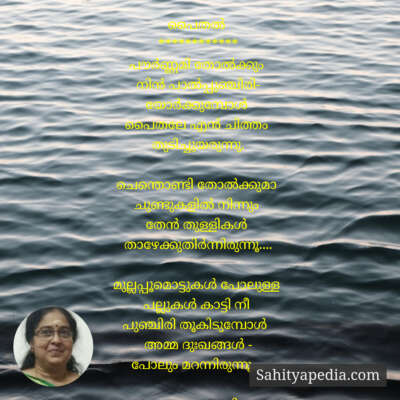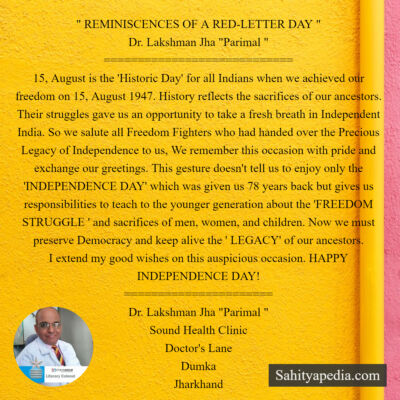नारी
जिसने नारी को देवी माना, हम उस धरा की बेटी हैं
बदल गया लेकिन अब क्या जो आज कफ़न में लेटी हैं…
तेरी अस्मिता की बात लगती क्या तुझे ही गौण है
तेरी कलम की धार ही बस बोल अब क्यूँ मौन है..
सिसकियाँ जो हैं गले में, चीखती तू क्यूँ नहीं
कल को तेरा ही आँचल ये छीन लें ना फिर कहीं..
जिनको पैदा करती हम, हम दुनिया दिखलाती हैं
कोख़ से लेकर गोदी तक इनका बोझ उठाती हैं..
वही एक दिन वहशी बनकर नोंच रहे हैं जिस्म तेरा
भूल गयी क्यूँ तूने ही था कभी ‘काली’ का रूप धरा..
कहने को ये धरती को भी माँ कहकर बुलाते हैं
पर अपने वहशीपन में माँ ही की कोख लजाते हैं
जिस्म नोंचकर भेड़िये फिर ओट धर्म की लेते हैं
पागल है जैसे जननी इनकी, धोखा किसको देते हैं…
अलग तो इनसे धर्म नहीं है, इस दुनिया में नारी का
फिर क्यूँ सीना छलनी होता हर बार इसी बेचारी का…
क्यूँ नहीं है अस्मत जाती कभी किसी भी आदम की
क्यूँ नहीं है फिक्र इन्हें भी तार-तार से दामन की…
अपनी करनी को छुपाने, कोस रहे जिन धर्मों को
कभी मिलाकर देखो उनकी सीख से अपने कर्मों को…
सुरेखा कादियान ‘सृजना’