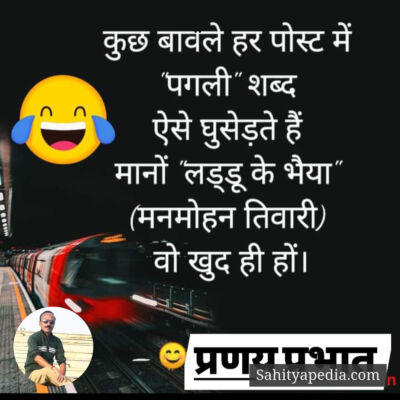थम सी जाती है जीने की ख्वाहिशें
थम सी जाती है जीने की ख्वाहिशें
थम सी जाती है जीने की ख्वाहिशें,
दुखों का पहाड़ जब टूटता है।
नहीं होता बर्दाश्त चिराग तले अंधेरा,
घर का चिराग जब बुझता है।
हो जाता है इंसान बेजान यारो,
भाग्य जब पूरी तरह रूठता है।
तराशा होता है जिसे प्रेम से,
माटी का वही मटका ही क्यों फूटता है?
ये कैसी दराज़दस्ती खुदा मेरे,
गरीबों का घर ही क्यों उजड़ता है?
इस जहाँ में बहुत है ज़मींदार,
फिर तू बेबसों को ही क्यों लूटता है?
दिल ही समझता है उस ज़हमत को,
साथ अपनों का जब छूटता है।
थम सी जाती है जीने की ख्वाहिशें,
दुखों का पहाड़ जब टूटता है।
रचनाकार — सुशील भारती, नित्थर, कुल्लू, (हि.प्र.)