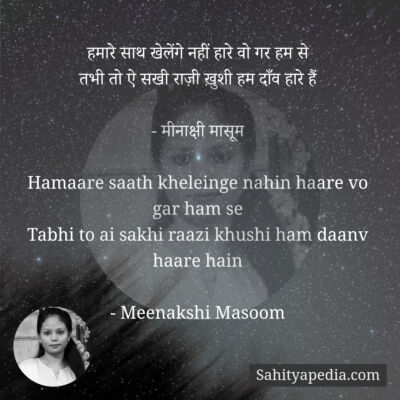जब सांझ ढले तुम आती हो

1- “जब सांझ ढले तुम आती हो “
जब सांझ ढले तुम आती हो
आती है तब इक मंद बयार
छेड़े गए हों जैसे मन के तार
झंकृत होता है ज्यों अंतर्मन
जैसे दूर कहीं रहा हो कीर्तन
जैसे कोई अधखिली कली धूप में
ज्यों मंद -मंद मुस्काती हो
जब सांझ ढले तुम आती हो
दुनिया –जहान की उलझन मन पर मेरे
यूँ तो रहती है मुझको हर दम घेरे
तब बस इक उम्मीद ही मीते
तुम्हारी
मेरे हर दुख पर पड़ती है भारी
कोई राग मन में नया मेरे जैसे
तुम हँस -हँस के
छेड़ जाती हो
जब शाम ढले तुम आती हो
आहत होता मन, निष्फल उम्मीदें
जब पूरे दिन मुझे हराती रहती हैं
तब प्रेम की लौ तुम्हारी, इक प्रत्याशा है मन में लाती
पछुआ में जैसे जूझ रहे हों,
इक साथ दिया और बाती
इक उम्मीद मेरे हारे मन में
तुम न जाने कैसे भर जाती हो
जब शाम ढले तुम आती हो
ये धूप -छांव ही है मितवा अपने जीवन का खेल
संभव ही नहीं लगता है संध्या और प्रभात का मेल
नाउम्मीद मैं बहुत पहले से हूँ
फिर भी ना जाने क्यों एक उम्मीद ,तुम्हारी उम्मीद जगाती है
जब सांझ ढले तुम आती हो
हम इसी उम्मीद के सहारे मितवा, किसी तरह जी लेंगे
जीवन रस कितना भी कड़वा हो
मन मार के किसी तरह पी लेंगे
जब मन के सारे दुख मेरे
बारी -बारी से बोलेंगे
तब तुमसे ही तो अपने मन की सारी गाठें खोलेंगे ,
मेरे इस सुख -दुख को सुनकर मीते
तुम अनायास क्यों मुस्काती हो
जब शाम ढले तुम आती हो।
समाप्त