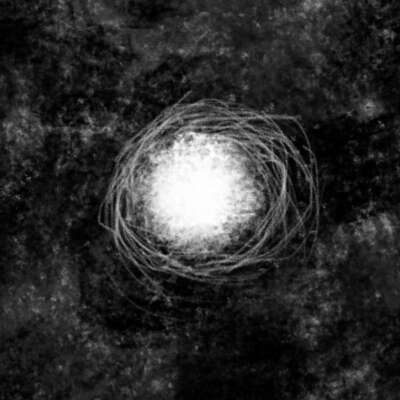छंदमुत रचना
मुक्त छंद रचना
“एकाकार”
सुनो,
तुमने क्या सोचा…..
तुम्हारे जाने के बाद-
मैं टूटे तारों की
रागहीन वीणा बन जाऊँगी?
स्पर्श करती
सुरमयी तरंगों से
तुम्हारा पता पूछूँगी?
अब्धि की
रजत रेणु पर अंकित
तुम्हारे पद चिह्नों पर
अपने पग रखती हुई
ऊर्मि में विलुप्त निशानों से
भ्रमित हो जाऊँगी?
थक-हारकर
निराशा की चादर में
मुँह ढाँपकर सिसकूँगी?
शायद तुम भूल गए कि
रजनी की छाँव में
निद्रा की गोद में
मौन जब मुखरित होता है
तब तुम बिन बुलाए
अतिथि की तरह
मेरे सपनों में आकर
बाँसुरी की तान छेड़ते हो
और मुझमें समाहित होकर
राधामयी हो जाते हो।
डॉ. रजनी अग्रवाल ‘वाग्देवी रत्ना’
कैसा ये
मधुमास प्रिये!
जीवन की
मधुरिम राहों में
पाया नव
अहसास प्रिये!
झुलस गए
आशा के पौधे
यौवन झरता
पातों से
सूख गयीं
खुशियों की क्यारी
गजरा रूँठा बालों से
बंद नयन से
गिरते आँसू
मुरझाता
शृंगार प्रिये!
कैसा ये
विश्वास प्रिये !
शुष्क अधर पर
पुष्प खिला दे
बूँद सुख पर्याप्त है
आस जीने
की बँधा दे
संग दुख पर्याप्त है
हौसलों के
पर लगाकर
प्रेरणा न
बन सके
हरित आभा
पीत हरके
वेदना न
सह सके
कोकिला की
कूँक से उल्लास
छिनता है प्रिये!
कैसा ये
वनवास प्रिये!
‘यादें’
सुनो!
तुम्हारी यादें
बंद दरवाज़े पर आकर
दस्तक देती हैं,
जैसे
आज भी वो मेरा
पता पूछ रही हों।
उन्हें क्या मालूम
तुम्हारे बिना
ये शहर, ये गलियाँ ,
ये घर और इसकी दीवारें
सब गुमनाम हो गए हैं।
छत से लटकते
मकड़ी के जाले
और रात के
सन्नाटे में पलटते
किताबों के ज़र्जर पन्ने
आज भी
किसी की उजड़ी
मुहब्बत का
मातम मना रहे हैं।
डॉ. रजनी अग्रवाल ‘वाग्देवी रत्ना’
‘तुम क्या जानो?’
कौन समझेगा
मेरे अंतस की घुटन को
तानों की चुभन को
श्वास की तपन को ?
भोर में
जब लाली की रौनक
छितराती है,
दूर बगिया में
खिली कोई कली
कुम्हलाती है।
तुम क्या जानो –
नीलांबर में
छायी संध्या
जब रागिनी सुनाती है,
तब नयनों में नीर भरकर
तरिणी में झाँकती
गोरी की छवि
धुँधलाती है।
तुमने कहा था-
दायित्व निभाने आओगे,
भूल क्रिया-कलापों को
मेरे संग मुस्काओगे ।
झूठे उन वादों को जीकर
सपनों में मैं खोयी हूँ,
यादों के
ख़त रखे सिरहाने
रातों को मैं रोयी हूँ।
कभी बनी मैं चाँद
कभी खामोश निगाहें,
उठे रह गए हाथ
दे रही स्वयं दुआएँ।
टूट गया भ्रमजाल
हँस रही भावुक होकर,
हारी हूँ पर आज
जीत तुमसे जीवन भर।
डॉ. रजनी अग्रवाल ‘वाग्देवी रत्ना’
ये
कैसा खुमार है ?
भावों का
ताना-बाना
पहनने को
आतुर शब्द
कलम का
मनुहार
कर रहे हैं
और
अंतस से
अभिसिंचित हो
रचना का उपहार
दे रहे हैं।
मैं बावली सी
सुधबुध बिसराकर
पन्ने भर रही हूँ
नहीं जानती थी
कि मैं स्वयं ही
खुद की पीड़ा
हर रही हूँ।
डॉ. रजनी अग्रवाल ‘वाग्देवी रत्ना’