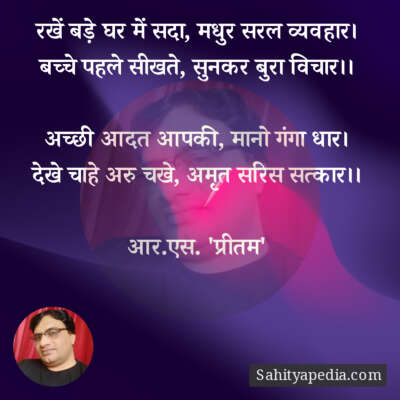घरखर्च
“आज पिताश्री फ़ोन पर पैसों की माँग कर रहे थे।” बैग मेज़ के ऊपर रखते हुए मैंने बड़े ही भारी स्वर में कहा और कुर्सी पर पसर गया। फिर अपनी घरवाली सावित्री से इशारे में पानी पिलाने को कहा।
“यहाँ तो जैसे पैसों का झाड़ लगा है।” सावित्री ने पानी का भरा गिलास थमाते हुए कहा। इसके पश्चात वह बोली, “आप हाथ-मुँह धो लीजिये। चाय भी तैयार है।”
हाथ-मुँह धोने के उपरांत मैं तौलिये से मुँह पोछता हुआ कक्ष में पहुँचा तो मेज़ पर प्याले में चाय प्रस्तुत थी। मैं चुपचाप चाय पीने लगा। चाय के अमृतनुमा घूंटों ने दफ़्तर की थकान को मिटाने में काफ़ी सहायता की। तत्पश्चात मैंने सोचना आरम्भ किया। फ़ोन पर पिताजी ने हालचाल पूछने की औपचारिकता के बाद पारिवारिक मज़बूरियों का उल्लेख करते हुए कई बातें कहीं। जैसे छोटे भाई की कॉलेज फ़ीस। बहन के विवाह की चिन्ता के अलावा मुख्यरूप से खेती-बाड़ी में इस बार कुछ ख़ास फ़सल का न होना। लगभग पाँच-दस हज़ार रूपये की माँग। सोचते-सोचते दुबारा थकावट-सी होने लगी अपने भीतर कहीं। चाय के ख़ाली कप को मैंने मेज़ पर रख दिया।
शहरी ज़िन्दगी कुछ-कुछ ऐसी ही है जैसे मेज़ पर पड़ा ख़ाली कप। जो बाहर से दिखने में सुन्दर और बेशक़ीमती है, मगर अंदर से एकदम खोखला। मन में कुछ ऐसे विचार स्वतः ही तैरने लगे। जब तक प्याला भरा है। हर जगह पूछ है। क़ीमत है। ख़ाली हो जाने पर कुछ भी नहीं। वाह री दुनिया।
“देखो जी, भावुक होने की ज़रूरत नहीं। मैंने महीनेभर का बजट पहले ही बना लिया है। एक नज़र इस पर भी डाल लेना। फिर राजा हरिश्चन्द बनने की कोशिश करना।” श्रीमतीजी के स्वर ने मेरी तन्द्रा तोड़ी। एक काग़ज़ का पुर्ज़ा मेरे हाथ में थमाकर जूठा कप लिए पैर पटकते हुए पुनः रसोई में चली गई।
काग़ज़ के पुर्ज़े पर नज़रें दौड़ाई तो पाया घर-ख़र्च की लम्बी-चौड़ी रुपरेखा मुँह उठाये प्रस्तुत थी। मकान का किराया। दूधवाले का बकाया। राशन-पानी का ख़र्चा। बच्चे के पब्लिक स्कूल की भारी-भरकम फ़ीस। स्कूटर का पेट्रोल। बिजली का बिल। मोबाईल फ़ोन की सिरदर्दी इत्यादि। महीनेभर के अनेक ज़रूरी ख़र्चे थे। जिनसे मुँह मोड़ना संभव न था।
‘क्या होता है बारह-पन्द्रह हज़ार रूपये में आजकल? यदि ओवर टाइम न करूँ तो मैं खुद ही क़र्ज़ में डूब जाऊँ।’मैंने जैसे अपने-आपसे ही प्रश्न किया, ‘क्या दिन थे वे भी, जब स्कूल लाइफ़ थी! कुँवारे थे। कोई चिंता न थी। खा-पीकर मस्त रहते थे। चिंता में तब भी पिताजी ही घुलते थे। सच ही कहा है कहनेवाले ने, बेटा बनकर सबने खाया मगर पिता बनकर किसी ने कुछ नहीं पाया।’
“क्या सोचने लगे? कल तनख़्वाह मिलेगी! इस लिस्ट में जो-जो लिखा है। वो सब कर दो तो कुछ भेज देना अपने बाबूजी को।” घरवाली ने मुझे लगभग नींद से जगाते हुए कहा।
“कैसे भेजें देवी जी, उसके बाद बचेगा कितना? यहाँ अम्बानी की तरह बड़ा बिजनेस थोड़े है… दो टके की नौकरी में ज़िन्दगी से जद्दोजहद कर रहे हैं!” कहकर मैंने जम्हाई ली।
“हज़ार या दो हज़ार भेज देना, नहीं तो गाँव भर में कहेंगे कि हमारा मुन्ना तो भेजता होगा मगर बहुरिया नहीं भेजने देती होगी…!” देवी जी ने खुद को अच्छा दिखाने की गरज से कहा।
“क्यों देवता स्वरुप पिताजी के विषय में ऐसा कह रही हो! तुम कुछ नहीं भी भेजेगी तो भी वो सारे गाँव में घूम-घूमकर आज भी कहते हैं हमारे मुन्ना और बहु की जोड़ी तो राम-सीता की जोड़ी है।” मैंने भावनात्मक कार्ड फेंका।
“पर भेजोगे कैसे?” सावित्री देवी बोली, “पिताश्री नेट बैंकिंग तो करते नहीं! पुराना नोकिया फ़ोन इस्तेमाल करते हैं!”
“हाँ ये बात तो सही है पिताश्री नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते! पुराना नोकिया फ़ोन वन जी वाले से ही काम चला रहे हैं गाँव में!” मैंने देवी जी की बात का समर्थन किया, “वैसे भी जहाँ नेटवर्क सरकारी योजनाओं की तरह ग़ायब ही रहता है, वहाँ फोर जी फ़ोन क्या करेगा?”
“क्या यह सच है, कभी-कभार नेटवर्क आ जाये तो आज भी मन्दिर में लड्डू चढ़ाये जाते हैं ग्रामीणों द्वारा!” धर्मपत्नी ने मुझसे प्रश्न किया।
“क्या तुम भी, ग्रामीणों के पास ज़हर खाने को तो पैसा नहीं है और तुम सौ-डेढ़ सौ रुपये किलो के लड्डू चढ़वाने की बात कर रही हो!” मैंने पत्नी जी की मूर्खता पर हँसते हुए प्रहार किया।
“क्या मनरेगा में रुपया नहीं मिलता?” देवीजी का नया प्रश्न!
“उसमें जितना मिलता है, आदमी अपना ही पेट नहीं भर सकता, तो परिवार का भरण-पोषण कैसे करे देवी जी?” मैंने कटाक्ष करते हुए कहा।
“सरकार तो विज्ञापन में ग्रामीणों के लिए बहुत सी योजनाओं का दावा करती है!” इस बार देवी जी के स्वर में आश्चर्य का भाव था।
“अरे सरकारी योजनाएँ नाममात्र की होती हैं,” मैंने प्रेमपूर्वक समझाया, “वो जनहित में नहीं, नेताओं के हित में ही बन रही हैं आजादी के बाद से! तभी तो स्विस बैंक में अरबों-ख़रबों का काला धन सड़ रहा है।”
“अब सो जाओ, अगले दिन ड्यूटी भी जाना है आपको!” कहकर देवी जी ने लाइट बन्द कर दी।
“न तुम ऐसी थी और न हम ऐसे थे! ये हालात हमें किस मोड़ पर ले आये? न ठीक से गुज़र है! न ठीक से बसर है! ये कैसा हादसों का शहर है?” अँधेरे कक्ष में सोचते-सोचते मेरी आवाज़ जैसे अपने आप से ही टकरा रही थी।
“शा’इर महाराज अब सो जाओ! मुझे भी सोने दो!” करवट बदल कर देवी जी तो सो गई मगर देर तक गाँव की यादें मेरे मनोमस्तिष्क पर हावी रही और कब मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया, मुझे पता भी न चला।
अगले दिन डाकघर पहुँचा तो पिताजी की चिंताओं को दरकिनार करते हुए मैंने पाँच-दस हज़ार रूपये की जगह उन्हें मात्र एक हज़ार रूपये का ई-मनीऑर्डर कर दिया।