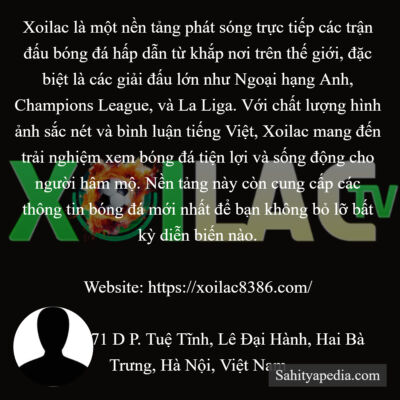*क्यों बुद्ध मैं कहलाऊं?*

सिद्दार्थ नहीं जो गृह त्याग कर,
वन को मैं चला जाऊं,
यशोधरा की सेज छीन कर,
राहुल को मैं ठुकराऊ।
जननी जनक के प्रेम को तज कर,
अनजाने प्रेम में पड़ जाऊं।
दायित्वों से मुख मोड़ कर,
कंधे सिकोड़ मैं भाग जाऊं।
रोग, बुढ़ापा, मृत्यु
क्या इस जीवन का सत्य नहीं?
क्या प्रकृति में हर जीवन का
यही निश्चित गत नही?
फिर किस सत्य की खोज में भटकु
और क्यों बुद्ध मैं कहलाऊं?
नौ मास तक खून से सींचा,
उस मां का अधिकार नहीं
उंगली धर संसार सिखाया,
उस पिता से प्यार नहीं।
जिस युवती को ब्याह के लाया,
उसके बाबुल के घर से।
कई कल्पना कई स्वप्न हैं,
उसको भी इस उपवन से।
जहां खेलते मेरे दो बच्चे,
निर्बोध क्रीड़ा में परिहास करते हैं
मटमैले बचपन से अपने,
दादा की झुर्रियों को साफ करते हैं।
क्यों त्यागू मैं इस माया को
क्यों महात्मा कहलाऊं?
फिर किस सत्य की खोज में भटकु
और क्यों बुद्ध मैं कहलाऊं?
सुदूर गृह से सभी बुद्ध हैं,
अपना अपना ज्ञान लिए।
शहर शहर जो भटक रहे हैं,
स्मृतियों का शमशान लिए।
आह! बच्चे बड़े हो गए,
माता बैकुंठ गई, पिता वृद्ध हो गए।
जिस रमणी ने घर सजाया, प्रेम दिया,
चेहरा बुझ गया, नयन निस्तेज हो गए।
हर रोज़ की सांसों का
क्या चुकाया है मैने?
सब मिलता गया मुझे फिर भी,
पूछता हूं क्या पाया है मैंने?
मुझे ज्ञान है, जीवन यही है,
जीवन रस का मज़ा यही है।
तो क्यों शिकवा करूं किसी से,
क्यों क्षुब्ध मैं हो जाऊं?
फिर किस सत्य की खोज में भटकु
और क्यों बुद्ध मैं कहलाऊं?