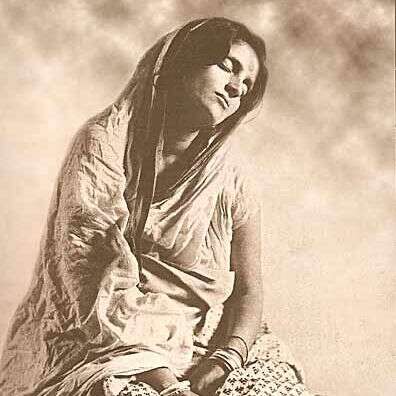क्या यही है हिन्दी-ग़ज़ल? *रमेशराज

तेवरी पर आये दिन यह आरोप जड़े जाते रहे हैं कि ‘तेवरी अनपढ़ और गँवारों का आत्मप्रलाप है। अपरिपक्व मस्तिष्कों की उपज है। यह ग़ज़ल की नकल का एक भौंडा नमूना है।’ यह आरेाप कितने दुराग्रहयुक्त या सार्थक हैं, इसका निर्णय तो समय ही करेगा। यहाँ सवाल दूसरा है-यदि तेवरी स्टंट या बकवास है तो क्या आज हिन्दी में लिखी जा रही कथित हिन्दी ग़ज़लें, ग़ज़ल के शास्त्राीय पक्ष और कथ्य का परिपक्व और विलक्षण नमूना प्रस्तुत कर रही हैं ? इसकी जाँच-पड़ताल के लिये ‘तुलसीप्रभा’ के हिन्दीग़ज़ल विशेषांक, सित-2000 की कुछ ग़ज़लों की थोड़ी बनागी प्रस्तुत है-
डॉ. अनिल गहलौत ‘हिन्दीग़ज़ल’ के चर्चित हस्ताक्षर हैं। उनका फिलहाल ही एक ग़ज़ल संग्रह ‘ सीप में समन्दर ‘ प्रकाशित हुआ है, जिसमें ग़ज़ल के शास्त्रीय स्वरूप को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं। अपनी गम्भीर बातों को लेकर वे स्वयं कितने गम्भीर है?आइये परखें-
तुलसीप्रभा के ग़ज़ल विशेषांक के पृ.29 पर छपी अपनी प्रथम ग़ज़ल में वे ‘कटा’, ‘अटपटा’ की तुक [ काफिया ] ‘बँटा’ से मिलाते हैं। उनकी दूसरी ग़ज़ल में ‘अनुबन्ध’ की तुक ‘सम्बन्ध’, ‘प्रतिबन्ध’ और ‘तटबन्ध’ से जुड़ी है। यह काफियों का कैसा नमूना है? क्या इसी तरह हिन्दी ग़ज़ल को ऊँचाइयाँ छूना है? ऐसे में इसी अंक में प्रकाशित श्री प्रदीप कुमार ‘रोशन’ की इन पंक्तियों को गुनगुनाने में कुछ ज्यादा ही आनंद आने लगता है-
बड़ी कशमकश में पड़ी है ग़ज़ल
अदब से बिछड़ के खड़ी है ग़ज़ल।
डॉ. अश्वघोष ने हिन्दी साहित्य में अच्छी-खासी ख्याति अर्जित की है। निस्संदेह वे एक सार्थक रचनाकार हैं, किन्तु पृ.30 पर प्रकाशित उनकी ग़ज़ल के काफिये का ‘धुआं’ ‘पगडंडियाँ’, खिड़कियाँ’ तय करते हुए ‘बयाँ’ होता है और ‘सुर्खियाँ’ बन जाता है। यह काफियों का कैसा शास्त्रीय नाता है? ऐसे में इस अंक के सम्पादक श्री प्रेम मंधान के स्वर में ही अपना स्वर सम्मिलित करते हुए, उनकी ही एक ग़ज़ल के शे’र के माध्यम से ‘हिन्दी ग़ज़ल के प्रति अपना दृष्टिकोण रखना चाहूँगा-
प्रेम हमारे मतभेदों का कारण बस इतना-सा है
हम कहते हैं ग़ज़ल कही है, वो कहते झक मारी है।
ग़ज़ल के क्षेत्र में ‘झक मारने की कला’ में माहिर हिन्दी ग़ज़लकारों का ग़ज़ल के मूल स्त्रोत, चरित्र [ कथ्य ] और शास्त्रीयता से पिण्ड छुड़ाकर ग़ज़ल कहने का यह हिन्दी अन्दाज अब बह्रों की हत्या कर, हिन्दी छन्दों के साथ प्रस्तुत होने पर आमादा है। इसमें ग़ज़ल के ग़ज़लपन का एहसास कम, उपहास ज्यादा है।
श्री पुरुषोत्तम यकीन भी हिन्दी ग़ज़ल के एक चर्चित हस्ताक्षर हैं। ग़ज़ल की ग़ज़लियत की हत्या करना कोई इनसे सीखे! इसी विशेषांक के पृ.47 पर उनकी एक ‘दोहा ग़ज़ल’ प्रकाशित है, जिसने हिन्दी ग़ज़ल के क्षेत्र में छन्दों के नाम के आधार पर ग़ज़ल के अनेक नामकरणों के द्वार खोल दिये हैं और अब लग रहा है कि हिन्दी ग़ज़ल के नाम पर चौपाई ग़ज़ल, गीतिका ग़ज़ल, सोरठा ग़ज़ल, पीयूषवर्ष ग़ज़ल, घनाक्षरी ग़ज़ल, कवित्त और सवैया ग़ज़ल आदि-आदि ग़ज़लें सामने आयेंगी जो ग़ज़ल के क्षेत्र में निस्संदेह एक नया इन्कलाब लायेंगी।
श्री पुरुषोत्तम यकीन की यह ‘दोहा ग़ज़ल’ प्रथम तो दोहा छन्द का निर्वाह करने में ही असफल है। इसकी दूसरी पंक्ति के प्रथम चरण में जहाँ अल्पविराम लिया जाता है, वहाँ ‘मेरे’ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें दोनों मात्राएँ दीर्घ हैं, जबकि यहाँ लघु के बाद दीर्घ स्वर की व्यवस्था होनी चाहिए। हिन्दी ग़ज़ल के कुछ विद्वान इसे उर्दू वालों की तरह मात्रा या स्वर गिराकर ‘मिरे’ पढ़ना-लिखना चाहें तो यह पंक्ति मात्रा के अपने ऐब को ढँकने में सफल हो सकती है। हिन्दी ग़ज़ल के होहल्ला के इस दौर में ऐसे विद्वान ऐसा करेंगे भी, एक चतुर सुनार की तरह सोने में पीतल भरेंगे भी, ऐसा विश्वास है। यही तो ग़ज़ल का अनुप्रास है, मधुमास है। इसलिए यकीनजी की इस ग़ज़ल के दूसरे पहलू पर आते हैं। इस ग़ज़ल में ‘के दीप’ की पुनरावृत्ति यह कहती है कि यह इस ग़ज़ल का रदीफ है। चलो हम भी माने लेते हैं, किन्तु इसकी दूसरी पंक्ति से ‘के’ का दीप के आगे से गायब हो जाना यह सिद्ध करता है कि रदीफ का इस ग़ज़ल में सफल निर्वाह नहीं हो पाया है। ग़ज़ल में यह कैसी प्रेत-छाया है? इस कथित ग़ज़ल में काफियों की व्यवस्था क्या है? ‘के दीप’ रदीफ से पूर्व ‘आखों’, ‘गरीब’, ‘सोने’, ‘खुशियों’ और ‘ग़ज़ल’ शब्द आये हैं। इन शब्दों के द्वारा कौन-सी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नहीं तो निकृष्ट तुक बनती है? क्या यहाँ भी तुकों की भाँग छनती है? इस भाँग का आनन्द लेते हुए ‘यकीनजी’ के आखिरी शे’र के कथन में आइए हम भी मन लगायें और गुनगुनायें-
आया लुत्फ यकीन जी, सुने करारे शे’र
दोहे के घर में जले, खूब ग़ज़ल के दीप।’’
ग़ज़ल की मातमपुर्सी करते हुए ग़ज़ल के दीप जलाने की यह फनकारी आजकल हिन्दी ग़ज़ल वालों के बीच पूरे शबाब पर है, लेकिन ग़ज़ल की सिसकन, सुबकन से हिन्दी ग़ज़लकार बेखबर हैं।
साथी छतारवी अच्छे गीतकार हैं। उनके ‘विषैले गीत’ संग्रह की गीतात्मकता असंदिग्ध है। किंतु उनकी ग़ज़ल पर जोर आजमाइश उनके भीतर छुपे कुशल रचनाकार को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर देती है। पृ.85 पर वे ‘डर’ की तुक ‘जड़’ और ‘धड़’ से मिलाते हैं। उनकी दूसरी ग़ज़ल में ‘ग़ज़ल’ की तुक ‘शक़ल’ से अगर ठीक है तो ‘नकल’ ‘सकल’, ‘अकल’ में काफिया सिसकता हुआ महसूस होता है और ग़ज़ल की आँख को ‘सजल’ कर देता है। उन्हीं के शब्दों में ग़ज़ल के प्रति उनकी असमर्थता यूँ व्यक्त होती है-
जैसी आयी, मन में आयी, मित्र ग़ज़ल लिख दी
कभी न देखी-भाली उसकी किन्तु शक़ल लिख दी।
बिना शक़ल देखे ग़ज़ल लिखने की यह प्रक्रिया, निराकार को साकार में बदलने का उपक्रम है। अतः निराकार का यह साकार रूप अगर हिन्दी ग़ज़ल है तो ऐसी ग़ज़लें, हिन्दी ग़ज़ल को नये आयाम जरूर देंगी, अब न सही आगे चलकर नूर देंगी।
श्री नूर मोहम्मद ‘नूर’ ने भी हिन्दी ग़ज़ल के क्षेत्र में खूब नूर बिखेरा है। तुलसी प्रभा के पृ. 80 पर मतला शे’र में ‘सदी’ की तुक ‘नदी’ से मिलाने के बाद वे ‘रोशनी’ की ‘खलबली’ बड़ी ‘बेदिली’ के साथ करते हुए ‘शाइरी’ का आभास देते हैं। मतला शे’र में ही काफिया तंग होने के कारण सब तुकें ‘दलदली’ हो जाती हैं। ग़ज़ल के इस दलदल के बीच वे अनायास इस सच्चाई को उजागर कर बैठते हैं-
हारी-हारी ग़ज़ल, कारी-कारी ग़ज़ल
आजकल कहूँ मैं ढेर सारी ग़ज़ल।
तुम सुनो, मत सुनो, ‘नूर’ को मत गुनो
वह कहेगा मगर उम्र सारी ग़ज़ल।
पृ. 82 पर डॉ. पांडेय आशुतोष अपनी पहली ग़ज़ल में ‘एक’ का ‘अभिषेक’ करते हुए इतनी ‘दिलफैंक’ तुकों का ‘अभिलेख’ प्रस्तुत करते हैं कि सम्पूर्ण ग़ज़ल की तुकान्त व्यवस्था खस्ता बन जाती है। दूसरी ग़ज़ल में मतला शे’र गायब है, पर यह हिन्दी ग़ज़ल है इसलिए सफल है? इस ग़ज़ल में ‘वंचना’ की तुकें ‘चना’, ‘याचना’, ‘आलोचना’, कुल मिलाकर ‘चना’, घना प्रकाश फैलाने के स्थान पर, अंधकार ही अन्धकार फैलाती हैं। ग़ज़ल के नाम पर ग़ज़ल के काफियों को खाती है।
ग़ज़ल के प्रखर व्याख्याता श्री अनिरुद्ध सिन्हा की पृ. 31 पर प्रकाशित दूसरी ग़ज़ल के छः काफियों में ‘शाम’ और ‘काम’ को छोड़कर ‘नाम’ काफिया चार बार आया है। काफिया के रूप में ‘नाम’ की यह तुक क्या स्वर परिवर्तन का सही आधार खड़ा कर सकती है? यह उनके ही लेख ‘ग़ज़ल की समझ के विरोध’ को कैसे दबा सकती है? उसे बस बड़ा कर सकती है।
डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल हिन्दी ग़ज़ल के चर्चित हस्ताक्षर ही नहीं, ग़ज़ल के एक अच्छे प्रवर्त्तक और उद्घोषक हैं। ग़ज़ल की हिन्दी में चर्चा कराने का श्रेय भी काफी हद तक उनके हिस्से में हैं। लेकिन पृ.76 पर प्रकाशित उनकी दूसरी ग़ज़ल के मतला में ‘चाँदनी’ की तुक ‘रोशनी’ से मिलने के बाद आगे चलकर ‘आदमी’, और ‘नदी’ की ‘फुलझड़ी’ बन जाती है। यह ग़ज़ल इस प्रकार सुबकते हुए काफियों के बीच ‘हिन्दी ग़ज़ल’ कहलाती है।
पृ. 56 पर रसल विश्वामित्र हिन्दी ग़ज़ल से ‘रदीफ’ गायब कर ग़ज़ल को एक नया आयाम देते हैं। ‘रदीफ’ से मुक्ति का यह प्रयास आगे चलकर हिन्दी ग़ज़ल की शास्त्रीयता का शायद कोई मान बन जाये, पहचान बन जाये तो आश्चर्य कैसा? हिन्दी ग़ज़ल में होता है ऐसा। ‘जि़न्दगी’ से ‘आशिकी’, ‘रोशनी’, ‘आदमी’, ‘रागनी’ आदि ‘शायरी’ के लिये अनुकूल तुकें हो सकती हैं, लेकिन ग़ज़ल में रदीफ के बिना इनका औचित्य समझ से परे है। संयुक्त रदीफ- काफिये की यह ग़ज़ल कैसा कमाल करे है?
पृ. 51 पर ग़ज़ल के महारथी श्री महेश अनघ विराजमान हैं। उनकी ग़ज़लों की तुकें उत्कृष्ट हैं। लेकिन प्रथम ग़ज़ल कौन-सी बह्र में कही गयी है? इसकी हर पंक्ति मात्रादोष और लय-भंगता की शिकार है। हिन्दी ग़ज़ल का यह कैसा चमत्कार है। मूँगफलियाँ खा चुकने के बाद ‘जन गण मन’ सुनने का कथन प्रभावशाली है-मौलिक है। परेशानी बस यह इक है-
यह दौरे-ग़ज़ल है नरेद्र, दौरे-ग़ज़ल में
बेवज्न तवाजुन की बह्र देखते चलो।
‘आजकल’ मासिक के मार्च-2000 अंक में श्री आलम खुरशीद की दूसरी ग़ज़ल के काफिये ‘बरसते’ ‘तरसते’ ‘दस्ते’, ‘गुलदस्ते’ से मिलाये गये हैं। ये कैसे निभाये गये हैं?
इसी अंक में ग़ज़ल के विद्वान कवि ज्ञानप्रकाश विवेक की पृ. 24 पर दूसरी ग़ज़ल में ‘तर’ से ‘कर’ की तुक पांच बार मिलायी गयी है। क्या ग़ज़ल में शुद्ध काफियों का निर्वाह हुआ है? विवेकजी ने इस ग़ज़ल में कौन-सी तकनीकी को छुआ है?
सार यह है कि बेवज़्न बह्रों, मतला के अभावों, काफियों के अशुद्ध प्रयोगों, रदीफों या काफियों का ग़ज़लों से गायब हो जाना, मक्ता से मुक्ति, बह्रों के स्थान पर हिन्दी के छन्दों की त्रुटिपूर्ण घुसपैंठों अर्थात् ग़ज़ल के शिल्प की हत्या कर, मरी हुई ग़ज़ल को ओजस्-प्राणवान बतलाना, अपने इस कर्म पर मंत्रमुग्ध होते हुए तेवरीकारों को गरियाना, उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, हरिगढ़ी या हरिपुरी बतलाना, अगर हिन्दी ग़ज़लकारों की यही समझदारी है तो यह निस्संदेह मानसिक बीमारी है, तेवरी के खिलाफ आँख मूँदकर बयान देने की तैयारी है।
हिन्दी ग़ज़लकारों ने सिर्फ ग़ज़ल के ही शिल्प की हत्या की हो और यहीं अपनी यह शिल्प-क्रिया रोक ली हो, ऐसा नहीं। ये ग़ज़ल की आत्मा [ कथ्य ] पर भी लगातार चोट कर रहे हैं। मूल चरित्र की हत्या करने में इन्हें आनंद का अनुभव हो रहा है। श्री अनुरुद्ध सिन्हा अपने ‘ग़ज़ल की समझ का विरोध’ आलेख में फरमाते हैं कि ‘‘ मैं मानता हूँ कि ग़ज़ल हुस्नो-इश्क से ताल्लुक रखती है। यह इसका अपना सौन्दर्यबोध है, साथ ही जीवन का एक अहम् पक्ष भी। मगर दूसरी ओर जीवन का कटुपक्ष भी इसके हिस्से में आता है।’’
मतलब यह कि अब ग़ज़ल प्रणयात्मकता के साथ-साथ समकालीन विकृतियों, विसंगतियों और शोषण के प्रति आक्रामकता का आभास भी देती है। श्री अनिरुद्ध सिन्हा या उन जैसे ग़ज़ल के समझदारों की दृष्टि में ऐसे तर्क इसलिये सही हैं क्योंकि इनके लिये सूपनखा और सीता में कोई फर्क नहीं है, हैं तो दोनों स्त्रिायाँ ही। ऐसे विद्वानों के हिसाब से तो किसी की पत्नी किसी गैरमर्द के साथ बार-बार सो सकती है। वह तो ‘पत्नी’ ही कहलायेगी, ‘रखैल’ कैसे हो जायेगी? ऐसे विद्वान, सचिवालय, विद्यालय, मदिरालय, पुस्तकालय और वैश्यालय के अन्तर को आखिर समझने की कोशिश करें तो क्यों करें, आखिर हैं तो सब ये ‘आलय’ ही। माँ, भाभी, बुआ, दादी, चाची, मौसी, बहिन, बेटी कहकर ऐसे सुधी लोग स्त्री के व्यक्तित्व को खण्डित करने का प्रयास क्यों करें? स्त्री अन्ततः स्त्री ही है। गुण्डे और शरीफ, अध्यापक और विद्यार्थी, शासक और शासित, भोगी और योगी में ये विद्वान भेद मानें तो क्यों मानें? ये सब भी तो ‘आदमी’ के ही रूप हैं। इनकी दृष्टि में यदि कोई ‘हत्यारा’ दुधारा त्यागकर ‘बुद्ध’ बना है तो उसे शुद्ध मानकर विवाद को क्यों बढ़ायें। अतः उसे हत्यारा ही बतायें, क्योंकि था तो हत्यारा, क्या हुआ जो त्याग दी दुधारा?
ग़ज़ल के पाँवों से घुँघरू छीनकर, लबों से शराब का स्वाद हटाकर, उसके हाथों में क्रान्ति की मशाल और तलवार थमाने वाले हिन्दी ग़ज़ल के समझदारों को इतना तो बताना ही चाहिए कि ‘सहवास के चुम्बन’ और ‘बलात्कार के क्रन्दन’ में क्या कोई फर्क नहीं होता? अगर नहीं तो ग़ज़ल की हू-ब-हू टैक्निक में रची गयी ‘हज़्ल’, ग़ज़ल से अलग कैसे हो गयी? ‘प्रेमपूर्ण बातचीत की शालीनता’ और ‘अश्लीलता’ एक ही फार्म में ‘ग़ज़ल’ और ‘हज़्ल’ को मान्यता प्रदान करने वाले विद्वान क्या मानसिक रूप से विक्षप्त थे?
उक्त बातों, तथ्यों या चरित्र की सही पहचान को ध्यान में रखते हुए ही यदि तेवरीकारों ने तेवरी को ग़ज़ल से अलग किया तो यह अलीगढ़ को हरीगढ़ बनाने की साजिश कैसे हुई? इसके लिये क्या कोई सतर्क तथ्य सामने नहीं आना चाहिए? तेवरी से ग़ज़ल को अलग करने की यह मंशा अगर कोई साजिश मानी जायेगी या मानी जा रही है तो ऐसी ही साजिश की दुर्गन्ध इन ग़ज़ल-भक्तों को आरती और वंदना, नाटक और एकांकी, ‘चुटकुला और लघुकथा, उलटबाँसी और बारहमासी, दोहा और साखी, खण्ड काव्य और महाकाव्य के साथ-साथ प्रेम और वासना आदि में अन्तर करने वाले अभिप्रायों में भी आयेगी, लेकिन यहाँ वे चुप ही रहेंगे, बस तेवरीकारों को ही साजिशी कहेंगे।
चुम्बन और बलात्कार के क्रन्दन को एक ही आत्मा के खाने में ठूँसकर ग़ज़ल को ‘परम-आत्मा’ का स्वरूप प्रदान करने वाले ये ग़ज़लकार अगर शराब के स्थान पर ग़ज़ल के हिस्से में यातना, बेबसी, लाचारी, तल्खी को लाते हैं और इस तरह ग़ज़ल के कथन चाकू की तरह तन जाते हैं, लेकिन यह आक्रोश, विरोध, विद्रोह और असंतोष की अनुभावमय शक़ल फिर भी ग़ज़ल कहलाती है तो ऐसे ग़ज़ल के परमात्माओं के समक्ष अनुनय-विनय का अर्थ और असमर्थ ही होना है। फिर भी निवेदन के साथ कुछ बात-अगर ग़ज़ल के हिस्से में प्रणात्मकता के साथ-साथ आक्रामकता भी आती है तो क्या भजन के हिस्से में नेताजी के चमचों के व्याख्यान भी आ सकते हैं? क्या विनय, अग्निलय बनकर ‘विनय’ का ही परिचय दे सकती है? वन्दना के हिस्से में क्या उल्लू निन्दा आ सकती है?
उक्त सारी दलीलों को ‘ग़ज़ल के कथ्य के परिवर्तन की तर्ज’ पर क्या ग़ज़ल के कथित पंडित अपने गले उतार सकते हैं? ग़ज़ल जैसा अलौकिक कारनामा [ जिसमें चरित्र तो बदला हो लेकिन नाम नहीं ] ग़ज़ल को छोड़, कहीं और गिना सकते हैं? क्या वे हज़्ल को ग़ज़ल बता सकते हैं? श्री रतीलाल शाहीन [ आजकल मार्च-2000 ] तेवरी की सार्थकता को खारिज करते हुए कहते हैं कि-‘‘नाम बदल लेने से गुण या स्वभाव नहीं बदल जाता।…..ग़ज़ल का तेवरी नाम ऐसा ही लगता है जैसे अलीगढ़ को कोई हरिपुर कहे।’’
अलीगढ़ को हरिपुर में बदलने के पीछे जो साम्प्रदायिक दुर्गन्ध छुपी हुई है, उसे शाहीनजी नहीं महसूसते तो इसमें तेवरीकारों का क्या दोष? अगर इस दुर्गन्ध को वे तेवरीकारों के मत्थे मढ़ना चाहते हैं तो ग़ज़ल को हिन्दी ग़ज़ल बनाने वाले ग़ज़लकार पहले अपने अन्दर की साम्प्रदायिक दुर्गन्ध को महसूस करें। दूसरों की आँख में टेंट देखने से पहले इस प्रश्न का उत्तर दें- ‘माना नाम बदलने से गुण या स्वभाव नहीं बदल जाता, पर गुण या स्वभाव बदलें तो… और कुछ हो न हो ग़ज़ल कैसे हज़्ल हो जाती है?
———————————————————
रमेशराज, 15/109, ईसानगर, अलीगढ-202001