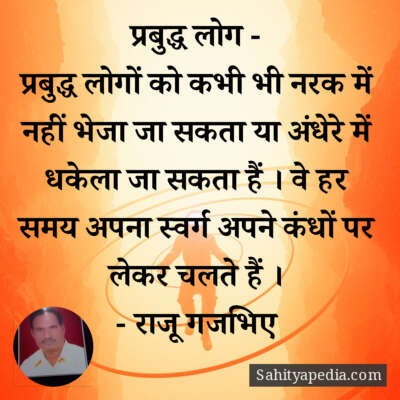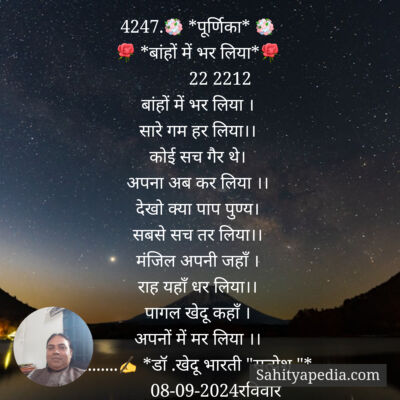कविता – नदी का वजूद

पड़ी हुई थी शांत
नही था मेरा वजूद कुछ
विशाल पर्वत के किसी कोने से गुजरते हुए
जहाँ मुझे रास्ता मिलता गया
मैं बढ़ती गई।
कभी हिमालय की गोद से
तो कहीँ विंध्य की गोद
तो कहीं अरावली की चोटी से
तो कभी सतपुडा की चोटी से।
मैं न जाने किन – किन ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से
पठारों, पथरीले रास्तों से अपना मार्ग कब से ढूंढ रही हूँ।
मेरा वजूद मुझे तलाश करता हुआ जा पहुँचता है जमीन में
वहाँ मैं विभिन्न नामो से पुकारी जाती हूँ।
कोई गंगा कोई यमुना ,घाघरा, बेतवा ,कोसी,ब्रह्मपुत्र, कहता है,
मैं जीवन दायनी बन जाती हूँ तो कभी मैं विकराल हो जाती हूँ।
लोग मुझे पीकर तृप्त होते हैं,
मैं इंसानों की हमेशा मदद करती हूँ।
जिसको जैसी जरूरत होती है वो मुझसे ले कर जाता है,
मैंने कभी किसी से कुछ भी नही मांगा।
आज मैं बहुत दुःखी हूँ क्यों कि,
कभी मेरे साथ ऐसा नही हुआ जैसा अब मेरे साथ हो रहा है।
लोगों में मेरे वजूद को
खत्म करने की होड़ लगी है।
आँचल मैला करना प्रारम्भ कर दिया है।
लोगो की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे सताने लगे हैं।
मुझे रोक दिया है बढ़ने से,
प्रदूषण में भला कौन जीता है?
यकीनन,
मैं भी मर जाऊँगी,
और नष्ट हो जायेगा मेरा वजूद ।
क्या, मेरे वजूद के खत्म होने पर
इंसानी वजूद बना रहेगा?