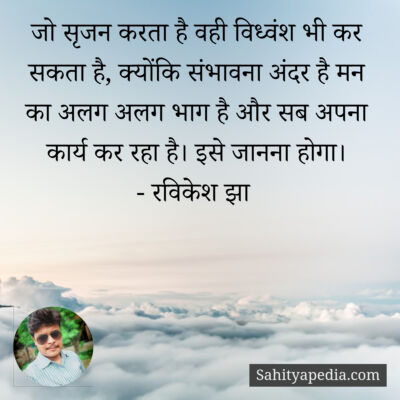आलोचना के स्वर
सत्य सहता झूठ के ही
रात दिन नश्तर,
शान्त होते जा रहे आलोचना के स्वर,
जूझता नर-दंभ से
नर ही बना काया,
धूप ही अब आग भी है धूप ही छाया,
अब न शीतलता लिए बहते यहाँ निर्झर
कैद है वह आचरण
वह हृदय की भाषा,
अब निराशा की सुरंगों में कहाँ आशा,
क्रांति के सन्देश थोथे लिख रहे बंजर
चीर हरते तंत्र का
जनतंत्र के दानव,
कष्ट में हैं सभ्यता ओढा हुआ मानव,
कर रहा संघर्ष पिछड़ा आज हर आखर
#
अशोक रक्ताले ‘फणीन्द्र’
उज्जैन