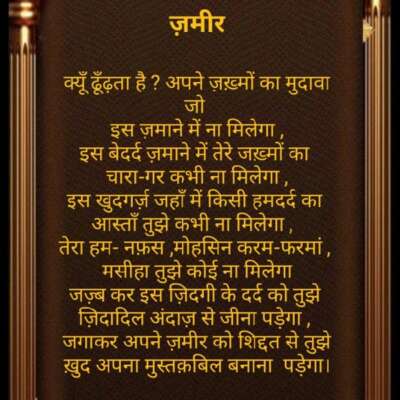अंधेरे
डूबते सूरज की तरह आकाश से दूर
एक छोर पर
खो रही हूं या उग रहीं हूँ
नहीं पता
पर थकन इतनी की
अब जी चाहता है
बस उतार दूं ये लबादा
जो ओढ़ रखा है,
धर्म का, समाज का,
या स्त्री होने का…
बोझ इतना कि,
झुकी जाती है कमर
टूटने की हद तक
और पैर
जैसे लिपटे जाते हों
धरती में
बिल्कुल ख्वाब की तरह
की एक कदम भी न चल सकूँ
ऐसा अंत , ऐसी भयावहता..
छल रहें है तन, आत्मा
घोंट रहें है सांसे
शरीर के तपन ने इस तरह
लाल कर दिया है क्षितिज
की लगता है
खून तैर रहा हो पानी में
और सांसे बस बढ़ती शाम के साथ
रात के अंधेरों में डूबती चली जाए…