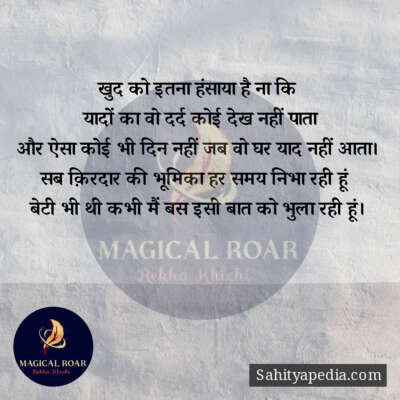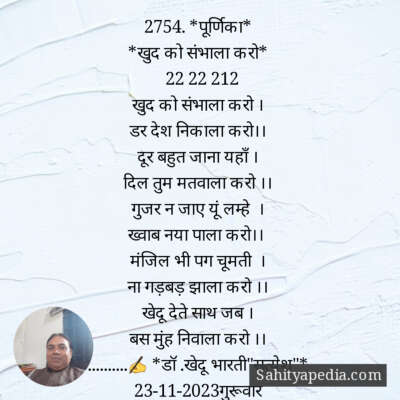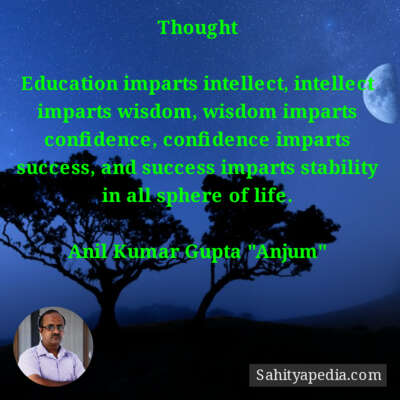तेवरी का सौन्दर्य-बोध +रमेशराज

लोक या जगत के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध, हमारी उस वैचारिक प्रक्रिया के परिणाम होते हैं, जिसके अन्तर्गत हम यह निर्णय लेते हैं कि अमुक वस्तु वा प्राणी अच्छा या बुरा है, हमें दुःख देता है या सुख देता है, हमारा हित करता है या अहित करता है, हमें संकट में डालता है या संकट से उबारता है। रागात्मक सम्बन्धों के इस प्रकार के निर्णयों तक पहुंचने की वैचारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही सौन्दर्य-बोध की सत्ता को देखा जा सकता है।
डॉ. राम विलास शर्मा अपने एक निबंध में कहते हैं कि-‘‘सौन्दर्य की वस्तुगत सत्ता मनुष्य के व्यवहार के कारण ही नहीं है, उसकी वस्तुगत सत्ता स्वयं वस्तुओं में भी है, जिनके गुण पहचान कर हम उन्हें सुन्दर की संज्ञा देते हैं।’’
वस्तुओं के गुणों की पहचान किस प्रकार होती हैं, इसे समझाते हुए वे लिखते हैं-‘‘ गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु से रामकथा सुनी, तब अचेत होने के कारण उनकी समझ में कम आयी। लेकिन गुरु ने उसे बार-बार सुनाया। उनकी चेतना विकसित हुई और रामकथा के गुणों का उन्हें पता लगा। लेकिन रामकथा में मुनष्य के लिये जो ज्ञान था या चरित्र-चित्रण और कथा की बुनावट थी, वह उसमें तुलसी के अचेत रहने पर भी थी और सचेत रहने पर भी रही। रामकथा के गुण तुलसी की इच्छा-अनिच्छा पर निर्भर न थे, वे रामकथा के वस्तुगत गुण थे, जिन्हें सचेत होने पर तुलसी ने पहचाना।’’
डॉ. रामविलास शर्मा के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम यह बात तो निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का सौन्दर्य-बोध हमारे उन निर्णयों की देन होता है, जिनके अन्तर्गत हम वस्तुओं के गुणों की परख कर उन्हें आत्मसात करते हैं या उन्हें अपनी रागात्मक चेतना का विषय बना लेते हैं। लेकिन वस्तुओं के आत्मसात करने के पीछे हमारे पूर्वानुभव या निर्णय कार्य न कर करते हों, ऐसा कदापि नहीं होता। इसलिये सौन्दर्य की व्याख्या करते-करते ‘सौन्दर्य की उपयोगिता’ शीर्षक लेख में डॉ. रामविलास शर्मा एक ऐसी भारी चूक कर गये हैं, जिसके कारण सौन्दर्य का प्रश्न सुलझते-सुलझते ज्यों का त्यों उलझ गया। कुछ सुन्दर वस्तुओं की मिसालें देते हुए वे लिखते हैं कि- ‘‘ताजमहल, तारों भरी रात, भादों की यमुना, अवध के बाग, तुलसीकृत रामायण, देश-प्रेम, संसार में मानवमात्र का भाईचारा और शान्ति-ये सभी सुन्दर हैं। हो सकता है-कुछ लोगों को ताजमहल भयानक मालूम हो, तारों भरी रात में भूत दिखाई दें, भादों की यमुना देखकर मन में आत्महत्या के भाव उठते हों, अवध के बागों में आग लगा देने को जी चाहे, तुलसीकृत रामायण निहायत प्रतिक्रियावादी लगती हो, देश-प्रेम के नाम से चिढ़ हो और शान्ति तथा भाईचारे की बातों में कम्युनिज्म की गंध आती हो। ….ताजमहल अगर आपको भयावना लगता है तो शायद इसलिये कि एक बादशाह ने आप जैसे मुफलिसों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है।’’
जिस असौन्दर्य-बोध का जिक्र डॉ. शर्मा उपरोक्त लेख में करते हैं, इस असौन्दर्य-बोध के कारण का पता लगाते-लगाते डॉ. शर्माजी ने ‘शायद’ लिखकर उन सारे तथ्यों को दरकिनार कर डाला जिनके द्वारा सौन्दर्य-असौन्दर्य के प्रश्नों का समाधान हो सकता था। सौन्दर्य के प्रश्न का समाधान वस्तु की वस्तुगत सत्ता में खोजते-खोजते वे इस मूलभूत प्रश्न से ही किनारा कर गये कि जो वस्तुएं डॉ. रामविलास शर्मा को सुन्दर महसूस हो रही है, वही दूसरे व्यक्तियों को असौन्दर्य के बोध से आखिर क्यों सिक्त कर रही हैं? डॉक्टर साहब के लिये इसका समाधान चार कथित भले लोगों की गवाही या ऐसे मनुष्यों के अस्पतालों में भर्ती कराना, भूत निवारण के लिये ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ, आत्म-हत्या से बचने के लिये अच्छे साहित्य का पठन-पाठन आदि भले ही रहा हो, लेकिन असौन्दर्य के प्रश्न का समाधान इस प्रकार की दलीलों से हल नहीं किया जा सकता। यदि इसका समाधान यही है तो तुलसी के काव्य की प्रतिक्रियावादी घोषित करने वाले, डॉ. रामविलास शर्मा को भी किसी पागलखाने में भर्ती होने की सलाह दे सकते हैं। सामंती वैभव के चितेरे नारी के मातृरूप, भगिनीरूप की सार्थकता को एक सिरफिरे आलोचक का अनर्गल प्रलाप बता सकते हैं। ऐसे में क्या इस तरह की उठापटक या अनर्गल बहस सौन्दर्य-असौन्दर्य की गुत्थी को सुलझा सकेगी? इसलिये आवश्यक यह है कि एक व्यक्ति को जो वस्तु गुणों के आधार पर सुन्दर दिखायी देती है, वही वस्तु दूसरे व्यक्ति में असौन्दर्य का बोध क्यों जाग्रत करती है। इस प्रश्न का समाधान हम तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से करते हुए किसी सार्थक हल तक पहुंचें।
जैसा कि इस लेख के पूर्व में कहा जा चुका हैं कि सौन्दर्यबोध की सत्ता को मनुष्य की रागात्मक चेतना की वैचारिक प्रक्रिया के निर्णीत मूल्यों के अन्तर्गत ही देखा जा सकता है। अतः सौन्दर्य की सत्ता भले ही वस्तु के गुणों में अन्तनिर्हित हो लेकिन उसका बोध मनुष्य अपने आत्म अर्थात रागात्मक चेतना के अनुसार ही करता है। इसलिये सौन्दर्य के प्रश्न को हल करने से पूर्व आवश्यक यह हो जाता है कि पहले मनुष्य या प्राणी के आत्म अर्थात् रागात्मक चेतना को परखा जाये।
दरअसल सौन्दर्य के प्रश्न का समाधान वस्तु की वस्तुगत सत्ता के साथ-साथ, मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता पर भी निर्भर है। इसलिये कोई भी वस्तु हमें सुन्दर तभी लगेगी या महसूस होगी जबकि-
1. उस वस्तु के व्यवहार अर्थात् उसकी गुणवत्ता से हमारे आत्म को कोई खतरा न हो
2. वह वस्तु अपनी गुणवत्ता से हमारे आत्म को संतुष्टि भी प्रदान करे।
बात को स्पष्ट करने के लिये यदि हम डॉ. रामविलास शर्मा के ही तथ्यों को लें तो माना ताजमहल के वस्तुगत गुणों से किसी को भी खतरा महसूस नहीं होता, मतलब यह कि हमारे किसी भी प्रकार के इन्द्रिय-बोध में उसकी दुःखानुभूति सघन नहीं होती, लेकिन प्रख्यात शायर साहिर लुधियानवी को फिर भी ताजमहल असुन्दर दिखाई देता है तो इसका कारण उनका वह आत्म या रागात्मक चेतना है, जो जनता के खून-पसीने की कमाई से बने भव्य ताजमहल में, एक शहंशाह की अलोकतांत्रिक, जनघाती नीतियों का साक्षात्कार करती है और शायर को लगता है कि ताजमहल चाहे कितना भी भव्य और कथित रूप से सुन्दर क्यों न हो, लेकिन इसके निर्माण में एक बादशाह ने [मात्र अपनी तुष्टि के लिये] मुल्क का पैसा स्वाहा कर डाला है। चूंकि साहिर साहब की रागात्मक चेतना का विषय मुल्क की गरीब और शोषित जनता है, इसलिये एक बादशाह की शोषक और जनघाती नीतियों उसे कैसे पसंद आ सकती हैं? और यही कारण है कि ताजमहल के ‘लाख हसीन होने के बावजूद’ उनके आत्म अर्थात् रागात्मक चेतना को इससे संन्तुष्टि नहीं मिलती। और वह कह उठते हैं कि ‘‘एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।’’
ठीक इसी प्रकार तारों भरी रात किसी को भुतहा लगती है तो इसका कारण उसके आत्म का असुरक्षा में पड़ना है। तुलसीकृत रामचरित मानस किसी को प्रतिक्रियावादी लगती है तो इसका एक सीधा-सीधा कारण उसकी वह वैचारिक अवधारणाएं हैं, जो डॉ. रामविलास शर्मा की वैचारिक अवधारणाओं के एकदम विपरीत जाती हैं। अतः जो वस्तु डॉक्टर साहब को सुन्दर लगे, यह कोई आवश्यक नहीं कि वह किसी अन्य को भी सुन्दर लगे।
सौन्दर्य के विषय में इस सारी भूमिका को बांधने का उद्देश्य सिर्फ इतना-सा है कि वर्तमान कविता के रूप में तेवरी के सौन्दर्य-बोध को स्पष्ट करने में आत्म-सुरक्षा और आत्म-सन्तुष्टि जैसे दो तत्त्व किस प्रकार सौन्दर्य का विषय बनते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिये वैज्ञानिक और तार्किक प्रयास किये जायें।
लेकिन सौन्दर्य के साथ चूंकि सत्य और शिव का पक्ष भी जुड़ा हुआ है, इसलिये वास्तविक और सत्योन्मुखी सौन्दर्य की प्रतीति तभी सम्भव है, जबकि कोई प्राणी अपने व्यवहार को पूरे लोक या मानवमंगल का विषय बनाये। व्यवहार का यह पक्ष ही सही अर्थों में वस्तुओं की वस्तुगत सत्ता का वास्तविक और सत्योन्मुखी सौन्दर्य होगा।
अतः जब तक हमारी रागात्मक चेतना मानवतावादी नहीं होगी, तब तक हम सच्चे अर्थों में सौन्दर्य की वास्तविक पकड़ से परे ही रहेंगे। इसलिये किसी भी वस्तु की गुणवत्ता हमें अच्छी लगती है, तो वह वस्तु सुन्दर है, प्रश्न का समाधान यहीं नहीं हो जाता, इससे भी आगे उस वस्तु के गुण कितने मानव मंगलकारी हैं, प्रश्न का समाधान इस बिन्दु पर आकर मिलेगा।
वस्तुओं या मनुष्यों के इस प्रकार के मानव-मंगलकारी गुण या व्यवहार की अभिव्यक्ति जब हमें काव्य के स्तर पर रसात्मकबोध से सिक्त करती है तो उसके सौन्दर्य की छटा वास्तव में अनूठी, निराली, सत्यमय और शिवमय दिखलायी देती है।
तेवरी के सौन्दर्य का आलोक, मनुष्य के कर्मक्षेत्र का वह आलोक है, जो आस्वादक के रूप में पाठक या श्रोता को निम्न बिन्दुओं पर सचेत या उर्जस्व करता है-
1. तेवरी के आत्म का सम्बन्ध चूंकि मानव की समस्त प्रकार की रागात्मक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, अतः तेवरी इस प्रकार के रागात्मक सम्बन्धों में प्रगाढ़ता लाने के लिये, इन रागात्मक सम्बन्धों की प्रस्तुति उन नैतिक मूल्यों की स्थापनार्थ करती है, जो मानव से मानव के बीच एक पुल का कार्य करें। नैतिक मूल्यों की यह रागात्मक प्रस्तुति, लोक या समाज की सत्योन्मुखी रागात्मक चेतना का एक ऐसा विकास होता है, जिसके सौन्दर्य की प्रतीति एक तरफ जहां व्यक्तिवादी मूल्यों को अ-रागात्मक बनाती चली जाती है, वहीं समाजिक दायित्वों की रसात्मकता उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। समाज-हित या मानव-हित का यह दायित्व-बोध तेवरी का वह आत्म-भाव है, जिसकी वैचारिक प्रक्रिया लोकोन्मुखी कर्तव्यों के विचारों को दृढ़ता प्रदान करती है।
2. तेवरी इस प्रकार की मान्यताओं कि ‘सच्चा कलाकार सौन्दर्य की सृष्टि के लिये कला की साधना करता है- अपनी भावनाओं, मान्यताओं, विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता’, का इस कारण विरोध करती है या अपनी इन मान्यताओं को अपनी आत्मभिव्यक्ति की विषय नहीं बनाती है क्यों कि इस प्रकार की दलीलें उन सामंती वैभव के चितेरों की हैं, जो सौन्दर्य के नाम पर समूचे लोक को भोग और विलास की वस्तु मानकर रस-सिक्त होना चाहते हैं।
यदि सौन्दर्य-सृष्टि के लिये नैतिकताविहीन कला की साधना होती है, तो ऐसे सामंती वैभव के चितेरे मां, बहिन, बेटियों के साथ उन रागात्मक मूल्यों की अभिव्यक्ति को सौन्दर्य और कला की विषय बनाकर क्यों नहीं प्रस्तुत करते, जो उन्होंने एक कथित प्रेमिका में तलाशे हैं। विचार के इस बिन्दु पर आकर उनके मन में नैतिकता का प्रश्न क्यों उफान लेने लगता है? अतः कहना अनुचित होगा कि कला की साधना का सौन्दर्य नैतिकता के बिना एक विकृत मानसिकता का ही वास्तविक बोध रह जायेगा।
तेवरी इस प्रकार की विकृत रसात्मकता को वर्जित कर, अपने उस रसात्मक-बोध की अभिव्यक्ति करती है, जिसमें डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार ‘शक्ति और शील की बात भूलकर निरुद्देश्य साहित्य के सौन्दर्य की बात नहीं की जा सकती’, बल्कि उन्हीं के शब्दों में-‘इससे जरा ऊंचे उठकर जब हम भावना और विचार के सौन्दर्य के स्तर पर आते हैं तो वहीं नैतिकता का सवाल सामने आ खड़ा होता है। साहित्य से आनंद मिलता है, यह अनुभव सिद्ध बात है, लेकिन साहित्य-शास्त्र यहां समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि यही से उसका श्री गणेश होता है।’’
3. भावना और विचारों के कर्मक्षेत्र सम्बन्धी सौन्दर्य का आलोक, तेवरी के आत्म का वह आलोक है, जिसकी रागात्मकता, सौन्दर्यात्मकता, रसात्मकता, तेवरी के उस नैतिक कर्म में देखी जा सकती है, जिसमें मनुष्य से मनुष्य का सम्बन्ध मात्र निस्वार्थ और लोकोन्मुखी होकर ही प्रस्तुत नहीं होता बल्कि इससे भी आगे बढ़कर लोक की समस्याएं जैसे विषमता, शोषण, अराजकता, उत्पीड़न विसंगति, असंगति आदि का उपचार भी तेवरी में अभिव्यक्ति का विषय बनकर उभरता है। चूंकि तेवरी का आत्म अन्ततः लोक या मानव का ही आत्म है, अतः इस आत्म की सुरक्षा एक तरफ जहां तेवरी शोषित, पीडि़त एवं दलित वर्ग के प्रति करुणा से सिक्त होकर करती है, वहीं करुणा का गत्यात्मक स्वरूप शोषक और आतातायी वर्ग के प्रति विरोध और विद्रोह में तब्दील होकर पाठक या श्रोता को आताताई वर्ग से मुक्त होने के उपाय सुझाता है। इस संदर्भ में तेवरी की आत्मसंतुष्टि का विषय लोक या मानव की यथार्थपरक और शत्रुवर्ग पर लगातार प्रहार करना है। अतः हम कह सकते हैं कि तेवरी की सौन्दर्यात्मकता उसके आत्म-सुरक्षा और आत्मसुतंष्टि के सत्योन्मुखी संघर्ष में अन्तर्निहित है।
————————————————————————
+रमेशराज, 15/109, ईसानगर, अलीगढ़-202001