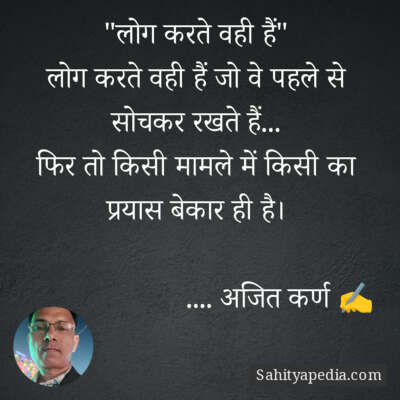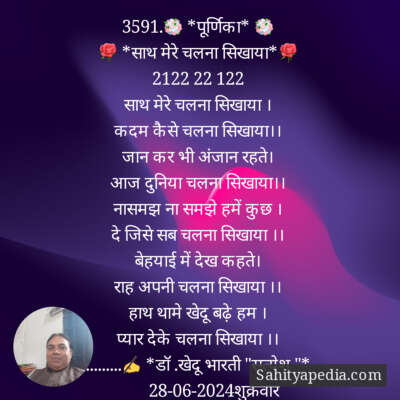■ चुनावी_मुद्दा

#चुनावी_मुद्दा
■ “अटल टेंशन” बनाम “ओल्ड पेंशन।”
【प्रणय प्रभात】
“आदमी दो और गोलियां तीन। बहोत नाइंसाफ़ी है ये, बहोत नाइंसाफ़ी है।”
वर्ष 1975 में रजतपट पर आई ब्लॉक-बस्टर फ़िल्म “शोले” का यह डायलॉग भला कौन भूल सकता है। जो गब्बर सिंह अपने नाकारा साथियों की ज़िंदगी का फ़ैसला करने से पहले बोलता है। आज लगता है यही संवाद मामूली बदलाव के साथ अब राज्य कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को बोलना पड़ेगा। वो भी पूरी दमखम के साथ। इस साल के अंतिम और अहम चुनावी दंगल से पहले। अपने आने वाले कल के उस आर्थिक क्लेश को टालने के लिए, जिसका वास्ता उनके अपने जीवन से है। बदले हुए हालात में गब्बर का रोल उन कर्मचारी संगठनों को अदा करना पड़ेगा, जो झूठे आश्वासन का झुनझुना लेकर सत्ता की गोद मे बैठते आए हैं और अभी भी इस ज्वलंत मुद्दे को ल कर मुंह में बताशे रखे बैठे हैं। वजह है सत्ता के मठाधीशों और आला-अफ़सरों के कृपा-पात्र बने रह कर खुरचन चाटने की चाह। इससे अधिक कुछ नहीं।
ऐसे में यदि 2024 के आम चुनाव से पहले 2023 में संगठन ताल ठोकने से चूके तो उनके पास भविष्य में बाल नोचने के सिवाय शायद ही कोई चारा बचेगा। क्योंकि इस बार की रहम-दिली उनके अपने लिए मुसीबत का सबब बनेगी। नहीं भूला जाना चाहिए कि ग़ैर-भाजपा शासित कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को वह हक़ लौटा चुके हैं, जो “अटल सरकार” के कार्यकाल में छीन लिया गया था। वहीं कुछ दल चुनाव जीतने के बाद यह सौगात देने का संकल्प जता रहे हैं। जिनसे केंद्र सरकार कतई सहमत नज़र नहीं आती। यह वही सरकार है, जो देश के पांचवी आर्थिक शक्ति बनने के दावे करते हुए 80 करोड़ लोगोम को मुफ़्त राशन बांटने को घाटे का सौदा मानने को राज़ी नहीं। तरह-तरह के इवेंट्स और उनके प्रचार-प्रसार पर आए दिन करोड़ों फूंक देने वाली इस सरकार के ख़ज़ाने पर वित्तीय भार केवल उस पेंशन के कारण पड़ता है, जो उनका विधिमान्य हक़ रहा है।
गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से “ओल्ड पेंशन” की बहाली को लेकर दबी हुई सी आवाज़ें उठती नज़र आ रही हैं। यह अलग बात है कि मांग की गूंज धमकदार न होने की वजह से सत्ता के नक्कारखाने में तूती से अधिक कुछ साबित नहीं हो सकी है। जिसकी बड़ी वजह कर्मचारियों की कमज़ोर इच्छाशक्ति के साथ कुछ संगठनों की सत्ता-भक्ति भी है। जो मठाधीशों से थोड़ी सी मलाई के चक्कर में खुरचन को अपना सौभाग्य मानते आ रहे हैं। कर्मचारी नेताओं के इसी छल-चरित्र के कारण पूर्ववर्ती कई आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंचने से पहले टांय-टांय फुस्स हो चुके हैं। जबकि समय की मांग एक परिणाममूलक संघर्ष की है। जिसके लिए नवम्बर 2023 से अच्छा अवसर शायद दूसरा नहीं।
चर्चाएं तो यहां तक हैं कि प्रदेश की सरकार “पुरानी पेंशन” की बहाली को लेकर कतई गंभीर नहीं है तथा “अटल टेंशन स्कीम” पर ही अडिग रहने के मूड में है। चर्चाएं तो “ओल्ड पेंशन बहाली” के लिए मजबूर होने की स्थिति में “कट-मनी फार्मूला” लागू करने तक की भी हैं। जिसके तहत पुरानी पेंशन देने के एवज में कर्मचारियों की वो राशि हड़पी जा सकती है, जो “न्यू पेंशन स्कीम” के अंतर्गत हर महीने काटी जाती रही है और जिसके लेखे-जोखे को लेकर स्थिति संदेह के दायरे से बाहर नहीं। ऐसे में चुगने आई चिड़िया की पूंछ काटने वाला इस तरह का कोई भी प्रयास सफल न हो, यह भी कर्मचारी संघों की बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। वैसे स्थिति कर्मचारियों के वेतन से कटने और सरकार की ओर से मिलाई जाने वाली रक़म की भी संदेह से परे नहीं है। इस कटोत्री व अंशदान के समय पर सही जगह जमा न होने की अटकलें भी समय-समय पर सिर उठाती आ रही हैं। जिन्हें आंकड़ों के बाज़ीगर येन-केन-प्रकारेण झुठलाने या दबाने में कामयाब होते आ रहे हैं।
अनुत्पादक योजनाओं और थोथे कार्यक्रमों पर पानी की तरह पैसा बहाने वाली सरकार निःसंदेह आर्थिक संकट का रोना 2023 के बाद आम चुनाव में भी रोएगी। बशर्ते जाते साल के अंतिम माह की शुरुआत में सामने आने वाला जनादेश उसके पक्ष में पूरी तरह से आ जाए। जिसके विरुध्द संगठनों को आम चुनाव से पहले मज़बूत तर्क व तथ्यों को हथियार बनाना ही पड़ेगा। बेहतर होगा कि संगठन अभी से उन तथ्यों का खुलासा शुरू करें, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को रसातल की ओर ले जाने वाले साबित हो रहे हैं। ऋषि चार्वाक की “कर्ज़ ले कर घी पीने वाली” नीति पर चलती सूबे की सरकार से तीखे व साहसिक सवाल पूछने के लिए कर्मचारियों के परिवारों को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि भविष्य अकेले कर्मचारी नहीं परिजनों व आश्रितों का भी दांव पर लगा हुआ है।
सवाल अब यह भी उठना चाहिए कि जिस प्रदेश में चार दशक सेवा देने वालों को पेंशन देने की क्षमता नहीं, उस राज्य में चार दिनों के लिए चुने गए माननीयों को आजीवन पेंशन व अन्य सुविधाएं क्यों मिलनी चाहिए? यही सवाल राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी शिद्दत से उठाए जाने की दरकार है। जिसका सूत्रपात 2023 के अंत से पहले चुनावी दंगल में होना ज़रूरी है। राष्ट्र-निर्माण और विकास का ठेका सिर्फ़ आयकर-दाता मध्यवर्गीय नागरिकों का ही क्यों? यह सवाल भी छोटे व मंझोले अधिकारियों-कर्मचारियों और कारोबारियों को मिलकर उठाना होगा। जिनकी जेबें कथित राष्ट्रवाद के उस्तरे से लगातार काटी जा रही हैं। वो भी इसलिए ताकि सत्ता के सूरमा मुफ्तखोरों को रेवड़ियां बांट कर राजा बलि की तरह सिंहासन पर बने रहें।
एक देश के अनेक राज्यों में एक समान पेंशन क्यों नहीं, यह सवाल अब उठना लाजमी हो चुका है। इससे भी कहीं बड़ा सवाल यह कि किसी एक ही राज्य में आधे कर्मचारियों को नई व आधों को पुरानी पेंशन कितनी न्यायोचित है? सवाल यह भी कि “न्यू पेंशन स्कीम” पुरानी से बेहतर है तो इसे बड़े अफ़सरों और नेताओं के लिए लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
कुल मिला कर इस बार का चुनाव लोक-लुभावन राष्ट्रीय मुद्दों नहीं राज्य के अपने हित से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक वैसे ही, जैसे पंचायतों व निकायों के चुनाव स्थानीय व आंचलिक मुद्दों पर केंद्रित होते आए हैं। मतदाताओं को भावनात्मक के बजाय भविष्य के लिहाज से व्यावसायिक रुख अपनाना चाहिए, ताकि उसके हितों के साथ तमाम बार हो चुके छल की पुनरावृत्ति एक और बार न हो सके। आज़ादी के 75 साल में यह तो साबित हो ही चुका है कि मूर्ख मतदाता धूर्त सियासत के बबूल सींच कर आम की उम्मीद पालते आए हैं, जो उनके अपने ही कपड़े फाड़ने का काम करते रहे हैं। इस सच के तमाम प्रमाण हैं, जो पग-पग पर बिखरे पड़े हैं।
याद रखा जाना चाहिए कि देश में जनता केवल मतदान तक जनार्दन होती है। इसके बाद ख़ुद को जनता का उपासक बताने वाले आराध्य बनते ज़रा भी देरी नहीं लगाते। बेहतर होगा यदि महीने, पखवाड़े के लिए देवता बन कर झूठा अहम पालने वाले आम जन अपने वहम को दूर कर उस सच को समझें, जो चुनाव के बाद पांच साल तक बेताल बन कर उनके कमज़ोर कंधों पर सवारी करता है। सियासी दावों के जंतर-मंतर और वादों की भूल-भुलैया में भटकने से बचने के बारे में अब विवेकपूर्वक सोचने का वक़्त आ चुका है। राहत देने वाले अलावों के नाम पर आहत करने वाले छलावों से भरपूर आज़ादी के 75 सालों का मूल्यांकन अब सियासी जमातों के गिरते हुए मूल्यों के आधार पर करने का समय आ चुका है।
राष्ट्रीय स्तर के किसी एक चेहरे के बलबूते राज्य की नैया का खिवैया चुनना इस बार भी घाटे का सौदा होगा। यह सच कम से कम भविष्य की दशा व दिशा तय करने वाले चुनावी साल में तो स्वीकारा ही जाना चाहिए। सत्ता की नीयत को अपनी नियति मान कर भोगते रहने की मंशा हो तो बात अलग है। याद रहे कि 2023 चेहरे नहीं चाल व चरित्र की बारीक़ी से परख का साल है। सत्ता-समर के फाइनल में आपकी पूछ-परख व अहमियत बनी रहे, इसके लिए अब आम मतदाताओं को अपने तेवर का अंदाज़ा कराना ही होगा। इनमेंअग्रणी भूमिका बदहाल भविष्य की कगार पर खड़े राज्य कर्मचारियों व उनके परिवारों को निभानी होगी। सभी कर्मचारी संगठनों को अमन की आड़ में दमन का रामगढ़ बन चुके सूबे में ज़ंजीरों से बंधे ठाकुर की जगह गब्बर बनना होगा। जो हाथों में मताधिकार की तलवार उठा कर ललकार भरे लहजे में यह नया और मिला-जुला डायलॉग बोलने का दम दिखा सके कि-
“दस जनों का परिवार और पेंशन बस दो हज़ार! बहोत नाइंसाफ़ी है ये, बहोत नाइंसाफ़ी। वही पुरानी पेंशन हमें दे दे ठाकुर!!”
अब तय आपको करना है कि “ओल्ड पेंशन” चाहिए या फिर “अटल टेंशन” उम्र के अंतिम पल तक के लिए। ध्यान रहे कि मसला केवल कर्मचारियों के भविष्य नहीं, उस मनमानी का है, जो मनमाने तऱीके से थोपी गई है। शर्मनाक विडम्बना यह है कि इस बड़े और गम्भीर मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की दिशा में कोई संवैधानिक संस्था भी स्वप्रेरित संज्ञान लेने को तैयार नहीं। यही वजह है कि इस बारे में आदेश तो दूर एक अदद टिप्पणी तक किसी दिशा से नहीं उपजी है।
अब यह देखना बाक़ी है कि अपने कल से जुड़े इस अहम मुद्दे को लेकर अधिकारी-कर्मचारी वर्ग क्या रुख अपनाता है। जहां तक सत्ता मद में चूर दलों का सवाल है, उनके प्रवक्ता चैनलों पर कर्मचारियों के विरोध को खोखला बता ही चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा चुका है कि कर्मचारी अपने वोट से कुछ बनाने बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखते। क्योंकि उन्हें चुनावी ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं। वो शायद यह भूल गए कि एक कर्मचारी कम से कम 10 लोगों के परिवार का मुखिया भी होता है। बहरहाल, फैसले की घड़ी नज़दीक है। जो बहुत कुछ तय करेगी।।
■ प्रणय प्रभात ■
श्योपुर (मध्यप्रदेश)
8959493240